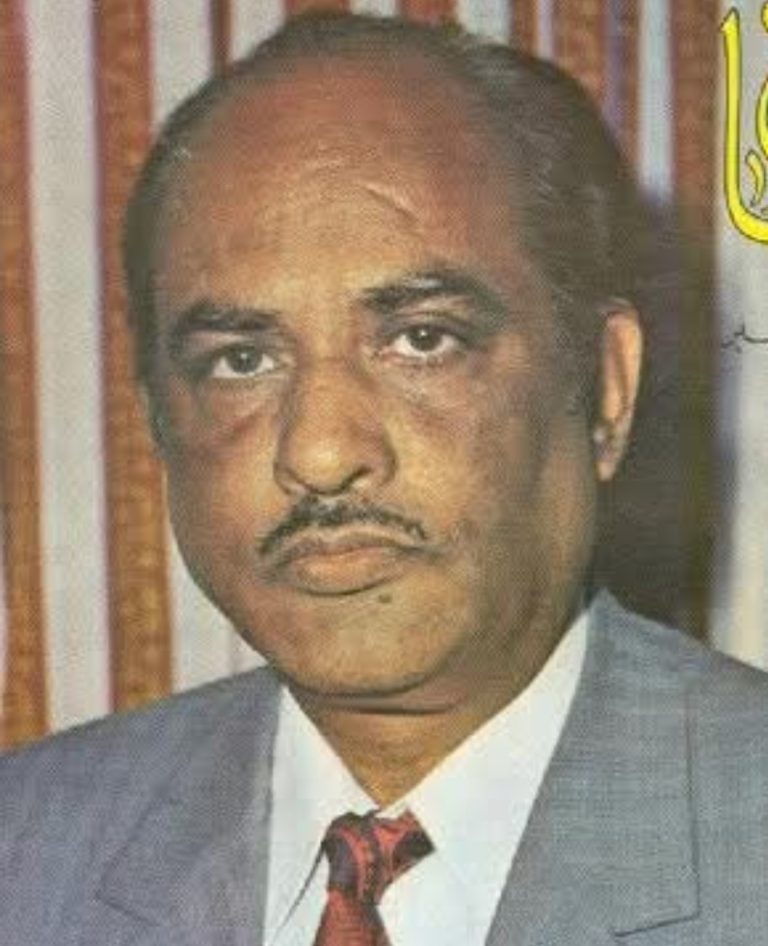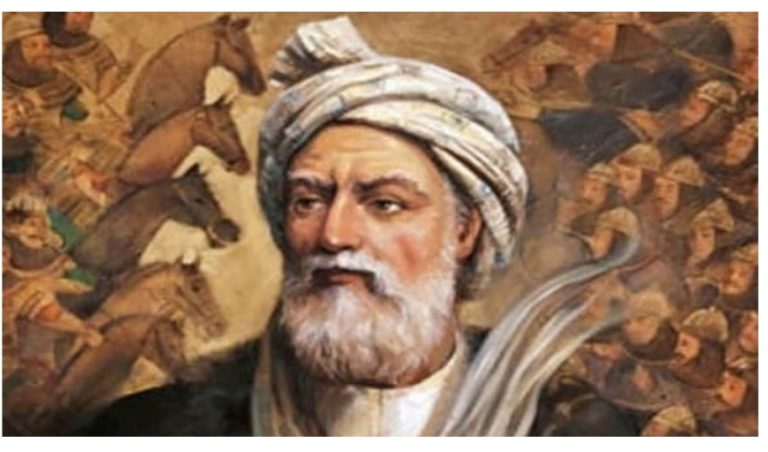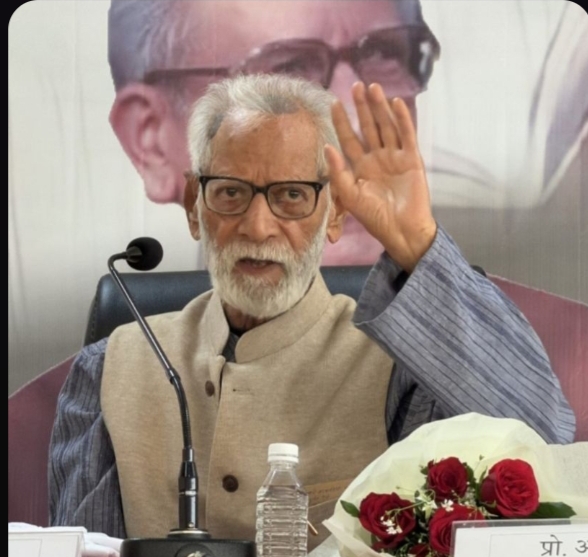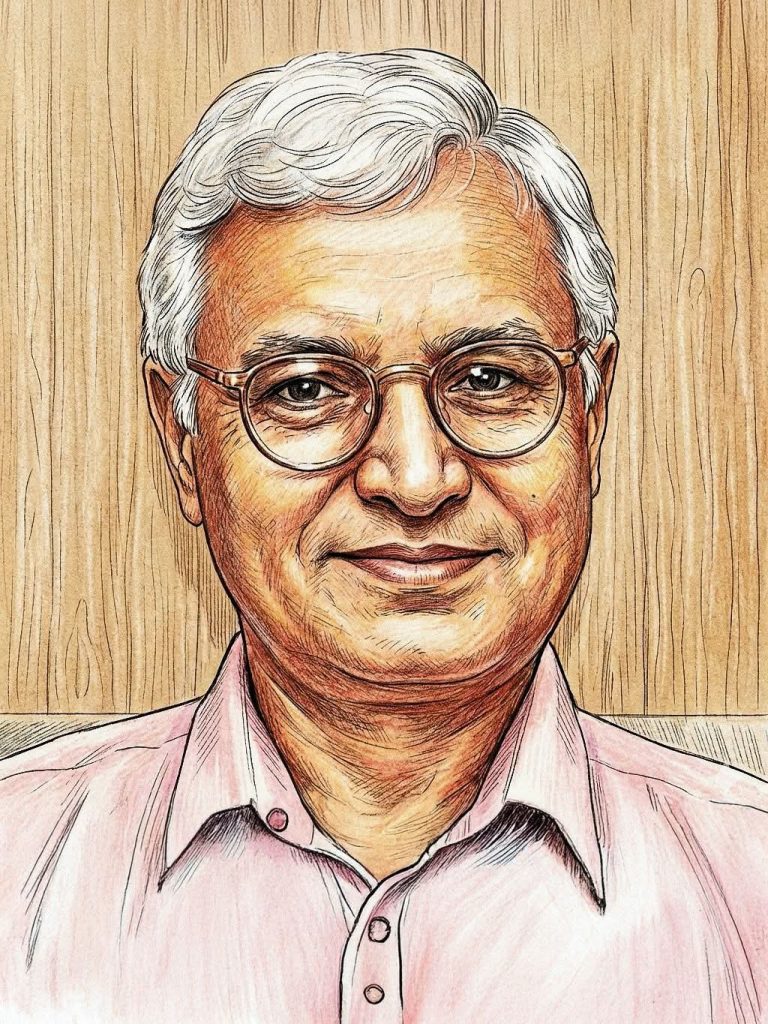जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने जस्टिस सुरेश शाह मेमोरियल लेक्चर देते हुए एक आलेख पढ़ा, ‘सुप्रीम कोर्ट का पतन, भूली हुई आज़ादी और घटे हुए अधिकार’। उसके मुख्य अंशों का अनुवाद पढ़ें–
मुझे लगता है कि हमारे समय की सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली घटना है-सुप्रीम कोर्ट का पतन। इसके एक पूर्व जज के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं कम से कम चेतावनी की घंटी तो बजा दूं। राजनीतिक चिंतक एडमंड बर्क ने कहा है कि जजों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे सरकार की गड़बड़ियों का पता लगा लें और ‘हर राजनीतिक बयार के पहले ही उससे होने वाले उत्पीड़न को सूंघ लें।‘ हमें इस तरह के अदालतों की ज़रूरत है, पर दुर्भाग्यवश हमारी अदालतें ऐसी नहीं हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का गौरवशाली अतीत रहा है और इसे इस पर गर्व होना चाहिए। इसके 13 जजों के संविधान पीठ ने केशवानंद भारती मामले में राजनीतिक कौशल दिखाया था, जब बुनियादी संरचना के सिद्धांत की रक्षा की थी और संविधान पर न्यायपालिका की पकड़ को पुनर्स्थापित किया था। यह तो एक चमकता हुआ उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कर सकता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने ठीक ही कहा था कि अदालत ने अपने आप को संविधान के ‘तार्किक, प्राथमिक रक्षक और व्याख्या करने वाले‘ और उसकी ‘रक्षा करने वाले‘ के रूप में स्थापित किया था।
एक्टिविस्ट की भूमिका
सर्वोच्च अदालत की शुरुआत दब्बू निष्क्रिय अदालत के रूप में हुई। पर धीरे-धीरे और निश्चित रूप से देश के शासन में अपनी भूमिका को समझा और अपनी ताक़त का विस्तार किया और इस तरह भविष्य में एक्टिविस्ट की भूमिका की आधारशिला रखी। केशवानंद भारती मामले से इसकी बस शुरुआत हुई थी। इसके बाद कई ऐसे फ़ैसले आए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पहचान को पुख़्ता किया। इनमें महत्वपूर्ण हैं मेनका गांधी मामला, फ्रांसिस कोरेली मलिन और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों का विस्तार हुआ।
ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का उत्थान-पतन नहीं हुआ। सबसे बदनामी जबलपुर एडीएम के मामले में हुई, जिसमें लगा कि अदालत बर्बाद हो गई और उसके बाद अदालत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में कई साल लग गए। उन्नीस सौ अस्सी और नब्बे के दशक में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और थोड़े समय के लिए ऐसा लगने लगा मानो सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रहरी की भूमिका ले ली है, जैसा कि पहली पीढ़ी के जजों ने इसके बारे में उम्मीद की थी, वैसा ही हो रहा है। खैर, ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर पीछे की ओर लौट चले हैं और आपातकाल जैसी विपदा से बचने के लिए गुहार लगाने की ज़रूरत है।
ताक़तवर कार्यपालिका
आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आज यह प्रासंगिक क्यों है। काग़ज़ पर तो हम एक उदार, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य हैं, जिसकी सारी संस्थाएं अपनी-अपनी जगह ठीक हैं। हमारे मौलिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोई उन्हें छू नहीं सकता। सरकार की संसदीय प्रणाली, सत्ता का बँटवारा, राज्य और केंद्र के बीच ज़िम्मेदारियों का बँटवारा, हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, जिससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। काग़ज़ पर सर्वशक्तिमान कार्यकापालिका को संसद के जरिए जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, संविधान और न्यायपालिका के ज़रिए शासन का राज हमारी व्यवस्था में है। हमारे पास ऑडिटर जनरल और चुनाव आयोग जैसे संस्थान, मानवाधिकार पर नज़र रखने वाले समूह, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, प्रेस, अकादमिक जगत और सिविल सोसाइटी, सबकुछ तो है। पर दुर्भाग्यवश जैसा मैंने पहले कहा था, ये सबकुछ सिर्फ़ काग़ज़ पर हैं।
आजकल भारत में हर उस संस्था को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया जा रहा है जो किसी भी रूप में कार्यपालिका को किसी तरह से उत्तरदायी ठहराता है। यह बर्बादी 2014 में ही शुरू हुई, जब बीजेपी सत्ता में आई।
इंदिरा गांधी सरकार ने जिस तरह से संस्थाओं को चौपट किया था, कुछ लोग उससे मौजूदा बर्बादी की तुलना कर सकते हैं, पर यह तुलना ग़लत है। हम आज यह देख रहे हैं कि एक ताक़त सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय लोकतंत्र को कोमा की स्थिति में पहुँचा रहे हैं और सारी शक्तियाँ कार्यपालिका के हाथों सौंप रहे हैं।
संसद
संसद की कई ख़ामियों के बावजूद यह सच है कि कोरोना शुरू होने के बाद से संसद की बैठक नहीं हुई है और अब हो रही है तो इसमें प्रश्न काल नहीं है। लोकपाल के बारे में अब तक हमने कुछ नहीं सुना है। मानवाधिकार आयोग सोया पड़ा है। चुनाव आयोग ने गुपचुप समझौता कर लिया है। सूचना आयोग लगभग निष्क्रिय पड़ा है। यह सूची लंबी और परेशान करने वाली है। अकदामिक जगत, प्रेस और सिविल सोसाइटी को योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, चुप करा दिया गया है। कई तरीकों से सिविल सोसाइटी का गला धीरे धीरे घोंटा जा रहा है।
विश्वविद्यालयों पर रोज़ हमले हो रहे हैं, छात्रों पर दंगे के आरोप लग रहे हैं या शिक्षकों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। निष्पक्ष मुख्य धारा के चौथे खंभे की अवधारण बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है।
न्यायपालिका
पर सबसे अधिक चिंता न्यायपालिका की स्थिति पर होती है। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर बहस होनी चाहिए। संसद के पहले ही कमज़ोर होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट वह दूसरी सबसे अहम जगह हो सकती थी जहां कश्मीर को तीन टुकड़ों में बाँटने की बात, नागरिकता संशोधन क़ानून, विरोध प्रदर्शन को कुचलने और उसका आपराधीकरण करने, राजद्रोह के दुरूपयोग, अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ प्रीवेन्शन एक्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर बहस हो सकती थी।
यह दुखद है कि इन मुद्दों की या तो अनदेखी की जाती है या उन्हें दबा दिया जाता है या उन्हें टाल दिया जाता है। हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, पर आपातकाल की स्थिति में है जो कई पीढ़ियों ने नहीं देखी है। इसके केंद्र में है और मुझे सबसे अधिक चिंता जिस बात की है वह सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में गिरावट।
मेरे विचार से सर्वोच्च न्यायालय का पतन बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एनडीए की सरकार एक नए राजनीतिक लहर, एक विचारधारा के रूप में तेजी से उभर कर सत्ता में आ गयी जो काफी दक्षिणपंथी है, जितना यह पहले के रूप में दिखती थी, दरअसल उससे कहीं अधिक दक्षिणपंथी है।
सुप्रीम कोर्ट का पतन संयोगवश नहीं हुआ, यह सोच समझ कर तैयार की गई एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, यह इस तरह किया गया कि कार्यपालिका पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ले और अपने राजनीतिक अजेंडे को आगे बढ़ाए।
कार्यपालिका से टकराव
एनडीए के सत्ता में आने के तुरन्त बाद न्यायपालिका के साथ सरकार का पहला टकराव राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क़ानून 2015 की क़ानून वैधता के रूप में हुआ। अदालत ने इस क़ानून को खारिज कर दिया। निश्चित तौर पर नई सरकार के साथ 2014 न्यापालिका का अच्छा टकराव हुआ। अदालत निश्चित तौर पर अपनी जगह अडिग रही और उसने न्यायिक नियुक्तियों में अपनी चमक दिखला दी। पर दुखद बात यह है कि अब यह अतीत की बात हो चुकी है।
जनवरी 2018 में एक छोटा सा लेकिन युगान्तकारी मौका आया जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अभूतपूर्व रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायिक प्रशासन और प्रबंधन की बातें सार्वजनिक कर दीं। बीच बीच में किसी किसी जज ने अपनी प्रतिभा भी दिखाई, ऐसा ही एक मामला पुत्तुस्वामी या श्रेया सिंघल मामले में हुआ, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून की धारा 66 ‘ए‘ को खारिज कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करने के लिए किसी धारा को खारिज किया गया है या समलैंगिकता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया हो या ट्रांसजेंडरों के अधिकार की रक्षा की बात कही गई हो। पर ऐसे मामलों में जिसमे कार्यपालिका अपने राजनीतिक अजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, आप पाएंगे कि अदालत को एक कोने में धकेल दिया जाता है।
झुकी हुई न्यायपालिका?
जिन मामलों में कार्यपालिका के ख़िलाफ़ कोई स्टैंड लेना हो, उनमें अदालत के झुकने की प्रवृत्ति पर भी लोगों का ध्यान गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक ख़बर में कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 10 मामलों में चार में ही इस आज़ादी की मांग करने वाले के पक्ष में फ़ैसला हुआ होगा। इन चार मामलों में भी यदि सरकार ने याचिकाकर्ता का समर्थन किया या चुप रही तभी यह फ़ैसला उसके पक्ष में गया। लेकिन यदि सरकार ने उस याचिका का विरोध किया तो फ़ैसला उसके पक्ष में नहीं हुआ है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में अदालत चिढ़ जाता है जैसा कि प्रशांत भूषण के मामले में हुआ। अदालत की अवमानना के मामले में कोर्ट ने ‘बडृा दिल’ दिखाते हुए प्रशांत भूषण को एक रुपया का ज़ुर्माना देकर छोड़ दिया, पर उसके पहले उनके व्यवहार की आलोचना की। इस पूरी सुनवाई में एक बात साफ हो गई कि अदालत एक असहिष्णु संस्थान बन चुकी है।
सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय शास्त्र के गौरवशाली युग का अंत हो चुका है। हमारे पास इसके गौरवशाली अतीत की सिर्फ स्मृतियाँ हैं, जिन्हें हम याद करते रह सकते हैं। पुत्तुस्वामी मामले में हमें कहा गया है कि एडीएम जबलपुर का भूत दफ़ना दिया गया है, पर मुझे डर है कि यह भूत बीच बीच में आता रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट का पतन
सुप्रीम कोर्ट के पतन का सबसे बड़ा उदाहरण बहुसंख्यकवाद के विरोधी कोर्ट के रूप में इसकी भूमिका निभाने में नाकामी है। मैं बहुसंख्यकवाद के विरोध की बात पर इसलिए ज़ोर दे रहा हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अधिक अहम है। लोकतंत्र की वैधता बहुसंख्यक के हितों का प्रतिनिधित्व करने में है। पर इस वैधता की एक कीमत है और यह कीमत अल्पसंख्यक समूह चुकाते हैं और विशेष रूप से वे जो अलोकप्रिय हैं या संसद को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों को बचाने का ज़रिया न्यायिक पुनर्विचार है, जो अदालतों को यह हक़ देता है कि वह संविधान का उल्लंघन करने वाले क़ानून को निरस्त कर दे
पर अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दशकों पुराने इतिहास को छोड़ कर बग़ैर कोई सवाल किए बहुसंख्यकवाद के साथ खड़ा होने लगा है। सबरीमला और अयोध्या, दो मामलों में यह साफ दिखा है। सबरीमला पर 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला प्रगतिशील था, इसमें महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। पर बाद में जब केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करना चाहा तो बीजेपी की केंद्र सरकार ने अयप्पा के भक्तों का साथ दिया। कुछ दिनों तक मामले को बड़ी बेंच को सौंपने के बहाने लटकाए रखा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्टे तो नहीं दिया, पर यह कहा कि यह अंतिम फ़ैसला नहीं है और सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ी याचिका पर निर्देश देने से इनकार कर दिया।
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मीन को तीन हिस्सों में बाँटने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय शांति बनाए रखने को देखते हुए व्यावहारिक नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पूर्ण न्याय हुआ? साल 1949 और 1992 में हिन्दुओं के कृत्य को ग़ैरक़ानूनी मानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने यह ग़लत काम करने वालों को ही पुरस्कृत किया। निश्चित रूप से यह बराबरी के सिद्धान्त के ख़िलाफ़ है। हिन्दू महासभा ने 1992 में कारसेवकों पर लगे हिंसा और विध्वंस के मामले को वापस लेने का दबाव बनाया। उसने यह मांग भी कि कारसेवकों को पेंशन दी जाए और मंदिर की दीवाल पर उनके नाम उकेरे जाएं मानो वे स्वतंत्रता सेनानी हों। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मुक़दमा चलते रहने देने की बात कही, पर मुझे संदेह है कि इसका कोई अर्थपूर्ण नतीजा निकलेगा।
संविधान के प्रति समर्पित नहीं
सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रति समर्पित रहने में नाकाम रहा है, जैसा कि अनच्छेद 21 पर अदालत के न्याय क्षेत्र से साफ होता है। कोरोना महामारी की वजह से प्रवासी मज़दूरों की स्थिति उलट-पलट गई, उनके पास काम नहीं है, आय का दूसरा कोई साधन नहीं है, बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं है, घर लौटने का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में इन स्थितियों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को स्वीकार करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन याचिकाओं पर स्थगन लगा दिया। अदालत ने कह दिया कि सरकार उन मजदूरों को दो वक़्त का खाना मुहैया करा रही है तो और क्या करे और यह भी कि रेलवे लाइन पर सो रहे मजदूर यदि कुचल कर मारे गए तो इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान बहुत बाद में लिया। इसके बदले हाई कोर्ट ने तर्क, हिम्मत और सदाशयता दिखाई और प्रवासी मजदूरों पर सरकार से सवाल किए। इसकी तुलना सुप्रीम कोर्ट की उस प्रतिक्रिया से कीजिए जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने अजीब तर्क दिया कि प्रवासी मज़दूरों का पलायन फ़ेक न्यूज़ की वजह से हुआ और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और मीडिया से कहा कि वे ज़िम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें।
हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक अरबपति क्रिकेट प्रशासन या हाई प्रोफाइल पत्रकार के लिए समय है, पर उसने इन बेसहारा करोड़ों मजदूरों की स्थिति को नजरअंदाज किया।
उत्पीड़न
भारत में एक और तरह का अभूतपूर्व उत्पीड़न अब हो रहा है और वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन के अधिकार को कुचलने का काम। कार्यपालिका यह काम खुले आम कर रही है, न्यायपालिका या तो इसे परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है या इस पर चुप्पी साधे हुए है।
स्पष्ट रूप से असंवैधानिक नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को ही लें। इसकी संवैधानिकता को अदालत में चुनौती दी गई, पर कोर्ट बहुत ही सतही कारणों से इसे लेने से बचता रहा। इस बीच सरकार ने इस विरोध को कुचलने की भरपूर कोशिश की और असहमति के सुर को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। न्यायपालिका चुप रही और एक शब्द नहीं कहा।
उत्पीड़न की रणनीति
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रणनीति अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विरोध प्रदर्शन करने वालों से बदला लेंगे और आज़ादी का नारा लगाना राजद्रोह माना जाएगा। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीकों से कुचलने की छूट पुलिस को दे दी गई है। निशाने पर मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून और गुन्डा एक्ट के तहत आरोप लगाए गए।
पर इस मामले में ज्वलंत उदाहरण दिल्ली दंगे का मामला है। ईमानदारी से एक दृष्टि रखने और ईमानदारी से प्रदर्शन करने वालों, यहां तक कि नाटक का मंचन करने वालों तक को सरकार निशाना बना रही है। पुलिस निहत्थे छात्रों पर हमला करती है। व्यवस्था का विरोध करने वाले किसी भी आदमी को चाहे उसकी मंशा कुछ भी क्यों न हो, थोड़ा सा मौका मिलते ही सरकार फंसा देती है जैसे अपूर्वानंद और योगेंद्र यादव के मामलों में हुआ है।
दिल्ली में रणनीति के तहत लोगों को दंगा, ग़ैरक़ानूनी रूप से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश रचने और राजद्रोह और अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ प्रीवेन्शन एक्ट जैसे औपनिवेशक क़ानून का प्रयोग करना है। इसकी तुलना बीजेपी के बड़े नेताओं से कीजिए जो भड़काऊ भाषण देते फिर रहे हैं। ताज्जुब है कि उनके खिलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है।
दंगे की निष्पक्ष जाँच नहीं
पूर्व पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो ने दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जाँच नहीं होने की ओर ध्यान दिलाते हुए इसकी तुलना 1984 के दंगों से की है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारत में दंगे इसलिए होते हैं कि राजनीतिक प्रतिष्ठान समाज के एक वर्ग को कुछ भी करने की छूट दे देता है। पुलिस की पूरी जाँच सिर्फ बयानों पर आधारित है, कोई पुख़्ता सबूत नहीं है। यह निष्पक्ष जाँच के सिद्धान्त के ख़िलाफ़ है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालो के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और उन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करने, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और उन भाषणों की वजह से ही दंगे भड़के उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करने से दिल्ली पुलिस पर भेदभाव बरतने और राजनीतिक मक़सद से जाँच करने के आरोप लगे हैं।
राजनीतिक प्रतिष्ठानों और पुलिस का मनोबल इतना बढ़ा हुआ क्यों है? निःसंदेह ऐसा इसलिए है कि भारत में न्यायपालिका कमज़ोर है। कई हफ़्तों तक इन मामलों की सुनवाई स्थगित होती रही, जिन मामलों सुनवाई हुई और अपील की गई, उनमें भी न्यायिक चुप्पी बरती गई।
जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों की तसवीरें होर्डिंग से हटाने को कहा क्योंकि यह ग़ैरक़ानूनी था, सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच इससे सहमत थी कि यह ग़ैरक़ानूनी है, उसके बाद भी उसने इस मामले को तीन सदस्यों की एक बेंच को भेज दिया जिससे राज्य को यह छूट मिल गई कि वह हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करे।
एनआईए बनाम ज़हूर वताली
इससे भी अधिक बुरा तो यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में एनआईए बनाम ज़हूर वताली के मामले में यूएपीए की व्याख्या की, जिसका असर इस तरह के बाद के तमाम फ़ैसलों पर पड़ा। इस निर्णय ने एक नए न्यायिक सिद्धान्त को जन्म दिया। इसका मतलब यह है कि एक अभियुक्त पूरी सुनवाई के दौरान जेल में बंद रहे भले ही उसके ख़िलाफ़ साक्ष्य स्वीकार करने लायक न हों और अंत में वह निर्दोष ही क्यों न साबित हो जाए। इसके पीछे का तर्क एकदम बकवास है, कोई अभियुक्त क्यों जेल में रहे यदि उसे दोषमुक्त होना ही है?
जस्टिस खानविलकर और जस्टिस रस्तोगी के फ़ैसले का मतलब यह हुआ कि अदालत यह मान ले कि एफ़आईआर में दर्ज सभी आरोप सही हैं। दूसरे शब्दों में, खुद को निर्दोष साबित करने की ज़िम्मेदारी अभियुक्त पर है।
सरकार, पुलिस और अभियोजन पक्ष इसका जम कर दुरुपयोग कर रहे हैं। पर असहमति रखने वालों के मामलों में राजद्रोह, आपराधिक साजिश और यूएपीए लगा दिया जाता है और ज़मानत से इनकार कर दिया जाता है।
ज़मानत नहीं
असहमित रखने वालों की साख यूएपीए के दुरुपयोग और लगातार ज़मानत अर्जी को खारिज कर असहमित रखने वालों को चुप करने का मामला भीमा कोरेगाँव मामले में देखा जा सकता है। इस मामले में कथित साक्ष्य टाइप किया हुआ, बगैर दस्तखत के, बग़ैर तारीख के काग़ज़ है जो पहले से ही मौजूद है। इसे उठा कर वरवर राव और गौतम नवलखा पर लगा दिया गया। छह साल पहले छपी एक किताब में ‘स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन‘ का हवाला दिया गया है। यह दस्तावेज ऑनलाइन भी उपलब्ध है। सुधा भारद्वाज के मामले में धारा 161 के तहत गवाह का बयान भी नहीं है। पर यूएपीए लगा देने के बाद अभियुक्त को ज़मानत तक नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से अदालत मामले की तहकीकात नहीं कर सकती।
सुधा भारद्वाज जेल में दो साल से हैं, कोरोना के रोगी वरवर राव को बाहर जाकर अपना इलाज कराने की छूट नहीं है। नवलखा का मामला क्लासिक मामला है यह दिखाने के लिए कि हाई कोर्टों को कुछ करने से निरुत्साहित किया जाता है। जब नवलखा की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हो रही थी, उन्हें मुंबई जेल भेज दिया गया। जब अदालत ने पूछा कि यह क्यों और कैसे हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। इसके उलट स़ॉलिसिटर जनरल यह मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए और उसने ज़मानत अर्जी खारिज कर दी और इस तरह हाई कोर्ट की सुनवाई ही ख़त्म कर दी गई।
न्याय करने का बुनियादी हक़
सुप्रीम कोर्ट के पतन का अगला मामला न्याय करने वाले के बुनियादी हक का त्याग करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर मामले में तो अपनी भूमिका ही छोड़ दी। इंटरनेट बंद करने के मामले में अदालत का फैसला कई मामलों प्रशंसनीय था, पर पर निर्णय देने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन के मामले में मई 2020 के निर्णय में अनुच्छेद 14, 19, 21 में अनुपात के सिद्धांत को लागू करने के बजाय अदालत और प्रशासन को पुनिर्विचार के लिए अपील करने की सलाह दी। कोर्ट को इसके बदले कार्यपालिका के किए हुए की न्यायिक समीक्षा करनी चाहिए थी। जैसा कि अनुमान था, पुनिर्विचार कमिटी ने इसे खारिज कर दिया और पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य को 4-जी सेवा से महरूम कर दिया। वरिष्ठ वकील अरविंद दातार के शब्दों में यह न्याय व्यवस्था को ‘आउटसोर्स’ करना है, जिसे न्याय देने से इनकार करना माना जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट कश्मीर के मामले में न्यायिक प्रक्रिया से बचने का काम भी कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई कि इंटरनेट बंद करने से किस तरह जन स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाई कोर्ट जाए। जम्मू-कश्मीर की 1.3 करोड़ जनता का स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय सबकुछ चौपट हो रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट वास्तविक दुनिया की समस्यायों से निपटना ही नहीं चाहता है।
इसकी तुलना इससे कीजिए कि न्यायापालिका ने निजी आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में क्या किया है। लिवरसिज़ बनाम एंडरसन मामले में लॉर्ड मैकमिलन ने कहा कि देश युद्ध कर रहा है, इस आधार पर इसकी छूट नहीं दी जा सकती है कि अदालत इस पर ध्यान न दे कि सभी क़ानून का पालन ठीक से हो रहा है।
न्यायपालिका निष्पक्ष संस्थान बने रहने में असफल हो रही है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए कार्यपालिका ज़िम्मेदार है, यह भी सबको पता है। कार्यपालिका यह कैसे कर रहा है, यह भी सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार समर्थक जजों को ठूंसने की ज़रूरत नहीं है।
निष्पक्ष नहीं?
एक समान सोचने वाले 30 जजों को चुनना नामुमकिन नहीं तो कठिन ज़रूर है। अपारदर्शी मास्टर ऑफ रोस्टर प्रणाली, एक ख़ास किस्म के मुख्य न्यायाधीश और ‘विश्वासपात्र’ जज निष्पक्ष न्यायपालिका को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त हैं। यह काल्पनिक स्थिति नहीं है और मौजूदा समय में भारत पूरी तरह से लागू है।
आज की स्थिति का अनुमान जस्टिस वाई. वी. चंद्रचूड़ ने 1985 में ही लगा लिया था जब उन्होंने कहा था, ‘निष्पक्ष न्यायपालिका को बहुत बड़ा ख़तरा बाहर से नहीं, अंदर से ही है।‘
इन स्थितियों में भी जो एक संस्था इस स्थिति को बदलने में सक्षम है, वह है न्यापालिका। दुर्भाग्यवश यह अपने रास्ते से भटक गई है। इतिहास में ऐसा ही एक समय था इमर्जेंसी के दौरा जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र को निराश किया था, पर इसने अपनी ग़लतियां समझीं और समय के साथ ही अपने स्वाभाविक रास्ते पर लौट आयी। अभी भी कई जज और वरिष्ठ वकील हैं जो संवैधानिकता में विश्वास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे सही अवसर पर उठ खड़े होंगे। वह अवसर अभी ही है।
संविधान सभा में 70 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसे जज चाहिए जो सर्वोच्च सत्यनिष्ठा के हों, जो सरकार, कार्यपालिका या उनके रास्ते आने वाले किसी के भी ख़िलाफ़ तन कर खड़े हो सकें। मुझे उम्मीद है कि हम अभी भी भारत में इस तरह के जजों को फलते -फूलते देखेंगे।
सौज- सत्यहिन्दीः लिंक नीचे दी गई है-
https://www.satyahindi.com/opinion/a-p-shah-supreme-court-in-decline-113426.html