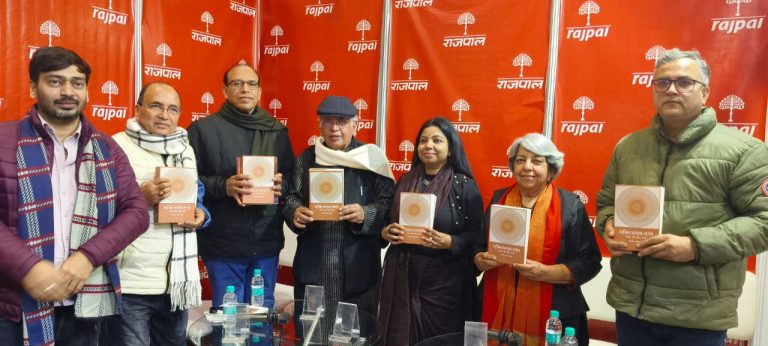कलकत्ता के गवर्नमेंट हाउस से सन् 1779 में भेजा गया एक दावतनामा ग़ौर करने लायक़ है. अंग्रेज़ी में लिखे इस आमंत्रण का मजमून हैः ‘श्री और श्रीमती हेस्टिंग्ज़ श्री…को अपनी ओर से शुभकामनाएं भेजते हुए अगले बृहस्पतिवार को आयोजित संगीत-सन्ध्या और रात्रिभोज में शरीक होने का आग्रह करते हैं. श्री…से यह आग्रह भी है कि अपने हुक़्क़ाबरदार के सिवाय कोई और सेवक साथ न लाएं.’ यह न्योता तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज़ की ओर से था.
दक्षिणी फ़ारस के शासक करीम ख़ान ज़न्द के नाम का बिगड़ा हुआ उच्चारण है. शिराज़ के शाही दरबार की सन् 1755 की एक पेंटिंग में दरबारियों के साथ बैठे करीम ख़ान को ‘क़ाएल्यन’ यानी हुक़्क़ा पीते हुए दिखाया गया है. और शायद बम्बई में उन दिनों प्रचलित हुक़्क़ों की बनावट करीम ख़ान के हुक़्क़े सी होने की वजह से उसे यह नाम मिला होगा. उस दौर के तिजारतियों के ज़रिये हुक़्क़े की पहुंच के विस्तार को समझने भर के लिए यह पेंटिंग देखी जा सकती है. अरब के मुल्क़ों में ‘शीशा’ या ‘नारगिला’, अल्बानिया, बोस्निया में ‘लुला’ या ‘लुलावा’ कहलाने वाला हुक़्क़ा उज़बेकिस्तान में जाकर ‘चिलम’ हो जाता है मगर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या मेक्सिको में इसकी पहचान हुक़्क़े के नाम से ही है. अपने यहां सूरत में भी यह ‘नरगिल’ कहलाया तो कलकत्ते में आम आदमी का हुक़्क़ा ‘गड़गड़ा’ कहा गया. पूरब में यही ‘गुड़गुड़ी’ हो गया. लखनऊ और राजस्थान की रियासतों में हुक़्क़े को ओहदे के मुताबिक़ भव्यता देने के लिए अलंकृत करके सजाने पर ख़ूब काम हुआ.
अमीर का हुक़्क़ाअसद बेग़ के ब्योरे की तरह ही अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में हुक़्क़े के महत्व के बारे में तमाम दिलचस्प दस्तावेज़ मौजूद है, साथ ही मुहावरों और कहावतों में हुक़्क़े का ज़िक्र आम आदमी की ज़िंदगी में इसके दख़ल की पहचान भी कराता है. ‘हुक्का हर का लाड़ला, रक्खे सबका मान. भरी सभा में यूं फिरे, ज्यूं गोपिन में कान’ सरीखी हिन्दुस्तानी कहावत के साथ ही फ़ारसी की एक और कहावत है, ‘हुक्का यकदम, दो दम, सिह दम बाशद, न कि मीरासे-जद्दो-आम बाशद’. इसका मतलब यह कि हुक़्क़ा एक फूंक, दो फूंक, या तीन फूंक पीना चाहिए, उसे अपनी जायदाद नहीं समझ लेना चाहिए. यानी जहां चार आदमी बैठे हों, वहां बारी-बारी से हुक़्क़ा सबको देना चाहिए, यह नहीं कि ख़ुद ही बैठे गुड़गुड़ाते रहें. ये दोनों ही कहावतें महफ़िल में हुक़्क़ा पीने के सलीक़े पर ज़ोर देती हैं, इसे सामुदायिक गतिविधि के तौर पर रेखांकित करती हैं. हालांकि कुलीनों की दावत में अनिवार्य रूप से शामिल हुक़्क़े को बरतने का ढंग इससे अलग होता था. खाने के बाद हर मेहमान की मेज़ के क़रीब एक छोटी मेज़ पर हुक़्क़ा लगता और हुक़्क़ाबरदार बड़े अदब से निगाली पेश करके पीछे खड़ा हो जाता.
हिन्दुस्तान आए अंग्रेज़ व्यापारियों और अफ़सरों ने यहां के जिन तौर-तरीकों को बेहिचक अपनाया, हुक़्क़ा पीना उनमें से एक था. और तत्कालीन कुलीन समाज में हुक़्क़े के जो ठाठ थे, हुक़्क़ाबरदार के ओहदे वाला सेवक उसकी एक झलक है. हुक़्क़ाबरदार के ज़िम्मे एक ही काम था, अपने मालिक की तलब के वक़्त तैयार हुक़्क़ा पेश करना और जब भी ज़रूरत पड़े फौरन चिलम बदलना. नई चिलम यानी सुलगे हुए कोयलों के साथ नई तम्बाकू मुहैया कराना. हुक़्क़े की साफ़-सफ़ाई के साथ ही हुक़्क़ा पीने के तजुर्बे में ताज़गी और नयेपन के लिए तम्बाकू को सुवासित करने की नई तरकीबें तलाश करना भी उसके ज़िम्मे होता. सूखे मेवे, गुलकंद, विभिन्न जड़ियों और मसालों के अलावा सुगंध वाली चीज़ों को तम्बाकू में मिलाकर अलग-अलग स्वाद और गंध वाली तम्बाकू तैयार करते. हुक़्क़े के तले में पानी के साथ फूलों-फलों का रस मिलाने या निगाली में गुलाबजल डालने की रवायत भी इसी लिहाज़ से शुरू हुई. यों कहावत तो यह भी प्रचलित थी कि ‘हुक्का चार वक्त अच्छा, सो के, मुंह धो के, खा के, नहा के. और चार वक्त बुरा- आंधी में, अंधेरे में, भूक में और धूप में’ मगर यह बात रईसों पर लागू नहीं होती थी. वे जब पालकी में सवार होकर चलते तो कन्हारों के साथ ही हुक़्क़ा लिए हुक़्क़ाबरदार भी साथ-साथ दौड़ते, वक़्त या मौसम कोई भी हो.
कलकत्ता के गवर्नमेंट हाउस से सन् 1779 में भेजा गया एक दावतनामा ग़ौर करने लायक़ है. अंग्रेज़ी में लिखे इस आमंत्रण का मजमून हैः ‘श्री और श्रीमती हेस्टिंग्ज़ श्री…को अपनी ओर से शुभकामनाएं भेजते हुए अगले बृहस्पतिवार को आयोजित संगीत-सन्ध्या और रात्रिभोज में शरीक होने का आग्रह करते हैं. श्री…से यह आग्रह भी है कि अपने हुक़्क़ाबरदार के सिवाय कोई और सेवक साथ न लाएं.’ यह न्योता तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज़ की ओर से था.
चिलमनों के पार तक हुक़्क़े की रसाई हमेशा ही रही.सन् 1789 में कलकत्ता आए एक फ़्रांसिसी घुमक्कड़ ग्रां पियरे की डायरी में दर्ज़ ब्योरे से अभिजात वर्ग की महिलाओं में भी हुक़्क़े की लोकप्रियता का पता चलता है. उन्होंने लिखा है – खाना ख़त्म होने के बाद डेज़र्ट के साथ हुक़्क़ाबरदार भी अंदर दाख़िल होते हैं और हुक़्क़ा रखकर अपने मालिक की कुर्सी के पीछे खड़े हो जाते हैं. फिर तो आधे घंटे तक हुक़्क़े की गड़गड़ाहट इस क़दर गूंजती रहती है कि आपस में बात नहीं कर सकते. कमरे में छा गए धुंए के बादलों के बीच कुछ साफ़ देख पाना भी मुश्किल होता है. किसी अजनबी के लिए यह माहौल ख़ासा अटपटा हो सकता है और अगर वह अपना हुक़्क़ा साथ नहीं लाया है तो और भी ज्यादा. महिलाएं भी इस शौक में बराबर साझीदार होती हैं. अगर वे किसी और का पेश किया हुआ हुक़्क़ा पीना क़बूल कर लें तो यह उनकी नज़रे इनायत मानी जाती. हां, यह सभ्यता का तकाज़ा और सलीका भी है कि उन्हें हुक़्क़ा देने वाला पहले नय (पाइप) के सिरे पर लगी निगाली (माउथपीस) बदलकर उसकी जगह नई निगाली लगा दें. यों दो-एक कश के बाद वह नय लौटा देती हैं, मगर उसे क़बूल कर लेना कोई मामूली मान की बात नहीं समझी जाती.
तत्कालीन कुलीनों के शौक और दिखावे की तमाम चीज़ों में हुक़्क़ा इतना अहम् था कि उसका आधार क़ीमती धातुओं और बहुमूल्य नगीनों से सजाया जाने लगा, लोग इस पर अपने नाम खुदाते, चांदी के तारों में लिपटी नय और सोने, चांदी या हाथीदांत की बनी निगाली. हुक़्क़ा रखने के लिए मेज़ पर बिछाया जाने वाला कालीन की तरह का छोटा सा टुकड़ा ख़ासतौर पर बनाया जाने लगा और आपस में तोहफ़ा देने की चीज़ बन गया. और हुक़्क़ा शान की ऐसी पहचान कि उसकी नय पर किसी का पांव पड़ना ऐसी बेइज्ज़ती मान ली जाती कि तलवारें खिंच जातीं. उस दौर में हुक़्क़े के बहाने हुई बेइज्ज़ती का बदला लेने के लिए डुएल (द्वंद्वयुद्ध) के कितने ही क़िस्से मशहूर हुए.
हुक़्क़ा बार के इस दौर में यह दास्तान किसी और दुनिया की लग सकती है. हुक़्क़ा और हुक़्क़े की एक्सेसरीज़ के साथ ही तरह-तरह की तम्बाकू और यहां तक कि ख़ास कोयले की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के दौर में हुक़्क़ाबरदार के बारे में सोच पाना भले मुमकिन न हो मगर यह याद रखने में क्या हर्ज है कि इन सबके पीछे ऐसे पुरखों का शौक और उनकी सनक का बड़ा योगदान है. उम्मीद है कि आइंदा किसी अजायबघर में कोई हुक़्क़ा दिखाई देगा तो उसे ग़ौर से देखेंगे!
(साभार संवाद)