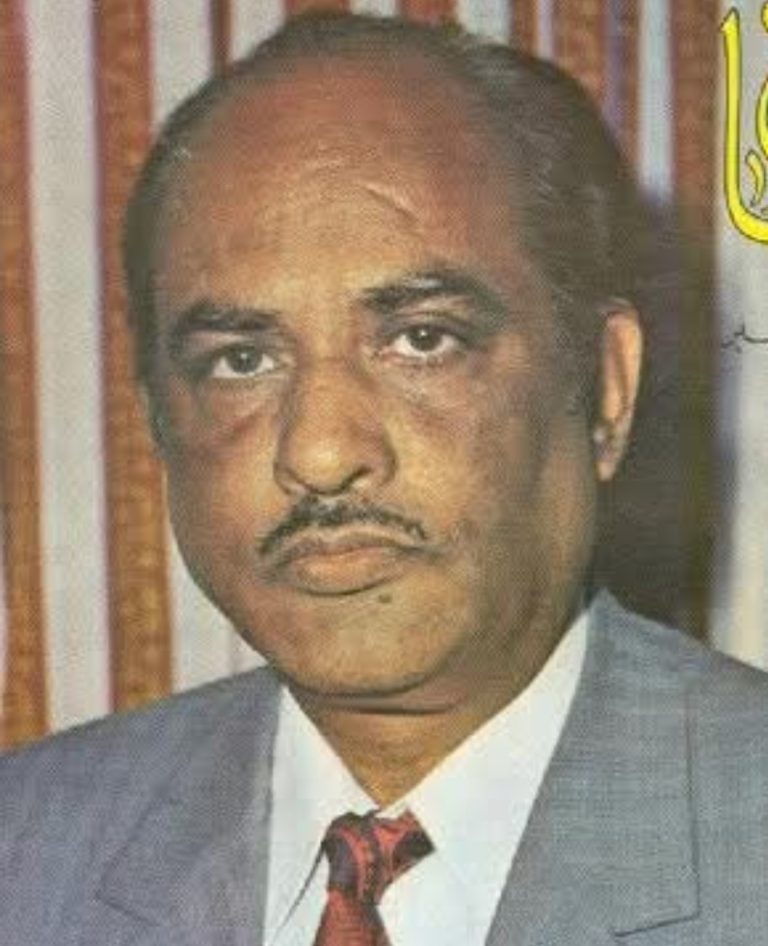असग़र वजाहत (जन्म – 5 जुलाई 1946) – हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण कहानीकार एवं नाटककार के रूप में सम्मानित नाम हैं। इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा-वृत्तांत, फिल्म तथा चित्रकला आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण रचनात्मक योगदान किया है। इन्होने दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन किया एवं हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रहे । हम उनके जामिया से जुड़े संस्मरण धारावाहिक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं । ( संपादक)
संघर्ष के उन दिनों में भी ज़ाकिर साहब दिल्ली ही, नहीं देश के बहुत सम्मानित लोगों में गिने जाते थे। उनकी बुध्दिमानी, त्याग और प्रतिध्दता का सर्वथा सम्मान होता था। कसाई ज़ाकिर साहब के कमरे में घुसता चला गया और वहाँ जाकर उसने ऊँ ची आवाज् ा में अपने पैसों का तकाज़ा करना शुरू कर दिया। ज़ाकिर साहब ने अपने सेकेट्ररी को बुलाया और उससे कहा-देखो, इनके पैसे तो हमें देने ही देने हैं। जामिया में पैसा नहीं है लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका कर्ज़ा चुकाऊँ… देखो, ऐसा करो कि मेरी किताबें बेचने की कोशिश करो…जो पैसा आये उससे इनका हिसाब चुकता कर दो…अगर किताबों से इतना पैसा न आ सके…तो मेरे घर का फर्नीचर…नीलाम कर दो…उसे भी काम न चले तो घर…।’
कसाई ये सब सुन रहा था और हैरान था। उसे यह भी लग रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ज़ाकिर साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा -और अगर फर्नीचर और घर बेचने से भी इतना पैसा न मिल सके तो…।’
यह सब सुन कर कसाई की सिट्टी-पिट्टी ग़ुम हो गई। उसने सोचा अपने थोड़े से पैसों के लिए मैं इतने बड़े आदमी की किताबें, फर्नीचर और कपड़े नीलाम करा दूँगा तो लोग क्या कहेंगे। यह सोच कर वह बोला – नहीं-नहीं जी, इसकी ज़रूरत नहीं है… मैं बाद में ले लूँगा।’
ज़ाकिर साहब ने कहा- ‘बाद में क्या हम आपका हिसाब अभी चुकाये देते हैं।’ लेकिन कसाई इतना घबरा गया था कि उसने उनके हाथ जोड़े और कमरे से बाहर निकल गया।
पुरानी जामिया और उसकी प्रयोगधर्मिता के बारे में एक रोचक घटना मुजीब भाई बताया करते थे। एक बार यह विचार किया गया कि जामिया के ‘कानवोकेशन’ में हर वर्ष किसी बुध्दिजीवी या राष्ट्रीय नेता आदि को बुलाया जाता है। लेकिन समाज में दूसरे लोग भी हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में महत्तवपूर्ण काम कर रहे हैं। उन लोगों को ‘कानवोकेशन’ में मुख्य अतिथि के रूप में क्यों नहीं बुलाया जाए। बात होते-होते ंगुलाम मोहम्मद उर्फ गामा पहलवान (1878-1960) पर आ गयी। उस ज़माने में गामा पहलवान का बड़ा चर्चा था। उन्होंने सन् 1910 में लंदन जाकर यह चुनौती दी थी कि वे इंग्लैंड के किसी भी पहलवान को तीस मिनट के अंदर चित्त कर सकते हैं। उनकी चुनौती को ‘बेनजामिन रोलर’ ने स्वीकार किया था जिसे गामा ने एक मिनट चालीस सेंकेड में चित कर दिया था। इस तरह गामा पहलवान राष्ट्रीय अस्मिता के एक प्रतीक बन गये थे।

जामिया का अलीगढ़ से विद्रोह केवल अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का ही विरोधी नहीं था, बल्कि शक्तिशाली मुस्लिम सामंतशाही का विरोध भी था जो उस जमाने में बहुत शक्तिशाली थी। चंदे से संस्था चलाना और वह भी सरकार विरोधी संस्था चलाना कितना कठिन रहा होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लोग बताया करते थे कि ज् ााकिर साहब की एक ऑंख भी पैसे के अभाव के कारण ऑपरेशन न करा पाने की स्थिति में खराब हो गई थी।
तय पाया कि ‘कानवोकेशन’ में मुख्य अतिथि के रूप में गामा पहलवान को बुलाना चाहिए। गामा पहलवान आये। उनको मुख्य अतिथि का गाउन वगैरा पहनाया गया। दो-तीन हज् ाार लोग पंडाल में मौजूद थे। एकेडेमिक प्रोसेशन के साथ गामा पहलवान पंडाल में आये। सब मंच पर जाकर बैठ गये और ‘कानवोकेशन’ की कार्यवाही शुरू हुई। जब गामा पहलवान भाषण देने खड़े हुए तब वे पत्ते की तरह काँप रहे थे। उन्होंने कहा-”मैं दुनिया के बड़े-से-बड़े पहलवान को चित्त कर सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता।” इतना कह कर गामा पहलवान अपनी सीट पर आ कर बैठ गये, लेकिन उनके इस भाषण पर पाँच मिनट तक तालियाँ बजती रहीं।
अलीगढ़ से दिल्ली आने के बाद जामिया करोल बाग की कोठियों में थी। यहीं पढ़ाई होती थी और यहीं खपरैल के घरों में अध्यापक रहा करते थे। अध्यापकों की कोई श्रेणी न थी। वाइस चांसलर से लेकर छोटे-से-छोटे अध्यापक तक को उस्ताद कहा और माना जाता था। किसी तरह के वेतनमान नहीं थे। अध्यापकों और कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार वेतन मिला करता था। नियुक्ति करने के बाद अध्यापक से पूछा जाता था कि उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और उसी हिसाब से उसे वेतन दिया जाता था। इस संबंध में एक रोचक बात यह है, एक क्रिश्यिचन अध्यापक, ई.जे. कैलाट (1871-1951) की नियुक्ति के बाद उनसे पूछा गया था कि उनके क्या-क्या खर्चे हैं ताकि उसी हिसाब से उनका वेतन तय किया जाए। कैलाट साहब ने दीगर खर्चो के आलावा बताया कि वे रोज़ शाम को व्हिस्की पीते हैं जिसमें इतना-इतना पैसा खर्च होता है। सेलेक्शन कमेटी ने व्हिस्की के खर्चे को मिलाकर जब हिसाब लगाया तो पता चला कैलाट साहब का वेतन इतना ज्यादा हो गया है कि वह दिया ही नहीं जा सकेगा। ऐसी स्थिति में सेलेक्शन कमेटी ने यह माना कि नियमानुसार कैलाट साहब को उतना वेतन मिलना चाहिए जितना जोड़ा गया है, लेकिन चूंकि जामिया के पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए उतना वेतन नहीं मिल सकेगा। कैलाट साहब ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था और यह कहा था कि वे व्हिस्की के लिए अपना पैसा खर्च करेंगे। कैलाट साहब पूरे जीवन जामिया में रहे। वे अंग्रेज़ी और स्पोट्र्स के टीचर रहे।
यह आश्चर्य की बात है कि इस्लामी संस्था होने के बाद भी जामिया कितनी उदार थी। आज भी नर्सरी से लेकर पी-एच.डी. तक जामिया में को-ऐजूकेशन है। यह बड़े महत्त्व की बात है। जामिया में हिन्दू छात्रों के लिए हिन्दू धर्म शास्त्र पढ़ने की सुविधा है। बी.ए. में जो छात्र एडमिशन लेता है उसके लिए हिन्दू धर्म शास्त्र या मुस्लिम धर्म शास्त्र या भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक प्रश्नपत्र अनिवार्य होता है।
जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, यह जामिया का संक्रमण काल था। कॉलेज के ढाँचे से निकल कर विश्वविद्यालय के ढाँचे में ढलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मुजीब भाई ‘हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट’ थे लेकिन उनका कोई ऑफिस न था। विभाग संबंधी सभी कागज् ाात उनके थैले में रहा करते थे। सभी लोग स्टाफ रूम में बैठते थे। यह इस प्रकार से बहुत अच्छा था कि सभी विषय के लोगों की आपस में मुलाकात हो जाती थी और कभी-कभार ‘इंटर डिसेप्लनरी’ बातचीत हो जाया करती थी।
मैं शाम को अक्सर मुजीब भाई के घर चला जाता था । साहित्य, समाज, राजनीति पर बातचीत होती थी। वे जामिया की राजनीति में बहुत प्रमुख थे लेकिन मुझसे कभी जामिया की राजनीति के संबंध में बातचीत नहीं करते थे। वे अपने बारे में भी कम बताते थे लेकिन बहुत लम्बे समय तक साथ काम करने के कारण, अक्सर कभी-कभी उनके अतीत की झलकियाँ मिल जाती थीं।
मुजीब भाई इलाहाबाद की ‘चायल तहसील’ के बिसौना गाँव के थे। उनकी पढ़ाई इलाहाबाद में हुई थी। वे जब कॉलेज में थे तो एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिदंगी को एक नया मोड़ दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के दिन थे। गाँधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज़ादी के संघर्ष में लगा हुआ था। भगत सिंह और राजगुरु आदि को फाँसी पर चढ़ा दिया गया था। पूरे देश में ब्रिटिश सरकार भयानक अत्याचार कर रही थी। इन्हीं दिनों इलाहाबाद में प्रसिध्द स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान पं. सुंदरलाल आये हुए थे। मुजीब भाई उनसे मिलने गये। पंड़ित जी ने उनसे पूछा, ‘तुम क्या कर रहे हो’, तो इन्होंने कहा – ‘बी.ए. का इम्तिहान दे रहा हूँ’ जवाब में पंडित जी ने कहा-हाँ अब इससे बड़ा काम तो देश में बचा ही नहीं।’
यह बात युवा मुजीब भाई के दिल को लग गयी। अगले दिन वे अपने सारे सार्टिफिकेट, मार्कशीट आदि लेकर पंड़ित सुंदरलाल के पास पहुँचे और उनके सामने अपने सारे सार्टिफिकेट, मार्कशीट फाड़ डाले और कहा- ‘अब बताइये मैं क्या करूँ।’ पंड़ित जी ने मुजीब भाई से कहा कि तुम मेरे साथ काम करो और मुजीब भाई घर और पढ़ाई छोड़ कर पंडित सुंदरलाल के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े।
पंडित सुंदरलाल के साथ उनको बहुत महत्त्वपूर्ण अनुभव हुए। गाँधी जी के सदाकत आश्रम के अलावा उनका परिचय राष्ट्रीय स्तर के अन्य नेताओं से हुआ। हैदराबाद स्टेट के भारत में विलय संबंधी प्रयासों में भी पंडित सुंदरलाल के सचिव के रूप में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। पंडित जी के साथ उन्होंने चीन की यात्रा भी की थी। मुजीब भाई के ये सब अनुभव इस संस्मरण में धीरे-धीरे आयेंगे।
आज़ादी मिलने के बाद मुजीब भाई ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और लम्बे ‘गैप’ के बाद फिर पढ़ाई शुरू की थी। उन्होंने हिन्दी में एम.ए. करने का फैसला किया था। यह अपने आप में बहुत महत्तवपूर्ण और विचारणीय है कि उन्होंने हिन्दी में एम.ए. करने का क्यों फैसला क्यों किया था, जबकि वे उर्दू, अंग्रेज् ाी या इतिहास जैसे विषयों में भी एम.ए. कर सकते थे। इन विषयों में भी उनकी बहुत अधिक रुचि थी। हिन्दी में एम.ए. करने के पीछे उनकी समझ यही रही होगी कि हिन्दी बहुसंख्यक की भाषा है। हिन्दी भारत को जोड़ने का काम कर सकती है। हिन्दी भारत का भविष्य है। अलीगढ़ से हिन्दी में एम.ए. करने के बाद उन्हें जामिया में नौकरी मिल गयी थी और वे लेक्चरर से रीडर भी हो गये थे लेकिन उन्होंने पी-एच.डी. नहीं की थी।

अलीगढ़ में जायसी पर पी-एच.डी. करने के लिए उनका पंजीकरण था पर मुजीब भाई पुराने ज़माने की उस परम्परा के थे जो वाचक परम्परा कही जाती है। जहाँ ज्ञान का आदान-प्रदान बोले हुए शब्दों के माध्यम से होता है न कि कांगज् ा पर लिखे गये। इसलिए उनका पी-एच.डी. का काम बहुत सालों से रुका पड़ा था। भाभी (अज़रा रिज़वी, मुजीब रिज़वी साहब की पत्नी) उनको थीसिस लिखने की याद दिलाती रहतीं थीं और वो तरह-तरह के बहाने बनाते थे। जैसे-अरे भई लिखूँ कैसे, शाम को चार बजे कॉलेज से लौटकर आता हूँ और उसके बाद यहाँ कोई-न-कोई आ जाता है…आठ-नौ बजे रात को खाना खाने के बाद तो मैं बैठ नहीं सकता लिखने को।’ या कभी कहते थे- ‘काम करने की जगह तो है नहीं…मैं क्या काम करूँ’…घर में किताबें बिखरी पड़ी हैं…और कुछ किताबें तुमने ऊपर रखवा दीं…अब किताबों को ढँढ़ना और जमा करना यह तो मुश्किल काम है न।’ एक दिन कहने लगे- ‘भई, मैं लिखा करता था एक चिकने से कांगज् ा पर …जो जर्मन पेपर कहलाता था…मुझे आजकल जो कांगज् ा मिलते हैं उन पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है…अब कहीं से वह जर्मन कांगज् ा मिले तो मैं लिखना शुरू करूँ।’
अज़रा भाभी ने जर्मन कागज़ ढूँढ़ने का काम मुझे सौंप दिया था। सन् 1947 से पहले जो जर्मन पेपर आया करता था उसे 1972 में चावड़ी बाजार में तलाश करना मेरे लिए यह दिलचस्प काम था। मैंने इस चुनौती को गंभीरता से लिया था। मैंने चावड़ी बाज् ाार के बहुत चक्कर लगाये थे। कई दुकानदारों ने मेरा मज् ााक भी उड़ाया था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। जिसने जिस दुकान का पता बताया था वहाँ गया था। हद यह है कि कांगज् ा के कुछ गोदामों में जा कर भी मैंने चिकने जर्मन कांगज् ा को ढूँढ़ने की कोशिश की थी। ख्याल यह था कि अगर एक-आध रिम भी मिल गया तो मुजीब भाई की थीसिस लिख जायेगी। लेकिन मैं कामयाब न हो सका।

अकार’ से साभार – आगे जारी…..