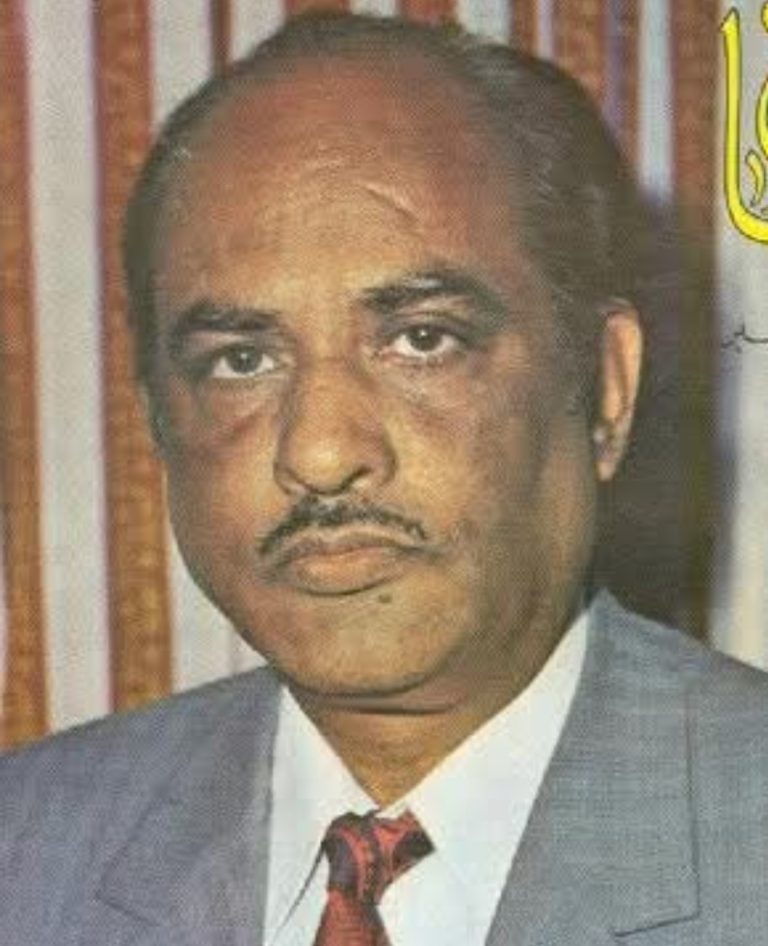जिस वक़्त देश के माहौल में प्यार करना सबसे मुश्किल बात हो गई हो वैसे में इन दोनों की दोस्ती किसी ‘क्रांति’ से कम नहीं लग रही थी। ये वो ‘बग़ावत’ कर रहे थे जिससे नफ़रत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा लग रहा था! इनके इस ‘गुनाह’ को मैं ‘रिपोर्ट’ करना चाहती थी।
देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बना दी गईं ये कैसी सरहदें हैं, जिनकी एक-एक कील दिलों में गहरे ज़ख़्म की तरह उतर गई है। सिंघु बॉर्डर पर राह चलते लोगों को मैं ग़ौर से देख रही थी क्या वाकई उनके दिलों में दूरियां आ गई होंगी?
मैं लगातार सिंघु बॉर्डर आती-जाती रही हूं लेकिन 26 जनवरी के बाद माहौल कुछ अलग था। हां, कुछ अलग। कैसे अलग था और कितना अलग था ये बयां करने के लिए मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, वो सिर्फ़ महसूस किया जा सकता था, मैं एक मंच से दूसरे मंच की तरफ़ बढ़ी टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर निकलता रास्ता, बहती गंदी नाली, सालों पहले बंद हो चुकी फ़ैक्ट्री का खंडहर, ये शहर में बसा गांव और गांव में छुपा वो रास्ता था जो सिंघु बॉर्डर पर चल रहे प्रोटेस्ट के दो स्टेजों को जोड़ रहा था। हम इस कच्चे-पक्के रास्ते से गुज़र रहे थे कि एक जत्था मेरे सामने से निकला उनके हाथों में तिरंगा था और वो नारे लगा रहे थे। ये आंदोलन के अंदर निकल रहा एक छोटा सा जुलूस था, शाम हो चुकी थी और डूबते सूरत में हक़ की लड़ाई के नारे बुलंद किए जा रहे थे। इस तस्वीर ने जैसे मुझे मॉर्डन इंडियन की सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा की किताबों में पहुंचा दिया जिससे हमने फ़्रीडम फ़ाइट की तारीख़ों को रटा था और उस दौर के नौजवानों को अपना हीरो माना था जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। किताबों को पढ़ते हुए जहां गांधी जी के विचार सत्य और अहिंसा की टेक्निक जायज़ लगती थी वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राज गुरू, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाक़-उल्लाह-ख़ान फ़ेवरेट हो गए थे। और ये माहौल देखकर नैनो सेकेंड के लिए मेरा विज़न ब्लर हो गया और ऐसा लगा कि मेरे सामने से गुज़रे जुलूस में मैंने एक झटके में उन सबको यहां एक साथ देख लिया। बेशक मेरा इमेजिनेशन बिल्कुल फ़िल्मी हो रहा था लेकिन यकीन मानिए वो माहौल देखकर मुझे गूज़बम्पस (Goosebumps ) आ रहे थे।
हर किसी की तरह मैं भी फ़ील्ड पर जाने से पहले स्टोरी प्लान करके ही निकलती हूं, हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही किया लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस बार सिंघु बॉर्डर का माहौल कुछ अलग था। पता चला कि मैं जिसे तलाश रही थी वो गांव वापस लौट गए हैं और कुछ दिन बाद वापस आएंगे। अपनी स्टोरी के पीछे एक पत्रकार को कितना भटकना पड़ता है शायद इसका अंदाज़ पढ़ने वाले कभी नहीं लगा सकते।
बहरहाल मैं अपनी जिस स्टोरी के लिए पहुंची थी उसकी तलाश के दौरान मेरी मुलाक़ात सिंघु बॉर्डर के मेन मंच के क़रीब बनाई गई लाइब्रेरी ‘जंगी किताब घर’ में कुछ ख़ास नौजवानों से करवा दी। लाइब्रेरी पर कुछ गहमागहमी का माहौल था तीन-चार लड़के किताबें सहेज रहे थे, कुछ लोगों की मदद कर रहे थे उनकी मांग के हिसाब से किताबों के बारे में बता रहे थे। यहां कोई हिस्ट्री की किताब मांग रहा था तो कोई पंजाब के बारे में पूछ रहा था, यहां फैली किताबों में अरुंधति की किताब ‘आज़ादी’ भी दिखी और मिर्ज़ा ग़ालिब का दीवान भी सजा था। ये लड़के आपस में बातें कर रहे थे लेकिन इन सबके बीच बैठे ज़िया-उल-रहमान पर मेरी नज़र पड़ी मुस्कुराता चेहरा और आगे बढ़-बढ़कर लोगों की मदद करने वाला। मैं अपनी स्टोरी के सिलिसिले में बातचीत कर रही थी कि तभी वो मेरे साथ आए दोस्त से बहुत ही घुलमिलकर बातें करते दिखे, मैंने पता किया कि क्या उन दोनों की पुरानी जान पहचान है? लेकिन मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बिल्कुल अभी मुलाक़ात के दौरान ही पहचान बनी है। मैं हैरान थी कोई पांच मिनट में किसी से इतना कैसे घुल-मिल सकता है? बहरहाल, जब हम बात कर रहे थे कि तभी हबड़-तबड़ करते हुए रोहित पहुंचें, चूंकि उन्हें पहले से पता था कि मैं आ रही हूं इसलिए वो मेरी स्टोरी में मदद करने की कोशिश में जुट गए। मैं, रोहित, ज़िया और मेरे साथ आए एक दोस्त स्टोरी की तलाश में निकल पड़े। तलाश स्टोरी की थी लेकिन क़िस्से आंदोलन के बारे में सुनने को मिले।
दो-दो की जोड़ी में आगे-पीछे होते हुए हम चारों चल रहे थे, कभी मैं रोहित से आंदोलन के बारे में पूछ रही थी तो कभी ज़िया से मज़ाक़ हो रहा था। वो मेरी खिंचाई करने लगते ”एक तो लड़की, ऊपर से मुसलमान, ऊपर से फ्रीलांस जर्नलिस्ट क्या मैडम आपको डर-वर नहीं लगता? ” तो मैं भी ज़िया से कहती ”क्यों ज़िया आप को डर नहीं लगता मुसलमान होकर आंदोलन के साथ जुड़े हो, तो वो मुस्कुरा दिए, उनकी इस मुस्कुराहट में मुसलमान होने के दर्द को मैं महसूस कर सकती थी, जिसका सरकारों के आने जाने से कोई मतलब नहीं था वो हमेशा से ही हुक़ूमत के मारे होने की कहानी बयां कर रही थी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो मैंने रोहित से नेट के बंद होने पर आई परेशानी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस दौरान वो क़रीब के ही नरेला के इलाक़े में जाकर पूरे दिन की ख़बरों को देख कर ख़ुद को अपडेट करते थे, मैं सोच रही थी कि ये कैसा ‘डिजिटल इंडिया’ बना जिसकी राजधानी में इंटरनेट लोगों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा? बिंदास ज़िया और अपने में ही गुम रहने वाले रोहित मेरे साथ चलते जा रहे थे। क़रीब 8 से 10 किलोमीटर में फैले सिंघु बॉर्डर में बिना फ़ोन नम्बर के किसी को तलाश करना बिल्कुल आसान नहीं था। उनके साथ स्टोरी की तलाश में मुझे क़रीब दो-ढाई घंटे हो चुके थे ये दोनों किसान आंदोलन के कोई बड़े नेता नहीं थे और ना ही कोई किसान, ये बस आम दो नौजवान लड़के थे, एक सिख और दूसरा मुसलमान। ये दोनों देश के किसानों के साथ खड़े थे और जैसे भी हो सके उन्हें अपना समर्थन दे रहे थे।
दोपहर से स्टोरी की तलाश में शाम हो चली थी हम चलते-चलते थक चुके थे। ज़रा रुक कर बैठ गए और पानी पीने लगे रोहित और ज़िया आपस में बातें कर रहे थे दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त बांडिंग ( Bonding ) थी। चलते-चलते कभी दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेते तो कभी मेरी स्टोरी के बारे में अपने आंदोलन के सर्कल में फ़ोन नम्बर तलाश करने लगते, तो कभी किसी मुसलमान को देखकर ज़िया दूर से ही ‘अस्सलाम…वालेकुम’ बोलता? मैं हैरान थी कैसे कोई मुसलमान इतने बिंदास तरीक़े से दुआ सलाम करते हुए चल रहा है। सब पानी पी रहे थे मैं चुपचाप इन दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि मैं स्टोरी की तलाश में भटक रही हूं जबकि स्टोरी मेरे साथ चल रही थी।
जिस वक़्त देश के माहौल में प्यार करना सबसे मुश्किल बात हो गई हो वैसे में इन दोनों की दोस्ती किसी ‘क्रांति’ से कम नहीं लग रही थी। ये वो ‘बग़ावत’ कर रहे थे जिससे नफ़रत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा लग रहा था? इनके इस ‘गुनाह’ को मैं ‘रिपोर्ट’ करना चाहती थी। जिस दौर में हमने बचपन के दोस्तों को मुल्क़ की बदली फ़िज़ा की वजह से खो दिया था उस वक़्त में इन दोनों की दोस्ती किसी मरहम से कम नहीं लग रही थी। सोशल मीडिया भले ही लोगों की दोस्ती के दायरे को बढ़ाता होगा लेकिन पिछले कुछ एक साल में, मैंने तो उन तमाम अज़ीज़ों को दूर जाते देखा है जिन्हें अब मुझ में दोस्त नहीं बल्कि एक मुसलमान दिखाई देने लगा। जिस दौर में सोच कर दोस्ती करने का नया दस्तूर बन गया हो वहां इन दोनों की दोस्ती को देखना बहुत सुकून देना वाला लगा। मैंने दोनों से पूछा क्या तुम मुझे इंटरव्यू दोगे ? ज़िया तो तुरंत तैयार हो गया लेकिन रोहित थोड़ा हिचकिचा रहा था पर उसने भी हां बोल दिया। और अजीब इत्तेफ़ाक देखिए जिस लाइब्रेरी में हमें इनका इंटरव्यू करना था उसके गेट पर भगत सिंह और अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान के बड़े-बड़े कट आउट आस-पास लगे थे। ये मेरी स्टोरी के लिए एक ख़ूबसूरत पैग़ाम था।
जब तक मैंने अपना इंटरव्यू शुरू नहीं किया था मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ज़िया हैदराबाद से हैं, मुझे लगा वो पंजाब से हैं क्योंकि मैंने उन्हें लोगों से पंजाबी में बातचीत करते हुए देखा था। मैं हैरान हो गई जब मुझे पता चला कि वो आंदोलन को समर्थन देने के लिए हैदराबाद से आ गए और 29 दिसंबर से यहीं जमे हैं। लेकिन जब मैंने पूछा ये दोस्ती, ये bond कैसा है? क्या ये मुस्लिम-सिख माइनॉरिटी कनेक्शन है? इससे पहले कि मैं अपना सवाल भी पूरा कर पाती ज़िया तपाक से बोल उठे ”नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ये इंसानियत का रिश्ता है। वो बताते हैं कि जब एनआरसी-सीएए प्रोटेस्ट हुआ था तो पंजाब से लोग पहुंचे थे उन्होंने लंगर लगाया था। उन्होंने साथ दिया था इसलिए मुझे लगा कि अब हमारी बारी है इसलिए हमें वहां पहुंचना चाहिए। वो बताते हैं कि हालांकि उन्हें घर से निकलते वक़्त इस बात का डर ज़रूर था कि पता नहीं आंदोलन में लोग उनके साथ घुले-मिलेंगे कि नहीं पर वो ख़ुशनसीब थे कि उन्हें पहले दिन ही यहां रोहित मिल गए जो 24 दिसंबर से इस आंदोलन से जुड़े हैं। ज़िया बताते हैं कि रोहित से जान-पहचान सालों पुरानी लगती है। ज़िया की ये बात मुझे भी सच लगी उन दोनों की दोस्ती वाकई सालों पुरानी लग रही थी। लेकिन जब मैंने पूछा एक मुसलमान होने के नाते उन्हें इस आंदोलन के साथ जुड़ने में डर नहीं लगा? तो वो कहते हैं कि ”मुसलमान होने के नाते सीएए से पहले डर-वर लगता था अब कोई डर नहीं लगता और अब तो इस आंदोलन में मैंने बहुत सारे मुसलमानों को जुड़ते देखा है, बहुत से मुसलमान आ रहे हैं”।

वहीं दिल्ली के ही रहने वाले सिख रोहित सिंह ने इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए एक दिन की छुट्टी मांगी थी नहीं मिली तो उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। मैंने रोहित से पूछा कि जब आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो क्या करोगे अब तो नौकरी भी नहीं है आपके पास? तो कहने लगे नौकरी तो आती जाती रहेगी इस वक़्त आंदोलन को मेरी ज़रूरत है इसलिए मुझे यहीं रहना है। रोहित को कल की चिंता नहीं इस वक़्त वो आंदोलन की रौ में बह रहे थे। मैंने रोहित से पूछा 26 जनवरी के बाद आंदोलन में कितना अंतर आ गया है तो वो बताते हैं कि 26 और 27 जनवरी के दिन आंदोलन पर बहुत भारी थे एक पल को ऐसा लग रहा था कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा जो संगतें 26 जनवरी के लिए ख़ासतौर पर आई थीं वो लौटने लगी थीं हमारा दिल डूब रहा था कि जिस आंदोलन के लिए हमने इतनी मेहनत की है वो कहीं बीच राह में ख़त्म ना हो जाए?
और पुलिस भी जब-तब आपको सिर्फ़ इस लिए रोककर पूछताछ कर रही थी कि आपके सिर पर पग बंधी हुई है। जिस वक़्त रोहित ये बात कर रहे थे मेरे ज़ेहन में उन मुसलमान लोगों की आपबीती तैरने लगी जिन्हें अक्सर महज़ इसलिए रोककर पूछताछ की जाती है क्योंकि उनका हुलिया मुसलमानों वाला है। सिर परskull cap है और सुन्नती दाढ़ी। क्या अपने मज़हब की पहचान को बरकरार रखना किसी को शक के घेरे में क़ैद कर सकता है? ख़ैर, रोहित आगे बताते हैं कि एक बार फिर सिंघु बॉर्डर के स्टेज ने सबकुछ संभाल लिया और इस बार मज़बूती पहले से कहीं ज़्यादा है। लेकिन जब मैंने पुलिस की नाक़ेबंदी पर सवाल पूछा तो रोहित कहने लगे मैडम उनकी ग़लती नहीं है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उन्होंने ख़ुद के साथ हुए एक वाक्या सुनाया कि कैसे वो इंटरनेट चलाने के लिए जब नरेला की तरफ जा रहे थे तो सादी वर्दी में तैनात कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया पूछा कहां जा रहे हो तो उन्होंने बताया कि पास में ही नरेला जा रहे हूं, तो उन पुलिस वालों ने कहां इस तरह अकेले घूमना अच्छा नहीं है। रोहित कुछ आगे बढ़े तो उन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने रोक लिया और एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया रोहित ने फिर से वही बातें दोहरा दी लेकिन इस बार सवाल कुछ और थे जैसे वो नीले पग वाले कौन होते हैं? वो तलवारें लेकर क्यों चलते हैं? वो इतने ख़तरनाक़ क्यों होते हैं? फिर पूछा क्या तुम्हारे पास भी तलवार है तो रोहित ने जवाब दिया कि मेरे पास तलवार तो नहीं लेकिन हां मैं कृपाण ज़रूर रखता हूं।
रोहित को वैसे तो कोई डर नहीं क्योंकि वो इस बात को लेकर बहुत श्योर है कि वो कुछ ग़लत नहीं कर रहा तो उसे किस बात का डर? उसका ये विश्वास ही उसे मज़बूती से इस आंदोलन के साथ जोड़े हुए है। लेकिन जब मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या पुलिस-प्रशासन का लोगों को आंदोलन में ना आने देना सही है? तो इसका जवाब ज़िया ने दिया वो कहते हैं कि इस आंदोलन को मज़बूती इसी बात से मिल रही है कि लोग जानना चाहते हैं कि रोका क्यों जा रहा है? जो लोग आ रहे हैं वो आंदोलन से जुड़ने से ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं कि हमें रोका क्यों जा रहा है? जिस दिन मैं ज़िया और रोहित का ये इंटरव्यू करके लौटी थी उसके अगले दिन ही रिएना का ट्वीट भी आ गया और उसमें भी कुछ वही बात थी जो ज़िया कह रहे थे। फिर क्या जिस आंदोलन को सरहदों में लपेट कर अपने ही देश के लोगों से काटने का काम किया जा रहा था उसके पैग़ाम को ट्वीट नाम की चिड़िया ने सोशल मीडिया के आसमान पर ऐसा फैला दिया कि फिर किसी सरहद का कोई मतलब ही नहीं बचा। ज़िया और रोहित दोनों ही चाहते हैं कि उनके इस आंदोलन से पूरा देश जुड़े या फिर सरकार जल्द ही किसानों की मांग मान ले। हालांकि 26 जनवरी की घटना के बाद आंदोलन के नेचर में कुछ बदलाव ज़रूर आया है।
हम चल रहे थे तो भूख लग गई लेकिन रास्ते में पंजाब के मलेरकोटला का लंगर दिखा, जहां गुड़ के चावल और चने डाल कर बनाई गई लज़ीज़ बिरयानी परोसी जा रही थी। ज़ायक़ा लाजवाब था इसलिए लंगर में भीड़ भी ठीक-ठाक थी। यहां मुझे लोगों को लंगर बांटने में मसरूफ़ इलियास क़ामिल साहब दिखे, जिन्होंने बताया कि 26 जनवरी की घटना के बाद गोदी मीडिया ने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की इसलिए हम और जोश के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। वो बताते है कि सिंघु बॉर्डर पर मलेरकोटला के पहले से ही दो लंगर चल रहे थे लेकिन हमने 26 के बाद एक तीसरा लंगर भी लगा दिया है। भाईचारे और मोहब्बत का पैग़ाम बांटने की कोशिश में लगे इलियास कहते हैं कि 26 के बाद लोगों की भीड़ और बढ़ गई है, और साथ ही गोदी मीडिया के मुंह पर चपेड़ (थप्पड़) भी लग गया है। वो कहते हैं कि जिन्हें भी आंदोलन को लेकर कोई शक है वो इस आंदोलन को गोदी मीडिया की नज़र से देखने की बजाए ख़ुद आकर देखें। (शायद वो कंगना को दावत दे रहे थे) साथ ही वो देशवासियों से गुज़ारिश करते हैं कि हमें मिलकर नफ़रत से लड़ना है। मलेरकोटला पंजाब को वो इलाक़ा है जहां के मुसलमान और सिखों की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं।
अक्सर सवाल उठता हैं कि 70 साल में देश को क्या मिला? इस सवाल का जवाब कौन देगा मैं नहीं जानती ? लेकिन जिसे हम देश का सोशल फैब्रिक कहते हैं उसे शायद 70 साल में हर लम्हा, हर दिन, हर साल विश्वास, भाईचारे, मोहब्बत के धागों से बहुत ही मुश्किल से बुना गया था। इसे तैयार करने में कड़ी मेहनत लगी थी बच्चों को किताबों में ही नहीं बल्कि उनकी तर्बियत में हिन्दू-मुस्लिम मोहब्बत का सबक पढ़ाया, सिखाया, रटाया गया था। और जब भी ये धागा कमज़ोर या ढीला पड़ता दिखता था उसे फिर से मज़बूत किया जाता था। लेकिन अब लगता है कि 70 साल की मेहनत को एक झटके में तबाह कर दिया गया है अब क्या पता उस गंगा-जमुनी तहबीज़ के रेशमी धागे को तैयार करने में कितना वक़्त लगेगा एक-दो पांच या फिर पचास साल?
(नाज़मा ख़ान स्वतंत्र पत्रकार हैं।) ये उनके निजी विचार हैं। सौज- न्यूजक्लिक