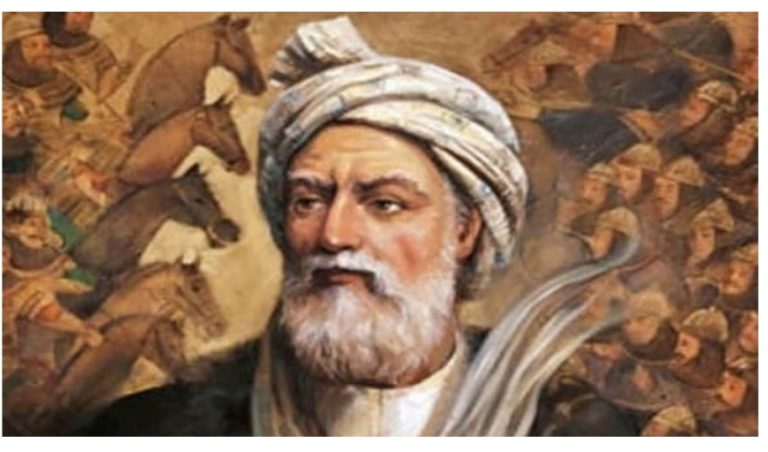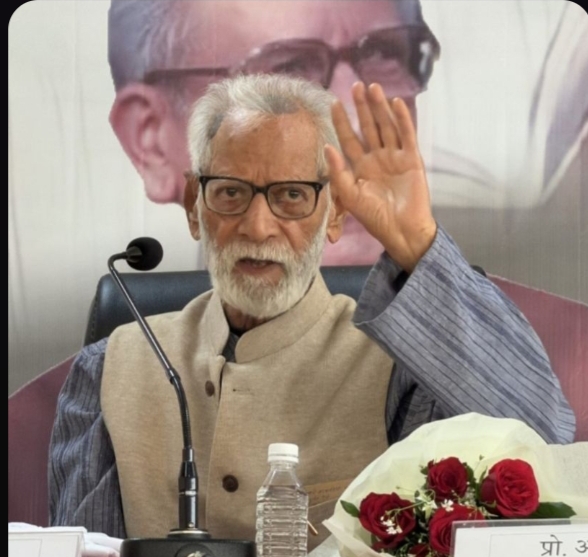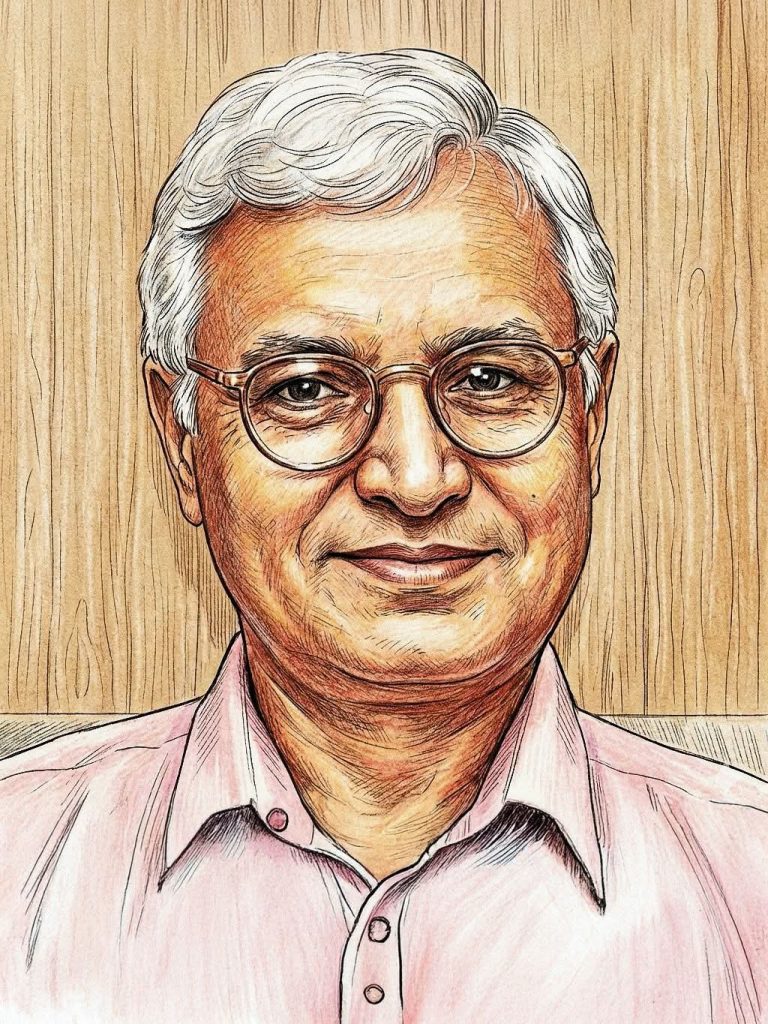मैं बैठा हूँ। सामने वह बैठी है। दावत खत्म हो चुकी है और लोग जा चुके हैं। मगर लगता है हर व्यक्ति अपनी एक एक आहट और एक-एक परछाई छोड़ गया है। हम अकेले हैं मगर इन आकृतियों और आहटों से घिरे हुए हैं।

मैं सोफे पर हूँ, वह सामने दीवान पर पैर चढ़ा कर। अक्सर ऐसा होता है कि मैं दीवान पर अधलेटा, वह सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी रहती है। मगर आज जगह उलट-पुलट हो गई है। दावतें कई हुई हैं, मगर याद नहीं आ रहा है कि जगहें पहले भी उलट-पुलट हुई हों। शायद हुई हों, मगर विचार कभी उलट-पुलट नहीं हुए। या हो सकता है हमारे जाने-अनजाने हुए हों। कभी-कभी कोई मामूली अन्तर विचारों को छू जाता है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। एक अरसे से आमने-सामने बैठे रहने वाले दो लोग। जरूर हमने आपस में कई महत्वपूर्ण कार्य किये होंगे। मगर अभी लग रहा है जैसे सारी जिन्दगी बस यूं ही आमने-सामने बैठे रहे हैं। बस, आज बैठने की जगह भर बदल गई है।
उसका नाम नीरा है, मेरा आकाष। दावत में कई नाम के स्त्री पुरुष आए। फिर सारे नाम चले गये। रह गए नीरा और आकाष। आकाष और नीरा- आमने-सामने। ऐसा भी हो सकता था कि जाने वाले नामों के साथ एक आकाष नाम चला जाता और एक राकेष नाम रह जाता। तब यहाँ राकेष और नीरा आमने-सामने बैठे रह जाते। यूँ, या किसी और अपने ही खास अंदाज में। हो सकता है, राकेष उठकर नाइटगाउन पहनने चला जाता और नीरा सोफे पर बैठी निटिंग करने लगती। मगर हकीकत यह है कि अभी यहाँ यही दो नाम बचे हैं – नीरा और आकाष।
नीरा सामने बैठी है और कभी-कभी मुझे देख ले रही है। मानो कुछ पूछना चाहती हो। मगर पूछने की जरूरत समझ नहीं पा रही हो। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मगर जैसे बोलना भूल गया हूँ। लगता ही नहीं इस कमरे में बैठकर हम लोग काफी देर तक बातें करते रहे हैं। ढेर सारे लोगों से घुलते-मिलते रहे हैं। साथ-साथ बैठकर चाय पी है। सिर्फ एक बोझ- पीठ, कंधो, कानों, भवों पर सवार है। यह उन अलग-अलग जेहनों का बोझ है जो वह और मैं अभी तक ढोते आए हैं। बोझ, जैसे एक बेहद ठोस और ठण्डे लोहे के संदूक का वजन। वह शांत बैठी हुई है, लेकिन दरअसल उसने बहुत मेहनत से अपने बक्से को उठा रखा है। वह चाहती है कोई एक खाली जगह, जहाँ वह अपने बक्से को उतार कर रख दे। मगर यहाँ आसपास बक्से ही बक्से छितराए पड़े हैं।
यह महज आज की ही बात नहीं है, जाने कब से हम लोग यूँ ही एक-एक बक्सा उठाए हुए हैं। हम जहाँ भी जाएँ, ये बक्से हमारे साथ-साथ जाते हैं। कभी सर पर सवार, कभी पैरों से बंधे घसीटाते हुए। अक्सर, हमने अपने बक्से अदल-बदल भी किये हैं। जैसे अभी पार्टी में। अनगिन अदल- बदलियाँ। मगर बक्से-धीरे-धीरे अपनी जगह पर वापस लौट आते हैं। कभी-कभी अपने जैसे किसी बक्से से रगड़ाने-टकराने के चलते उनमें एक चमक-सी फूटती है। और हम मान बैठते हैं कि कोई अन्तर आ गया।
बगल के कमरे में कुछ बच्चे सोये हुए हैं। ये बच्चे न जाने कब, कहाँ से, अचानक यहाँ आकर रहने लगे। घर की दीवारों, कोनों, सीढ़ियों और छज्जों पर अचानक फूट पड़ने वाले तरह-तरह के पौधों की तरह ये भी धीरे-धीरे घर में उग कर यहाँ की फ़ज़ा पर हावी होते चले गए। ये सोये बच्चे। अंतरिक्ष के सितारों की तरह सुदूर और निस्संग। अपनी अपनी कक्षा में। अपनी अपनी धुरी पर कायम।
नीरा के हाथों ने अभी-अभी हरकत की है। मानो कोई ठोस निर्णय लिया हो। भविष्य को प्रभावित करने वाला निर्णय। दाएँ हाथ से आंचल को व्यवस्थित करना और अखबार उठाकर वापस पूर्ववत रख देना। इससे मुझे फिर पार्टी की याद आ गई है। और उस गहमागहमी में शरीक वे तमाम नाम। हरेक के आगे-पीछे ठोस सख्त शून्य। और उन शून्यों के बीच की हरकतें, जो हमेषा ठोस निर्णय सी लगती हैं।
और वे अक्स! नमों के साथ खास-खास तरह के ऑंख, भँव, हाथ, बाल, कहकहे और इषारे। अक्स जो नामों के थे। नाम जो गम्ज़ों और इषारों के हैं। नीरा एक खास प्रकार की अदा का नाम है। अगर किसी शीला या राधा पर यही अदा प्रक्षेपित कर दी जाय तो! इससे भी आसान- इस सामने बैठे नीले ब्लाउज को हरे या पीले ब्लाउज में बदल दिया जाय तो! मेरे ही कंधे यदि थोड़े झुक जाएँ तो शायद मैं आकाष से किसी प्रदीप की तरह प्रस्थान कर जाऊँ। हाँ हो सकता है पूरा-पूरा प्रदीप भी न बन पाऊँ। बीच का कोई हरी या महेष बनकर रह जाऊँ।
जैसे अभी-अभी मुझे लगा था कि नीरा अखबार उठाते-उठाते कुछ-कुछ पूनम बन गई थी। मगर ऑंचल को ठीक करते वक्त वह वापस नीरा बन गई फिर उसने जिस चप्पल में पैर डाला वह नीरा का ही था। अच्छा हुआ पार्टी में आए किसी नाम ने नीरा की चप्पल पहन कर जाने की गलती नहीं की। वर्ना नीरा षायद पूनम में बदल जाती। पूनम जो आकाष की पत्नी नहीं है। या कौन जाने! क्या पता इसी बीच नीरा ने मुझमें किसी अखिलेष या प्रवीण को देख लिया हो। और चौंकने से पहले आकाष को वापस कर खीज गई हो!
दरअसल हम दोनो लगातार खीजे रहने वाले लोग हैं। कभी किसी अवसर पर- किसी पार्टी या समारोह के बीच या बाद में, या बाजार में फुटपाथ पर चलते हुए- किसी अन्य में बदलते-बदलते वापस खुद में डूब कर खीजना। नीरा और आकाष दो अलग-अलग खीजों के नाम हैं जो अंतरिक्ष में उड़ते-उड़ते अचानक टकरा गए। फिर एक दूसरे की गुरूत्वकक्षा में आकर परस्पर लिपटे-लिपटे सूर्य की परिक्रमा किये जा रहे हैं।
या ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों में कोई एक वास्तविक हो, दूसरा छद्म। यानी ‘मैं’, अपनी तमाम सूक्ष्मताओं स्थूलताओं और जटिलताओं के साथ एक पूर्ण ‘मैं’- एक स्वप्न मात्र हूँ, जिसे नीरा नाम की खीज देख रही है। सघन निद्रा में खोई खीज का स्वप्न होना, यह एक अच्छा ख्याल है जो मुझे बहुत सी दुष्चिन्ताओं से मुक्ति दिला रहा है। कुंठा और अपराध बोध की तो यहाँ जगह ही नहीं रह जाती है। आह, यह कैसी सुखद अनुभूति, इसमें स्वर्ग की शराब का नषा है!
यह घर, जो मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। और उसे चारों ओर से घरेता एक और- घर का घर। मुझे हमेषा लगता रहा है कि इस घर का भी एक घर है। जिसके अन्दर तरह तरह के रूपों में, अलग-अलग अदाओं के साथ, यह घर रहता है। अभी पार्टी से पहले यह एक अन्य घर था। फिर एक दूसरा घर हो गया। और अब धीरे-धीरे यह अपने पुराने रूप-रंग में लौट रहा है। अभी-अभी दीवालों का प्लास्टर अपने पुराने रूप में आया है। कुछ ही देर में फर्ष, खिड़कियाँ, छत और छज्जे- पोचाड़ा और रंगरोगन- सुबह वाले घर जैसे हो जाएँगे। फिर पर्दे लौटेंगे, फिर नल का टप-टप टपकता पानी पहले की सी आवाज को पहन लेगा, फिर स्टोव की चमक। कभी-कभी पूर्ववत होने का यह काम बड़ी तेजी से होता है। सनाक-से, पलक झपकते ही, जैसे कोई रिफलेक्स-ऐक्सन हो। मुझे पता भी नहीं चल पाता। कभी बहुत धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता। जैसे अभी हो रहा है।
घर का इस तरह रूप बदलना, एक सफर की तरह या जैसे कोई छोटा बच्चा पार्क में जाए और लौटे। मैंने बहुत से घरों को व्यस्क उम्र की लम्बी यात्राओं पर जाते और अर्से बाद थके-हारे लौटते देखा है। कुछ ऐसे भी घर हैं जो जाकर लौटे ही नहीं। शुक्र है, अपना घर अभी ऐसी सनक का षिकार नहीं हुआ है- अभी तक तो नहीं। अभी तो बस, छोटी-छोटी भटकनें हैं। कहीं जाना, और फिर धीरे-धीरे लौट आना। जैसे इस वक्त हो रहा है- पूरी तरह अपने में वापस आता हुआ घर। कल सुबह, या हद से हद दोपहर तक सब कुछ पूर्ववत हो जायेगा। सब कुछ- या हो सकता है इसी बीच वह कहीं, किसी पड़ाव पर ठहर जाए। कल हो सकता है इसी घर में कोई आए और मेरी जगह किसी सुकांत या सुधीर को खोजे।
अभी-अभी मेरे सामने टंगी दीवाल घड़ी जरा-सी हिली है। मैंने गौर किया है, स्तब्ध पलों में घड़ियाँ इसी तरह हिल उठती हैं। लगता है, एक पल के लिए किसी और ब्रम्हाण्ड का समय भटक कर इस ब्रह्माण्ड के समय से टकरा गया हो। या हो सकता है, यह ब्रह्माण्ड ही, यानी एक पल के लिये, अपने होने से उकता जाता हो। और रूप बदल लेता हो। फिर खीज के साथ पूर्वस्थिति में लौटता हो। अपना ब्रह्माण्ड अभी षिषु है। छोटी-मोटी भटकनों के बाद वापस लौट आने वाला। कुछ ऐसे भी ब्रह्माण्ड होंगे जो अनिष्चित काल के लिए भटक गए होंगे।
नीरा कब की उठकर जा चुकी है। सामने की जगह खाली है। मैं जैसे अनंत काल से यहाँ इसी प्रकार बैठा हूँ, एक नाम के बारे में सोचता हुआ जिससे मेरा जुड़ाव सिर्फ इसलिए है कि मैंने उसके बारे में सोच रखा है। यह सोच ही मेरी कृति है। अपनी कृति के बारे में शायद इसी प्रकार का लगाव पैदा होता है। भगवान ने भी शायद दुनिया को सोच ही रखा है। ईष्वर यानी आकाष, और दुनिया यानी नीरा। या शायद ईष्वर- नीरा और दुनिया- आकाष। दोनाें आमने-सामने। एक दिन भगवान या दुनिया- कोई एक हट जाएगा। तब उसके द्वारा खाली की गई जगह, सामने वाली भरी जगह को वैसे ही घूरेगी, जैसे अभी खाली दीवान सोफे को घूर रहा है।

अभी एक खाली दीवान, एक भरे हुए सोफे को घूर रहा है। जैसे चुनौती दे रहा हो। कुछ समय बाद, हो सकता है एक खाली सोफा एक खाली दीवान को ताके। यह भी एक खेल ही है जिसे हम चारों खेलते रहे हैं- मैं, नीरा, सोफा और दीवान। कभी वह उठ जाती है तो कभी मैं, और खेल शुरू हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि कभी हम दोनों एक साथ उठे। इसलिए यह पता ही नहीं लग पाया कि एक साथ उठ जाने से सोफा और दीवान कैसे लगने लगते हैं, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है, तब वे अपने आपे में आ जाते होंगे। खालीपन, जो उन पर हमारे बैठ कर काबिज हो जाने से उनके व्यक्तित्व में घर कर जाता होगा, हमारे उठते ही धीरे-धीरे भरने लगता होगा। और भरेपन का अहसास, आहिस्ता-आहिस्ता भीतर पैठता जाता होगा-जैसे कुएँ में पानी सीपाता है।
बिजली चली गई है। सब कुछ फुस्स- होकर रह गया है। अब यहाँ कोई सृष्टि नहीं है। मेरा विष्वास भी थोड़ा डगमगा-सा गया है। यह चलते-चलते अचानक रुक जाने जैसा कुछ। अन्दर बेडरूम से जुगनू जैसी एक टिमटिमाहट आई है। टार्च या मोमबत्ती। नीरा ने, या किसी और ने जलाई होगी। किसी और कौन ? दरअसल यहाँ एक स्त्री और भी है। मेरे जेहन के भीतर समाई एक दूसरी। उजाले वाली नीरा, और अंधेरे वाली एक कोई और। जैसे ही अंधेरा होता है, यह औरत उपस्थित हो जाती है। क्या नीरा के पास भी दो आकाष हैं ? शुरू-षुरू में मुझे लगा था। हल्का-सा आभास भर, मगर उसके बाद नीरा ने बड़ी चतुराई के साथ दूसरे वाले को मार डाला। औरतें यह काम बड़ी आसानी से अंजाम दे लेती है, कसाईवाला।
बिजली आ गई है। एक नई दुनिया, अपार संभावनाओं भरी। चमकती-कौंधती, नवजात-क्रंदन करती हुई। मगर फिर बहुत जल्द बूढ़ी होती हुई। जर्जर होती, रंग और चमक खोती हुई। और अब, यह सामने मटमैली सी, उनींदी, उदास-उदास दुनिया। यह एक दूसरा ही खेल है। कभी किसी लम्हे नीरा और मैं- दोनों बीस वर्ष पहले जैसे खिलकर-चमककर, अगले ही पल जैसे बुढ़ा जाते हैं। यह लुकाछिपी का खेल, मानो किसी सुरंग में घुस जाना और फिसलते हुए दूसरी तरफ तेजी से बाहर निकल जाना।
नीरा ने भीतर से दो-एक बार आवाज़ दी है। आवाज़ें मगर किस काम की ? जब हम सभी रंगों को चुगने वाले मुर्गे बन चुके हैं। जब कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ होना- सन्नाटों के रंगों को चुगने के समान होता है। इतनी अनगिनत विडम्बनाओं के बीच!
रंग- कितनी जल्दी हरे होते और कितनी तेज़ी से मुर्झाते हैं! देखते-देखते हरे भरे, चटख रंग- धूसर, फिर मटमैले, फिर काले-स्याह हो जाते हैं। जिस जनरल स्टोर की सीढ़ी पर नीरा और मैं मिले थे, वहाँ कितने चटख रंग छिटके पड़े थे! और अब, यही एक धूसर लकीर बाकी बची है।
भीतर से फिर कुछ आवाजें आई हैं। मैंने अभी-अभी कमरे का स्विच ऑफ किया है। स्विच ऑफ होते ही चाराें तरफ फैली अस्तव्यस्तता मिट-सी गई है। यह भी आष्वासन करने वाला मामला है। यह भीतर तक धंसती हुई शांति और ठण्डापन।
शांति और ठंडापन।
आनंद बहादुर वरिष्ठ कथाकार हैं । पिछले चार दशक से उनकी कहानियां,कविताएं, गज़ल, अनुवाद और लेख देश की प्रमुख हिन्दी पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहे हैं । हाल ही में उनका कहानी संग्रह ‘ढेला और अन्य कहानियां’ प्रकाशित हुआ है। साहित्य के साथ उनकी रुचि संगीत में भी है। वर्तमान में केटीयू पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलसचिव हैं। संपर्क- 8103372201