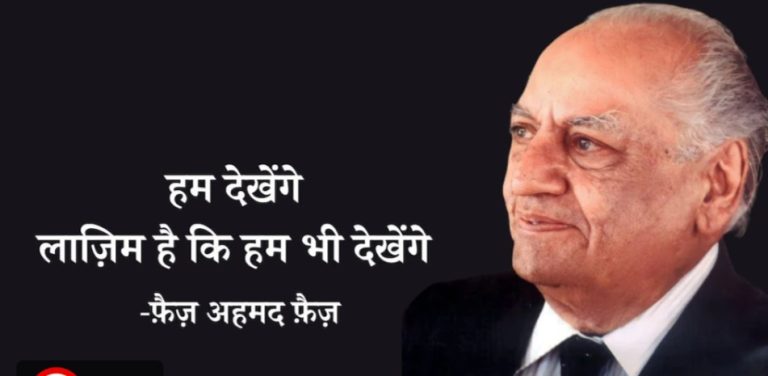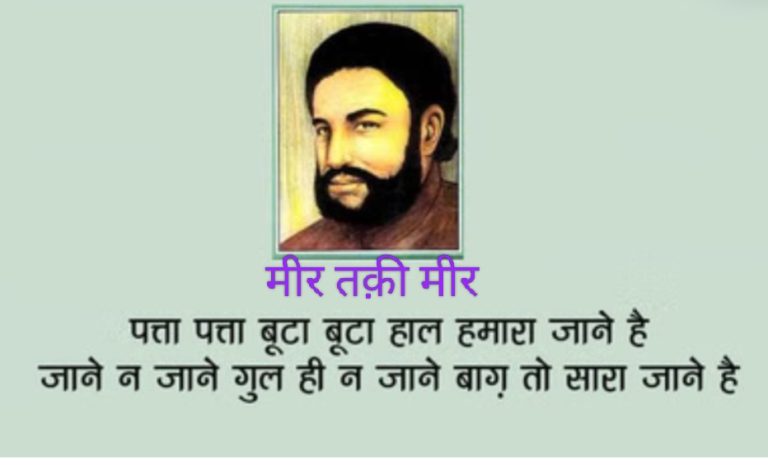विकास बहुगुणा
इन दिनों समाज के एक बड़े तबके में बुद्धिजीवी निंदा और कटाक्ष का विषय हैं .‘एक वक्त था, जब मूर्ख होना गाली था. अब बुद्धिजीवी होना गाली है…. बात गाली तक होती तब भी ठीक था. समाज में बुद्धिजीवियों से नफरत इस तरह है कि उन्हें मिटाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं.’
एक व्यंग्य में लिखी गई चर्चित लेखक राकेश कायस्थ की यह बात मौजूदा समय का कड़वा सच है. इन दिनों समाज के एक बड़े तबके में बुद्धिजीवी निंदा और कटाक्ष का विषय हैं. उनके लिए टुकड़े-टुकड़े गैंग और सिकुलर्स जैसे तमाम शब्द गढ़ लिए गए हैं. सोशल मीडिया में उन पर कीचड़ उछाला जाता है. असल जिंदगी में भी उनके मुंह पर कालिख मलने की घटनाएं हो चुकी हैं. उन्हें जेल भेजने की मांग होती है. गोविंद पानसारे और एमएम कलबुर्गी जैसे बुद्धिजीवियों की तो हत्या तक हो चुकी है.
बुद्धिजीवी समाज की चेतना माने जाते हैं. कहा जाता है कि उनके बिना समाज अंधा हो जाता है. इतिहास में झांकें तो कई बड़े सामाजिक-राजनीतिक बदलावों के उत्प्रेरक और अगुवा बुद्धिजीवी ही रहे हैं. अपने एक लेख में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू लिखते हैं, ‘प्रत्येक महान क्रांति का नेतृत्व बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया. उदाहरण के लिए – फ्रांसीसी क्रांति में रोबेस्पियर और डैंटन, अमेरिकी क्रांति में जेफ़रसन, जेम्स मैडिसन और जॉन एडम्स और रूसी क्रांति में लेनिन.’ वे आगे कहते हैं कि बुद्धिजीवी एक सोशल इंजीनियर होने के अलावा जनमत को दिशा देने और नए विचारों को फैलाने वाला भी होता है जो उन आदर्शों का प्रचार करता है जिनके लिए लोगों को संघर्ष करना चाहिए.’
भारत के संदर्भ में इस बात को और सरल तरीके से समझा जा सकता है. महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई बुद्धिजीवियों ने देश की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी. स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का स्वरूप क्या हो, यह तय करने में भी उनकी अहम भूमिका रही. सामाजिक सुधार के मोर्चे पर भी उन्होंने कई असाधारण काम किए. इसके चलते देश-समाज से उन्हें खूब समर्थन और सम्मान भी मिला.
तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज बुद्धिजीवियों के खिलाफ नफरत की आंधी चलती दिख रही है?

इस सवाल के जवाब को समझने की शुरुआत मानव स्वभाव को समझने से की जा सकती है. मनोविज्ञानी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों में खुद से ज्यादा तेज दिमाग वाले किसी शख्स के लिए एक सहज ईर्ष्या का भाव रहता ही है. यानी ऐसे लोगों के लिए एक स्वाभाविक नापंसदगी इसलिए भी होती है कि वे बाकी लोगों को हीन महसूस करवाते हैं. यह नापसंदगी अपना हीनताबोध कम करने में इन लोगों की मदद करती है.
लेकिन यह नापसंदगी सामाजिक रूप से इस कदर व्यापक और गहरी कैसे हो जाती है कि बुद्धिजीवियों की जान को ही आफत हो जाए जैसा कि इन दिनों भारत में हो रहा है? इस सवाल के जवाब के लिए दोनों तरफ देखना होगा. बुद्धिजीवियों के खिलाफ नफरत की कुछ वजहें बाहरी हैं तो झोल उनकी खुद की तरफ से भी कम नहीं हैं.
अगर पहली श्रेणी के कारकों को देखें तो पहली और सबसे साफ बात तो यही है कि आज बुद्धिजीवियों के खिलाफ एक तरह का संगठित अभियान चलाया जा रहा है. जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी कहते हैं, ‘सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि कोई बुद्धिजीवी – जिसने अपने जीवन के कई दशक गहन अध्ययन को दिए हैं – कोई बात कहता है तो ट्रोल तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं. उसे कुछ भी कह देते हैं. और ये सिलसिला सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े व्यक्तियों तक जाता है.’
कई लोगों के अनुसार इस मामले में स्थिति इसलिए भी इतनी गंभीर है क्योंकि वर्तमान समय में तमाम तरह के विचारों को ही एक गैरजरूरी चीज़ माना जा रहा है. उदाहरण के तौर पर आज मानवता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति में मौजूद रहे समावेशी तत्वों आदि से जुड़े विचार न केवल एक बड़े तबके को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं बल्कि इनमें भरोसा रखने वाले और इनकी बात करने वाले लोग भी उन्हें अपने, समाज और देश के दुश्मन या मूर्ख लगते हैं. ‘आज माहौल ऐसा बना दिया गया है जिसमें अनपढ़ता आपका गहना है और पढ़ा-लिखा-समझदार होना आपकी मूर्खता’ हृदयेश जोशी कहते हैं.
इस प्रक्रिया में अक्सर उस सच को संदिग्ध बनाने की कोशिश की जाती है जो बुद्धिजीवियों के विचारों को संदर्भ या आधार देते हैं. जैसा कि अपने एक लेख में वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी कहते हैं, ‘कभी कहा गया था कि बुद्धिजीवी का काम सत्ता से निडर होकर सच बोलना है और अब कहा जा रहा है कि सच क्या है यह बेहद संदिग्ध मामला हो गया है.’ इस वजह से ऐसे सच पर टिके विचार और उन्हें हमारे सामने रखने वाले बुद्धिजीवी भी संदिग्ध लगने लगते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर गांधी, नेहरू, संविधान, धर्म की पुरानी मान्यताओं आदि को ही अगर संदिग्ध बना दिया जाए तो अपने विचारों में उन्हें शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा.
इतिहास बताता है कि विचारों और सवालों को खतरा मानने वाली सत्ताएं हमेशा से समाज के लिए एक नई सच्चाई गढ़ने की कोशिश करती रही हैं और फिर इनके आधार पर बुद्धिजीवियों की एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है मानो वे किसी एजेंडे के तहत ही किसी विचारधारा या वर्ग का समर्थन या विरोध करते हैं, सही या गलत के आधार पर नहीं. लेकिन इस आरोप को अगर बुद्धिजीवी वर्ग चाहे तो पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय गायक-संगीतकार कबीर सुमन के जरिये नकारने की कोशिश कर सकता है. कभी उन्होंने राज्य में सत्ताधारी सीपीएम की बर्बरताओं का तीखा प्रतिरोध किया था. कबीर सुमन बाद में तृणमूल के सांसद बन गये. फिर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया.
अपने एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन कहते हैं, ‘लेखक और संस्कृतिकर्मी हमेशा प्रतिपक्ष में ही रह सकते हैं.’ उनके मुताबिक ‘इमरजेंसी में फणीश्वरनाथ रेणु और शिवराम कारंत ने अपने पद्मसम्मान लौटाए. रेणु, नागार्जुन, रघुवंश, हंसराज रहबर, गिरधर राठी, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जैसे लेखकों, कुमार प्रशांत जैसे गांधीवादी और कुलदीप नैयर जैसे पत्रकारों सहित अलग-अलग भाषाओं से जुड़े ढेर सारे प्राध्यापकों और बुद्धिजीवियों ने जेल काटी. यह सिलसिला हमेशा बना रहा है. 2009 में शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ सात लोगों ने अपने घोषित पुरस्कार लेने से इनकार किया.’
लेकिन कुछ समय पहले जब देश में बढ़ती असहिष्णुता का हवाला देकर लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटाए या फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी तो केंद्र में सत्तासीन भाजपा द्वारा इसे इस तरह पेश किया गया मानो बुद्धिजीवी हमेशा भाजपा के खिलाफ रहे हों. तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था कि ये लोग दशकों से भाजपा के पीछे पड़े हैं और 2002 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी वैचारिक असहिष्णुता के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं. उधर बुद्धिजीवियों का आरोप है कि चूंकि निष्पक्ष मीडिया और प्रभावी विपक्ष के अभाव को वे लोग अपने विचारों और क्रियाकलापों से भरने की कोशिश कर रहे थे इसलिए सत्ता पक्ष द्वारा येन-केन प्रकारेण उन्हें बदनाम करके अपना रास्ता निष्कंटक करने के प्रयास किये जाते रहे हैं.
यह तो हुई एक पक्ष की बात. लेकिन बहुतों का मानना है कि सवाल दूसरी तरफ भी हैं. यानी मौजूदा हालात का दोष काफी हद तक बुद्धिजीवियों पर भी आता है. यह सही है कि कई बुद्धिजीवी अपनी विद्धता की वजह से सामान्य लोगों को हीनता का अनुभव करा सकते हैं लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती. अपने एक आलेख में शिव विश्वनाथन लिखते हैं कि लेफ्ट लिबरल्स ने भारतीय मध्यवर्ग को उनकी परंपराओं और विश्वासों को लेकर भी शर्मिंदा किया और नीचा दिखाया. उनके धार्मिक होने को लगभग सांप्रदायिक होना करार दे दिया. सरकार बनाने के बाद दक्षिणपंथी नेताओं ने उन्हें इस शर्म से बाहर निकालते हुए यकीन दिलाया कि उनकी परंपरा और विश्वास सर्वश्रेष्ठ हैं. और उनका दिल जीत लिया.
‘बुद्धिजीवियों के साथ दिक्कत ये भी है कि उनमें बहुत हद तक बौद्धिक बेईमानी रही है और इसने लोगों को उन पर हमला करने का मौका दे गया है जो उनसे घृणा करते हैं. मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की 215 घटनाओं की जांच की मांग खारिज कर दी. लेकिन भारत के बुद्धिजीवियों ने इस पर कोई विमर्श नहीं किया. बहुतों को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं होगा. अब इसकी तुलना 2002 के गुजरात दंगों से कीजिए. 1990 में कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से निकाला गया जो बहुत दुखद घटना थी. मुस्लिम कट्टरपंथियों ने यह काम किया. मस्जिदों से ऐलान हुए. ये इस्लाम का एक भद्दा चेहरा था. लेकिन आप उस पर बोलना तक नहीं चाहते’ हृदयेश जोशी कहते हैं.
आरोप यह भी लगते हैं कि बुद्धिजीवियों ने इतिहास लेखन में भी पूरी ईमानदारी नहीं बरती. जैसा कि हृृदयेश जोशी कहते हैं, ‘हम मुस्लिम-दलित एकता की बात करते हैं. जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री थे. उन्होंने विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया था. लेकिन वहां उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत इतनी सांप्रदायिक थी कि वे व्यथित होकर भारत वापस आ गए. लेकिन इन बातों पर ज्यादातर बुद्धिजीवी बात नहीं करते.’ वे आगे जोड़ते हैं, ‘इसी तरह डॉ भीमराव अंबेडकर ने हिंदुओं को कितनी गालियां दीं, इस पर खूब बात होती है लेकिन मुस्लिमों के बारे में उनके क्या विचार थे. अंबेडकर ने उन्हें कितनी फटकार लगाई थी, ये बात बुद्धिजीवी नहीं लिखते.’
दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय तक पढ़ा चुके और इन दिनों अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर दिलीप सिमियन का मानना है कि बुद्धिजीवियों के लिए पैदा हुई यह नफरत असल में एक लंबे अरसे में घटित हुई प्रक्रिया का परिणाम है. एक समय नक्सल आंदोलन से जुड़े रहे प्रोफेसर दिलीप सिमियन कहते हैं, ‘असल में हर तरह के बुद्धिजीवियों ने पक्षपात किया. पक्षपात का मतलब यह नहीं कि सही-गलत का अंतर करना, या सच्चाई और झूठ का भेद करना. वो तो हर बुद्धिजीवी को करना ही पड़ेगा. लेकिन अगर पहले से ही सामने वाला आदमी पहचान लेता है कि ये बुद्धिजीवी क्या बोलने वाला है. वह क्या उजाले में लाएगा और क्या अंधेरे में रखेगा तो यह बात सही नहीं है. यह बात मैं बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों के बारे में कह सकता हूं और कइयों को तो यह अहसास भी नहीं होगा. आप मेरा सम्मान तभी करेंगे जब आप मेरे पास कोई प्रश्न लेकर आएंगे और आपको जिज्ञासा होगी ये जानने की कि मैं क्या कहता हूं. अगर आपको पता ही है कि मैं किस दिशा में क्या कहूंगा तो आप मेरे पास क्यों आएंगे. समस्या यही है.’
हृदयेश जोशी की बात आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर दिलीप सिमियन यह भी कहते हैं कि बुद्धिजीवी असल में जिसे विचारधारा कहते हैं वह उनकी मोहमाया है. क्योंकि धारा तो चलने का नाम है जबकि बुद्धिजीवी जड़ हो जाते हैं. वे कहते हैं, ‘सच्चाई किसी खेमे की संपत्ति नहीं हो सकती. अगर बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी वजह से सच्चाई का एक हिस्सा छिपा रहे हैं. मैं पिछले 15-20 साल से कश्मीरी पंडितों की बात भी करता रहा हूं. तो मेरे कई साथी कहते हैं कि आप तो प्रतिक्रियावादी ताकतों का साथ दे रहे हो. लेकिन ज्यादती हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ या फिर किसी भी समुदाय के व्यक्ति के साथ, वह तो ज्यादती ही होती है.’
कई और लोग भी मानते हैं कि भारत के बुद्धिजीवी तबके का एक बड़ा वर्ग बहुत पहले ही खुला दिमाग, निष्पक्षता और दूसरे विचारों के प्रति सहिष्णुता जैसे उन गुणों से दूर हो चुका था जो बुद्धिजीवी होने की जरूरी शर्त होते हैं. अपनी एक टिप्पणी में चर्चित लेखक मिन्हाज मर्चेंट कहते हैं, ‘भाजपा निश्चित रूप से उदारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन विपक्ष उससे भी कम उदारवादी है. कांग्रेस को ही देखिए जो उदारवाद के हर सिद्धांत को धता बताती हुई गुणों से ऊपर गांंधी परिवार के प्रति वफादारी को तरजीह देती है. तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा और आरजेडी ने धर्म और जाति को भाजपा की तुलना में ज्यादा बुरी तरह इस्तेमाल किया है.’ वे आगे लिखते हैं कि इसके बावजूद भारत के बुद्धिजीवी इस मामले में अपनी आलोचना में हमेशा एकपक्षीय रहे. यानी उन्होंने धर्म के इस्तेमाल को लेकर भाजपा पर तो सवाल उठाए, लेकिन दूसरी पार्टियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न वर्गों के तुष्टिकरण पर चुप्पी साधे रखी.
मिन्हाज मर्चेंट की बात सरसरी तौर पर सही तो लगती है लेकिन इससे जुड़ा एक पहलू और है. ऐसा नहीं है कि हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने दूसरी राजनीतिक पार्टियों के गलत कामों को गलत नहीं कहा. लेकिन ज्यादातर मामले में अपेक्षाकृत हल्के तरीके से ऐसा तब किया गया जब भाजपा पर गंभीर सवाल उठाने से पहले खुद को निष्पक्ष दिखाने की जरूरत महसूस हो रही हो. या फिर ऐसा लग रहा हो कि अब भाजपा के बारे में बहुत लिख-बोल लिया तो थोड़ा कांग्रेस या दूसरी पार्टियों पर भी विमर्श कर लिया जाये.
जानकारों के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ कि भारत में अधिकांश बुद्धिजीवी उस खेमे के हैं जिसे वामपंथ कहा जाता है और जो हिंदुत्व की विचारधारा को सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है. मिन्हाज मर्चेंट लिखते हैं, ‘बुद्धिजीवियों का काम बहस का स्तर समृद्ध करना होता है, दूसरी विचारधाराओं से हिसाब बराबर करना नहीं.’ उनके मुताबिक यही वजह है कि लोगों ने बुद्धिजीवियों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया.
चर्चित राजनीतिक चिंतक अभय दुबे ने अपनी हालिया किताब ‘हिंदुत्व बनाम ज्ञान की राजनीति’ में बड़े साफ तरीके से इस बारे में लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग आज हिंदू या बहुसंख्यक विरोधी क्यों दिखते हैं. वे इसका कारण अल्पसंख्यकों के अधिकारों व हिंदू सांप्रदायिकता पर ही ध्यान देने और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की अनदेखी के साथ-साथ धर्मनिरपेक्षता के मामले में कांग्रेस पार्टी के दोगले व्यवहार से मुंह फेर लेने को मानते हैं. अभय दुबे मानते हैं कि अपनी विचारधारा और विरासत के चलते वामपंथी बुद्धिजीवियों संघ परिवार से जुड़े उन तथ्यों को अनदेखा किया जो उन्हें असुविधाजनक लगते थे. उन्होंने संघ और उससे जुड़े संगठनों को सांप्रदायिक, ब्राह्मणवादी और फासीवादी कहा लेकिन इन तथ्यों को अनदेखा किया कि मुसलमानों को अपने से अलग मानने वाले ये संगठन धीरे-धीरे निचले समुदायों को भी मुख्यधारा में प्रवेश देने के काम में लगे हुए हैं. और किस तरह से ये संगठन दूसरों की कमियों को ही अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
बुद्धिजीवियों की यह सीमित दृष्टि तब और स्पष्ट हो जाती है जब हम इस ओर ध्यान देते हैं कि उन्होंने कभी इस बात को नहीं माना कि हिंदू समुदाय कभी इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से भी एक हो सकता है कि अकेले ही सत्ता स्थापित करने का कारण बन जाए. उन्हें हमेशा यह लगता रहा कि हमारे समाज में इतनी विभिन्नताएं हैं और हमारी संस्कृति इतनी गंगा-जमुनी रही है कि ऐसा होना लगभग असंभव है. लेकिन ऐसा हुआ तो उसने यह भी साबित कर दिया कि हमारा ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग जमीनी सच्चाइयों से कितना कटा हुआ है.
लेकिन हमारे बुद्धिजीवी न केवल सच्चाई से दूर हो गये बल्कि कुछ लोगों के मुताबिक भारत में उनके प्रति बढ़ती नाराजगी की वजह उनके विचार और कर्म में बढ़ती दूरी भी है. इसी देश ने महात्मा गांधी को भी देखा है जिनके विचार और कर्म में असाधारण एकरूपता थी. बीबीसी हिंदी पर अपने एक लेख में गांधी दर्शन के अध्येता कुमार प्रशांत कहते हैं, ‘महात्मा गांधी इतिहास के उन थोड़े से लोगों में एक हैं जिन्होंने अपने मन, वचन और कर्म में ऐसी एकरूपता साध रखी थी कि किसी भ्रम या अस्पष्टता की गुंजाइश बची नहीं रहती बशर्ते कि आप ही कुछ मलिन मन से इतिहास के पन्ने न पलट रहे हों.’ यही वजह है कि भारत का जनमानस उनके साथ खड़ा हो गया था.
लेकिन हालिया समय के बुद्धिजीवियों के एक बड़े हिस्से की तस्वीर इसके उलट दिखती है. जैसा कि एनडीटीवी से जुड़े एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, ‘मैंने ऐसे भी बुद्धिजीवी देखे हैं जो जल संरक्षण पर बड़े-बड़े लेख लिखते हैं और रोज अपनी अपनी गाड़ी की धुलाई पर बेतहाशा पानी भी बर्बाद करते हैं. दिन में उन्हें भारत की गरीबी की चिंता सताती है. रात को पार्टियों में उनकी बातचीत अपनी विदेश यात्रा और वहां खरीदे गए लुई वितॉन के पर्स पर केंद्रित होती है.’
वे आगे कहते हैं, ‘फिर भी 2014 तक इन बुद्धिजीवियों का एक आभामंडल हुआ करता था क्योंकि तब तक उस मीडिया का भी इस कदर ध्रुवीकरण नहीं हुआ था जिसमें वे छपा-दिखा करते थे और इससे अपनी ताकत हासिल करते थे. अब तो कुछेक अपवादों को छोड़कर मीडिया सत्ता प्रतिष्ठान के साथ खड़ा दिखता है. इसलिए बुद्धिजीवियों का वह स्पेस काफी कम हो गया है.’ और न केवल स्पेस कम हुआ बल्कि ज्यादातर मीडिया सत्ता या उसकी विचारधारा का विरोध करने पर उनके विरोध में ही खड़ा दिखाई देता है.
भारत में बुद्धिजीवियों के उतार की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि बीते कुछ समय के दौरान समाज में हर तरह के विचारों का महत्व घटा है. जैसा कि अशोक वाजपेयी कहते हैं, ‘विचार अपने आप में गौण होता जा रहा है.’ उनके मुताबिक विचार बहुत तेजी से राय में बदल रहा है और मीडिया के असाधारण प्रसार के चलते यह भी माना जाने लगा है कि मीडिया में आये बगैर विचार की प्रासंगिकता अधूरी है. और मीडिया में आने की एक ही शर्त है साफ-साफ इस या उस तरफ होना. ऐसे में ‘मीडिया की तरह अब कई बुद्धिजीवी भी उस चलन का शिकार हो गए हैं जिसमें चीजें सिर्फ श्वेत-श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट में देखी जाती हैं’ प्रोफेसर दिलीप सिमियन कहते हैं.
मार्कंडेय काटजू तो यह भी मानते हैं कि इन दिनों एक असल तो 10 फर्जी बुद्धिजीवी होते हैं. वे भारत के अधिकांश पत्रकारों और लेखकों को इस श्रेणी में रखते हैं. काटजू लिखते हैं, ‘इनमें से अधिकांश घमंड और दंभ से भरे होते हैं, इनमें विनय का अभाव होता है और ये ख़ुद को बहुत बड़ा समझते हैं. उन्हें ऐतिहासिक प्रक्रियाओं या सामाजिक विकास के नियमों की कोई गहरी समझ नहीं है, लेकिन वे समाज में चारों ओर अपने सतही किताबी ज्ञान और आधी पकी हुई समझ की अकड़ दिखाते फिरते हैं. वे केवल अपने स्वयं के आराम की परवाह करते हैं और जनता के लिए उन्हें कोई वास्तविक प्रेम नहीं है.’
दुनिया का हर समाज प्रश्नवाचकता, जिज्ञासा, असहमति और बहुलता से ही आगे बढ़ता और सशक्त होता रहा है. तो कहा जा सकता है कि बुद्धिजीवियों के प्रति द्वेष का कारण जो भी हो, उससे समाज को आखिर में नुकसान ही होना है. ऐसे में सवाल उठता है कि बुद्धिजीवी अपनी खोई जमीन कैसे हासिल करें. प्रोफेसर दिलीप सिमियन का मानना है इसके लिए बुद्धिजीवियों को आत्ममंथन करके अपनी गलतियों को स्वीकारना होगा, तभी वह खाई पाटी जा सकती है जो उनके और शेष समाज के बीच है. मार्कंडेय काटजू कहते हैं, ‘केवल बुद्धिजीवी ही समाज को सही नेतृत्व दे सकते हैं. लेकिन लोगों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए वर्तमान बुद्धिजीवियों’ को एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक प्रक्रिया से गुज़र कर अपनी मानसिकता बदलनी होगी, अन्यथा यह अंधे द्वारा अंधे को रास्ता दिखाना जैसा होगा.’
सौज- सत्याग्रहः लिंक नीचे दी गई है-