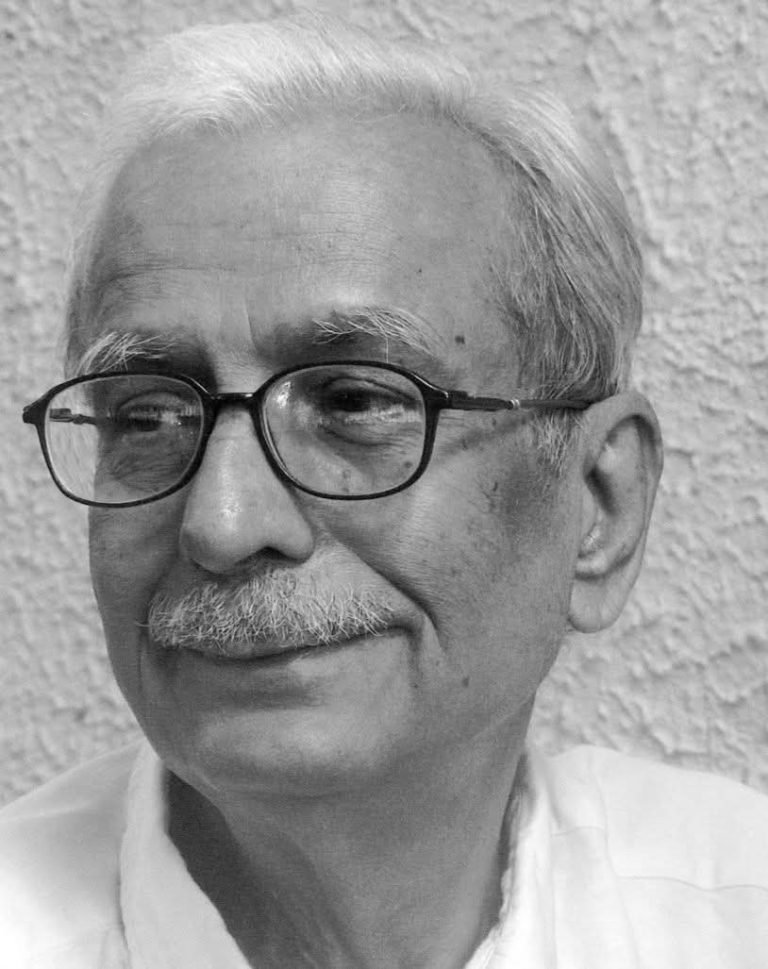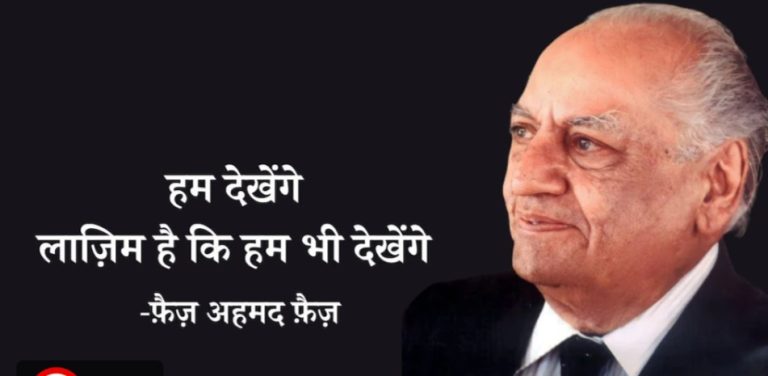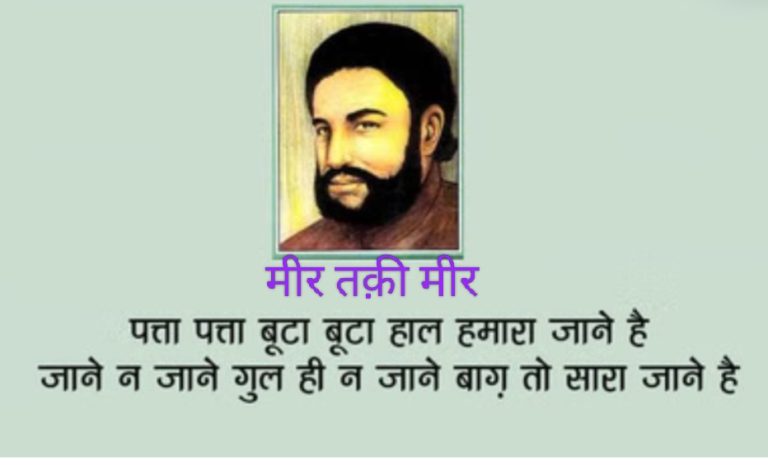विकास बहुगुणा
भगत सिंह कोश्यारी की एक चिट्ठी के बाद यह बहस फिर से छिड़ गई है कि क्या राज्यपाल नाम की संस्था उन उम्मीदों को पूरा कर रही है जिनकी उससे अपेक्षा की गई थी. राज्यपालों पर इस तरह के आरोप अब इतने आम हो चुके हैं कि इनसे कोई चौंकता नहीं है. कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस पद की एक ऐसी संस्था के रूप में कल्पना की थी जो निष्पक्ष होगी और संवैधानिक संरक्षक की अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए देश के संघीय ढांचे को मजबूत करेगी. लेकिन आज स्थिति इससे मीलों दूर दिखती है.
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इसकी वजह उनकी वह चिट्ठी है जो उन्होंने कोरोना वायरस से उपजे हालात के बीच राज्य में मंदिर खोलने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी है. तंज भरी इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, ‘ये विडंबना ही है कि राज्य में बार और रेस्तरां खुल गए हैं लेकिन मंदिर अब भी बंद पड़े हैं. कभी हिंदुत्व का कट्टर समर्थन करने वाले आप क्या अचानक सेक्युलर हो गए हैं?’ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी भेजकर इसका जवाब दिया है. इसमें उन्होंने लिखा है, ‘मेरे हिंदुत्व को आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है.’
राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी की यह पहली घटना नहीं है. हाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी इसी कारण के चलते सुर्खियों में आए थे. उनका कहना था कि ‘अगर संविधान की रक्षा नहीं हुई तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी. राज्यपाल के पद की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है. मुझे संविधान केअनुच्छेद 154 पर विचार करने को बाध्य होना पड़ेगा.’ यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल पर अपने पद की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया था. पार्टी का कहना था कि जगदीप धनखड़ को इस पद के बजाय प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष पद संभालना चाहिए.
इससे पहले राजस्थान में चली सियासी उथल-पुथल के दौरान वहां सत्ताधारी कांग्रेस ने राज्यपाल कलराज मिश्र पर कई बार पक्षपात के आरोप लगाए थे. उस समय पार्टी का कहना था कि राज्यपाल का आचरण देखकर लगता है कि जैसे वे एक पार्टी विशेष के हितों की पूर्ति कर रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उस समय सीधे-सीधे यह आरोप लगाया था कि कलराज मिश्र केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं.
राज्यपालों पर इस तरह के आरोप अब इतने आम हो चुके हैं कि इनसे कोई चौंकता नहीं है. कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस पद की एक ऐसी संस्था के रूप में कल्पना की थी जो निष्पक्ष होगी और संवैधानिक संरक्षक की अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए देश के संघीय ढांचे को मजबूत करेगी. लेकिन आज स्थिति इससे मीलों दूर दिखती है. आज राज्यपाल अपने आचरण में केंद्रीय सत्ता के ऐसे एजेंट के तौर पर दिखते हैं जिनके लिए इस सत्ता को थामे पार्टी के हित ही सबसे ऊपर होते हैं.
इस लिहाज से ऐसा लगता है कि राज्यपालों के मामले में वही परंपरा चल रही है जो सदियों पहले शुरू हुई थी. असल में जब राज्यपाल जैसे पद की अवधारणा अस्तित्व में आई थी तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि राज्यों पर केंद्रीय सत्ता की पकड़ मजबूत रहे. इतिहास पर नजर डालें तो जब भी कोई राजा किसी नए राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाता था तो प्रशासन के सुभीते के लिए उसकी कमान अपने विश्वासपात्र किसी सगे-संबंधी या अन्य शख्स को थमा देता था. भारत में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले मौर्य वंश के राजा बिंदुसार ने उज्जयिनी का राज्यपाल अपने पुत्र अशोक को बनाया था जो बाद में सम्राट बना. इस तरह की व्यवस्था मौर्य वंश के बाद आए शुंग वंश से लेकर गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट और मुगल वंश तक रही. अकबर के समय कुल प्रांतों की संख्या 15 थी जिनमें से एक गुजरात भी था और एक समय वहां के सूबेदार यानी राज्यपाल टोडरमल भी थे.

मुगलिया सल्तनत गई और ब्रिटिश राज आया, लेकिन राज्यपालों की भूमिका वही रही. दिलचस्प है कि 17वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन की महारानी ने भारत में व्यापार के लिए बनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो पहला चार्टर यानी राजपत्र जारी किया उसमें भारत के संदर्भ में पहली बार गवर्नर शब्द का इस्तेमाल हुआ था. इस चार्टर में कंपनी को ‘गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज’ कहकर परिभाषित किया गया. चार्टर के जरिये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन की कमान गवर्नर और उसे सलाह देने वाले 24 सदस्यों के हाथ में दी गई थी. गवर्नर कंपनी के हित के लिए काम करता था और कंपनी ब्रिटेन के हित के लिए.
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपना राजनीतिक उपनिवेश बनाने की भी शुरूआत की तो कुछ और चार्टरों के जरिये गवर्नर की शक्तियां बढ़ाई गईं. अब गवर्नर कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ब्रिटेन के सिविल और आपराधिक कानूनों को लागू कर सकता था. बाद में उसे भारत के हालात के हिसाब से अलग कानून बनाने और उनके उल्लंघन पर दंड देने का अधिकार भी दे दिया गया. जैसे-जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया, गवर्नरों की संख्या भी बढ़ने लगी. बाद में इन सबके ऊपर एक गवर्नर जनरल बिठा दिया गया. 1857 के गदर के बाद जब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आई तो तो गवर्नर जनरल, जिसे अब वायसराय कहा जाने लगा था, और गवर्नर अब पूरी तरह से ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिनिधि हो गए.
19वीं सदी खत्म होते-होते भारत में फिर से आजादी की अलख जग चुकी थी. 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम बनाया गया. इसके जरिये प्रांतों में चुनावों के आधार पर सरकारों के गठन की व्यवस्था हुई. अब राज्यपाल का काम इन सरकारों पर केंद्र की औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित रखना था. यही वजह है कि आजादी के बाद जब संविधान सभा बनी तो इस मुद्दे पर बहुत तीखी बहस हुई. इस पर सभी एकराय थे कि राज्यपाल एक ऐसा निष्पक्ष और सम्माननीय व्यक्ति होना चाहिए जो अपने आपको राजनीति से अलग कर चुका हो, लेकिन उसे चुना कैसे जाए इस पर राय बंटी हुई थी.
मसलन कुछ लोगों का मत था कि राज्यपाल को विधानसभा या विधानसभा और विधानपरिषद मिलकर चुनें. लेकिन यह प्रस्ताव इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विधायिका अगर राज्यपाल का चुनाव करेगी तो वह बहुमत वाले दल या गठबंधन का खिलौना बनकर रह जाएगा. दूसरा सुझाव यह था कि विधायिका का निचला सदन यानी विधानसभा नामों का एक पैनल बनाए और राष्ट्रपति उसमें से एक नाम चुने. लेकिन यह भी खारिज हो गया क्योंकि संविधान सभा के बहुत से सदस्यों की राय थी कि इससे चुनाव की एक सीमा बंध जाती है. एक सुझाव राज्यपाल के जनता द्वारा चुनाव का भी था. इस पर काफी सदस्य एकराय थे. एकबारगी ऐसा लगा कि यही तय हो जएगा. लेकिन हैदराबाद के निजाम के भारत में मिलने से इनकार और कश्मीर में तनाव जैसी कुछ घटनाओं के चलते संविधान निर्माताओं को लगा कि मजबूत केंद्र होने का संदेश देना जरूरी है.
इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य सदस्यों का यह भी मानना था कि जनता द्वारा चुना गया राज्यपाल विधायकों द्वारा यानी परोक्ष रूप से चुने गए मुख्यमंत्री की तुलना में मजबूत हो सकता है. उन्हें डर था कि ऐसे में वह मुख्यमंत्री से इस आधार पर होड़ कर सकता है कि उसे जनता का विश्वास हासिल है और इससे प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. कुछ सदस्यों का यह भी मानना था कि जनता द्वारा चुने जाने की हालत में हो सकता है कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी का ही कोई सदस्य वहां का गवर्नर भी चुन लिया जाए. ऐसे में आजादी के ठीक बाद यह अंदेशा भी था कि अगर दोनों एक साथ मिल गए तो इससे पृथकतावादी भावनाओं को बल मिल सकता है. या सामान्य हालत में केंद्र के हितों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकता है. इसलिए आखिर में सहमति यह बनी कि एक मजबूत केंद्र का संदेश दिया जाना जरूरी है. इस तरह संविधान में अनुच्छेद 155 जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा. राष्ट्रपति केंद्र में संवैधानिक प्रमुख था तो राज्य में राज्यपाल को यह जिम्मेदारी दी गई. वह राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि हो गया.
लेकिन 1952 में पहले आम चुनाव के बाद से ही इस संस्था के भविष्य के संकेतदिखने लगे. मद्रास में आम चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को झटका लगा था. वह 375 में से 152 सीटें ही जीत सकी. यानी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी वह बहुमत से दूर थी. उधर, कम्युनिस्टों सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन कर संयुक्त मोर्चा बना लिया और बहुमत का दावा किया. कांग्रेस में खलबली मच गई. राज्य के धाकड़ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तब तक सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे. आनन-फानन में उन्हें खूब मनाकर वापस लाया गया. कांग्रेस को उम्मीद थी कि अब राजगोपालाचारी का कद और कौशल ही कम्युनिस्टों को सत्ता में आने से रोक सकता है. इसके बाद राज्यपाल ने कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दिया. शपथ ग्रहण के बाद विपक्षी खेमे में सेंध लगाने के प्रयास शुरू हुए. आखिरकार सरकार बनाने का न्योता मिलने के तीन महीने बाद तीन जुलाई 1952 को राजगोपालाचारी ने 200 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया.
इसके बाद तो राज्यपालों के ऐसे कारनामों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया. 1954 में पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद थे. 1959 में केरल की नम्बूदरीपाद सरकार बर्खास्त की गयी. इसके बाद केंद्र में सत्ताधारी दल द्वारा राज्यपालों को अपने एजेंट की तरह बरतने की यह सूची लंबी होती गयी. हाल में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखकर कहा जा सकता है कि यह सिलसिला अब तक न केवल जारी है बल्कि इसकी गति और तेज़ हो चुकी है. संविधान लागू होने के बाद से राज्यपाल की सिफारिश पर किसी राज्य की सरकार को भंग करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 100 से भी ज्यादा उदाहरण हैं लेकिन इनमें से गिने-चुने ही ऐसे होंगे जब वास्तव में संवैधानिक संकट की वजह से ऐसा करने की नौबत आई हो. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 15 साल के कार्यकाल में तो 50 बार राष्ट्रपति शासन लगा जो एक रिकॉर्ड है.
इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने की संकल्पना के साथ जारी रखा गया यह पद उसी संघीय ढांचे पर चोट का सबब बन गया है. इसलिए कोई हैरत नहीं कि बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि राज्यपाल नाम की इस संस्था को खत्म कर दिया जाना चाहिए. जाहिर सी बात है कि इनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. कुछ साल पहले अंतरराज्यीय परिषद की एक बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि राज्यपाल का पद खत्म कर दिया जाए.
जानकारों के मुताबिक इन नेताओं की ऐसी इच्छा का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि राज्यपाल नाम की इस संस्था का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है. पहले अक्सर राज्यपाल को चुनते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जाती थी जो अब बीते कल की बात हो चुकी है. अब इस पद पर अधिकतर ऐसे ही लोगों को चुना जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि वे ‘अपने लोग’ हैं उन्हें उपकृत किया गया है. पार्टी के बुजुर्ग नेताओं से लेकर सरकार के चहेते जैसी छवि रखने वाले रिटायर्ड नौकरशाह, पूर्व सैन्य अधिकारी और मुख्य न्यायाधीश तक रह चुके लोगों के नाम इस सूची में शामिल हो चुके हैं. पहले एक रिवाज यह भी था कि किसी व्यक्ति को उसी के राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा ताकि वह स्थानीय राजनीति और दबावों आदि से मुक्त रहे. लेकिन अब ऐसा हो ही यह भी जरूरी नहीं है.
इस वक्त जो एक चलन बेहद मजबूत होता जा रहा है वह यह कि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार आते ही राज्यपालों के भी बदले जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है. यह चलन कितना व्यापक है यह इस बात से ही समझा जा सकता है कि वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आते ही सभी राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया था. इससे पहले आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने भी कई राज्यपालों को उनके पद से हटा दिया था. पिछली यूपीए सरकार ने भी 2004 में सत्ता में आते ही चार राज्यपालों को हटा दिया था. वर्तमान मोदी सरकार ने भी इससे कुछ अलग नहीं किया. दरअसल राज्यपालों की नियुक्ति भले राष्ट्रपति करते हैं लेकिन, उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री कार्यालय की दया का मोहताज दिखता है.
ऐसा नहीं है कि इस संस्था का स्वरूप बेहतर करने की कोशिशें नहीं की गईं. सरकारिया आयोग से लेकर प्रशानिक सुधार आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए. इन्हें हटाने के लिए एक अलग प्रक्रिया (अभी केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा सकता है) की भी बात हुई. सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कहा कि केंद्र में सरकार बदलते ही राज्यपालों को नहीं हटाया जा सकता. लेकिन इसके बाद भी मामला वहीं का वहीं है. और जब भी राज्यपालों में से कोई खबर में आता है तो सबसे पहले यही बात सामने आती है कि संबंधित राज्य में केंद्र में सत्ताधारी दल से अलग पार्टी की सरकार है. महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक तमाम राज्यों में यह देखा जा सकता है.
राज्यपालों के बयान भी जब खबर बनते हैं तो कई बार इसकी वजह यही होती है कि वे विवादित और अपने पद की गरिमा गिराने वाले होते हैं. मसलन भाजपा के नेता रहे और अब मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने पिछले साल कहा कि देश के लोगों को कश्मीरियों और उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामान का बहिष्कार करना चाहिए. दिलचस्प बात है कि बीते दिनों अपने पद पर रहते हुए ही उन्होंने वापस सक्रिय राजनीति में लौटने की इच्छा जताई है. उनका कहना है, ‘राज्यपाल के तौर पर मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद, मैं सक्रिय राजनीति में लौटना और पश्चिम बंगाल की सेवा करना चाहूंगा. मैं अपने राज्य लौटने के बाद पार्टी से (इस बारे में) बात करूंगा. इसे स्वीकारना या खारिज करना उस पर है.’
वैसे राज्यपालों का फिर से सक्रिय राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे और शीला दीक्षित ऐसा कर चुके हैं. शिंदे आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनने के बाद केंद्र में ऊर्जा मंत्री बन गए और दीक्षित केरल की राज्यपाल रहने के बाद उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थीं. भाजपा के मदन लाल खुराना भी ऐसा ही एक उदाहरण हैं जो राजस्थान का गवर्नर बनने के बाद फिर से सक्रिय राजनीति में आ गए थे. इससे साफ होता है कि राज्यपाल बनने वाले ऐसे ज्यादातर लोगों की राजनीतिक लालसाएं और पार्टीगत निष्ठाएं जिंदा रहती हैं. सवाल है कि क्या इससे अराजनीतिक और निष्पक्ष होने की वह अवधारणा ही ध्वस्त होती नहीं दिखती जिसके आधार पर संविधान निर्माताओं ने इस संस्था को जारी रखा था. ऐसे भी उदाहरण हैं जब राज्यपालों की सिफारिश पर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के फैसले को अदालतों ने पलट दिया. और आगे जाएं तो एनडी तिवारी और वी षण्मुगनाथन जैसे भी मामले हैं जिन्होंने इस पद की गरिमा को और भी पाताल में पहुंचाने का काम किया.
केंद्र से अलग पार्टी की सत्ता वाले राज्यों के मुखिया राज्यपाल पर भरोसा करते नहीं दिखते और ऐसा भी नहीं लगता कि केंद्र भी राज्यपाल पर पूरी तरह से भरोसा करता है. संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति केंद्र ने अपने पास रखी है तो इसमें यह भी व्यवस्था है कि ऐसा करने के लिए वह सिर्फ राज्यपाल की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं है.
केंद्र-राज्य संबंधों के इतर देखें तो राज्यपालों की गतिविधियां सार्वजनिक आयोजनों में भाग लेने और नियमित दिल्ली दौरों तक सिमटी दिखती हैं. या फिर वे जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने जैसे चुनिंदा मौकों पर ही याद किए जाते हैं. कई लोग मानते हैं कि ऐसे कुछ मौकों के लिए बिना झंझट के एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है और इसलिए राज्यपाल जैसे अनावश्यक और खर्चीले पद को ढोने का कोई तुक नहीं है.
जैसा कि अपनी एक टिप्पणी में वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौबे लिखते हैं, ‘जहां तक पद की शपथ दिलाने या यह सुनिश्चित करने की बात है कि संवैधानिक व्यवस्था ठीक से चल रही है या नहीं तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट और वहां के मुख्य न्यायाधीश हैं ही. तो हमें राज्यपालों का यह बोझ क्यों उठाना चाहिए?’ उनके मुताबिक इतिहास को देखें तो राज्यपाल सिर्फ केंद्र के मोहरे रहे हैं जिनका देश के निर्माण में शायद ही कोई योगदान रहा हो. संतोष चौबे के मुताबिक इसका एक ऑडिट होना चाहिए कि यह पद देश पर कितना वित्तीय बोझ डाल रहा है. वे कहते हैं, ‘ऐसी संस्था को क्यों नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए जो न राष्ट्रपिता और न ही हमारे संविधान की उम्मीदों पर खरी उतरी है और जिसने हमारे संघीय ढांचे का भी नुकसान किया है.’
सौज- सत्याग्रहः लिंक नीचे दी गई है-
https://satyagrah.scroll.in/article/135992/kya-desh-ko-rajyapaalon-ki-zaroorat-hai