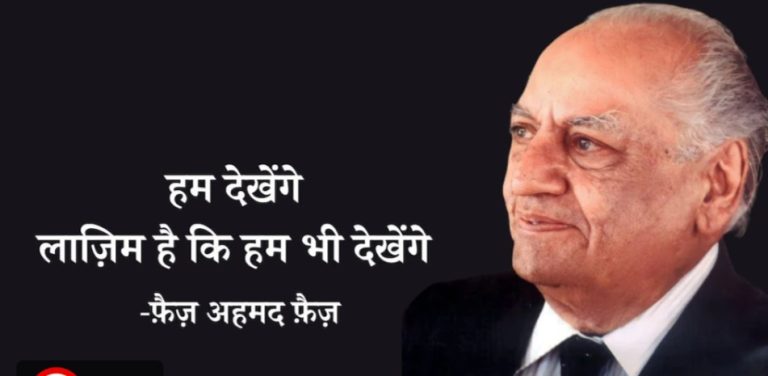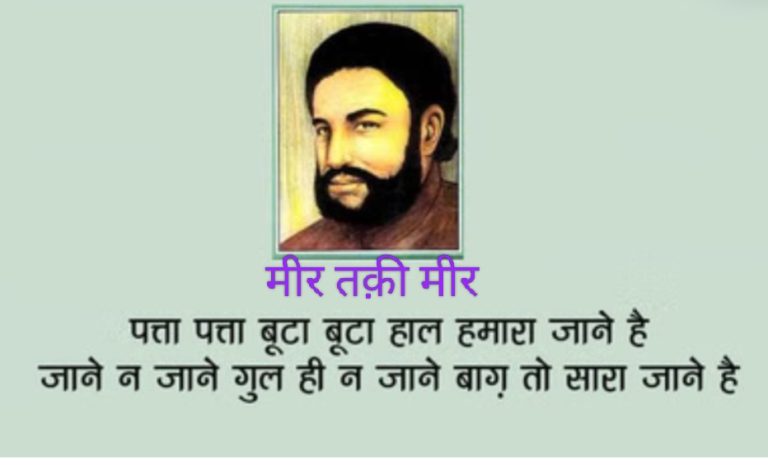हिंदी सिनेमा जिस ओम पुरी को याद करता है, वह अब भी सत्तर और अस्सी के दशकों में लरजती आंखों और खुरदरी आवाज़ वाला वह अभिनेता था जिसके बगैर कई फिल्में वह प्रामाणिकता हासिल न कर पातीं जो कर पाईं. यह कुछ उदास करने वाला अफ़साना है कि किस तरह समानांतर सिनेमा के सभी कलाकार धीरे-धीरे उस दुनिया से दूर होते चले गए.
एक दौर था जब ओम पुरी नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी के साथ मिलकर हिंदी के समानांतर सिनेमा की पहचान बनाते थे. किसी फिल्म में इन सबका या इनमें से किसी एक का होना भी उसके गंभीर होने की गारंटी माना जाता था. इनकी मौजूदगी भर किसी फिल्म को कला फिल्म का दर्जा दिला देती थी. यह वह दौर था जब सतही किस्म के ऐक्शन और रोमांस की फिल्मों से हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा बनती थी. निस्संदेह इसी दौर में कुछ ‘साफ़-सुथरी’ मानी जाने वाली पारिवारिक फिल्में और कुछ ‘स्वस्थ’ समझी जाने वाली हास्य फिल्में भी बनती रहीं, लेकिन उस दौर के सिनेमा के बौद्धिक विमर्श की केंद्रीय ज़मीन इन्हीं समानांतर, सोद्देश्यपूर्ण या कला फिल्मों से बनती थी.
आज कुछ दूरी से उन फिल्मों को याद करते हुए या उन्हें नए सिरे से देखते हुए कुछ अजीब सा लगता है. सिनेमा की अपनी उन दिनों की समझ कुछ संदेह में डालती है. जो फिल्में तब बेमिसाल लगती थीं, वे अचानक कृत्रिम और आडंबरी बौद्धिकता की शिकार जान पड़ती हैं. उनके संवाद नकली लगते हैं, उनके कथा सूत्र स्वाभाविक नहीं मालूम होते, उनका कैमरा बहुत सायास ढंग से कुछ दिखाने की कोशिश करता दिखता है, वे फिल्में ‘यथार्थ’ को यथार्थ के सरलीकरण के साथ पकड़ने वाली फिल्में थीं जो हमें इसलिए प्रिय थीं कि उस कारोबारी फिल्मी दुनिया के बहुत सारे भोंडेपन से दूर वे एक राजनीतिक-सामाजिक संदेश देने की कोशिश करती थीं.
लेकिन इन फिल्मों की कौन सी चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती थी? निस्संदेह, वह अभिनय जो इन फिल्मों को एक अलग तरह की आभा देता था. फिल्म ‘आक्रोश’ में आदिवासी ओम पुरी की सुलगती हुई ख़ामोश आंखें जैसे हमारा पीछा नहीं छोड़ती थीं. ‘अर्धसत्य’ में एक बेबस पुलिस इंस्पेक्टर के भीतर पैदा होने वाली कुंठा और गुस्से को ओम पुरी के अभिनय के साथ हम अपने भीतर लिए लौटते थे. ‘मिर्च मसाला’ का चौकन्ना चौकीदार यह भरोसा दिलाता था कि उसके होते लड़कियों का कुछ बिगड़ेगा नहीं. बेशक, यही बात कई अन्य फिल्मों के बारे में नसीर और स्मिता पाटिल को लेकर भी कही जा सकती है. यह उन फिल्मों का सौभाग्य था कि उन्हें इन जैसे विलक्षण अभिनेता मिले. ऐसी फिल्मों की फेहरिस्त बहुत लंबी है जिसमें इन सबने साथ या अलग-अलग काम किया और अपने अभिनय से इन्हें हमारे लिए यादगार बनाया.

ओम पुरी शायद इन सबमें सबसे अनगढ़ थे- बहुत ही सामान्य और खुरदरी शक्ल-सूरत के मालिक. बेशक उनकी आवाज़ में एक अलग तरह का खुरदरापन था. लेकिन वे इस आवाज़ का भी बहुत करीने से इस्तेमाल करते थे. शायद यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के प्रशिक्षण का असर रहा हो कि वे जटिल से जटिल भूमिकाएं बिल्कुल सहजता से कर जाते थे. रंगमंच, सिनेमा, टीवी हर जगह उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी. एनएसडी की कुछ बेहतरीन और यादगार प्रस्तुतियां उनके बिना अधूरी होतीं. ‘तमस”, ‘राग दरबारी’ और ‘कक्का जी कहिन’ जैसे टीवी सीरियलों में उनका अभिनय एक अलग आयाम जोड़ता था. बाद के दौर में वे मुख्यधारा वाली कारोबारी फिल्मों से भी जुड़े और कई चुलबुली और हास्य भूमिकाओं में भी दिखे जिनमें ख़ासकर चाची 420 और मालामाल वीकली में उनका काम यादगार कहा जा सकता है.
लेकिन यह सच है कि हिंदी सिनेमा जिस ओम पुरी को याद करता है, वह अब भी सत्तर और अस्सी के दशकों में लरजती आंखों और खुरदरी आवाज़ वाला वह अभिनेता था जिसके बगैर कई फिल्में वह प्रामाणिकता हासिल न कर पातीं जो कर पाईं. यह कुछ उदास करने वाला अफ़साना है कि किस तरह समानांतर सिनेमा के सभी कलाकार धीरे-धीरे उस दुनिया से दूर होते चले गए. स्मिता पाटिल तो सबसे पहले विदा हो गईं. अमरीश पुरी, ओम पुरी और नसीरुद्धीन शाह ने भी रास्ता बदल लिया. बाद में नसीरुद्दीन शाह ने तो समानांतर फिल्मों की नकली बौद्धिकता और कला के नाम पर कलाकारों के शोषण के प्रति अपनी चिढ़ को सार्वजनिक करने में कोई कोताही नहीं बरती.
मगर कारोबारी सिनेमा इन कलाकारों की ससुराल भले हो, मायका इनका वही अभिनय की दुनिया थी जो कभी रंगमंच में और कभी समानांतर फिल्मों में इनके भीतर के सर्वश्रेष्ठ को सामने लाती रही. यही वजह है कि ये सब उस दुनिया में बार-बार लौटते रहे. नसीर और ओम पुरी और कई दूसरे कलाकार गाहे-बगाहे अब भी नाटक करते रहे और ऐसी फिल्मों में दिखाई पड़ते रहे जो लगता है, उनके अभिनय के लिए ही बनी हैं.
लेकिन हिंदी सिनेमा अब पहले से बहुत बदल गया है. कई ऐसे निर्देशक जो पहले कला फिल्मों वाले दायरे में रख लिए जाते, आजकल कारोबारी फिल्मों के ही निर्देशक हैं और अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं. यही बात अभिनेताओं के बारे में कही जा सकती है. ओम पुरी के अभिनय की विरासत जिन दो कलाकारों में सबसे साफ़ ढंग से पहचानी जा सकती है, वे इरफ़ान और नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी हैं. वे किन्हीं कला फिल्मों के नहीं, ठेठ कारोबारी फिल्मों के अभिनेता हैं और अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख़ खान तक को अपने अभिनय से चुनौती देते हैं.
लेकिन आज का यह दौर किसी शून्य से पैदा नहीं हुआ है. उसको पुराने दिनों के कारोबारी और कलात्मक प्रयत्नों ने मिलकर बनाया है. सत्तर और अस्सी के दशक में अपने माध्यम के साथ प्रयोग की दुस्साहसिकता और उसके बीच लोगों को एक संदेश देने की प्रतिबद्धता कोई छोटी चीज़ नहीं थी. वे प्रयोग अब कुछ बदले हुए रूप में जारी हैं. सिनेमा बौद्धिक नहीं, बल्कि कस्बाई होने की कोशिश कर रहा है. संवादों का ढंग बदल गया है, कैमरे बहुत तेज़ हो गए हैं और ऐसे कोणों से ज़िंदगी को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिनमें वह बिल्कुल अपने कच्चे-अनगढ़ रूप में दिखाई पड़े. कहानियों में छिछले ऐक्शन और सतही रोमांस की जगह कम हो रही है. इस दौर में अच्छे अभिनेताओं की चुनौती भी बढ़ी है. इन सबके बीच ओम पुरी की विरासत का मोल समझ में आता है. अभिनय के जिस व्याकरण को उन्होंने अपने ढंग से साधा और इस्तेमाल किया, वह अब भी इतना कारगर और प्रामाणिक है कि नई पीढ़ियों के काम आता है और आता रहेगा. हां, यह मलाल ज़रूर बना रहेगा कि वह आक्रोश और प्रतिबद्धता शायद किन्हीं पुराने ज़मानों की चीज़ हो गए हैं जिनके बीच ओम पुरी और कई कलाकारों ने अपने-आप को रचा था. यह पता भले न चले, मगर दुनिया को ये सारी चीज़ें चुपचाप कुछ-कुछ बदलती रहती हैं.
सौज- सत्याग्रहः लिंक नीचे दी गई है