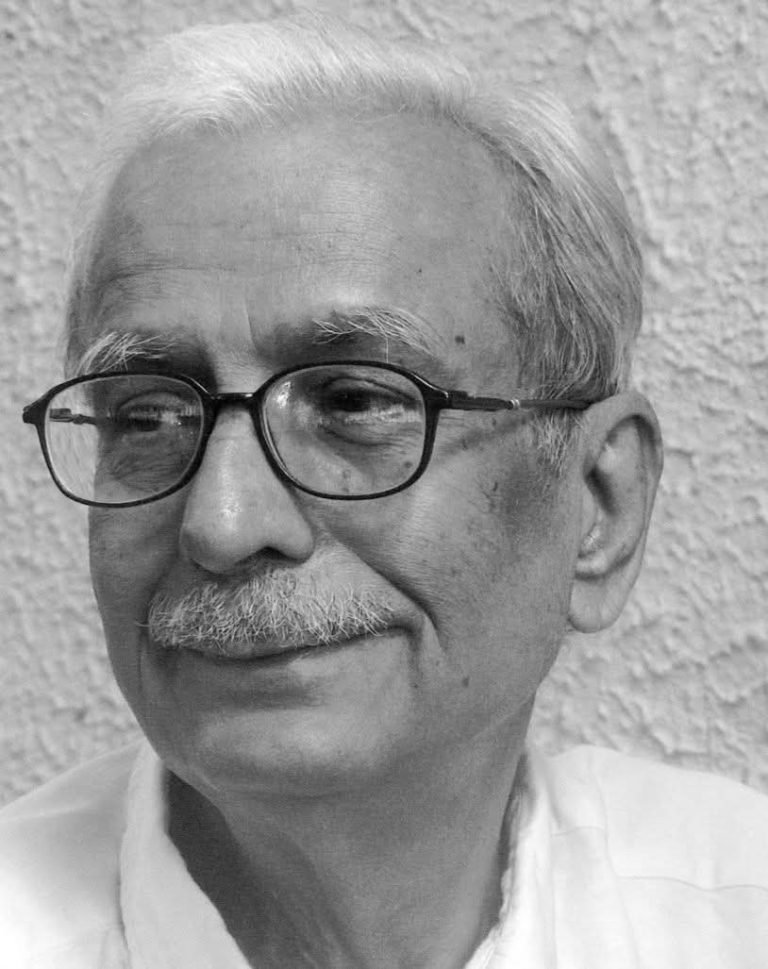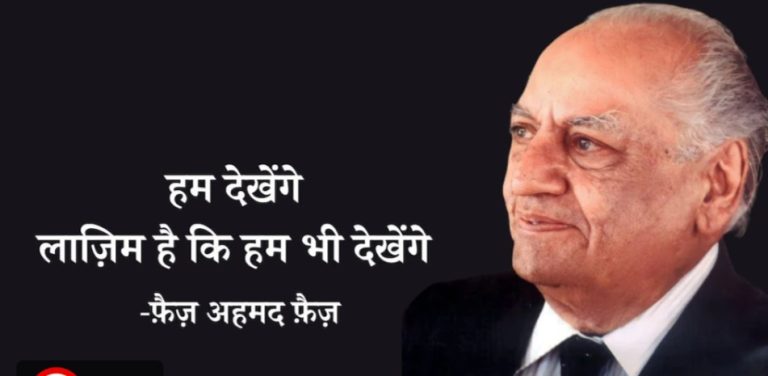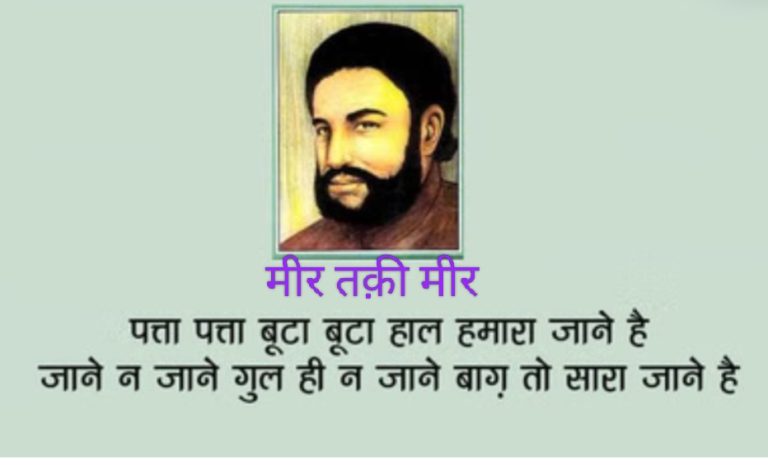बांग्लादेश के निर्माण के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह कर सबको हैरान कर दिया कि ढाका की मुक्ति के सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया था और इसके लिए वह जेल भी गए थे। हालाँकि प्रधानमंत्री के इस दावे पर भारत में लगातार सवाल खड़े होने शुरू हो गए, लेकिन यह मानना अतिरेक होगा कि जिस कार्यक्रम में ख़ुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना वाजेद मौजूद थीं, वहाँ प्रधानमंत्री ने कोई ग़लतबयानी की होगी।
वैसे भी उनके समर्थक यह साबित करने वाली कुछ पुरानी कतरनें ले आए हैं कि 1971 के उन दिनों में जनसंघ ने बांग्लादेश को मान्यता दिलाने के सवाल पर सत्याग्रह किया था- बेशक, इस दौर में ऐसी किसी भी कतरन की प्रामाणिकता की पुष्टि के बिना उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
मगर हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। निश्चय ही उन्होंने ऐसे किसी सत्याग्रह में हिस्सा लिया होगा, वरना इतनी बड़ी ग़लतबयानी वह नहीं करते। लेकिन इससे क्या होता है?
बांग्लादेश युद्ध का इतिहास इतना निकट और स्पष्ट है कि उसमें किसी पक्ष-विपक्ष की पहचान मुश्किल नहीं है। यह भारत था जिसकी मदद से बांग्लादेश बना- जाहिर है, इसका श्रेय उस समय की सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जाता है जिन्होंने अमेरिका के दबाव की परवाह न करते हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को समर्थन दिया और पाकिस्तान को युद्ध में शिकस्त दी। इस बात को शुक्रवार को हुए समारोह में भी दुहराया गया- ऐसी स्थिति में जनसंघ किस बात के लिए आंदोलन कर रहा था? इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष साथ थे। जाहिर है, वह कोई सत्याग्रह था तो वह बिना किसी जोखिम वाला सत्याग्रह रहा होगा और उस दौरान गिरफ़्तारी भी हुई तो तकनीकी गिरफ़्तारी हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी ही तकनीकी गिरफ़्तारी देने वालों की कतार में रहे हों तो यह असंभव नहीं। अपनी इस सत्याग्रहीय उपलब्धि का ढाका में बखान करने के लिए भी उन्हें माफ़ किया जा सकता है- आख़िर नेता कुछ बातों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा।
बांग्लादेश के निर्माण ने सबसे पहले द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चोट की- यानी धर्म के आधार पर राष्ट्रों के विभाजन पर। यह एक तरह से पाकिस्तान के बनने के तर्क पर चोट थी। बांग्लादेश ने साबित किया कि कोई कौम धर्म की वजह से नहीं, भाषा और संस्कृति की वजह से एक होती है या अलग होती है। बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास ही बहुलता के समावेशन के सिद्धांत पर हुआ। वैसे भी धर्म के आधार पर बंटे राष्ट्र नहीं दिखते हैं। पूरा यूरोप ईसाई है, लेकिन सब भाषा के आधार पर बंटे अलग-अलग देश हैं। यही बात पश्चिम एशिया के बारे में कही जा सकती है जहाँ इस्लाम की धार्मिक एकता के बावजूद राष्ट्रीयताएँ न सिर्फ़ विभाजित रही हैं, बल्कि अलग-अलग कालखंड में एक-दूसरे के ख़ून की प्यासी रही हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बांग्लादेश का पहला सबक़ यही था कि पाकिस्तान कृत्रिम आधार पर बना देश है, धर्म के आधार पर देश नहीं बंटते। बेशक, जब वे बंट जाते हैं तो फिर एक ठोस इकाई बन जाते हैं जिन्हें स्वीकार करना पड़ता है।
पाकिस्तान को भी इसलिए हम स्वीकार करने को मजबूर हैं। यह अलग बात है कि ख़ुद पाकिस्तान को बांग्लादेश की कोख से निकला तर्क मंज़ूर नहीं था, क्योंकि वह उसके आधार को ख़ारिज करता था। इसलिए उसने कुछ और ज़ोर-शोर से इस्लामी होने की कोशिश शुरू कर दी, इस्लामी बम बनाने की बात छेड़ी और कभी अमेरिका और कभी अल्लाह के बंदों के हाथ खेलता हुआ अचानक ऐसे कट्टरपंथी झमेले में फँस गया जिससे निकलना ख़ुद उसके लिए आसान साबित नहीं हो पा रहा है।
लेकिन हम भारत में क्या कर रहे हैं? हम भी अपनी भाषिक और सांस्कृतिक बहुलता को भूल कर अपने राजनीतिक चूल्हे पर जैसे धार्मिक उन्माद की एक कहाड़ी चढ़ाए हुए हैं और उसे गरम किए जा रहे हैं। हम हिंदू पाकिस्तान बनने पर तुले हुए हैं और यह देख नहीं रहे कि इसकी वजह से हमारे भीतर असंतोष के कुछ छोटे-छोटे बांग्लादेश तो नहीं बन रहे?
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में साझा विरासत और साझा चुनौती की बात उचित ही की, लेकिन भारत के मुक़ाबले बांग्लादेश ने सांप्रदायिक कट्टरता की मार भी ज़्यादा झेली और अपने लोकतंत्र को दाँव पर लगते भी देखा। निश्चय ही भारत को उस रास्ते पर ले जाना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देने वाली बहुसंख्यकवादी राजनीति बेलगाम न हो- अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के राजनीतिक मुहावरे का अधिकतम दोहन हो चुका है, इसे और ज़्यादा खींचना भारतीय राष्ट्र-राज्य के भीतर नए ज़ख़्म पैदा करने जैसा होगा- जो शायद पैदा हो रहे हैं।
बांग्लादेश से जुड़ी दो विडंबनाएँ और हैं जिन पर भारत को ध्यान देने की ज़रूरत है। 1971 में जिस बंग बंधु मुजीबुर्रहमान पर पूरा बांग्लादेश निसार होने को तैयार था, जिसके एक इशारे पर लाखों नौजवान गला कटाने को तैयार थे, महज 4 साल बाद 1975 में उसके सपरिवार क़त्लेआम पर वहाँ जैसे पत्ता भी नहीं खड़का।
क्या यह चरम लोकप्रियतावाद की विडंबनामूलक परिणति थी कि शेख मुजीब यह देख तक नहीं सके कि किस तरह उनकी लोकप्रियता उतार पर है?
दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचल कर पूरी फौज लगा दी, लेकिन इसी की वजह से बांग्लादेश का बनना सुनिश्चित होता चला गया। अगर 1969 में किसी ने कल्पना की होती कि अवामी लीग को चुनावी जीत के बावजूद सत्ता न देने का परिणाम पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाने के रूप में सामने आएगा तो शायद यह नौबत नहीं आती। लेकिन इतिहास के सबक़ पीछे मुड़ कर देखने पर ही नज़र आते हैं। पाकिस्तान ने जितनी ताक़त इस्तेमाल की, पूर्वी पाकिस्तान उतना ही छिटकता चला गया।
कहने का मतलब यह कि देश फौजी ताक़त से सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन एकजुट वे लोकतांत्रिक साझेदारी से ही रहते हैं। यह सबक़ हमें अपने कई प्रदेशों में, कई आंदोलनों के बीच काम आ सकता है। कश्मीर को बीते लगभग डेढ़ साल से हमने फौज के बूते क़ाबू में रखा हुआ है। अनुच्छेद 370 को हटा कर कश्मीरी स्वाभिमान को ठेस पहुँचाते हुए हम उसे उपनिवेश की तरह बनाए तो रख सकते हैं, लेकिन देश के स्वाभाविक हिस्से की तरह उसके विकास के लिए ज़रूरी है कि वहाँ लोकतंत्र की हवा पहुँचे, बराबरी भरे सलूक का भरोसा पहुँचे। वहाँ तरह-तरह के चुनाव करवाने के बावजूद इस मोर्चे पर भारत सरकार की चुनौतियाँ अभी बची हुई हैं।
1971 के युद्ध ने दरअसल बांग्लादेश का ही नहीं, भारत का भी पुनर्निर्माण किया था। साठ के दशक में भारत कई तरह के द्वंद्व से गुज़रता राष्ट्र था। 1962 और 1965 के युद्ध, नेहरू और शास्त्री की मौत, कांग्रेस की टूटन, कई राज्यों में उसकी हार और राष्ट्रीयकरण के इंदिरा गांधी के एजेंडे के विरुद्ध दिख रही अंदरूनी हलचल- यह सब देखते हुए अंदेशा होता था कि भारत बिखर तो नहीं रहा। लेकिन 1971 के युद्ध ने सारे अंदेशों को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पर ऐसे विजेता के तौर पर उभरा जो सारी दुनिया से आँख मिला सकता था। यह भारतीय आत्मविश्वास की वापसी भी थी। दरअसल इसी आत्मविश्वास को इंदिरा गांधी ने अतिआत्मविश्वास की तरह लिया और 4 साल बाद इमरजेंसी थोप पर आज़ाद भारत के सबसे काले 19 महीनों की शुरुआत की।
राहत की बात है कि वे दिन टिके नहीं और भारत में लोकतंत्र कुछ और मज़बूत और अपरिहार्य होकर लौटा। बांग्लादेश के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि उसका इम्तिहान कुछ लंबा चला लेकिन वह अब एक स्पष्ट राह पर है और दूसरों के लिए मिसाल बनने लायक हो चला है।
बांग्लादेश से जुड़े दो सवाल और हैं जो हमें अपने से पूछने चाहिए। इत्तिफ़ाक से ये वे दिन हैं जब रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला सारी दुनिया- और ख़ासकर हमारे सामने है।
क्या हम रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में कोई ठोस-मानवीय दृष्टिकोण अपना पा रहे हैं? या रोहिंग्या समस्या को भी हम एक अल्पसंख्यक समस्या मान कर निबटा देने पर तुले हैं?
दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री भारत-बांग्लादेश की साझेदारी की चाहे जितनी बात करें, लेकिन ‘बांग्लादेशी’ शब्द को हमने जैसे गाली बना दिया है- उसके आगे या तो ‘अवैध’ उपसर्ग लगाते हैं या पीछे ‘घुसपैठिए’ प्रत्यय। दिलचस्प यह है कि हम उनकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाने से नहीं कतराते और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दुत्कारने से भी नहीं चूकते। कुछ साल पहले ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में यह मसला जिस तरह उठा था, उसे याद किया जा सकता है।
जाहिर है, एक राष्ट्र के तौर पर जो बड़प्पन हमने कभी तिब्बत या बांग्लादेश के संदर्भ में दिखाया था, वह अब नहीं दिखा पा रहे। अब अपने भीतर और बाहर झाँकने वाली हमारी दृष्टि पहले से ज़्यादा संकुचित और सीमित है जो अंततः एक देश के रूप में हमारी गरिमा कम करती है। अभी जब असम में एनआरसी का काम पूरा हो जाएगा तो जो लाखों लोग अवैध नागरिक के रूप में चिह्नित होंगे, क्या हम उन्हें बाड़ों में रखेंगे या बांग्लादेश भेजेंगे? और बांग्लादेश उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? ये वे सवाल हैं जिनके जवाब आसान नहीं हैं।
इस मोड़ पर भारत की आज़ादी के 75वें साल का जश्न हो या बांग्लादेश के निर्माण के 50 साल का- दोनों में हमें याद रखना होगा कि देश अंततः सबको साथ लेकर चलने से बनते और बचते हैं। लोकप्रियता से सरकार बन सकती है, समस्याओं का हल नहीं मिलता, बल्कि बाद में समस्याएँ पैदा होने लगती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भीतर ढाका के लिए किए गए सत्याग्रह की स्मृति अगर बची है तो उन्हें यह भी सोचना होगा कि क्या इस स्मृति का कोई रचनात्मक इस्तेमाल संभव है, कि क्या हम अपनी नागरिकता के आंगन को छोटे राजनीतिक स्वार्थों के कील-काँटे से भरें या इतना उदार बनाएँ कि उसमें बहुत सारे रंगों के लोग समा सकें।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं। सौज- सत्यहिन्दी