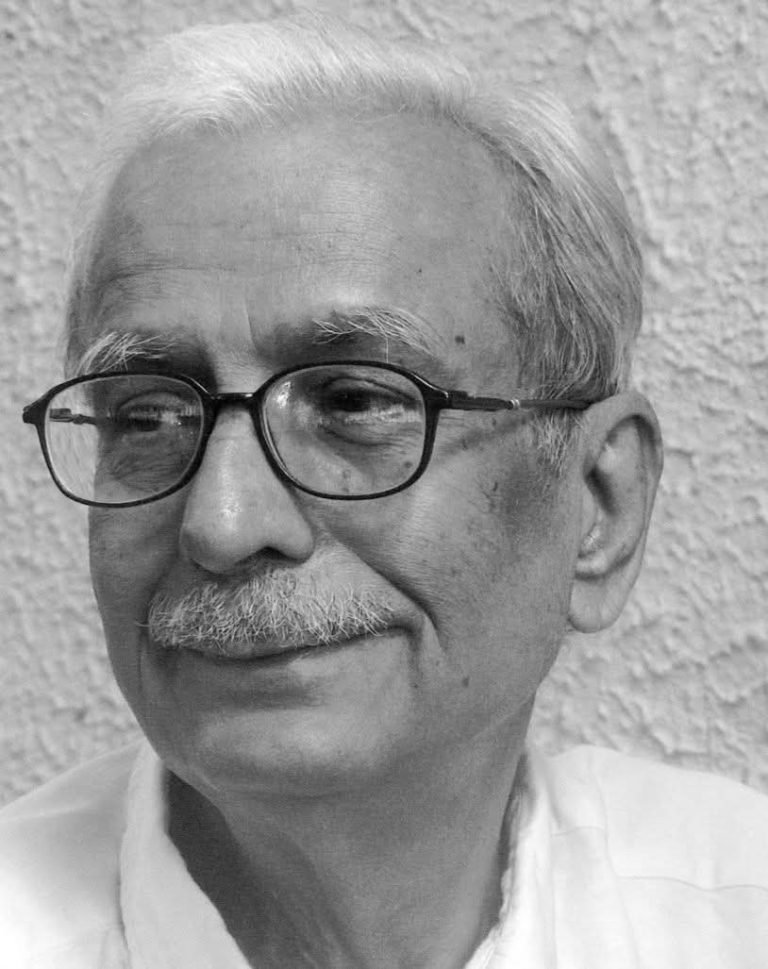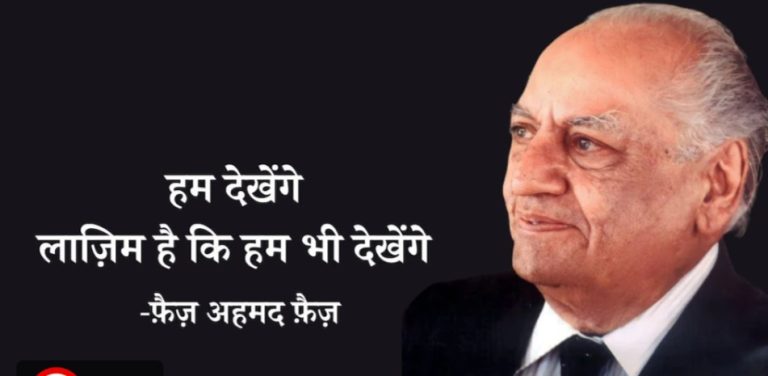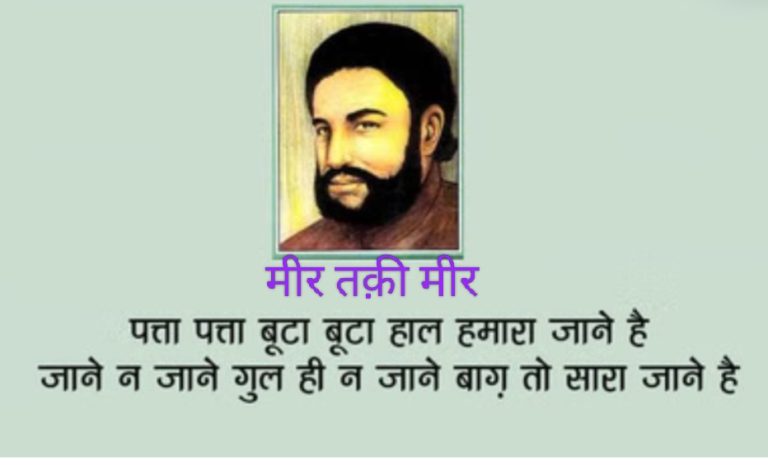टीके की कमी के चलते– एक बनावटी कमी जो निजी संपत्ति अधिकारों को बचाने के कारण से पैदा हुई है– एक वर्ग के लोगों की जिंदगी को दूसरे वर्ग के लोगों की ज़िंदगी के खिलाफ खड़ी कर दी गयी हैं। मौत के इस बढ़ते काफिले को एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वह है दुनिया की समूची आबादी का सार्वभौम टीकाकरण। सभी इस पर सहमत हैं, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी। लेकिन, अगर इस वाइरस के और करोड़ों की जान लेने से पहले ही सार्वभौम टीकाकरण को हमें वास्तविक रूप देना है, तो इसके लिए टीके के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी करनी होगी।
हमें बिना लाग लपेट के बात करनी चाहिए। आज जब कोरोना का वाइरस मानवता का संहार करने में लगा हुआ है, तब इस नरसंहार में उसकी सबसे बड़ी सहयोगी है, पूंजीवादी संपत्ति अधिकार नाम की संस्था। द इकॉनमिस्ट का मानना है कि इस वाइरस से अब तक दुनिया भर में हुई मौतों की संख्या 30 लाख नहीं है, जैसाकि सरकारों द्वारा दावा किया जा रहा है बल्कि यह संख्या एक करोड़ से भी अधिक है। और यह वाइरस अब भी खत्म होने से काफी दूर है। मौत के इस बढ़ते काफिले को एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वह है दुनिया की समूची आबादी का सार्वभौम टीकाकरण। सभी इस पर सहमत हैं, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी। लेकिन, अगर इस वाइरस के और करोड़ों की जान लेने से पहले ही सार्वभौम टीकाकरण को हमें वास्तविक रूप देना है, तो इसके लिए टीके के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी करनी होगी।
टीके के उत्पादन में इस तरह की जबरदस्त बढ़ोतरी में सबसे बड़ी बाधा है चंद बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के बौद्घिक संपदा अधिकार। इन कंपनियों ने भारी सार्वजनिक फंडों का इस्तेमाल कर के उन टीकों का विकास किया है, फिर भी उन्हें अपनी इस एकाधिपत्य बनाए रखने में कोई हिचक नहीं है, वे ऐसे समय में इंसानी तकलीफ में भी मुनाफाखोरी कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे वे अपने निवेश की उगाही की दलील दे रहे हैं, जो उन्होंने न के बरारबर किया है।
अमरीका के राष्टपति जो बाइडेन का टीकों पर पेटेंट अधिकारों के अस्थायी रूप से उठाए जाने के लिए मंजूरी देना, बेशक एक महत्वपूर्ण घटनाविकास है। लेकिन, जब तक विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे पर आम समझौता नहीं हो जाता है, इस तरह की छूट अमल में नहीं आ सकती है। और यूरोप की पूंजीवादी सरकारें, पेटेंट अधिकारों से ऐसी छूट का विरोध करने के बजाए ‘अपने’ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारों का का मजबूती से समर्थन कर रहे हैं।
यह अनुमान लगाया गया है कि अगर पेटेंट अधिकारों की इन बाधाओं से मुक्त होकर, टीकों के उत्पादन के लिए तमाम उपलब्ध क्षमता का उपयोग किया जाता है तो, दुनिया की 60 फीसद आबादी को चालू वर्ष के आखिर तक ही टीका लगाया जा सकता है– प्रभावशाली रूप से इस वाइरस के संक्रमण का खात्मा। लेकिन, विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर वार्ताओं में ही, जिनमें जर्मनी तथा अन्य कुछ देश पेटेंट अधिकारों के अस्थायी निलंबन का डटकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अभी कई महीने लग सकते हैं और ये वार्ताएं ही साल के आखिर तक खिंच सकती हैं।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन का मंसूबा जी-7 शिखर सम्मेलन के सामने इसका प्रस्ताव रखने का है कि 2022 के आखिर तक दुनिया भर का टीकाकरण कर दिया जाना चाहिए। लेकिन, अगर जी-7 इस मंसूबे को मंजूर भी कर लेता है और उक्त लक्ष्य को वास्तव में पूरा भी कर लिया जाता है, तब भी वहां तक पहुंचने तक तो करोड़ों और मौतें हो चुकी होंगी। इसलिए निष्कर्ष यही है कि निजी बौद्घिक संपदा अधिकारों को न्यून कर संभावित मौतों को टाला जाए।
बहुतों ने ‘टीका रंगभेद’ का जिक्र किया है। इसका संबंध इस तथ्य से है कि टीका उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा अब तक तो विकसित पूंजीवादी दुनिया ने ही कब्जाया हुआ है और तीसरी दुनिया के लिए उन्होंने टीकों का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा छोड़ा है। मिसाल के तौर पर अप्रैल के आखिर तक, जहां अमरीका की 40 फीसद आबादी और योरपीय यूनियन की 20 फीसद आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के लिए यही हिस्सा सिर्फ 2 फीसद ही था। भारत में तो अब तक कुल 3 फीसद आबादी का ही पूरी तरह से टीकाकरण हो पाया है। विकसित देशों ने सिर्फ अब तक ही नहीं बल्कि कल्पनीय भविष्य तक के टीका उत्पादन का भी बड़ा हिस्सा हथिया लिया है। उन्होंने इन टीकों के लिए अग्रिम आदेश दे रखे हैं और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ही नहीं बल्कि जखीरे जमा कर के रखने के लिए भी टीके खरीदने के आदेश दे दिए हैं।
बहरहाल, इस टीका रंगभेद के दो अलग-अलग घटक हैं, जो दोनों ही विकसित पूंजीवाद से सबंध रखते हैं। इनमें पहला घटक है, पेटेंट आधारित एकाधिपत्य पाबंदियों के चलते उत्पादन की अपर्याप्तता का। इसका नतीजा यह हो रहा है कि विकसित देश टीकों के इस उत्पादन में से अधिकांश हथियाने में कामयाब रहे हैं। जैसाकि हमने ऊपर कहा, इसका संबंध पेटेंट से जुड़े संपत्ति अधिकारों से है। दूसरा घटक है, विकसित देशों की तुलना में, तीसरी दुनिया के देशों में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए राजकोषीय मदद का उपलब्ध नहीं होना। दो अलग-अलग श्रेणी के देशों के बीच की यह विरोधाभास काफी समय से दिखाई दे रही थी। इस महामारी के दौरान अपनी आबादी को मदद पहुंचाने पर अनेक विकसित देशों की सरकारों ने अपने बजट का 20 फीसद हिस्सा तक खर्च किया है, जबकि तीसरी दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसी पर अपने बजट का मुश्किल से 2 फीसद या उससे भी कम खर्च किया है।
यही विरोधाभास टीके के लिए सब्सीडी दिए जाने में भी दिखाई देती है। इसका नतीजा यह है कि तीसरी दुनिया के गरीब ये टीके लगवा ही नहीं सकते हैं, जिनकी कीमत उनकी पहुंच से बाहर ही है।
विडंबना यह है कि वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसने सार्वभौम टीकाकरण का समर्थन किया है, तीसरी दुनिया के देशों की सरकारों पर उन्हें ऋण देने की शर्त के रूप में या उनके पहले के ऋणों के संबंध में पुनर्वाताओं में शर्त के रूप में, राजकोषीय कटौती के कदम थोपता है। इसलिए, टीका रंगभेद में योग देने वाले इस दूसरे घटक को वित्तीय पूंजी के उस वर्चस्व से जोड़ा जा सकता है, जो हर तरह की सरकारी सक्रियता का विरोध करता है, बस ऐसी सक्रियता को छोडक़र जो वित्तीय पूंजी के अपने हित में हो। बेशक, भारत में सरकार के सबके लिए मुफ्त टीके के प्रावधान न करने के पीछे कोई अंतर्राष्टï्रीय मुद्रा कोष की थोपी राजकोषीय कटौती की मांग नहीं है बल्कि इसके पीछे तो मोदी सरकार की अपनी रक्त पिपासा ही है।
यह अनुमान लगाया गया है कि सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम पर मुश्किल से करीब 50 अरब डालर का खर्चा आएगा। इतनी रकम तो विकसित पूंजीवादी दुनिया आराम से मुहैया करा सकती है और यह रकम तीसरी दुनिया को ऐसे हस्तांतरणों के रूप में दी जा सकती है, जिन्हें बाद में चुकाना नहीं पड़े। लेकिन, विडंबना यह है कि हालांकि इस तरह की सूक्तियां तो करीब-करीब सभी के मुंह से और अंतहीन पुनरावृत्ति में हमें सुनने को मिलती हैं कि, ‘जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है’, लेकिन इस तरह के हस्तांतरण के दूर-दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
अगर पेटेंट से छूट फौरन संभव नहीं भी हो तो, अनिवार्य लाइसेंसिंग के माध्यम से टीकों के उत्पादन का विस्तार किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत, ‘राष्टï्रीय आपात स्थितियों’ में इस प्रावधान के उपयोग का प्रावधान मौजूद है और मौजूदा हालात को ‘राष्टï्रीय आपत स्थिति’ कहना तो पूरी तरह से जायज है। भारतीय पेटेंट कानून के अध्याय-16 में भी, जिसे ‘ट्रिप्स-अनुरूप’ बनाने के लिए संशोधित किया गया था, अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान मौजूद है।
अनिवार्य लाइसेंसिंग के पक्ष में ठीक वही तर्क है, जो पेटेंट से माफी के पक्ष में है, कि ‘राष्टï्रीय आपत स्थिति’ के हालात हैं, जब टीका का उत्पादन तेजी से बढ़ाए जाने की जरूरत है और इन हालात में दुनिया इसका इंतजार करती नहीं रह सकती है कि मूल पेटेंट-धारक ही, अपनी फुर्सत के हिसाब से इन जरूरतों को पूरा करें। इसके बावजूद, अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान का सहारा लिए जाने का काफी विरोध हो रहा है और यह विरोध सिर्फ दवा बहुराष्टï्रीय निगमों तथा उनकी पीठ पर हाथ रखे विकसित देशों की सरकारों द्वारा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि ऐसी अनेक संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा भी किया जा रहा है, जो अन्यथा पेटेंट से छूट का समर्थन करते हैं। विचित्र तरीके से भारत सरकार ने भी, जिसने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर, पेटेंट से छूट की मांग उठायी थी, अनिवार्य लाइसेंसिंग की सारी मांगों को ठुकरा दिया है और सरकार के तथाकथि ‘‘थिंक टैंक’’, नीति आयोग ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचारों को वीटो ही कर दिया है।
ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह अब भी रहस्य ही बना हुआ है। शायद, इस मामले में मोदी सरकार की अनिच्छा को इससे समझा जा सकता है कि वह दवा बहुराष्ट्रीय निगमों को और इन बहुराष्ट्रीय निगमों की पीठ के पीछे खड़ी विकसित देशों की सरकारों को, ऐसा इकतरफा कदम उठाकर नाराज नहीं करना चाहती है और जाहिर है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग का सहारा लेना ऐसा इकतरफा कदम तो है ही। लेकिन, इस अनिच्छा का अर्थ हजारों जिंदगियां कुर्बान करना भी तो है। मोदी सरकार का यह दब्बूपन इसलिए खासतौर पर ध्यान खींचने वाला है क्यूँकि इन पंक्तियों के लिखे जाने (7 जून) तक, दो हफ्ते से राजधानी दिल्ली में टीके के स्टॉक जरूरत से बहुत कम बने हुए थे।
अंतर्राष्टï्रीय सहयोग के संबंध में या सार्वभौम टीकाकरण की जरूरत के संंबंध में, किसी भी सदाशयतापूर्ण घोषणा का तब तक कोई मतलब नहीं होगा, जब तक इसके साथ ही तत्काल पेटेंट के उठाए जाने की और ऐसा न हो पाने की सूरत में अनिवार्य लाइसेंसिंग की मांग नहीं की जाती है। इसकी वजह यह है कि यहां एक बुनियादी सिद्घांत दांव पर लगा है: क्या किसी भारतीय का या अफ्रीकी का या लातीनी अमरीकी का जीवन का अधिकार, किसी यूरोपीय या अमरीकी के जीवन के अधिकार से घटकर है? किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इस मौलिक पूर्वकल्पना को आधार बनाकर चलना चाहिए कि किसी गरीब देश के किसी व्यक्ति की जान की भी उतनी ही कीमत है, जितनी किसी धनी देश के किसी व्यक्ति की जान की। इस पूर्व-धारणा के नकारते हुए भी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बतकही करना, शुद्घ कपटलीला है।
बेशक, किसी भी सरकार को, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शर्त या दायित्व को पूरी करने से पहले, अपने नागरिकों की जिंदगियों को प्राथमिकता देने का अधिकार है। लेकिन, विकसित देशों की सरकारों के लिए आज प्रश्न वास्तव में यह तो है ही नहीं कि अपने देश के नागरिकों की जान बचाएं या दूसरे देशों के नागरिकों की जान बचाएं। बल्कि टीके की कमी के चलते– यह एक बनावटी कमी है जो निजी संपत्ति अधिकारों को बचाने के कारण से पैदा हुई है– एक वर्ग के लोगों की जिंदगियों को दूसरे वर्ग के लोगों की ज़िंदगी के खिलाफ खड़ी कर दी गयी हैं। संपत्ति अधिकारों का यही संरक्षण है जो टीके के उत्पादन में बढ़ोतरी को रोक रहा है। संक्षेप में यह मसला जनगण बनाम जनगण का नहीं है बल्कि जनगण बनाम मुनाफों का है।
उल्लेखनीय बात यह है कि विकसित देशों में लोग इस बात को समझते हैं। उनका विशाल बहुमत वास्तव में इसके पक्ष में है कि टीकों पर पेटेंट अधिकार को अस्थायी रूप से हटा दिया जाए। सरकारें और खासतौर पर यूरोप की सरकारें ही इस विचार का विरोध कर रही हैं। इससे इसी धारणा की पुष्टि होती है कि सरकारों को वर्गीय हितों की और उनसे जुड़े संपत्ति अधिकारों की ही हिफाजत करने की चिंता रहती है, केवल जनता ही अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के सच्ची वाहक है।
(लेखक प्रख्यात अर्थशास्त्री और राजीतिक विश्लेषक हैं।) सौज-न्यूजक्लिक
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें
https://www.newsclick.in/human-life-poor-country-precious-rich-country