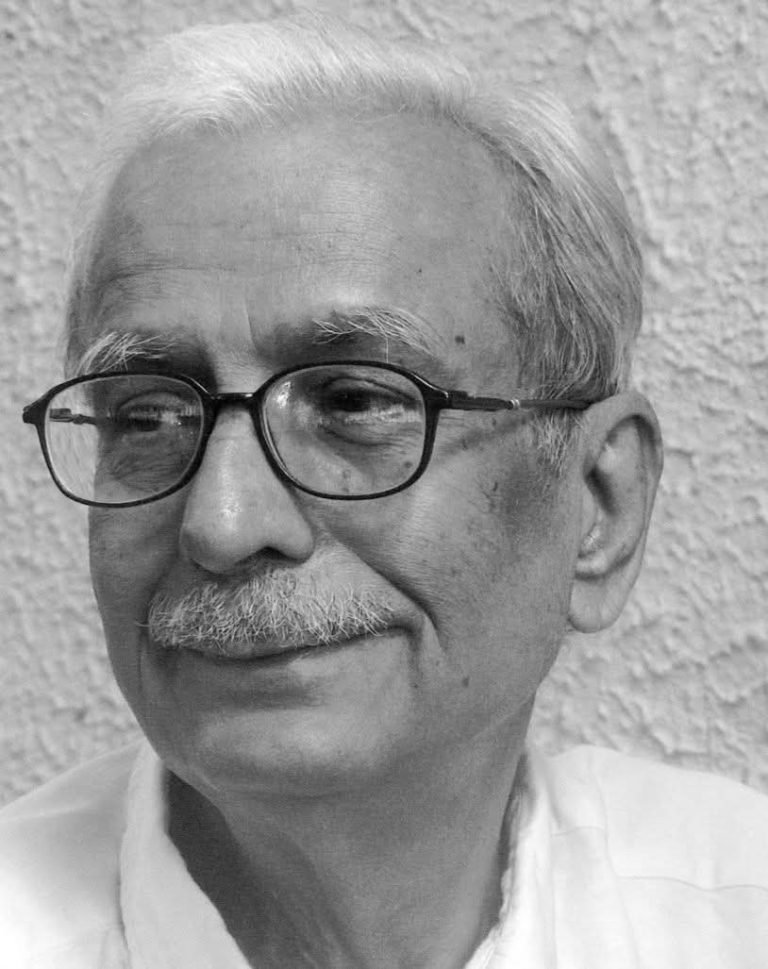राजस्थान की पिछली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गरीबों को सहायता देने से जुड़ी अनेक सरकारी योजनाओं को कतरने की तैयारियां कर रही थीं। उनका कहना था कि वह ऐसा इसलिए करना चाहती हैं ताकि, ”लोग शासन पर बहुत ज्यादा निर्भर न हो जाएं।” अगर वह पहले से जारी योजनाओं का पुनर्गठन ही कर रहीं होतीं या कुछ योजनाओं को खत्म कर उनकी जगह पर उसी तरह के लक्ष्यों वाली किन्तु कहीं ज्यादा कारगर योजनाएँ लागू कर रही होतीं या फिर गरीबों को किसी एक रूप में सहायता देना बंद कर, उसकी जगह पर दूसरे रूप में सहायता शुरू कर रही होतीं, तब भी उनके प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता था । ऐसा होने पर व्यवहारवादी तरीके से इस पर चर्चा की जा सकती थी कि कौन सा विकल्प ज्यादा कारगर रहेगा । लेकिन, वह तो गरीबों को सहायता देना कम करने का एक आम तर्क ही पेश कर रही थीं ।
वास्तव में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व में राजस्थान प्रतिक्रियावादी आर्थिक नीतियों को लागू करने के मामले में पूरे देश की अगुआई कर रहा था । मिसाल के तौर पर वह पहले ही ”श्रम बाजार में लचीलापन” लाने में यानी मजदूरों के कड़ी लड़ाइयों के बाद हासिल हुए अधिकारों को छीनने तथा ट्रेड यूनियनों को ध्वस्त करने में, आगे-आगे चल रहीं थीं । इसीलिए, इस दलील के झूठ को बेनकाब करना जरूरी हो जाता है कि ”लोगों को शासन पर अति-निर्भर” नहीं होने दिया जाना चाहिए ।
जॉन रॉल्स जैसे उदारपंथी भी, जिनके लिये व्यक्ति ही हर चीज का प्रस्थान बिंद है और जो शासन को, व्यक्तियों की सहमति पर ही टिका हुआ मानते हैं, कम से कम यह जरूर मानेंगे कि समाज में ”न्याय” होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो सबसे दरिद्र हैं, उन्हें भी कम से कम एक न्यूनतम जीवन स्तर तो हासिल हो । यह न्यूनतम सिर्फ शासन ही सुनिश्चित कर सकता है क्योंकि अगर शासन का इस तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, बाजार में विनिमय की प्रक्रिया में व्यक्तियों की हिस्सेदारी के क्रम में, नियमत: ही एक हिस्सा इस न्यूनतम से नीचे खिसक जाएगा ।
अब अगर गरीबों के हक में शासन का हस्तेक्षेप ”प्रवाहों” के स्तर पर होता है, मिसाल के तौर पर आय-सहायता के रूप में या कीमतें सब्सीडाइज करने के रूप में, तो इस तरह का हस्तक्षेप बराबर करते रहना होगा। दूसरी ओर, अगर शासन का हस्तक्षेप परिसंपत्तियों (स्टॉक्स) के स्तर पर होता है, मिसाल के तौर पर लोगों के हक में परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के रूप में, ताकि उनके हाथ में आयी इन अतिरिक्त परिसंपत्तियों से निकलने वाले प्रवाह उनके जीवन स्तर को न्यूनतम से ऊपर उठा सकें, उस सूरत में भी यह हस्तक्षेप भले ही एकमुश्त हुआ हो, इसके परिणाम बराबर अपना काम कर रहे होंगे । संक्षेप में यह कि गरीबों के हक में शासन के हस्तक्षेप का रूप चाहे जो भी हो, उदारपंथी सिद्धान्तकार भी यह मानते हैं कि गरीबों की मदद के लिये शासन के हस्तक्षेप की जरूरत इस माने में बराबर बनी रहने वाली है कि इस तरह के हस्तक्षेप के असर की हरेक दौर में जरूरत रहेगी । यानी ऐसे उदारपंथी सिद्धान्तकार भी ऐसी ही स्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ शासन पर गरीबों की ”निर्भरता”, हरेक दौर में स्वत: स्पष्ट रूप से मौजूद रहेगी ।
शासन की ओर से कल्याणकारी कदमों का दक्षिणपंथी विरोध या तो इस दलील का रूप लेता है कि हरेक लाभार्थी को बहुत ज्यादा लाभ दिया जा रहा है या फिर इस दलील का कि बहुत ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है । लेकिन, इस तरह की किसी भी दलील का वास्तव में तब तक कोई अर्थ ही नहीं होगा जब तक कि कोई ठोस मानक नहीं तय कर दिया जाता है, जिससे इसका माप हो सके कि क्या ”बहुत ज्यादा” है या ”बहुद ज्यादा हैं।” सामान्य रूप से दक्षिणपंथी तर्क में कभी भी इस तरह का कोई मानक पेश नहीं किया जाता है और इसलिए, इस तरह का तर्क वास्तव में बेमानी ही होता है ।
यही बात राजस्थान की पिछली मुख्यमंत्री की दलील पर भी लागू होती है । चूंकि वह इसका कोई मानक पेश ही नहीं कर रही थीं कि किन को शासन की सहायता का लाभ मिलना चाहिए और कितना लाभ मिलना चाहिए, उनकी दलील निरर्थक थी । मुद्दा इस दलील के स्वीकार्य होने न होने का नहीं है । मुद्दा यह है कि यह दलील ही निरर्थक है, सिवा इसके कि यह दलील आवरण में लपेट कर इसी आग्रह को पेश कर रही होती है कि शासन को गरीबों के हक में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करनी चाहिए । लेकिन, यह तो महज एक पूर्वाग्रह को पेश करना है और वह भी ऐसे पूर्वाग्रह को जो, शासन की भूमिका की उदारपंथी कल्पना तक के खिलाफ जाता है ।
लेकिन, यह विचार भी कि शासन को इस मामले में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, अपने आप में झूठा है । आखिरकार, शासन तो पहले ही हर जगह हस्तक्षेप कर रहा है । हरेक व्यक्ति का जन्म किसी समाज में होता है, उत्पादन के संगठन की ठोस सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच होता है । ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, जो परिकल्पना के रूप में समाज से पहले आया हो। व्यक्ति, इतिहास का प्रस्थान बिन्दु नहीं हो सकता है बल्कि कहना चाहिए कि वह तो इतिहास का उत्पाद होता है । एक श्रेणी के रूप में व्यक्ति, सामंतवाद के अंत और मुक्त प्रतियोगिता के पूंजीवाद नाम की संस्था के कायम होने के बाद ही सामने आता है ।
जैसा कि मार्क्स ने ग्रंड्रिसे में लिखा है : ”मुक्त प्रतियोगिता के समाज में, व्यक्ति उन प्राकृतिक रिश्तों आदि से कटकर सामने आता है, जो पहले के ऐतिहासिक दौरों में उसे एक निश्चित तथा सीमित मानव समूह का हिस्सा बनाते थे।” लेकिन, इस प्रतीति की वजह से हमें इस तथ्य की ओर से ऑंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए कि, ”समाज में उत्पादन कर रहा व्यक्ति — इसलिए सामाजिक रूप से निर्धारित व्यक्तिगत उत्पादन — बेशक प्रस्थान बिन्दु है।”
किसी व्यक्ति के जीवन की भौतिक दशा, यह दशा भले ही गरीबी की हो या फिर बहुत दौलतमंदी की, उस सामाजिक व्यवस्था से निर्धारित होती है, जिसमें वह व्यक्ति उत्पादन करता है यानी व्यक्ति के जीवन की भौतिक दशा, सामाजिक रूप से निर्धारित व्यक्तिगत उत्पादन की संबंधित व्यवस्था की अंतर्निहित प्रवृत्तियों से तय होती है । बेशक, कोई व्यक्ति बेरोजगार रहने का भी रास्ता चुन सकता है या फिर सन्यासी बनकर जंगल की राह भी ले सकता है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी भौतिक जीवन दशा का सामाजिक उत्पादन की चालू व्यवस्था से या कहीं ज्यादा प्रचलित संज्ञा का उपयोग करें तो चालू ”उत्पादन पद्धति” से नाता टूट जाएगा । लेकिन, जब हम ऐसे अपवादों की नहीं बल्कि साधारण लोगों की बात करते हैं, उनकी जीवन-दशा उनके व्यक्तिगत चुनाव से तय नहीं होती है बल्कि उन सामाजिक व्यवस्थाओं से तय होती है, जिनके दायरे में वे उत्पादन करते हैं । इन व्यवस्थाओं में अनिवार्य रूप से व्यक्ति को काम करने के लिये मजबूर करने वाले तंत्र भी होते हैं याने ऐसे तंत्र जो व्यक्तिगत इच्छाओं को बहुत हद तक अप्रासांगिक ही बना देते हैं ।
मिसाल के तौर पर यह कहना कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है कि वह आलसी या कामचोर है, तथ्यात्मक रूप से गलत तथा नैतिक रूप से जुगुप्सापूर्ण तो है ही, अपने आप में झूठा भी है क्योंकि समाज व्यवस्था इसकी कोई खास गुंजाइश ही नहीं छोड़ती है कि कोई आलसी रह जाए। सामंतवाद के दौर में तो आका के कोड़े की सटासट ही व्यक्ति को इस तरह के चुनाव का मौका ही नहीं देती थी । पूंजीवादी व्यवस्था में प्रकटत: जरूर व्यक्ति को ”आलसी” बने रहने का मौका होता है । लेकिन, इसका मतलब बेरोजगारों तथा कंगालों की फौज में धकेल दिए जाने का चुनाव करना होता है, जिसके परिणाम इतने भयानक होते हैं कि इक्का-दुक्का सन्यासी या समाज-विमुख व्यक्ति ही ऐसे विकल्प को अपनाने का बात सोच सकता है ।
इसका अर्थ यह हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत भी, जिसके दायरे में प्रकटत: व्यक्ति ”स्वतंत्र” तथा इसलिए अपनी नियति खुद तय करता नजर आता है, विडंबनापूर्ण तरीके से उसे इस व्यवस्था की स्वत: स्फूर्तता का शिकार बनना पड़ता है और उत्पादन व्यवस्था में किसी खास भूमिका को ही अदा करना पड़ता है । उसे, इस व्यवस्था की अंतर्निहित प्रवृत्तियों के नतीजे झेलने पड़ते हैं ।
इसलिए, भौतिक परिस्थितियों के स्तर पर व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होता है, सारत: उस समाज व्यवस्था के परिचालन का ही परिणाम होता है, जिसके दायरे में व्यक्ति उत्पादन कर रहा होता है । अगर कोई व्यक्ति गरीब है, तो यह उस सामाजिक व्यवस्था का फल है, जिसके दायरे में वह जीता है । इन सामाजिक व्यवस्थाओं के पीछे राज्य या शासन काम कर रहा होता । इसलिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य या शासन तो हमेशा ही ”तस्वीर में रहता” है । इसलिए, शासन को कृपापूर्वक ”तस्वीर में लाने” या फिर लोगों के शासन पर ज्यादा ”निर्भर हो जाने” का कोई सवाल ही नहीं उठता है । लोग तो पहले ही, चाहे नकारात्मक रूप से ही हों, इस अर्थ में शासन पर ”निर्भर” होते हैं कि उनके जीवन की भौतिक परिस्थितियाँ, उस सामाजिक व्यवस्था से तय होती हैं, जिसके अंतर्गत वे जीते हैं और इस समाज व्यवस्था को, अनिवार्य रूप से राज्य या शासन के सहारे कायम रखा जाता है। इस तरह वे तथ्यत: राज्य पर ”निर्भर” तो होते ही हैं ।
इसलिए, यह कहना कि शासन को आर्थिक मामलों से ”दूर ही रहने” की नीति पर चलना चाहिए, चूंकि वास्तव में शासन कभी ”दूर” हो ही नहीं सकता है, असल में यही कहना होता है कि शासन को, एक खास तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए न कि दूसरे तरीके से । इसमें तथाकथित हस्तक्षेप ही न करने की नीति भी शामिल है क्योंकि हस्तक्षेप न करना भी तो खास दिशा में हस्तक्षेप करना ही है । शासन से ”दूर रहने ” की माँग करना, वास्तव में इसी की माँग करना होता है कि इस तरह हस्तक्षेप करने के बाजए, जो सब के लिये एक निश्चित ”प्रवाह” आय सुनिश्चित करे, जिस प्रवाह का उदारपंथी सिद्धान्तकार तक समर्थन करेंगे, शासन को या तो इस पहलू से कुछ भी करना ही नहीं चाहिए या फिर इस तरह हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे ”व्यवस्था बेहतर तरीके से” काम करे । इसका अर्थ यह है कि शासन को पूंजीपतियों के हित साधने के लिये ही हस्तक्षेप करना चाहिए यानी उनके लिए ही और ”प्रोत्साहन” तथा हस्तांतरण मुहैया कराने चाहिए ।
इसलिए, इसकी शिकायत करना कि जनता शासन पर ”निर्भर” होती जा रही है, वास्तव में यह कहने जैसा है कि शासन को ऐसी नीतियाँ चलाने के लिए ही ”मुक्त” छोड़ दिया जाना चाहिए, जो पूंजी के स्वार्थो को ही आगे बढ़ाएं । इसका मतलब है ऐसी नीतियों पर चलने की स्वतंत्रता, जो सबसे बढ़कर कार्पोरेट-वित्तीय अल्पतंत्र के स्वार्थों को पूरा करे । शासन की इस उन्मुखता पर इसके दिखावे का पर्दा डालने की कोशिश की जाती है कि जनता के साथ जो भी होता है, उसकी अपनी करनियों से तय होता है और इसलिए अगर वह अपनी घोर दरिद्रता से उबरना चाहती है तो उसे ”अपनी चाल सुधारनी” चाहिए और शासन पर ”निर्भर” होने के बजाए, ”खुद अपने पांवों पर खड़े” होना चाहिए।
बेशक, यही तथ्य कि कोई व्यक्ति अपनी भौतिक अवस्था के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होता है और उसकी भौतिक अवस्था खुद ही उन सामाजिक व्यवस्थाओं का नतीजा होती है, जिनके बीच कोई व्यक्ति पैदा होता है, समाजवादी सिद्धान्त का प्रस्थान बिन्दु है । लेकिन, चूंकि उत्पादों का वितरण, जोकि किसी व्यक्ति के जीवन की भौतिक दशा का एक महत्वपूर्ण निर्धारत होता है, उत्पादन के साधनों के वितरण में पूर्वनिहित माना जा रहा होता है, व्यक्ति की भौतिक जीवन दशाओं में कोई भी बुनियादी बदलाव, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को बदले बिना नहीं लाया जा सकता है और चूंकि पहले से मौजूद राज्य शासन, जो कि उस विशेष उत्पादन पद्धति की हिफाजत करता है, इस तरह का बदलाव नहीं आने देगा, इसलिए उस शासन राज्य को ही बदलना जरूरी हो जाता है ।
लेकिन, वर्तमान राज्य व्यवस्था को बदलने की जरूरत इसलिए होती है कि वह जनता की भौतिक जीवन दशाओं में बुनियादी बदलाव नहीं लाने देगी, न कि इसलिए कि इन मामलों में पड़ना तथा ”जनता को अपने ऊपर निर्भर बनाना” राज्य का काम नहीं है, जैसा कि दक्षिणपंथी दावा करते हैं। सच्चाई यह है कि आदि से अंत तक, राज्य व्यवस्था हमेशा इन मामलों में दखलंदाजी करती रहती है और ठीक इसीलिये, उसे बदले जाने की जरूरत पैदा होती है ।
दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्तियों को अपनी भौतिक अवस्था के लिये खुद जिम्मेदार मानना, सामाजिक व्यवस्थाओं को पराभौतिक व्यवस्थाओं की तरह देखना हुआ । यह तो एक प्रकार से यही कहना हुआ कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाएँ तो आदर्श व्यवस्थाएं है और अगर इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोग दयनीय अवस्था में रह रहे हैं, तो यह जरूर उनका ही दोष होगा और इस सूरत में अगर शासन उनकी मदद करता है,तो वह इन लोगों के दोष को ही बनाए रख रहा होगा और इस तरह, उनका दोष दूर करानेके बजाए, उन्हें शासन पर ”निर्भर” ही बना रहना होगा । यह खांटी दक्षिणपंथी दलील है जो, मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाओं का दैवीकरण करती है और इसका औचित्य सिद्ध करती है कि शासन को सिर्फ कार्पोरेट-वित्तीय अल्पतंत्र के स्वार्थ साधने में जोता जाना चाहिए । बहरहाल, भारत में हम पहली ही बार एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की महत्वपूर्ण नेता के मुँह से यह तर्क सुन रहे हैं। बेशक, आने वाले दिनों में हमें बार-बार यह दलील सुनने को मिलने जा रही हैं ।
(लेखक मार्क्सवादी अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। यह लेख उनके निबंध संग्रह -भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति – से साभार)