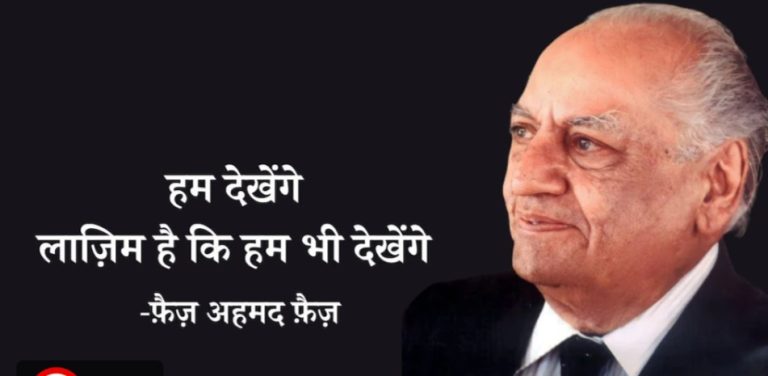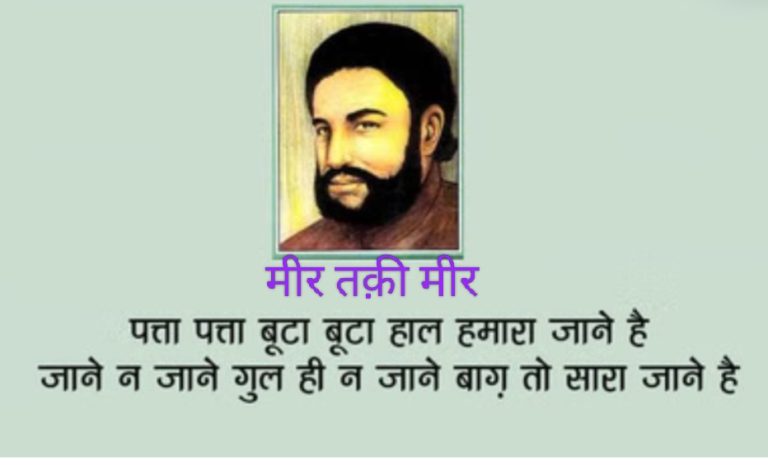सत्यम श्रीवास्तव
‘क्रिमिनल जस्टिस’ सीजन -1, ऐसे तो कानूनी पेचीदगियों से भरी एक कहानी है लेकिन यह दर्शकों को खुद जासूस हो जाने का मौका मुहैया कराती है और शायद यही वजह है कि लगभग आठ घंटे की इस वेब सीरीज़ को एक बार देखना शुरू करने पर आप अंत देखे बगैर उठ नहीं पाते.
यह बेहतर निर्देशन है या कथानक या बेहतरीन अभिनय लेकिन जितना सघन अनुभव इन सभी पक्षों से मिलकर यह सीरीज बनती है उसकी परिणति दर्शकों को आठ घंटे निरंतर अपने साथ बनाए रखने में होती है.
कहानी थोड़ा आम-सी ही है यानी हिन्दी सिनेमा में कई बार दोहराई- सी लेकिन इसे देखना बाकी तजुर्बों से अलग कैसे करता है? यही इस वेब सीरीज की समीक्षा के वो पहलू हैं जिन पर बात होगी और होनी भी चाहिए.
कहानी की शुरुआत में हमें महसूस करा दिया जाता है कि जिस युवा नायक पर उसके लिए अंजान लड़की के बेरहमी से बलात्कार व हत्या का आरोप साबित हो रहा है वो वाकई मासूम है और उसने ऐसा किया नहीं है तब भी जबकि सारे सबूत, गवाह और परिस्थितियां इसकी ताईद करती हैं. दर्शकों का यह भरोसा बना रहता है और शायद शुरुआत के इस भरोसे को अंत तक सही साबित होने की गर्ज़ से ही कोई इस सीरीज़ को पूरा देखता है.
कमाल यह है कि किसी भी घटनाक्रम का कोई भी ब्यौरा दर्शकों से छिपाया नहीं जाता. अगर नायक को कुछ ब्यौरे याद नहीं हैं तो वो दर्शकों को भी पता नहीं हैं. यानी नायक की याददाश्त जितनी है उतनी ही याददाश्त पर्दे पर देख रहे दर्शक के पास है. न उससे कम न ज़्यादा. इसलिए अदालत में जो लंबा मुक़द्दमा चल रहा है उसमें दर्शक नायक की तरफ से पैरवी करने लगता है. जहां नायक को लगता है कि वो अदालत को इतना ही बता पाएगा वहां दर्शक भी अपनी सीमा समझ लेता है. ऐसा नहीं है कि नायक कुछ ज़्यादा जानता था लेकिन किसी भी वजह से वो कुछ छिपा लेना चाहता है और यहां दर्शक को भी उतना ही पता होता है जितना कि नायक को.
यह सीरीज असल में महिला सुरक्षा के बढ़ते सरोकारों और उसके बीच युवाओं की बनाई गयी छवि के समानान्तर एक कथा रचती है. यह बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि घटनाक्रम ठीक वही हो जो हमें अदालतों में दिये गए ब्यौरों से मिलते हैं. संभव है कि पूरी जांच प्रक्रिया पूर्वाग्रहों से तय हुई हो और पूर्वाग्रह भी ऐसे जिन्हें वारदात से जुड़े तमाम पक्ष सही साबित कर रहे हों.
यह कहानी यह भी सुझाती है कि जरूरी तो यह भी नहीं कि कोई पुलिस अफसर या वकील जान-बूझकर किसी मामले में जांच करते समय कोई गलती कर रहा हो बल्कि जांच की दिशा कैसे उनकी मान्यताओं या धारणाओं से तय होती जाती है. इसमें यह भी बताया गया है कि किसी घटना के कई पहलू हो सकते हैं और हम केवल उन पहलुओं को सही मान लेना चाहते हैं जो हमें लगता है कि पहले ऐसा हो चुका है.
यानी यह सीरीज हमारी तमाम मान्यताओं, धारणाओं, पूर्वाग्रहों और पुराने तजुर्बों को चुनौती देती है. इसमें दिलचस्प केवल यह है कि यह चुनौती एक दर्शक को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सीरीज इस कदर कसी हुई और सघन है कि उसमें कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं मिलती कि दर्शक सही गलत के निर्णय पर पहुंच सके.
पुलिस की बनाई चार्जशीट में आपको चालाकी नहीं दिखाई देगी, सबूत जुटाने या पड़ताल की दिशा बदलने की कोई गैर ज़रूरी कोशिश नहीं दिखाई देगी, जबरदस्ती बयान तैयार करवाने के कुछ पैंतरे आपको मिल जाएंगे. तब भी पुलिस को ऐसा करने के पीछे कोई साजिश नहीं दिखाई देगी. अगर दिखाई भी देगा तो अनुभव जन्य और पेशेवर आत्म-विश्वास जो कोई पुलिस अफसर लंबे समय की अपनी नौकरी में पाता है. उसे कोई गवाह क्यों महत्वपूर्ण नहीं लगा या जांच में किसी व्यक्ति विशेष को क्यों नहीं शामिल किया गया, जैसे सवाल इसलिए नहीं उठते क्योंकि आप एक साथ पुलिस और कहानी के नायक दोनों के साथ चलते हैं और मज़ेदार बात यह है कि आप दोनों से ही असहमत नहीं होते. आपकी भावनाएं या शुभेच्छाएं भले ही नायक के साथ हों लेकिन आप पुलिस की थ्योरी पर रिएक्ट नहीं करते.
बहरहाल, बेहद चुस्त कहानी में अंतत: आपके भरोसे की जीत होती है लेकिन इस बहाने आप हिंदुस्तान के पेशेवर न्याय-तंत्र को बेहद करीब से देखते हैं और उतनी ही तीव्रता से आप हिंदुस्तान की जेलों को भी इस सीरीज में देख पाने का अवसर पाते हैं. अदालत और उसके आस-पास के ईको-सिस्टम और जेल-तंत्र का चित्रण इस सीरीज के दो मुख्य हिस्से हैं. इन दोनों के बीच मीडिया, समाज, पारिवारिक मामले आते जाते हैं लेकिन वो इन दो विषयों के इर्द-गिर्द पूरे समाज को देखने की सहज कोशिश करते हैं.
जेलों को लेकर जो समझ समाज में आम तौर पर व्याप्त है यह सीरीज उसे और पुख्ता ही करती है बल्कि ऐसा प्रामाणिक चित्रण भी करती है कि जेलों को लेकर आपकी समझ में ज़रूर इजाफा हो सकता है, लेकिन धारणाओं में कोई फर्क नहीं आयेगा बल्कि वो और पुष्ट ही होंगी. जेलों का जो चित्रण किया गया है वो थोड़ा उबाऊ लगता है लेकिन यह चूंकि खुद ही एक अलग मुद्दा है इसलिए जेल के अंदर भी एक कहानी आकार लेती रहती है. अंदर ट्रायल कैदियों की स्थिति को लेकर ऐसा विस्तार प्राय: देखने में नहीं आया जो इस सीरीज में दिखलाया गया है.
बलात्कार के जुर्म में जेल पहुंचे आरोपी के साथ पहले से जेल में बंद कैदियों का बर्ताव थोड़ी देर के लिए आपको मूल्य आधारित लग सकता है और यह बात आम समाज में भी ज़ाहिर है कि ऐसे अपराधियों के साथ जेल के अंदर कैदियों द्वारा ही बेहद अमानवीय हिंसा होती है. आम तौर पर ऐसे अपराधी जेल में भी यौन हिंसा का शिकार होते हैं. इसके पीछे शायद यही एकमात्र आधार है कि ये आरोपी या कैदी इसके लिए आसान शिकार मान लिए जाते हैं. या उनके पास अपराधी का लांछन होने के बावजूद इतनी नैतिकता शेष रहती है कि उनमें अपने अपराध को लेकर एक तरह की शर्मिंदगी का एहसास रहता है. और हत्या, चोरी, डकैती या अन्य अपराधों में सज़ा पाये कैदियों को लगता है कि उनमें नैतिकता शेष है भले ही वो जेल में हों. अपने किए अपराध की सज़ा काट रहे हों लेकिन महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले को सबक सिखाना उनका सामाजिक दायित्व है. जो भी हो लेकिन कैदियों की दुनिया में एक नैतिक ऊंचाई है जो फिर से अपराध के तौर पर अभिव्यक्त होती है.
विचाराधीन कैदियों या अंडर ट्रायल कैदियों के लिए जेल में सुरक्षा एक बड़ा सवाल है भले ही अदालत उन्हें न्यायिक हिरासत के नाम पर जेलों में भेजती है लेकिन एक बार जेल में पहुंच जाने के बाद वहां जेल से बाहर की किसी संस्था का अधिकार क्षेत्र जैसे खत्म हो जाता है. जेलों की दुर्दशा दिखलाने में इस सीरीज ने कुछ खास नहीं किया बल्कि इस तथ्य को स्थापित ही किया कि भारतीय जेलें मानव अधिकारों का न्यूनतम पालन करने में भी असमर्थ हैं. इसके लिए जेलों पर बढ़ते दबाव को एक समस्या माना भी जाये तब भी न्याय-व्यवस्था की मंथर गति इस स्थिति को और भयावह बना रही है. जहां बीस लोग ठीक से पांव फैलाकर सो नहीं सकते वहां इससे चार गुना कैदियों को रहना है. साफ सफाई, संडास, खाने पीने की अमानवीय परिस्थितियों में जेल सुधार गृह की अवधारणा से मुक्त हैं बल्कि जेलों की जो स्थितियां हैं उनमें गैर-आपराधिक मानसिकता का इंसान मानसिक रूप से अपराधी बनकर ही निकलेगा इसे विस्तार से इस सीरीज में दिखाया है.
कहानी और निर्देशन की सराहना इस मौंजू पर भी होगी कि जिस नायक को आप एक दर्शक के तौर पर आदतन या इरादतन अपराधी नहीं मानते हैं लेकिन जेल के अंदर उसका धीरे-धीरे अपराधी में बदलते जाना आपको चौंकाता नहीं है बल्कि यह उन परिस्थितियों में आपको सबसे मुनासिब लगने लगता है. यहां आकर कहानी जैसे आपका अनुकूलन करने लगती है. ‘लायक तालुकदार (देवयेन्दु भट्टाचार्य)’ जैसे अपराधी से निपटने का मामला हो या ‘मुस्तफा’ (जैकी श्राफ़) जैसे कैदी की दादागिरी हो, आपको सब कुछ सामान्य और सहज लगने लगता है. ‘अंतर्विरोधों में सामंजस्य’ या मनोवैज्ञानिक अनुकूलन के घनत्व को समझना हो तो हमें दो दृश्य याद रह जाते हैं.

एक जब पुराना कैदी मुस्तफा जो उस जेल का लगभग बादशाह है, आपके नायक यानी आदित्य शर्मा (विक्रांत मैसी) की जेल में सुरक्षा के लिए, वास्तव में लायक से उसके यौन शोषण से सुरक्षा करने के एवज़ में उससे पांच लाख रुपये मांगता है. तब आपको मुस्तफा से ठीक वही आपत्ति नहीं होती जो लायक से हो रही होती है. उसके बाद जब आपका नायक ही मुस्तफा की गद्दी छूट जाने से परेशान है और उसे वापिस वही रुतबा दिलाने के लिए तत्पर है तब आपको नायक की तमाम कोशिशें अच्छी लगने लगती हैं. वजह शायद एक और केवल एक है कि नायक इसका यौन शोषण करना चाहता है जबकि मुस्तफा केवल पैसों के लिए ऐसा करता है. यह इस सीरीज का ऐसा पहलू है जो समाज में गहरी पैठ यौन हिंसा के प्रति कई कसौटियों में हमें आंकता है और हमारे अनुकूलन को ठीक ढंग से प्रस्तुत करता है. जिसका सार यह है कि किसी भी प्रकार की यौन हिंसा को लेकर समाज में सामान्य स्वीकृति नहीं है.
यह सीरीज आधुनिक स्त्रियां, लड़कियों को लेकर भी जो सामान्य बोध बनाया गया है उसके बरक्स एक बेहद तार्किक हस्तक्षेप करती है. सनाया (मधुरिमा राव) का ड्रग एडिक्ट होना, सेक्सुअली एक्टिव होना या कैजुअल रिलेशनशिप बनाना उसके साथ हुई घटना को सही साबित करने की कोशिश नहीं करती बल्कि कहानी के अंत तक पहुंचते-पहुंचते यह कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता. रहस्य रोमांच के बाद सनाया के तमाम पक्ष उसकी ताकत के रूप में ही दिखाई देने लगते हैं.
ड्रग लेना, या कैजुअल होना किसी का नितांत निजी मसला हो सकता है. लेकिन अपने सामने हो रहे अन्याय को लेकर मुखर होना, परेशान होना और उससे लड़ने का माद्दा पैदा करना जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े, सनाया को इकीसवीं सदी की एक ताकतवर, तार्किक और चेतना सम्पन्न लड़की के रूप में चित्रित करता है. सनाया हमें ऐसे ही याद रह जाती है. यह कंट्रास्ट बेहद सलीके से पैदा किया गया है जो हमारे दिमाग में घर कर गए स्टीरियोटाइप को रचनात्मक ढंग से तोड़ता है. कमाल यह है कि अपने स्टीरियोटाइप को तोड़ना हमें बुरा नहीं लगता बल्कि यह इतना सहज और स्वाभाविक ढंग से हमारा नज़रिया बदल देता है कि अपने अंदर कुछ टूटने से ज़्यादा कुछ रचे जाने का एहसास पुख्ता होता है.
एम मध्यमवर्गीय मुंबईकर परिवार का बेहद प्रामाणिक चित्रण तो हुआ ही है पारिवारिक रिश्तों का महत्व भी ठोस ढंग से स्थापित हुआ है. विशेष रूप से आदित्य शर्मा की बहन अवनि के किरदार के साथ रुचा ईनामदार का अभिनय बहुत संजीदा और गंभीर रहा.
अभिनय के मामले में कोई किसी से उन्नीस -बीस नहीं है. यह तिग्मांशु धूलिया का निर्देश ही है कि सभी से उनका उत्कृष्ट हासिल कर सके. पंकज त्रिपाठी थोड़ा टाइप्ड हुए लगते हैं लेकिन दर्शक पंकज से उस बात की अपेक्षा नहीं करेंगे तो वो पर्दे पर पंकज को क्यों ही देखेंगे. केस को लीगली सोचने के बजाय हार्टली सोचने और देखने का सलीका रखने और उसके जोखिम लेने को तैयार जूनियर एडवोकेट निखत हुसैन (अनुप्रिया गोएनका) ने याद रखे जाने लायक अभिनय दिया है. अच्छा और संजीदा अभिनय किया है. रघु सालियान के तौर पर पंकज सारस्वत, एक बेहद संभावनाशील अभिनेता हैं जिन्हें आगे बहुत अच्छी भूमिकाएं करनी हैं.
विक्रांत मैसी उम्र से ज़्यादा परिपक्व अभिनेता हैं और अपने विक्रांत मैसी होने को चरित्र पर हावी नहीं देते. उनकी यही काबिलियत और मिजाज आज के दौर में उन्हें बाकियों से अलहदा करता है. पूरी सीरीज में आदित्य शर्मा ही लगे.
सीरीज को ज़रूर देखा जाना चाहिए. वक़्त की बर्बादी नहीं होगी क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ टूटेगा तो बहुत कुछ रचा भी जाएगा.
सौज- न्यूजलांड्री