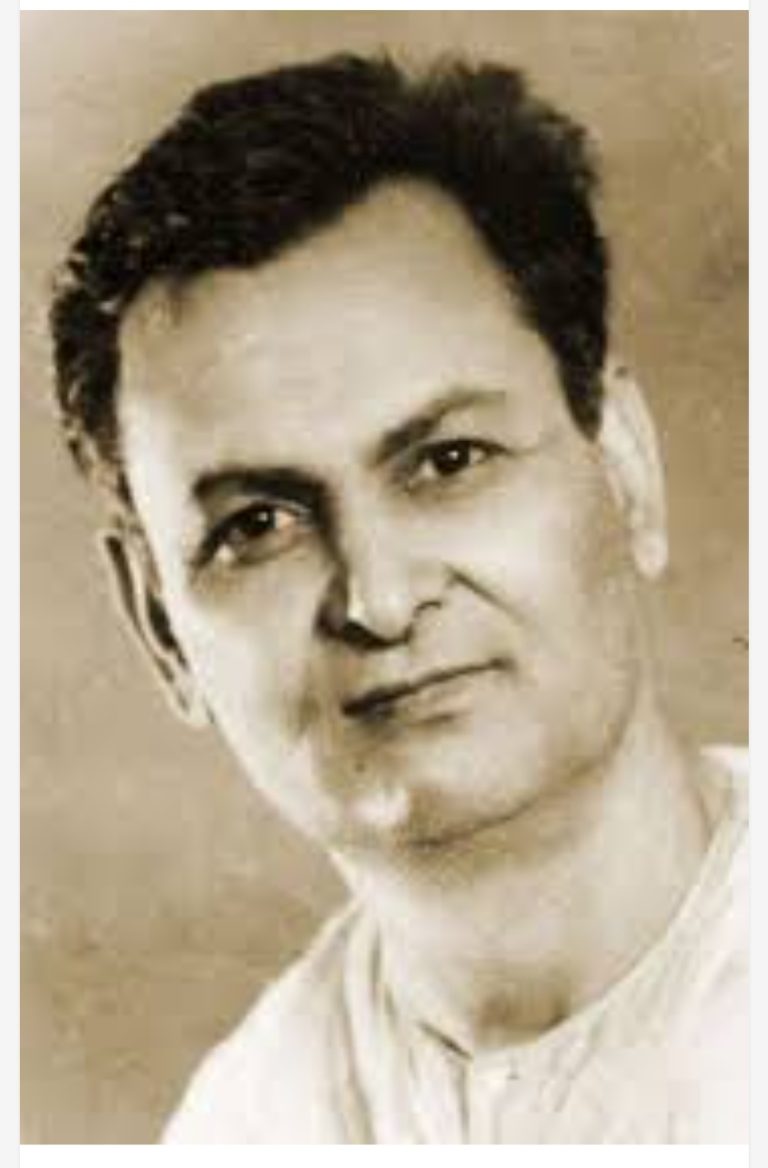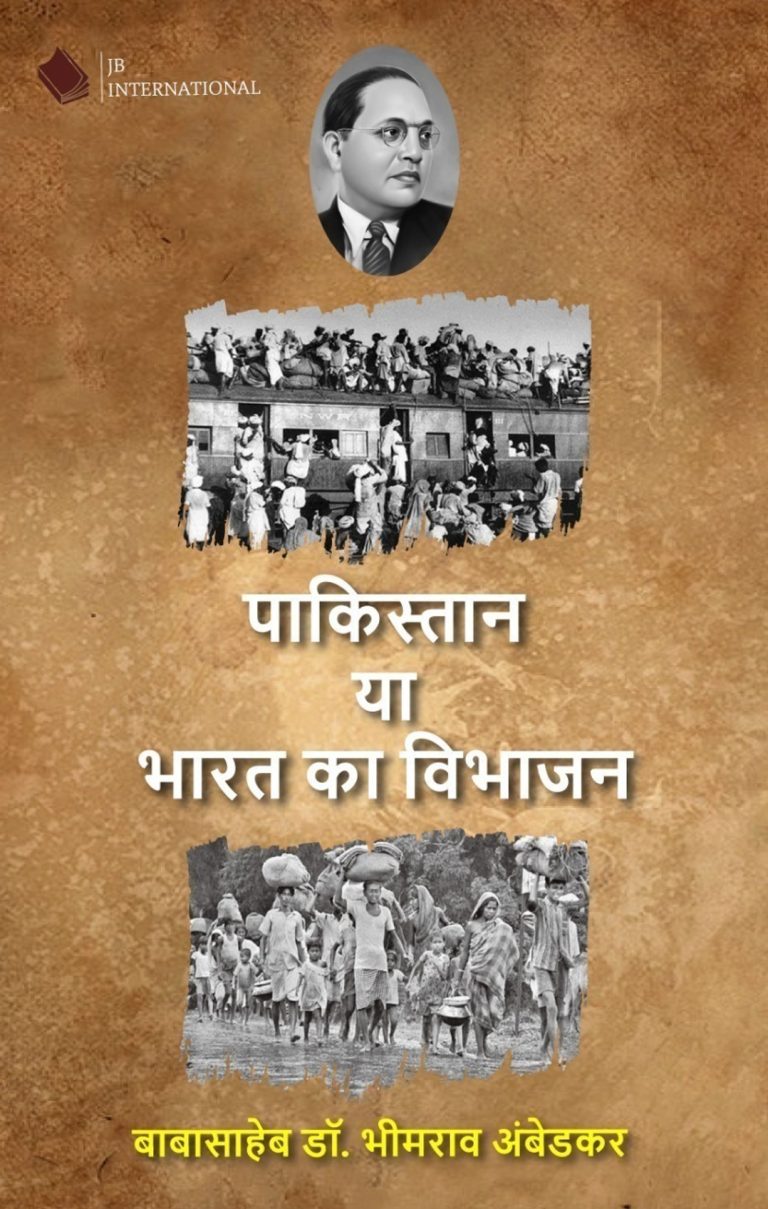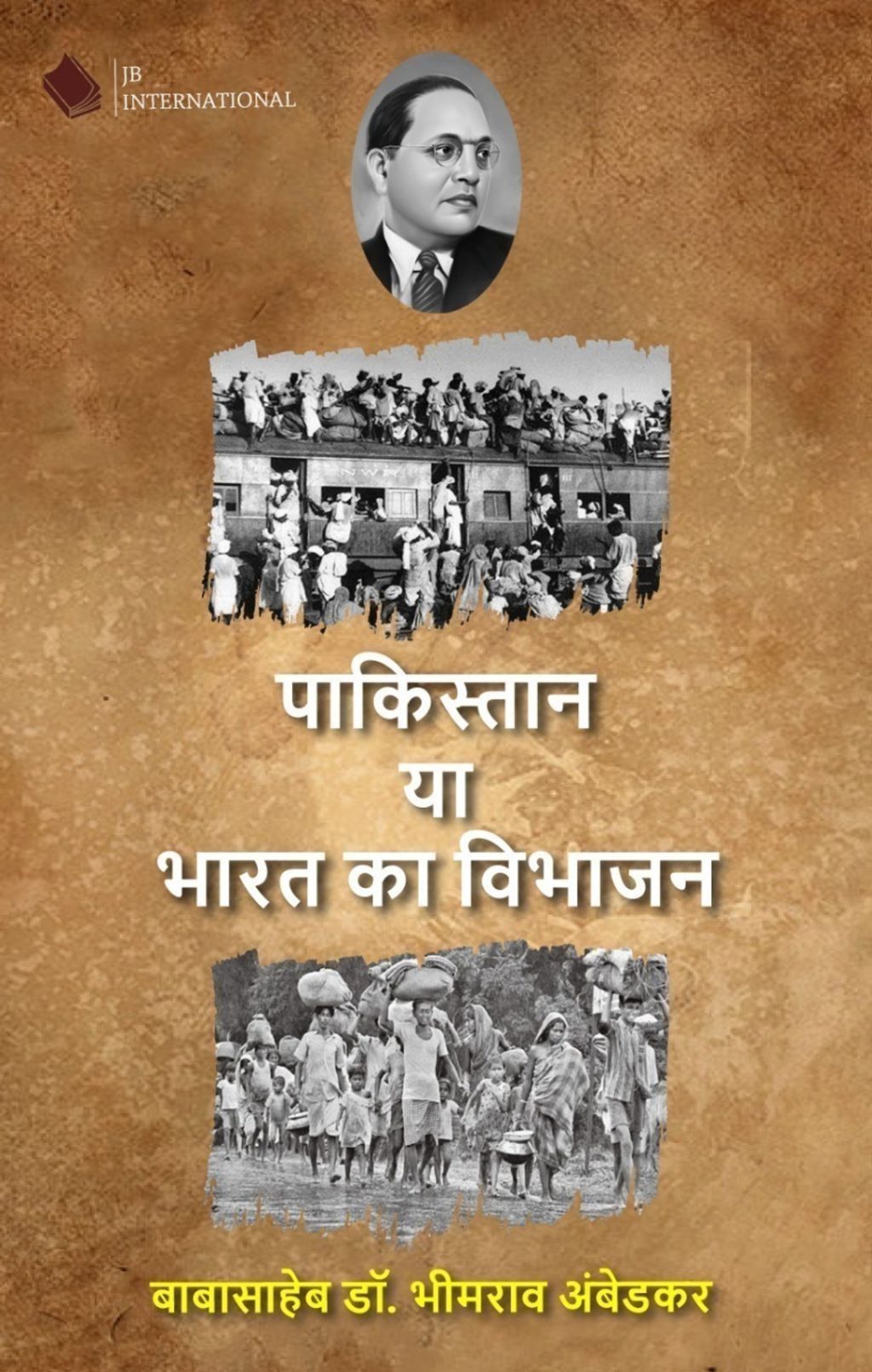
आंबेडकर के गंभीर अध्येता रामायन राम ने इस पुस्तक का सन्दर्भ सहित तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हुए यह विचारोत्तेजक आलेख तैयार किया है। यह लेख आंबेडकर द्वारा सावरकर की राजनीति के खुले विरोध को उद्घाटित करता है और दोनों को एक साथ लाने की सभी आशंकाओं का अंत कर देता है। इसे प्राथमिकता के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
‘भारत-विभाजन की माँग और उस के इर्द गिर्द की राजनीति पर अपनी पार्टी के नज़रिए को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर आंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। आंबेडकर के गंभीर अध्येता रामायन राम ने इस पुस्तक का सन्दर्भ सहित तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हुए यह विचारोत्तेजक आलेख तैयार किया है।
यह लेख आंबेडकर द्वारा सावरकर की राजनीति के खुले विरोध को उद्घाटित करता है और दोनों को एक साथ लाने की सभी आशंकाओं का अंत कर देता है। इसे प्राथमिकता के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
भारत–विभाजन की माँग और उस के इर्द गिर्द की राजनीति पर अपनी पार्टी के नज़रिए को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर आंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। आजकल इस पुस्तक के कुछ अंशों को सन्दर्भ से काटते हुए मनमाने ढँग से उद्धृत किया जाता है। ऐसा यह दिखाने के लिए किया जाता है कि डॉक्टर आंबेडकर भी उसी ढँग के मुस्लिम विरोधी थे, जिस ढँग के सावरकर थे! इस तरह यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि आंबेडकर और सावरकर की इतिहास दृष्टि और राष्ट्र दृष्टि एक जैसी थी! इस तरह आंबेडकर और सावरकर को साथ लाने यानी समतावादी आंबेडकर को हिंदुत्ववादी फ़ासीवाद की राजनीति में खपा लेने की ज़ुर्रत की जाती है।
इस लेख में पढ़ें
पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन : किताब की मूल अंतर्वस्तु
डॉ. आंबेडकर के मुसलमान सम्बन्धी विचारों का कुपाठ
आंबेडकर की इतिहास दृष्टि की समस्याएँ
आंबेडकर के मुस्लिम–राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारों का कुपाठ
भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को व्यवहार में लाने और औपनिवेशिक विभाजनकारी नीतियों का मुकम्मल जवाब देने की रणनीति विकसित करने का संघर्ष भी था। ब्रिटिश इतिहासकारों और अधिकारियों ने यह साबित करने में पूरा ज़ोर लगा दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग और विरोधी संस्कृतियाँ हैं जो एक राष्ट्र के भीतर संगठित होकर नहीं रह सकतीं। भले ही द्विराष्ट्र का सिद्धान्त सावरकर और जिन्ना लेकर आए हों लेकिन इस विचार को खाद पानी ब्रिटिश शासकों और उपनिवेशवादी इतिहासकारों द्वारा ही दिया जा रहा था। इसके प्रतिकार में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हिंदू–मुस्लिम एकता और इन दोनों धर्मों के बीच सांस्कृतिक एकता के अंत:सूत्रों को तलाश करने और उसे स्वराज का आधार बनाने पर काम किया। राजनीतिक मामले मे भी गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में जोड़े रखने के लिए बहुत आगे बढ़कर साहसिक फैसले भी लिए, लेकिन फिर भी आज़ादी की लड़ाई के दौरान न तो साम्प्रदायिक दंगों में कमी आयी और न ही इन दोनों धर्मों की नेताओं के बीच विश्वास पैदा हो सका। इस अविश्वास का परिणाम अंतत: भारत के विभाजन के रूप में हुआ।
एक निरपेक्ष विश्लेषक के रूप में डॉ. आंबेडकर ने भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या को दूर करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अपनायी जा रही रणनीति की आलोचना की थी। अपनी किताब ‘पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन’ में उन्होंने पाकिस्तान बनाए जाने की जरूरत का समर्थन और उसकी व्यावहारिकता को रेखांकित करते हुए भारत में साम्प्रदायिकता के इतिहास और तत्कालीन सन्दर्भों में उसके राजनीतिक घात प्रतिघात को उद्घाटित किया है। इस प्रक्रिया में आंबेडकर के दृष्टिकोण की तुलना कबीर से की जा सकती है जिसमें वे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों को कसौटी पर रखते हैं और साम्प्रदायिकता की समस्या को बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए दोनों पक्षों की आलोचना करते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में हिंदुत्व की वैचारिकी के लेखक–विचारक आंबेडकर द्वारा की गई मुसलमानों की आलोचनाओं और उनके ख़िलाफ़ आने वाले तर्कों को प्रचारित कर आंबेडकर को मुसलमानों का आलोचक सिद्ध करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदुत्व की राजनीति के समर्थकों द्वारा आंबेडकर कि किताब ‘पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन‘ से अपने अनुकूल उद्धरणों को व्यापक सन्दर्भ से काट कर प्रचारित किया जाता रहा है। जबकि जिस किताब के आधार पर आंबेडकर के खिलाफ़ दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार का जवाब उसी किताब में मौजूद है।
पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन : किताब की मूल अंतर्वस्तु
सन् 1939 व 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने परिषद् और कार्यकारिणी समिति की कई राउंड होने वाली बैठकों की जरिए पाकिस्तान की माँग को ठोस आधार दिया और भारत के उत्तर–पश्चिम और बंगाल–आसाम के मुस्लिम बहुल इलाक़ों को लेकर एक संवैधानिक रूप से स्वायत्त और प्रभुतासंपन्न इकाई का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया। ठोस शब्दों में यह भारत से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के माँग की आधारशिला थी। इस माँग के बाद भारत में इस विषय पर बहस तेज़ हो गई। इंडियन लेबर पार्टी की तरफ़ से डॉ. आंबेडकर ने 1940 में इस मुद्दे पर किताब लिख कर पार्टी का मत इस विषय पर स्पष्ट किया। इस किताब का पहला संस्करण जो दिसंबर 1940 में प्रकाशित हुआ था, का नाम डॉ. आंबेडकर ने ‘Thoughts on Pakistan’ रखा था। बदली हुई परिस्थितियों में पाकिस्तान का स्वरूप स्पष्ट होने और उस पर बदलती राजनीति और विकसित होती सोच के आधार पर इस किताब का दूसरा संस्करण सन् 1945 में आया जिसका नाम बदलकर ‘Pakistan Or Partition Of India’ (पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन) रखा गया।
पहले संस्करण में इस किताब में तीन भाग थे। पहला, ‘पाकिस्तान के लिए मुस्लिम पक्ष‘ ; दूसरा, ‘पाकिस्तान के खिलाफ़ हिंदू पक्ष‘ और तीसरा, ‘पाकिस्तान नहीं तो क्या?’ इन तीन भागों में प्रत्येक में तीन–तीन अध्यायों में डॉ. आंबेडकर ने पाकिस्तान के रूप में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के पक्ष में दलीलें दी हैं। पाकिस्तान का विरोध कर रहे कांग्रेस और अन्य हिंदू पक्ष की ओर से आने वाले हर तर्क का उन्होंने खंडन किया और भारत में राष्ट्र और संविधान के स्थायित्व के लिए पाकिस्तान के अलग हो जाने को उचित ठहराया।
इस किताब के दूसरे संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा कि पहले संस्करण को लेकर यह आलोचना हुई थी कि किताब में पाकिस्तान की समस्या के बारे में लिखते हुए पाकिस्तान को लेकर लेखक का दृष्टिकोण इसमें सामने नहीं आया है, इसीलिए डॉ. आंबेडकर ने 1945 में इस किताब के दूसरे संस्करण में दो और भाग जोड़े। चौथे भाग, ‘पाकिस्तान और व्याधियाँ’ (Pakistan And The Malaise) के अंतर्गत तीन अध्याय और पांचवें भाग में तीन अध्याय—’क्या पाकिस्तान बनना ही चाहिए‘, ‘पाकिस्तान की समस्याएँ‘ और ‘कौन निर्णय कर सकता है?’ हैं। इन दो भागों के जुड़ने से किताब पहले संस्करण की तुलना में संतुलित और मुकम्मल हो गई, क्योंकि 1945 तक पाकिस्तान के सन्दर्भ में राजनीतिक परिस्थितियाँ और अधिक परिपक्व हो चुकीं थीं। मुस्लिम लीग की माँगें और इस पर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक धड़ों का पक्ष अधिक स्पष्ट और ठोस रूप में सामने आ चुका था। इन दो भागों में अभिव्यक्त आंबेडकर के दृष्टिकोण को इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।
यह समझना जरूरी है कि डॉ. आंबेडकर इस किताब में कहना क्या चाहते हैं? आंबेडकर मुसलमानों द्वारा की जा रही पाकिस्तान की माँग की गंभीरता और औचित्य को समझ रहे थे। दूसरी तरफ़ हिंदू पक्ष के लोग (यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि आंबेडकर जिसे हिंदू पक्ष कह रहे हैं उसका नेतृत्व उस समय कांग्रेस के पास था और मुस्लिम पक्ष का राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः मुस्लिम लीग के पास था। आज की परिस्थिति में हिंदू पहचान का राजनीतिक नेतृत्व जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है, वह उस समय परिदृश्य में नहीं था, वह एक हाशिए की शक्ति थी। हिंदू महासभा के पास जरूर उल्लेखनीय ताक़त थी लेकिन वह भी बहुसंख्यक हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, यह नेतृत्व गांधी का प्राधिकार था।) पाकिस्तान की माँग को जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा दबाव की राजनीति के रूप में देख रहे थे, इसलिए वे पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और यह तर्क दे रहे थे कि इस माँग से भारतीयों की एकता खंडित होगी और एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संगठित होने का दावा कमजोर साबित होगा। इसके विपरीत आंबेडकर यह मानते थे कि पाकिस्तान की माँग के मुखर होने के बाद अगर मुस्लिमों को दबाव डालकर या समझौते के साथ भारतीय राष्ट्र में रहने के लिए मजबूर किया गया तो यह कहीं से भी सही कदम नहीं होगा बल्कि यह राष्ट्र के भविष्य के लिए ख़तरा ही होगा।
डॉ. आंबेडकर भारतीय राष्ट्र के लिए अखंड भारत की किसी वायवीय, व्यावहारिक योजना की बजाय ठोस ज़मीनी हक़ीक़त और तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से एक हल सुझा रहे थे, जिसमें साम्प्रदायिकता की समस्या को राजनीतिक समझौतों, एकता के संकल्पों के ज़रिए सुलझाने की बजाय स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षात्मक उपायों की बात कर रहे थे। पाकिस्तान की माँग को आंबेडकर ने ‘एक राष्ट्र का अपने घर के लिए आह्वान’ (A Nation calling for a Home) कहा। पाकिस्तान की माँग को वे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के आत्मनिर्णय के अधिकार के रूप में देखते है। किताब की भूमिका में वे लिखते है—“मुसलमानों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हिंदू राष्ट्रवादी जो आत्मनिर्णय पर भरोसा करते हैं और यह पूछते हैं कि जब विश्व को छोटे–छोटे राष्ट्रों के मामले में यह बात माननी पड़ी, तो ब्रिटेन भारत को उससे वंचित कैसे रख सकता है। इस तरह वे ब्रिटेन से यह नहीं कह सकते कि वह अल्पसंख्यकों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने से मना कर दे। हिंदू राष्ट्रवादी जो यह आशा करते हैं कि ब्रिटेन मुसलमानों पर पाकिस्तान की माँग त्यागने का दबाव डाले, वे यह भूल जाते हैं कि विदेशी आक्रामक साम्राज्यवाद से राष्ट्रीयता की आज़ादी का अधिकार और बहुसंख्यक आक्रामक राष्ट्रीयता से अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। दोनों का एक ही आधार है। वे तो स्वतंत्रता के संघर्ष के दो पहलू हैं और उनका नैतिक आधार भी बराबर है।”1
आंबेडकर स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं कि पाकिस्तान की माँग औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम जनता के राजनीतिक विकास के साथ प्रबल हुई है और इसे ‘रूपक अलंकारों से भरी बातों’ के बल पर मिटाया नहीं जा सकता, इस मामले में वे सभी पहलुओं का अध्ययन करके और उसकी परिणतियों को समझ कर कोई बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेने के पक्षधर थे। अपनी किताब में वे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तर्कों के सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से परीक्षण करते हैं।
किताब के पहले भाग में आंबेडकर ने मुस्लिम लीग द्वारा भारत के उत्तर–पश्चिम और पूर्वी मुस्लिम बहुल प्रांतों को लेकर एक स्वतंत्र राज्य के गठन की माँग को सामने रखते हुए, मुसलमानों के एक अलग राष्ट्र की माँग को उचित ठहराया और हिंदू पक्ष के इस दावे को खारिज किया है कि हिंदू और मुसलमान लम्बे समय से साथ रह रहे हैं और इसलिए उनके बीच एक सांस्कृतिक समरूपता पैदा हो चुकी है, भले ही मुसलमानों में एक राष्ट्र होने का एहसास जाग चुका है लेकिन सिर्फ़ इस आधार पर उन्हें पृथक राष्ट्र बना कर देना उचित नहीं है।
आंबेडकर ने कहा कि गांधी जी ने भाषायी आधार पर राज्य गठन का सिद्धान्त सामने रखा है और इसी आधार पर प्रांतों का गठन हो रहा है तब मुसलमानों द्वारा धार्मिक आधार पर राज्य गठन का विरोध वे कैसे कर सकते हैं जबकि भाषा और धर्म दोनों ही सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। इस सम्बंध में आंबेडकर हिंदू पक्ष का तर्क रखते हुए लिखते हैं—”राष्ट्रवाद से अनुप्राणित हुए बिना भी राष्ट्रों जैसी चेतना विद्यमान हो सकती है। इसी दलील के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि मुसलमान यह सोच तो सकते हैं कि वे एक राष्ट्र हैं, परन्तु उन्हें उसी कारण एक पृथक राष्ट्रीय अस्तित्व की माँग उठाने की जरूरत नहीं है, वे वैसी ही स्थिति से क्यों संतुष्ट नहीं हो सकते जो कनाडा में फ्रांसीसियों और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को प्राप्त है।” 2
यहाँ वे यह साफ़ कर देते हैं कि यह समाधान तब कारगर है जब मुसलमान विभाजन के लिए अड़ न जायें। यदि वे विभाजन पर ज़ोर देते हैं तो इस तर्क के आधार पर उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। हिंदू पक्ष के इस तर्क का जवाब देते हुए आंबेडकर लिखते हैं—”राष्ट्रीयता से राष्ट्रवाद उजागर होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। प्रथम, एक राष्ट्र के रूप में रहने की इच्छा का जाग्रत होना; दूसरी, एक क्षेत्र का होना जिसे राष्ट्रवाद अधिग्रहित कर एक राज्य या तथा राष्ट्र का सांस्कृतिक घर बना सके।…मुसलमानों ने एक राष्ट्र के रूप में रहने की इच्छा व्यक्त की है। उनके लिए प्रकृति ने एक ऐसा क्षेत्र तलाश लिया जिसे अधिगृहीत कर वे नवजात मुस्लिम राष्ट्र का सांस्कृतिक गृह और राज्य बना सकते हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों में यदि मुसलमान यह कहते हैं कि वे ऐसी स्थिति अपनाने में संतुष्ट नहीं हैं जिसे कनाडा में फ्रांसीसियों ने अपनाया है अथवा दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने अपनाया है और वे अपना एक राष्ट्रीय गृह चाहते हैं जिसे वे स्वयं का अपना कह सकें, तो उनके ऐसा कहने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए।” 3
इसके अंतर्गत आंबेडकर ने मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के रवैये का उल्लेख किया है। मुस्लिम लीग का दावा था कि संवैधानिक संरक्षण मुसलमानों को हिंदू बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचाने में में असफल रहे हैं और कांग्रेसी शासन के दौरान मुसलमानों का दमन हुआ है। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने से इनकार करना और कांग्रेस शासित प्रांतों में मिले–जुले (कांग्रेस और लीग के) मंत्रिमंडलों का गठन करने से इनकार ऐसी घटनाएँ थीं जिन्होंने मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया था।
आंबेडकर ने लिखा है कि मुसलमानों में यह भावना घर कर गई है कि भारत पर ब्रिटिश अधिकार के साथ ही भारत में उनका पराभव शुरू हो गया। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए प्रत्येक व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक और कानूनी परिवर्तनों ने मुसलमानों को एक शासक कौम से अधीनस्थ की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। मुस्लिम फ़ौजदारी कानून की जगह ब्रिटिश दंड संहिता का लागू होना, शरीयत और मुस्लिम नागरिक कानून का क्षेत्राधिकार घटा कर केवल विवाह और उत्तराधिकार तक सीमित कर देना, अदालतों से फ़ारसी को हटा कर अंग्रेजी और देशी भाषाओं को लागू किया जाना इत्यादि अनेक ऐसे परिवर्तन थे जिसे मुस्लिम नेता अपना अध:पतन मानते थे।
आंबेडकर कहते हैं कि 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने मुसलमान उच्च वर्गों को ख़ास तौर पर दंडित करने का अभियान चलाया। उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, इससे मुसलमान जनता चाहे वह उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के हों उनके गौरव को गहरा आघात लगा। आंबेडकर के शब्दों में—”उनमें निराशा बढ़ी और निर्धनता ही उनका प्रारब्ध बन गई। प्रतिष्ठा, शिक्षा और संसाधनों से वंचित मुसलमानों को हिंदुओं का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया।” 4
अंग्रेजों के जाने के बाद या डोमिनियन राज्य के दर्जे वाले भावी भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की प्रजा बनकर रहना मुसलमानों को स्वीकार नहीं हुआ, इस आधार पर आंबेडकर ने कहा कि मुसलमानों द्वारा विषम स्थिति से बचने के लिए और अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए पृथक राष्ट्र की माँग करना अस्वाभाविक नहीं है।
दूसरे भाग में डॉ. आंबेडकर ने पाकिस्तान बनने के विरोध में हिंदू पक्ष यानी कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी लोगों के तर्कों को सामने रखते हुए उनका खंडन किया है। हिंदू पक्ष के लोग पाकिस्तान की योजना पर तीन आधारों पर आपत्ति व्यक्त कर रहे थे—पहला, इससे भारत की एकता खंडित होगी; दूसरा, इससे भारत की प्राकृतिक सीमा असुरक्षित होगी और तीसरा, पाकिस्तान बनाने के बावजूद साम्प्रदायिक समस्या का समाधान नहीं होगा। आंबेडकर ने उपरोक्त सभी आपत्तियों को अपने विश्लेषण से निराधार साबित करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने जो बातें लिखीं उनको लेकर संदर्भ से काटकर एकतरफ़ा ढंग से उद्धृत कर आज के हिंदूवादी विचारक आंबेडकर को इस्लाम और मुस्लिम विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। इस विषय पर हम इस लेख में आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ डॉ. आंबेडकर ने इस सम्बंध में जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं।
डॉ. आंबेडकर कहते हैं कि जिसे हिंदू–मुस्लिम एकता पर आधारित अखंड भारत कहा जाता है क्या वह वास्तव में है भी? मुस्लिम आक्रमण और इस्लाम के आगमन के बाद पश्चिम–उत्तर भारत में जिस धार्मिक – सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ उसमें कई शताब्दियों में वह एकता कायम नहीं रह सकी। वे लिखते हैं कि मुस्लिमों के आगमन से पूर्व पश्चिम–उत्तर क्षेत्र वृहत्तर भारत का अंग था। ह्वेनसांग के विवरणों से यह स्पष्ट है न सिर्फ़ पंजाब, अपितु आज का अफ़गानिस्तान भी भारत का भाग था और उसके अलावा पंजाब और अफ़गानिस्तान के निवासी वैदिक अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ह्वेनसांग 630 ई. में भारत आया था और सन् 711 ई. में भारत पर मुहम्मद बिन क़ासिम ने पहली बार हमला किया। फिर एक के बाद एक अरबों, तुर्कों और अफ़गानों ने भारत पर आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में में पानीपत के युद्ध में मराठों को पराजित कर हिंदू पुनरुत्थान की कोशिशों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस अध्याय में आंबेडकर ने 711 ई. से लेकर 1761 ई. तक मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों, धर्मांतरण और मंदिरों को तोड़ने की परिघटनाओं का ज़िक्र किया है। अपने समय में उपलब्ध ब्रिटिश इतिहासकारों की सामग्री और इतिहास दृष्टि का इस्तेमाल यह दिखाने में किया कि मुहम्मद गजनवी के आने और अहमद शाह अब्दाली के वापसी के बीच 762 वर्षों तक अनवरत मुस्लिम आक्रमणों ने पश्चिमोत्तर भारत से सांस्कृतिक–धार्मिक रूप से अलग और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना दिया। आंबेडकर के शब्दों में—”हिंदुओं को कहाँ तक यह कहने का हक़ है कि उत्तरी भारत आर्यावर्त का भाग है? हिंदुओं को यह कहने का कितना अधिकार है कि चूँकि एक बार यह क्षेत्र उनका था, अतएव हमेशा ही भारत का अविभाज्य अंग रहना चाहिए? जो लोग पृथकता का विरोध करते हैं और अफ़गानिस्तान सहित उत्तरी भारत जो कभी भारत का अंग था और उस क्षेत्र के लोग बौद्ध अथवा हिंदू थे, इस प्राचीन तथ्य से उद्भूत ‘ऐतिहासिक भावना‘ पर बल देते हैं, उनसे पूछा ही जाना चाहिए कि क्या 762 वर्षों से अनवरत मुस्लिम आक्रमणों की घटनाओं को, जिस उद्देश्य से वे किए गए थे और अपने मक़सद को पूरा करने के लिए इन आक्रांताओं ने जो हथकंडे अपनाए थे, क्या उन्हें महत्वहीन मान लिया जाय?
इन आक्रमणों की जो अन्य परिणतियाँ हुईं, उनके अलावा भी मेरी राय में उन उत्तरी क्षेत्रों की संस्कृति और स्वरूप में बहुत ठोस बदलाव आया है जिसे अब पाकिस्तान में शामिल करना प्रस्तावित है। स्थिति यह है कि इस क्षेत्र और शेष भारत के बीच एकता तो है ही नहीं, अपितु दोनों के बीच वास्तविक विद्वेष एक तथ्य बन गया है। …आक्रांताओं ने जो हथकंडे अपनाए थे, वे भविष्य में आने वाले परिणाम छोड़ते गए। उनमें से ही एक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कटुता है, जो उन उपायों की देन है। दोनों के बीच यह कटुता इतनी गहरायी से पैठी हुई है कि एक शताब्दी का राजनीतिक जीवन इसे न तो शांत कर पाने में सफल हुआ है और न ही लोग उस कटुता को भुला पाए हैं।” 5
इस आधार पर आंबेडकर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि शेष भारत और पाकिस्तान के रूप में लीग द्वारा प्रस्तावित उत्तर–पश्चिम के प्रांतों के बीच यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कथित एकता का कोई सूत्र मौजूद ही नहीं है, इसलिए हिंदू पक्ष का यह तर्क कि पाकिस्तान बनाए जाने से भारत की एकता में विघटन होगा, बेमानी है।
इसी तरह पाकिस्तान की वजह से रक्षा व्यवस्था में कमजोरी के नाम पर आंबेडकर ने यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान के बनने से भारत के लिए कोई ‘वैज्ञानिक सीमा‘ नहीं रह जाएगी। आंबेडकर ने कहा कि भारत की ऐतिहासिक रूप से कोई वैज्ञानिक सीमा रही ही नहीं है। सरल शब्दों में समझें तो अंग्रेज़ों ने भारत की सीमा निश्चित करने में दो प्रकार की नीतियों पर विचार किया था, जिसमें पहली नीति अग्रगामी नीति के रूप में जानी जाती है जिसमें अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण कर आमू दरिया तक यानी अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा तक विस्तार किया जाय, या फिर अफ़गानिस्तान और सिंध के बीच की क़बायली पहाड़ियों को सीमा के रूप में प्रयोग किया जाय। दूसरी नीति ‘बैक टू सिंध‘ नीति कही जाती है, जिसमें सिंध नदी ही वास्तविक भौगोलिक सीमा मानी जाय। वैज्ञानिक सीमा की मूल बात है नदी, पहाड़ ,समुद्र या रेगिस्तान जैसी कोई प्राकृतिक सीमा हो जो सैन्य लिहाज़ से सुरक्षित होती है।
आंबेडकर ने कहा कि हिंदू यह तर्क दे सकते हैं कि पाकिस्तान बनाने से सिंध से बनने वाली वैज्ञानिक सीमा ख़त्म हो जाएगी। आंबेडकर ने इसको निराधार बताते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के सामने पुरातन प्राकृतिक सीमाओं का महत्व काफ़ी कम हो चुका है, जिन देशों में प्राकृतिक सीमाएँ नहीं होतीं वे इस कमी को कृत्रिम तरीके से पूरा करते हैं, जो प्राकृतिक बाधाओं से भी मजबूत होती हैं। आंबेडकर कहते हैं कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि हिंदू वह कार्य नहीं कर पाएँगे जो अन्य देशों ने किया है। इस तरह उन्होंने सीमाओं पर कमजोरी के तर्क को भी निर्माण सिद्ध करने की कोशिश की।
पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले प्रांतों से राजस्व और सेना में इन क्षेत्रों से आने वाले ‘मैन पावर‘ में कमी की दलील को भी आंबेडकर ने स्वीकार नहीं किया। आर्थिक संसाधनों के बँटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के संसाधन पाकिस्तान के संसाधनों के मुकाबले अधिक ही ठहरेंगे। चाहे क्षेत्रफल हो, राजस्व हो या जनसंख्या, इसलिए पाकिस्तान के अलग होने से हिंदुस्तान कमजोर स्थिति में नहीं आएगा। सशस्त्र सेनाओं की कमजोरी के प्रश्न पर आंबेडकर ने कहा कि 1879 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित स्पेशल आर्मी कमेटी ने मार्शल–नॉन मार्शल का भेद करके पंजाबी, सिख, जाट, पठान, गढ़वाली जैसे समुदायों को सेना में प्रमुखता देना शुरू किया क्योंकि इन्होंने 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए भारतीय फ़ौजों में पश्चिम–उत्तर प्रान्त के लोगों का बाहुल्य हो गया। आँकड़ों के ज़रिये उन्होंने एक अनुमान लगाया कि इनमें 50 से 60 प्रतिशत सैनिक मुसलमान थे, आंबेडकर यह तर्क देते हैं कि मुस्लिम लीग की माँगों के प्रबल होने के बाद इन मुस्लिम सैनिकों पर भारत की सीमाओं ख़ासकर अफ़गानिस्तान और क़बायली आक्रमणकारियों से महफूज़ रखने को लेकर भरोसा करना उचित होगा? इसलिए बेहतर यह होगा कि मार्शल–नॉन मार्शल के भेद को ख़त्म कर बाकी भारत से अन्य समुदायों से सैनिक भर्ती किए जाएँ। इस तरह रक्षा व्यवस्था में आने वाली कमजोरी की आशंका को खत्म किया जा सकता है।
क्या पाकिस्तान बनने से साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित हो जाएगी? इस प्रश्न के उत्तर में आंबेडकर ने यह बताया कि साम्प्रदायिकता की समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक एक एक शत्रुतापूर्ण बहुमत का सामना एक शत्रुतापूर्ण अल्पमत करता रहेगा। इसलिए मुस्लिम बहुल प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार और हिंदू बहुल प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की ‘धमाके के जवाब में धमाका‘ वाली नीति को समाप्त करना अनिवार्य है। इसलिए आंबेडकर ने पाकिस्तान के लिए ऐसे प्रांतों का गठन करने की बात कही जिसमें पंजाब, बंगाल और आसाम के प्रांतों का सीमांकन इस तरह किया जाय कि हिंदू बहुसंख्या वाले क्षेत्रों को अलग कर दिया जाय और मुस्लिम बहुसंख्या वाले सजातीय देश का निर्माण किया जा सके। उन्होंने यहाँ तक कि साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यकों की अदला–बदली का विकल्प भी सुझाया।
तीसरे भाग में आंबेडकर ने पाकिस्तान के विकल्पों के बारे में चर्चा की है जिसमें उन्होंने तीन अध्यायों के अंतर्गत पाकिस्तान का हिंदुओं द्वारा प्रस्तुत विकल्प, पाकिस्तान की माँग न माँगे जाने पर मुस्लिम पक्ष द्वारा लाए जाने वाले संभावित विकल्प और इस मामले में विदेशों से ली जा सकने वाली सीख के बारे में विश्लेषण किया है। पाकिस्तान का हिंदू विकल्प के अंतर्गत आंबेडकर ने मुख्यत: हिंदू महासभा के नेता सावरकर और महात्मा गांधी के विचारों और कार्य नीतियों की समीक्षा की। सावरकर की योजनाओं और मुस्लिम अल्पसंख्यक संबंधी उनकी भावी नीतियों के बारे में उन्होंने कहा कि यद्यपि सावरकर यह मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं इसके बावजूद वे चाहते हैं कि वे दोनों एक ही संविधान के तहत एक ही देश में रहें लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं के अधीनस्थ स्थिति में रहना स्वीकार करना होगा। सावरकर मुस्लिमों को ’एक वोट एक मूल्य’ का अधिकार देना चाहते हैं लेकिन लेकिन यह भी कहते हैं कि उन्हें नौकरियों और विधानमंडलों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मुस्लिम अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा अधिकारों की माँग नहीं कर सकते। आंबेडकर लिखते हैं—”यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर श्री सावरकर और श्री जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं : एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए।” 6
आंबेडकर कहते हैं कि सावरकर और हिंदू महासभा की योजना यदि विचित्र नहीं तो तर्कसंगत भी नहीं है। द्वि–राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता देने के बाद यदि वे हिंदुओं के लिए एक क़ौमी वतन का दावा करते हैं तो मुस्लिम राष्ट्र के क़ौमी वतन के दावे का विरोध वे कैसे कर सकते हैं? सावरकर पाकिस्तान बनने के विरोध में थे, पर साथ ही वह मुसलमानों को भारत में हिंदुओं के अधीनस्थ क़ौम के रूप में रखना चाहते थे। उनका कहना था कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है चाहे वह उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, परन्तु जिन धर्मों की पुण्य भूमि भारत से बाहर है उन्हें हिंदुओं अर्थात् जिनकी पितृ भूमि और पुण्य भूमि दोनो ही भारत में है, के अधीन रहना होगा।’ पितृ भूमि–पुण्य भूमि’ के आधार पर की गई हिंदू धर्म की इस व्याख्या को आंबेडकर ने चालाकी से बनायी गई परिभाषा कहा और लिखा कि इससे सावरकर के दो उद्देश्य पूरे होते हैं—पहला, इस परिभाषा के जरिए उन्होंने मुस्लिमों, ईसाईयों, यहूदियों और पारसियों को हिंदुओं से अलग कर दिया और दूसरे बौद्धों, जैनियों और सिखों आदि को हिंदू धारा में शामिल होने के लिए वेदों की पवित्रता पर आस्था रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इस तरह हिंदू पहचान को विस्तृत कर हिंदू राजनीति का बड़ा दायरा बनाने की कोशिश की।
सावरकर और हिंदू महासभा के प्रस्तावों की चर्चा के बाद इस अध्याय में आंबेडकर ने गांधी द्वारा हिंदू–मुस्लिम एकता के लिए की जाने वाली कोशिशों की समीक्षा की। उन्होंने ख़िलाफत आन्दोलन से शुरू करके भारत छोड़ो आन्दोलन तक लगभग तेईस–चौबीस साल तक गांधी जी द्वारा साम्प्रदायिक एकता की कोशिशों का जायजा लिया। ख़िलाफत का समर्थन करने की गांधी जी की रणनीति पर उन्होंने लिखा—“ख़िलाफत आन्दोलन का मुद्दा उठाकर श्री गांधी ने दो उद्देश्यों की पूर्ति की। एक तो मुस्लिमों का समर्थन पाने की कांग्रेसी योजना को उन्होंने पूरा कर दिखाया। दूसरे, उन्होंने कांग्रेस को देश में एक शक्ति बना दिया, क्योंकि यदि मुस्लिम कांग्रेस में शामिल न होते तो वह शक्ति नहीं बन सकती थी। मुसलमानों को राजनीतिक सुरक्षाओं की जगह ख़िलाफत का मुद्दा कहीं अधिक आकर्षक लगता था। इसका नतीजा यह निकला कि जो मुसलमान कांग्रेस के बाहर थे, वे भी भारी संख्या में कांग्रेस में शामिल हो गए। हिंदुओं ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह वे अंग्रेजों के विरुद्ध साझा मोर्चा खोल सकते हैं जो कि उनका उद्देश्य था। इसका श्रेय तो निश्चित रूप से श्री गांधी को जाता है। निस्संदेह यह एक बड़ा साहसपूर्ण काम था।” 7 लेकिन आंबेडकर ने गांधी की कोशिशों को बेनतीजा और व्यर्थ बताया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हर साल वार्षिक रिपोर्ट पेश करती थी, उन रिपोर्टों के हवाले से आंबेडकर ने बहुत विस्तार से 1920 से 1940 तक बीस वर्षों में पूरे भारत में हुए हिंदू–मुस्लिम दंगों का सिलसिलेवार उल्लेख यह सिद्ध करने के लिए किया कि इस दौरान हिंदू–मुस्लिम एकता के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ साबित हुए हैं, बावजूद इसके कि इस एकता को स्थापित करने के लिए गांधी ने कड़ी मेहनत की थी। इन बीस वर्षों के साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख करते हुए आंबेडकर ने कहा कि यह हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बीस सालों तक चलने वाले गृहयुद्ध का रिकॉर्ड है, जिसमें सशस्त्र शान्ति के छोटे–छोटे अंतराल गुज़रे हैं। वे कहते हैं कि हिंदुस्तानियों में एकता की भावना विकसित नहीं हो पायी है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में एकीकरण और सामाजिक एकता को लेकर कोई इच्छा नहीं है।
पाकिस्तान के मुस्लिम विकल्प के रूप में उन्होंने आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावों और हैदराबाद के निजाम द्वारा पेश किए संवैधानिक सुधारों के प्रावधानों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये विकल्प पाकिस्तान की माँग के बराबर ही हैं। भले ही आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग की विरोधी है लेकिन साथ की राष्ट्रवादी मुसलमानों से भी उनका विरोध है इसलिए उनकी माँगें भी पाकिस्तान से कम नहीं हैं। विदेशों से सीख के अंतर्गत आंबेडकर ने 1789 लेकर 1906 तक तुर्की साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी और चेकोस्लोवाकिया के विघटन के उदाहरणों के ज़रिए यह दलील दी कि एक भौगोलिक सीमा में अनेक राष्ट्रों को आश्रय देने और उन्हें समझौते या बलपूर्वक एक साथ रहने पर मजबूर करने का परिणाम विघटन और बिखराव ही होता है।
चौथे भाग ‘पाकिस्तान और व्याधियाँ’ में तीन अध्याय—सामाजिक निष्क्रियता, साम्प्रदायिक आक्रामकता और राष्ट्रीय कुंठा हैं। इनके अंतर्गत मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्याप्त सामाजिक बुराइयों और समाज सुधार के प्रति उपेक्षा, एक–दूसरे के ख़िलाफ़ साम्प्रदायिक आक्रामकता और मुसलमान नेताओं द्वारा अल्पसंख्यक होने के नाते अपनी विशेष स्थिति का फायदा उठाकर अनेक अनुचित और नाजायज माँगों को मनवाने का दबाव डालने की रणनीति की आलोचना डॉ. आंबेडकर द्वारा की गई है। आज़ाद भारतीय राष्ट्र में एक संविधान के नीचे रहने को लेकर दोनों ही क़ौमों की अनिच्छा को रेखांकित करते हुए आंबेडकर ने इन सारी समस्याओं का समाधान अलग पाकिस्तान के रूप में देखा। उन्होंने लिखा कि जितनी सामाजिक बुराइयाँ हिंदुओं में हैं, मुसलमानों में उससे कम बुराइयाँ नहीं है। उन्होंने बाल विवाह, जाति–प्रथा, महिलाओं की पराधीनता, पर्दा प्रथा आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि मुसलमानों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक गतिहीनता है। वे कहते हैं कि हिंदुओं में बहुत लोग हैं जो इन सामाजिक बुराइयों को लेकर सजग हैं और समाज सुधार आन्दोलन भी चल रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों में समाज सुधार का कोई संगठित आन्दोलन नहीं उभरा। निदान स्वरूप आंबेडकर लिखते हैं कि एक संविधान के नीचे एक राष्ट्रीय संघ में रहते हुए जब तक एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को ख़तरा मानता रहेगा, तब तक कोई सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। जब अपने ऊपर दूसरे के आधिपत्य हो जाने की आशंका से दोनों को मुक्ति मिल जाएगी तभी वे अपने भीतर की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
इस अध्याय के अंतर्गत मुस्लिम नेताओं की ओर से की जाने वाली राजनीतिक माँगों की भी समीक्षा की गई है। इसमें उन्होंने मुस्लिम नेतृत्व, ख़ास तौर से जिन्ना द्वारा की जाने वाली सौदेबाजी, जो एक तरफ़ ब्रिटिश सरकार के समर्थन के बदले फ़ायदे हासिल करने और दूसरी तरफ़ कांग्रेस पर दबाव डाल कर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकार हासिल करने की सौदेबाजी होती थी, की आलोचना की। इस सम्बंध में उन्होंने 1889 के इण्डियन कौंसिल्स एक्ट से लेकर 1916 के लखनऊ समझौते, 1927 में साइमन कमीशन के सामने रखी गई माँगों और गोलमेज सम्मेलन के बाद कम्युनल अवॉर्ड और पृथक निर्वाचन के अधिकार हासिल करने तक और उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष की ओर से की जाने वाली माँगों का विश्लेषण करते हुए कहा कि मुसलमानों की राजनीतिक माँगों की फेहरिस्त निरन्तर बढ़ती ही जाती है। लेकिन इसके खिलाफ़ हिंदू महासभा की गोलबंदियों और मुसलमानों को कोई विशेषाधिकार न देने की बात को लेकर आंबेडकर कहते हैं कि यह योजना किसी भी प्रकार एकता क़ायम करने के लिए नहीं है बल्कि उल्टे यह प्रगति में रुकावट पैदा करेगी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष का यह नारा कि ‘हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए’ न केवल अहंकारी है, बल्कि मूर्खतापूर्ण भी है। 8 इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी की लचीली और समझौते वाली नीति की भी आलोचना की।
‘राष्ट्रीय कुंठा’ अध्याय के अंतर्गत आंबेडकर ने बहुत विस्तार से उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्र की सीमा और संविधान के तहत शान्तिपूर्वक संगठित नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का कोई सूत्र मौजूद न होने को कारण माना। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक विश्वास, सामाजिक दृष्टिकोण और उनकी साम्प्रदायिक–राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ ऐसी हैं कि वे एक राष्ट्र या एक राष्ट्र के दो समुदायों के रूप में प्रेम और सद्भावना के माहौल में कभी नहीं रह सकते। हिंदुओं की बहुसंख्यक चेतना और मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण की उनकी योजनाओं पर पिछले अध्यायों में उल्लेख हो चुका है, इस अध्याय में आंबेडकर ने मुसलमानों में व्याप्त धर्मांन्धता और कट्टरपंथ पर प्रकाश डाला और कहा कि उनकी आस्था प्रथमत: इस्लाम पर है इसलिए वे हिंदुओं के नियंत्रण में और उनके साथ नहीं रहना चाहते। वे खुद को हिंदुओं से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इतिहास के मध्यकाल में उन्होंने हिंदुओं पर शासन किया है। इस तरह वे मानते हैं कि हिंदू–मुस्लिम एकता के प्रयास विफल हो चुके हैं क्योंकि उनके बीच अंतर्निहित विभाजन के तत्व बहुत ही मौलिक और प्रबल हैं। वे लिखते हैं—“अंग्रेज फूट डालो–राज करो की नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हमारे बीच ऐसे तत्व मौजूद न हों जो यह विभाजन सम्भव करा सकें, और यदि इतने लम्बे तक सफल होती रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे बीच विभाजन कराने वाले तत्व क़रीब–क़रीब ऐसे हैं कि उनमें कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता, वे क्षणिक नहीं हैं।” 9 ऐसा इसलिए है कि इस्लाम और हिंदू धर्म हिंदुओं और मुसलमानों को उनके निजी विश्वास के मामले में अलग रखते हैं और सामाजिक मेल–मिलाप से दूर रखते हैं। दोनों ही धर्म एक–दूसरे के बीच शादी– ब्याह पर प्रतिबंध लगाते हैं और एक–दूसरे के निषेध की अनेक संहिताओं का पालन करने को मजबूर करते हैं। इस सन्दर्भ में आगे वे लिखते हैं—“हिंदू धर्म और इस्लाम में और भी अनेक दोष हैं, जो हिंदुओं और मुसलमानों के घावों को कभी भरने नहीं देते। कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म लोगों को बाँटता है, जबकि इस्लाम धर्म उन्हें मिलाता है, लेकिन यह अर्धसत्य है क्योंकि इस्लाम भी लोगों को उतना ही बाँटता है जितना कि हिंदू धर्म। इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है, जो मुसलमान और ग़ैर–मुसलमान के बीच बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट भेद करता है। इस्लाम का भ्रातृत्व मानवता का भ्रातृत्व नहीं है, मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृत्व है। इस्लाम में बंधुत्व है परन्तु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर हैं, उनके उनके लिए इसमें सिर्फ़ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा अवगुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है जो स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वे हिस्सा हैं।” 10
ऐसी स्थिति में जबरन राजनीतिक एकता क़ायम करने का नुक़सान ही होगा, इससे हिंदुओं और मुसलमानों ने जो राजनीतिक लक्ष्य संजोया हुआ है उसने उन्हें नुक़सान ही होगा। इस समस्या के निदान स्वरूप उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के भय से मुक्त हो जाएँगे और दोनों के लिए राजनीतिक विकास का रास्ता सुगम हो जाएगा।
उपरोक्त चार भाग किताब के पहले संस्करण में शामिल थे, किताब के दूसरे संस्करण के प्रकाशन के समय इसमें पाँचवाँ भाग जोड़ा गया जिसमें तीन अध्याय हैं—क्या पाकिस्तान बनना चाहिए?, पाकिस्तान की समस्याएँ और कौन निर्णय कर सकता है। इस भाग को जोड़ने के पीछे आंबेडकर ने कारण बताया कि बहुत सारे लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान के प्रश्न पर लेखक ने हिंदू–मुस्लिम पक्ष के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की लेकिन इस सम्बंध में अपना विचार व्यक्त नहीं किया। दूसरा आरोप यह लगा कि लेखक ने अपने निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए जिन तथ्यों का सहारा लिया है, वे सामान्य सत्य की तरह ग्रहण किए गए हैं और उनके अपवादों, उनकी सीमाबद्धताओं और उनके सामान्य सत्य होने की किन्हीं शर्तों का परीक्षण नहीं किया है। आंबेडकर ने इन आलोचनाओं के महत्व को स्वीकारते हुए यह भाग लिखा।
इस हिस्से में आंबेडकर ने पिछले चार अध्यायों में पाकिस्तान बनने को लेकर व्यक्त किए गए अपने मत और उनके निष्कर्षों में एक स्तर तक परिवर्तन लाते हुए कहा कि अलग पाकिस्तान के बजाय संवैधानिक संरक्षण और अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकारों के साथ मुसलमानों को भारत में ही रहना चाहिए। इस अध्याय में उन्होंने मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान की माँग के पीछे पेश की जाने वाली हर दलील का खंडन किया। मुस्लिम जनसंख्या के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने, हिंदू और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक तनाव, कांग्रेस के प्रति अविश्वास, मुसलमानों के एक राष्ट्र होने की बात, और हिंदू राज के ख़तरे की बात—इन सभी आधारों को निर्मूल और आधारहीन सिद्ध करने के लिए उन्होंने विदेशों के कई उदाहरण सामने रखे और कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने पक्ष को मुसलमानों को सिद्ध करना पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान के पक्ष को कमजोर करने वाली सीमाएँ इतनी अधिक हैं कि उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
इस अध्याय में आंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण बात हिंदू राज के ख़तरे को लेकर कही है। मुसलमानों की यह आशंका कि आज़ाद भारत एक हिंदू राज होगा का उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि हिंदू बहुल रियासतों में लाखों मुस्लिम बिना किसी नियंत्रण के रहते हैं, वहाँ उन्हें हिंदू राज का भय नहीं है। इसी तरह ब्रिटिश राज के भीतर रहते हुए उन्हें यह खतरा नहीं है तो फिर आज़ाद भारत में उन्हें हिंदू राज का भय नहीं सताना चाहिए क्योंकि उस ख़तरे को दूर करने के सुरक्षात्मक उपाय मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि यह सही है कि हिंदू समाज एक अलोकतांत्रिक समाज है, लेकिन इन बुराइयों से सिर्फ़ मुसलमान ही पीड़ित नहीं हैं बल्कि करोड़ों गैर–ब्राह्मण, शूद्र और अस्पृश्य जातियाँ हिंदू समाज की अलोकतांत्रिक व्यवस्था से पीड़ित हैं। जिसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति, शिक्षा और लोक सेवाओं में हुए सुधारों का फायदा केवल उच्च वर्णीय हिंदुओं को मिला जो कुछ हिंदुओं की जनसंख्या का दस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। यही वो तबका है जिसका हिंदू राजनीति पर नियंत्रण है। इस शासक हिंदू तबके ने अस्पृश्यों को किसी भी तरह का राजनीतिक लाभ देने का विरोध किया लेकिन मुसलमानों के निहित स्वार्थों की सुरक्षा का ध्यान अधिक रखा है। उन्होंने कहा कि गांधी दलितों को राजनीतिक लाभ दिए जाने का विरोध करते हैं लेकिन मुसलमानों के पक्ष में कोरे चेक पर हस्ताक्षर करने को तैयार रहते हैं, इसलिए हिंदू राज कभी भी हक़ीक़त नहीं बन सकता। हिंदू बहुमत द्वारा उत्पीड़न की सम्भावना के विरुद्ध मुसलमानों को जरूर ही सुरक्षा दी जाएगी। यहीं पर आंबेडकर ने वे प्रसिद्ध पंक्तियाँ लिखीं जो आज के समय आंबेडकर का सबसे अधिक उद्धृत किए जाने वाले कथनों में से एक है। उन्होंने लिखा—“अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निस्संदेह वह इस देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए एक ख़तरा है। इस आधार पर यह लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर क़ीमत पर रोका जाना चाहिए। परन्तु क्या इसका वास्तविक उपचार पाकिस्तान का बन जाना ही है?” 11
हिंदू राज या मुस्लिम राज के ख़तरे और डर को निर्मूल करने के लिए उन्होंने सुझाया कि साम्प्रदायिक आधार पर और धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन न किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा और हिंदू राज की प्रतिक्रिया में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, यह क्रिया–प्रतिक्रिया है जो एक दूसरे को जन्म देती है। हिंदू राज के भूत को दफ़नाने के लिए पाकिस्तान बनने की बजाय मुस्लिम लीग और महासभा जैसी साम्प्रदायिक पार्टियों को भंग कर दिया जाना चाहिए और हिंदू–मुस्लिम दोनों के सम्मिश्रण से संयुक्त जनमत पर आधारित राजनीतिक पार्टियों का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कनाडा, दक्षिण अफ़्रीका और स्विट्जरलैंड के उदाहरणों से बताया कि कनाडा में कोई ब्रिटिश राज नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में कोई डच राज नहीं है और स्विट्जरलैंड में कोई जर्मन राज नहीं है क्योंकि उन्होंने साम्प्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक साम्प्रदायिक बहुमत का शासन रहेगा तब तक अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय का ख़तरा मौजूद रहेगा।
लेकिन आलोचकों द्वारा उठाए गए सवालों और आलोचनाओं का जवाब देने और पाकिस्तान की समस्याओं और उसके औचित्य पर अपनी राय रखते हुए आंबेडकर अपने पुराने मत पर कायम रहते हैं कि पाकिस्तान के मसले को बेहद सूझ–बूझ और राष्ट्रवादी भावुकता से मुक्त होकर विचार किया जाना चाहिए। यदि इस मसले पर मुस्लिम जनमत झुकता नहीं है तो पाकिस्तान बन कर रहेगा। अंतिम निष्कर्ष में वे कहते हैं—”जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, केवल यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मुसलमान पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं? या पाकिस्तान केवल एक पुकार है? क्या यह केवल क्षणिक विचार है या यह उनके स्थायी उत्साह का प्रतीक है? इस बात पर मतभेद हो सकता है। एक बार यह निश्चित हो जाने पर कि मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि इस सिद्धान्त को मान लेना ही बुद्धिमानी की बात होगी।” 12
डॉ. आंबेडकर के मुसलमान सम्बन्धी विचारों का कुपाठ
डॉ. आंबेडकर ने यह किताब पाकिस्तान और भारत विभाजन की समस्या के सभी पहलुओं का अध्ययन करने और एक व्यावहारिक समाधान सुझाने के मकसद से लिखी थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के विषय में प्रस्ताव पारित करने के बाद इंडियन लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पाकिस्तान के मुद्दे पर एक प्रतिवेदन तैयार करने की ज़िम्मेदारी आंबेडकर को सौंपी थी, वह प्रतिवेदन पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस किताब में आंबेडकर ने पाकिस्तान की माँग को समझने के लिए उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, जिसमें इतिहास, राजनीति, सामाजिक–आर्थिक मसलों पर व्यावहारिक नज़रिए से चिन्तन किया गया है। पाकिस्तान के प्रश्न को उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के तर्कों और उन तर्कों की सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा, वे किसी एक के पक्ष में खड़े होकर कोई निर्णय नहीं सुनाते हैं बल्कि सामने उत्पन्न समस्या पर तटस्थ होकर विचार करते हैं, उन समस्याओं के सन्दर्भ में वैश्विक दृष्टांत तलाशते हैं और भारत के सन्दर्भ में उसकी उपयोगिता पर बात करते हैं। भारत में हिंदू–मुस्लिम तनाव और साम्प्रदायिकता के इतिहास पर विचार करते हुए दोनों की आलोचना करते हैं। हिंदू धर्म की अलोकतांत्रिक चेतना और भ्रातृत्व की भावना के अभाव की बात करते हैं तो मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, सामाजिक गतिहीनता की भी आलोचना करते हैं। जिन्ना की राजनीतिक सौदेबाजियों की परतें खोलते हैं तो हिंदू महासभा और सावरकर के हिंदुत्व की भी बुराइयों को सामने रखते हैं। गांधी जी की साम्प्रदायिक एकता कायम करने की रणनीति के आलोचक वे थे ही। लेकिन आज संघ परिवार और समूचा धुर दक्षिणपंथी वैचारिक खेमा इस किताब से अपने अनुकूल हिस्सों को उद्धृत कर आंबेडकर को इस्लाम का आलोचक और मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। रोचक बात यह है की यह कोई आज की परिघटना नहीं है, इस किताब के प्रकाशन के साथ ही यह शुरू हो गया था। आंबेडकर ने द्वितीय संस्करण की भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक से हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से नाराज़ हुए और दोनों अलग–अलग कारणों से नाराज़ हुए, इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना व्यक्त नहीं की गई है, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता और निर्भीक दृष्टिकोण के चलते किसी का पक्ष–पोषण नहीं करती है।
इस किताब के मुख्यतः दो अध्यायों—’एकता में विघटन‘ और ‘राष्ट्रीय कुंठा‘ में व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर आंबेडकर का कुपाठ रचा जाता है। एकता में विघटन नामक अध्याय में आंबेडकर ने मध्यकाल में भारत में मुस्लिम आक्रमण और इस्लाम के प्रसार का विस्तार से वर्णन किया है, इसमें उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए बरती जाने वाली क्रूरताओं का लगभग एकांकी चित्रण किया है। ब्रिटिश प्राच्यवादी इतिहासकार लेन पूल की किताब ‘मिडिवल इंडिया‘ और अमेरिकी मूल के ईसाई मिशनरी और इस्लामिक स्कालर मरे थर्स्टन टाइटस की किताब ‘इंडियन इस्लाम: ए रिलीजियस हिस्ट्री आफ इस्लाम इन इंडिया‘ में दर्ज ब्योरों का सन्दर्भ लेकर आंबेडकर ने भारत में इस्लाम के आगमन और विस्तार की कहानी लिखी है। इस हिस्से को उसके वास्तविक सन्दर्भ से काट कर दक्षिणपंथी लेखक हिंदुओं पर मुस्लिम आधिपत्य और धार्मिक जिहाद की अपनी अवधारणा को फिट करना चाहते हैं। और अपने इस साम्प्रदायिक उन्मादी सिद्धान्त के लिए आंबेडकर की वैधता प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि आंबेडकर ने मुस्लिम आक्रमण का विस्तृत वर्णन इस बात को सिद्ध करने के लिए किया था कि पाकिस्तान का विरोध करने वाले हिंदू पक्ष के लोग मुस्लिम बहुल प्रांतों और शेष भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता का दावा करते हैं, वह आधारहीन है। इन प्रांतों के अलग हो जाने पर भारत की प्राचीन एकता में विखंडन और अखंड भारत में विघटन की बात गलत है, क्योंकि वह पहले से ही एक अलग रंगत में रंगा हुआ क्षेत्र रहा है। इस सन्दर्भ में आंबेडकर लिखते हैं—”भारत का यह पश्चिमोत्तर कोना एक ऐसा रंगमंच रहा है जिस पर एक निर्मम नाटक खेला जाता रहा है। मुसलमानों के दल एक के बाद दूसरी लहर के रूप में इस क्षेत्र पर चढ़ कर आते रहे हैं और वहाँ से उन्होंने स्वयं को शेष भारत में छितराया। ये छोटी–छोटी धाराओं के रूप में शेष भारत में पहुँचे। समय आने पर वे अपनी सुदूरतम सीमाओं से पीछे भी हटे, जबकि वे वहाँ रहे तो उन्होंने भारत के इस पश्चिमोत्तर कोने में आर्य–संस्कृति पर इस्लामी संस्कृति का गहन प्रभाव भी छोड़ा, जिसने धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से इसे एक सर्वथा अलग रंगत दे दी।” 13
यहाँ डॉ. आंबेडकर की इतिहास दृष्टि और मध्यकाल के ऐतिहासिक विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्षों पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें किसी हिंदुत्ववादी प्रोपेगैंडा का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।
आंबेडकर की इतिहास दृष्टि की समस्याएँ
वरिष्ठ आंबेडकरवादी लेखक और विद्वान आनंद तेलतुम्बडे ने आंबेडकर की इतिहास दृष्टि के बारे में ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। अपनी किताब Republic of Cast में उन्होंने लिखा है कि आंबेडकर इतिहास के किसी सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अपने प्रोफ़ेसर जॉन डीवी के प्रभाव में वे इतिहास को बरतने के मामले में हमेशा ही एक उपयोगितावादी (Pragmatist) बने रहे। उनकी ऐतिहासिक पद्धति में इस दार्शनिक सूत्र को आसानी से देखा जा सकता है। तेलतुम्बड़े कहते हैं कि आंबेडकरवाद की विचारधारा वास्तव में मौलिक रूप से उपयोगितावाद ही है, यानि किसी महाआख्यान और राजनीतिक कायापलट पर निर्भर होने की बजाय उपलब्ध संसाधनों को लेकर सामने खड़ी समस्या का व्यावहारिक समाधान करना। 14
डॉ. आंबेडकर के चिन्तन व व्यवहार में यह उपयोगितावाद कई जगहों पर दिखता है, जातियों की उत्पत्ति का इतिहास हो, शूद्रों और अछूत जातियों की उत्पत्ति का इतिहास हो, आंबेडकर ने अपने समय में उपलब्ध हर प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री का परीक्षण किया, लेकिन साथ ही वे औपनिवेशिक भारत में दलितों की समस्याओं और जाति उन्मूलन के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन ऐतिहासिक सामग्रियों का उपयोग करते हैं। वे खुद को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार व अनुसंधानों से प्राप्त नए ज्ञान के अनुरूप अपने दृष्टिकोण को बदलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते।
यहाँ सवाल आंबेडकर के ऐतिहासिक नज़रिए का है। यह स्पष्ट है कि आंबेडकर के पास भारत के मध्यकालीन इतिहास की ब्रिटिश सामग्री उपलब्ध थी जिसके आधार पर उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों का उल्लेख किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने मध्यकालीन इतिहास को साम्प्रदायिक रंग में रंग कर पेश किया था, जिसके बारे में हरबंस मुखिया कहते हैं कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने मध्यकाल में निहित साम्प्रदायिक स्वर को भारत के अतीत के एकरेखीय साम्प्रदायिक अध्ययन को प्रमुख बल्कि एकमात्र रुझान बनाने का प्रयास किया। जेम्स स्टुअर्ट मिल ने भारतीय इतिहास का हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालों में जो विभाजन किया, उसका यही अन्तिम परिणाम था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने मध्यकाल को मुस्लिम काल घोषित कर यह साबित किया की यह समय हिंदुओं पर मुसलमानों के विजय का समय है । उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टि का खंडन करते हुए राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा एक वैकल्पिक ऐतिहासिक नज़रिया विकसित किया जा रहा था लेकिन वह धारा उस समय बहुत क्षीण थी। समन्वयवादी राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा विकसित किए गए नज़रिये को लेकर हरबंस मुखिया कहते हैं—‘‘मध्यकालीन भारत के इस अनवरत साम्प्रदायिक संघर्ष के विचार का राष्ट्रवादी इतिहासकार खंडन करते थे। वे मध्यकालीन भारत के मुस्लिम शासकों की धार्मिक प्रेरणाओं की सच्चाई पर सवालिया निशान लगाते थे; उन्होंने मध्यकालीन भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए; उन्होंने विगत शताब्दियों में विचारों के, संस्कृति के, जीवनशैली के क्षेत्रों में दोनों बड़े सम्प्रदायों के बीच पर्याप्त अंत:क्रिया पर ज़ोर दिया। ‘समन्वित संस्कृति’ की अवधारणा का विकास इसी ज़ोर से हुआ।” 15
इतिहास को धर्म निरपेक्ष रूप प्रदान करने में इन इतिहासकारों की भूमिका को मुखिया स्वीकारते तो हैं पर यह कहते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकार साम्प्रदायिक इतिहास लेखन का मुक़ाबला उसी की ज़मीन पर कर रहे थे। वे बताते हैं कि पचास के दशक के बाद ही ऐसे अनुसंधान हुए जिसमें साम्प्रदायिक प्रवर्गों की कोई दखल नहीं थी। वर्गीय संरचना, किसानों के शोषण के रूप और परिणाम आदि विषयों के शामिल होने पर इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टि में बदलाव आया। इसलिए मध्यकाल के ऐतिहासिक निरूपण में आंबेडकर अगर औपनिवेशिक इतिहास लेखन के चंगुल में फँसते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि इस इतिहास दृष्टि से वे हासिल क्या करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि आंबेडकर इसके ज़रिए विभाजन की समस्या को यथार्थवादी ढंग से समझने का प्रयास कर रहे थे। हालाँकि इसके बावजूद आंबेडकर के इतिहास दृष्टि की कमज़ोरियों से मुँह फेर लेने का कोई करण नहीं है।
आंबेडकर के मुस्लिम–राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारों का कुपाठ
कुपाठ करने वालों को कुछ और सामग्री ‘राष्ट्रीय कुंठा‘ नामक अध्याय में मिलती है, इस अध्याय में आंबेडकर ने मुसलमानों के राष्ट्रीय चेतना पर इस्लाम के प्रभाव का विश्लेषण किया है। यहाँ व्यक्त विचारों का भी एक विशिष्ट सन्दर्भ है। आंबेडकर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के तमाम प्रयासों के बाद भी ये दोनों पक्ष ऐसे रहते हैं जैसे कि दो शत्रु सेनाएँ रहती हैं। ऐसे में यदि इन दोनों पक्षों को समझौते या बलपूर्वक एक प्रतिनिधि सरकार के अंतर्गत रहने के लिए मजबूर किया गया तो उससे समस्या कम होने के बजाय बढ़ेगी। वे कहते हैं कि हिंदू फ़िलहाल पाकिस्तान के विभाजन को रोकना चाहते हैं इसलिए वे अपनी बातों और मंशाओं को खुल कर नहीं बताते, लेकिन मुस्लिम पक्ष चूँकि हर हाल में पाकिस्तान चाहता है इसलिए वे अपनी बात मुखरता से रखते हैं।
इसके तहत उन्होंने मुस्लिम नेताओं के भाषणों, बयानों, प्रतिवेदनों में व्यक्त विचारों और आज़ाद भारत के लिए उसके निहितार्थों का विश्लेषण किया। जिसमें आंबेडकर यह बताते हैं कि पाकिस्तान की माँग के सन्दर्भ में मुसलमानों की आस्था इस्लाम के प्रति होगी न कि अखंड भारत के विचार के प्रति। वे कहते हैं की इस्लाम के अनुसार विश्व दो हिस्सों में विभाजित है—दार–उल–हर्ब और दार–उल–इस्लाम। मुस्लिम शासित देश दार–उल–इस्लाम हैं और ऐसे देश जहाँ मुस्लिम रहते तो हैं पर शासन नहीं करते वह दार–उल–हर्ब है। मुस्लिम धार्मिक क़ानून का ऐसा होने के कारण भारत हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की मातृभूमि नहीं हो सकती।
आंबेडकर यह मान कर चलते हैं कि अखंड भारत एक हिंदू साम्प्रदायिक बहुमत का शासन होगा इसलिए वे कहते हैं—”हिंदुओं से नियंत्रित एवं शासित सरकार की सत्ता को मुसलमान किस सीमा तक स्वीकार करेंगे, इस प्रश्न के उत्तर के लिए ज्यादा छान–बीन करने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों के लिए हिंदू काफ़िर हैं, और एक काफ़िर सम्मान के योग्य नहीं है। वह निम्न कुल में जन्मा होता है इसलिए उसकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं होती। इसलिए जिस देश में काफ़िरों का शासन हो वह मुसलमानों के लिए दार–उल–हर्ब है। ऐसी स्थिति में यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमान हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे।” 16
आंबेडकर ने कहा कि मुसलमानों के भीतर यह चेतना पहले से मौजूद नहीं थी, पाकिस्तान की माँग के बलवती होने के साथ–साथ यह भावना उनके अन्दर भरती गई कि आज़ाद भारत में अल्पसंख्यक के बतौर रहने में उनका दमन होगा इसलिए इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार पाकिस्तान ही उनकी समस्याओं का समाधान है। हालाँकि इसी किताब के पाँचवे भाग में ‘क्या पाकिस्तान बनना चाहिए‘ नामक अध्याय में आंबेडकर ने इस विषय पर पुनर्विचार किया और यह कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों को अपना अतीत भुला कर एक साथ आना होगा, तभी वे एक राष्ट्र में संगठित रह सकते हैं।
आंबेडकर के इन विचारों और तथ्यों को वर्तमान भारत के मुसलमानों की देशभक्ति का परीक्षण किए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुत्ववादी लेखक–विचारक बहुत जोर शोर से इसका प्रचार करते हैं कि डॉ. आंबेडकर ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमानों की आस्था राष्ट्र में नहीं इस्लाम में है। हालाँकि इसी किताब में आंबेडकर ने हिंदुओं की धर्मान्धता, साम्प्रदायिक उन्माद, हिंदू धर्म की अंतर्निहित असमानता और हिंदू राज के ख़तरों के प्रति भी आगाह किया था, लेकिन उस तथ्य को ये कुपाठी छिपा लेते हैं और प्रच्छन्न तरीके से दुष्प्रचार चलाते हैं।
भारत में साम्प्रदायिकता और उसके समाधान को लेकर डॉ. आंबेडकर के इन विचारों का एक विशेष सन्दर्भ और निश्चित देश काल और परिस्थिति है। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारत में साम्प्रदायिकता की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन आ चुका है। जिस समय आंबेडकर यह लिख रहे थे उस समय तक हिंदू और मुस्लिम दो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में उपस्थित थे। ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत मुसलमान को वे सभी सुविधाएँ व अधिकार शामिल थे जो हिंदुओं को प्राप्त थे। शासन, सम्पत्ति और राजनीतिक अधिकारों के मामले में मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हुए भी बेहतर स्थिति में थे, इसी आधार पर वे राजनीतिक सौदेबाजी की स्थिति में थे, यह सौदेबाजी आम मुसलमानों के हितों के नाम पर शुरू हुई पर धीरे–धीरे मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुसलमानों के प्रभावशाली तबके की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का ज़रिया बन गई।
मुस्लिम लीग की दबाव की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए आंबेडकर ने कहा था कि मुसलमानों की माँगे लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और कांग्रेस उनके दबाव में झुकती जा रही है। कम्यूनल अवॉर्ड के मामले में भी गोलमेज़ परिषद् में महात्मा गांधी ने मुस्लिम पक्ष की माँगों का समर्थन किया परन्तु अनुसूचित जातियों के मामले में कम्यूनल अवॉर्ड न मिले इसके लिए अड़ गए थे। यह निश्चित है कि आज यह परिस्थिति बदली हुई है। आज भारत के मुसलमान पहले की अपेक्षा विपन्न और राजनीतिक–सामाजिक अलगाव का शिकार हैं। ऐसे में आज भारत की साम्प्रदायिक शक्तियाँ ‘पाकिस्तान’ का राजनीतिक इस्तेमाल बहुसंख्यक हिंदुओं के ध्रुवीकरण के लिए करतीं हैं। पाकिस्तान आज एक विभाजनकारी परिघटना के रूप में भारत में शासक वर्गों के हाथ में व्यवहृत हो रहा है। आज हमें आंबेडकर के पाकिस्तान सम्बन्धी विचारों और साम्प्रदायिकता पर उनके दृष्टिकोण की संवेदनशीलता को समझने, सही ऐतिहासिक सन्दर्भों के साथ समझने, और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तियों द्वारा उनके सन्दर्भ रहित दुरुपयोग करने के कुत्सित प्रयासों के प्रति सचेत रहना चाहिए।
— रामायन राम
( आलोचना पत्रिका से साभार)