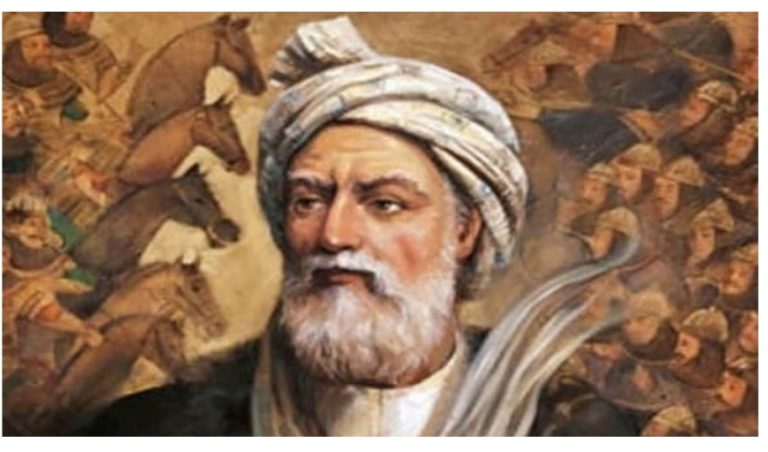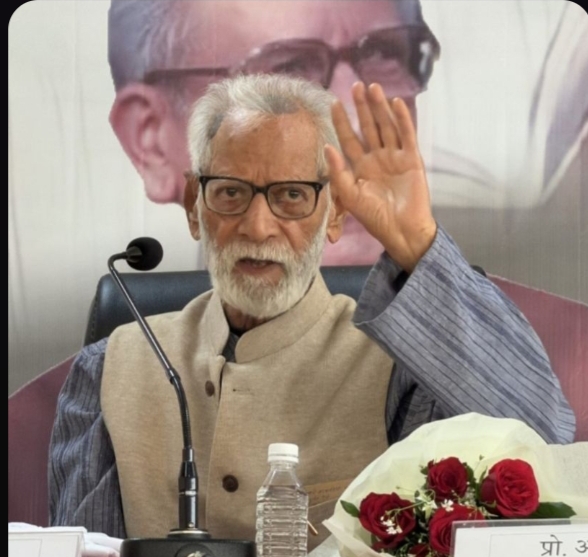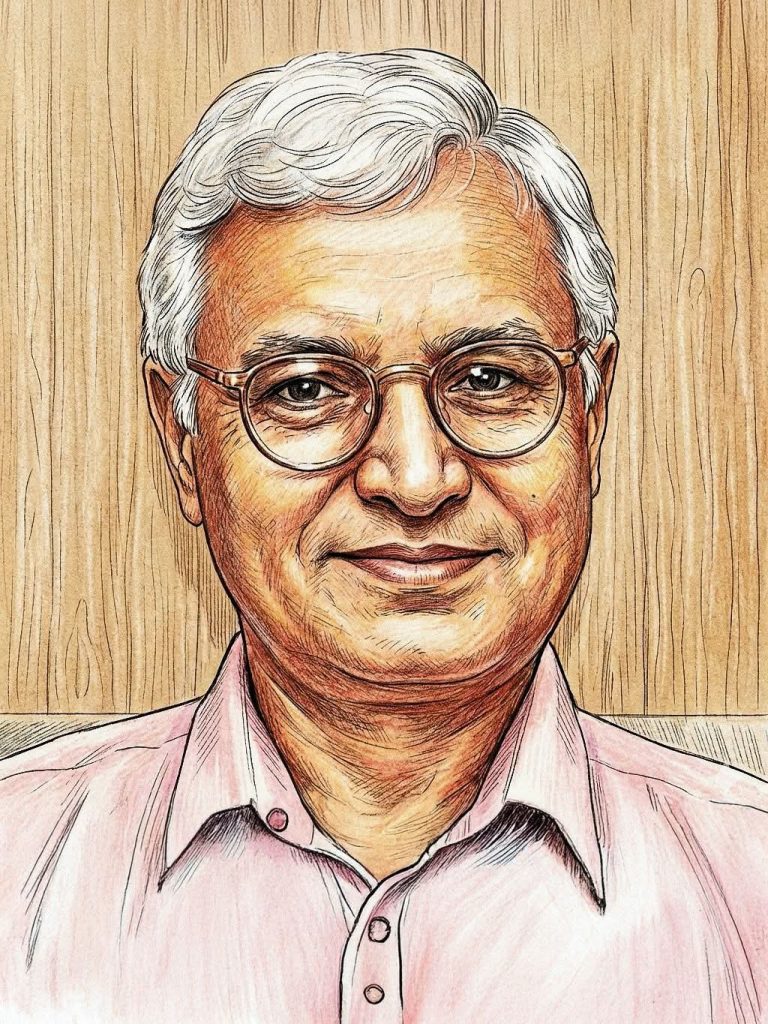– उषा वैरागकर आठले
छत्तीसगढ़ के कस्बेनुमा लोरमी शहर में बनी हुई यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत उत्सुकता से देखी गई। छत्तीसगढ़ के परिवेश, लोकधुनों का प्रयोग और कुछ छत्तीसगढ़ी परिचित कलाकारों की उपस्थिति ने फिल्म के प्रति बहुत सी अपेक्षाएँ जगा दी थीं। मगर सबसे बुरा तब लगा जब छत्तीसगढ़ की प्रसिध्द नृत्यांगना-अभिनेत्री अनुराधा दुबे का नाम स्टार कास्ट में कहीं दिखाई नहीं दिया ;क्या मेरी ऑंखें खराब हो गई हैं?;। शुरु के कुछ मिनटों में फिल्म बहुत दिलचस्प लगती है। चटपटे संवाद, कस्बाई तरूणाई के लटके-झटके, उनकी इंटर्नल फूहड़ सी राजनीति देखकर उत्सुकता जागती है कि आगे कहानी क्या मोड़ लेती है!! प्रकाश झा की फिल्मों में निर्देशन सहयोग कर चुके निर्देशक के प्रति भी एक आत्मीय भाव था। साथ ही छत्तीसगढ़ के सुपुत्र, छत्तीसगढ़ की कहानी आदि का भी एक प्रभाव था। मगर बहुत निराशा हाथ लगी।
एक कस्बाई युवक बिल्लू वन-विभाग की सुरक्षा चौकीदारी छोड़कर कुछ अपना धंधा करना चाहता है ताकि उसकी कोई पहचान बन सके। अच्छा लगा यह। शहर की बाहरी हाइवेनुमा सड़क के किनारे अपना पान ठेला खोलता है। सामने ही रास्ते के दूसरी ओर एक शासकीय आवास है। अचानक एक दिन सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर का परिवार वहाँ रहने आता है और फिल्म में रोमांच पैदा होता है। हरिशंकर परसाई की ‘एक लड़की पाँच दीवाने’ शुरु हो जाती है। इंजीनियर साहब की स्कूली किशोरी लड़की, जो शहरी लड़कियों की तरह शॉर्टस पहनती है, अपने पामेरियन कुत्ते को घुमाने के लिए घर के सामने वाली सड़क पर निकलती है। इस परिघटना में कोई भी असामान्य चीज़ नहीं है। मर्दवादी समाज के लिए असामान्य है, लड़की का बिना किसी रोकटोक के बाहर निकलकर एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करना।
कस्बेनुमा शहर में आज भी किसी स्वतंत्र खुले दिमाग के परिवार की लड़की का उन्मुक्त, मगर स्वाभाविक व्यवहार तमाम शहर के पुरुष वर्ग को उत्तेजित कर देता है। मर्दानगी तो होती ही इसमें है न कि, एक खूबसूरत लड़की आखिर उन्मुक्त होकर लड़कों की तरह शॉर्टस पहनकर कैसे घूम सकती है! वह बाहर निकलने के बाद भी किसी पुरुष को देखती तक नहीं, एक मुस्कान तक नहीं उछालती, बल्कि उन्हें नज़रअंदाज़ तक कर जाती है। उसकी इतनी हिम्मत!!! तमाम मर्दों को पूरा अधिकार मिल जाता है कि उस लड़की को केन्द्र में रखकर हरतरह की मर्दवादी हरकतें करें ;मानो वहाँ कोई स्वयंवर हो रहा हो और तमाम देशों के राजकुमार राजकुमारी से स्वयंवर रचाने की प्रतियोगिता में सम्मिलित हों। इसतरह की पौराणिक कथाएँ जनमानस में आदर्श के रूप में स्थापित हैं;। सुंदर कम उम्र की लड़की अगर पुरुषों से न डरे, सहमी-सिमटी न रहे, चहारदीवारी के भीतर छिपती न फिरे तो समाज का पितृसत्तात्मक ढाँचा चरमरा नहीं जाएगा? और अगर वह देखकर मुस्कुरा दे, बात कर ले, तो वह ‘पट गई’ कहते हुए एक पक्ष खुश और दूसरा नाराज़ हो जाए!!

मज़े की बात यह है कि इस फिल्म में न तो किशोरी रिंकू किसी को कुछ दिखाना चाहती है और न ही कोई मर्दों को आकर्षित करने वाला व्यवहार करती है। उसकी सामान्य सी दिनचर्या है। वह दिन में अपने छोटे भाई को स्कूटी से स्कूल छोड़ने जाती है, खुद स्कूल जाती है और अपने कुत्ते को सड़क पर घुमाते हुए चहलकदमी करती है। अगर यही दिनचर्या इंजीनियर साहब के बेटे की होती तो क्या बिल्लू के पान ठेले के आसपास इतनी भीड़ जमा होती ;लड़कियों की!! ओह… यह फिल्म अतियथार्थवादी भी तो नहीं है!;। मगर लड़की तो मनोरंजन का सबसे आसान उपलब्ध साधन है… सॉफ्ट टार्गेट, जिससे मन बहलाने, उस पर अपना अधिकार दिखाने, उसके बहाने अपनी मर्दानगी को सिध्द करने की प्रतियोगिता समाज में आसानी से देखी जाती है। चाहे वह लड़की घर की छोटी बच्ची हो, बेटी हो, बहू हो या कोई और; उसे अपने परिवार के या बाहर के हर उम्र के पुरुष से डरना ही होगा, उससे दबकर रहना ही होगा, किसी मर्द की तरह ;लोकतांत्रिक देश के इंसान की तरह तो कतई नहीं; मनचाही गतिविधियाँ करने से बाज आना ही होगा। अगर कोई लड़की ऐसा नहीं करती, तो काफी बड़ा मर्दवादी तबका कमर कस लेता है कि ‘लड़की को लड़की की तरह ही रहना होगा, वर्ना उसकी औकात दिखा दी जाएगी।’
मर्दवादी व्यवहार का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कोई लड़की या स्त्री, पुरुष का नोटिस न ले। इससे उसका मर्दवादी अहंकार चोट खा जाता है। अधिकांश परिवारों में बच्चे के पैदा होते ही लड़की या लड़के का पालन-पोषण्ा स्टीरियोटाइप स्त्री और पुरुष बनाने की मशीन के रूप में होता है। अत: किशोर लड़के का माइंडसेट भी लड़की को कमतर मानने की ओर ही अग्रसर होता है। लड़की को अपने समान एक ‘व्यक्ति’ के रूप में न देखकर किसी मज़ेदार खिलौने जैसी ‘चीज़’ ;माल; के रूप में देखने की दृष्टि समूची आसपास की दुनिया से उसे मिलती है। असमानता पर आधारित समाज ही तमाम व्यक्तियों को लिंगगत, वर्णगत, वर्गगत, उम्रगत विभेदों में बाँटकर सबके लिए उनके व्यवहारों के स्टीरियोटाइप गढ़ता है। हमारे देश में ‘सोनम गुप्ता बेवफा है’ लिखकर किसी काल्पनिक लड़की के वफादार नहीं होने के रूपक के माध्यम से नोटबंदी की घोषणा से अचानक नोटों या प्रचलित करेंसी का नहीं चलना बेवफाई के स्वांग को अभिव्यक्त कर रहा था। मगर रूपक में भी लड़की ही टार्गेट थी। उसमें कोई ‘सोनू गुप्ता’ बेवफा नहीं हुआ था। इसी तर्ज़ पर ‘चमन बहार’ फिल्म में भी उस किशोरी रिंकू द्वारा किसी को तरजीह न दिये जाने और उस पर एकाधिकार ;?; जमाने का इच्छुक पान वाला बिल्लू पुलिस द्वारा पीटे जाने और उसकी दुकान तोड़ दिये जाने पर अपने पास के तमाम नोटों पर ‘रिंकू ननोरिया बेवफा है’ लिखकर अपने आक्रोश को बाहर निकालता है मगर उसके पास क्या कोई ठोस कारण्ा है कि रिंकू को उससे किसतरह की ‘वफा’ करनी चाहिए थी?
जिन्हें यह फिल्म अच्छी लग रही है, उन्हें आनंद पटवर्धन की बहुत ज़रूरी फिल्म ‘पिता, पुत्र और धर्मयुध्द’ ज़रूर देखना चाहिए। हम सब समाज में व्याप्त हिंसा, अन्याय, असमानता, विषमता, यौन अपराध, वर्चस्ववाद से चिंतित हैं। इनकी जड़ें कहाँ पर हैं? पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमें ढाल रही है और हम ढल रहे हैं। ‘चमन बहार’ अगर इन परिस्थितियों पर किसी भी दृश्य में व्यंग्य करती नज़र आती, कोई सवाल उठाती तो शायद सार्थक फिल्म बनती। सबसे ज्यादा तकलीफदेह है फिल्म में प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका। सिर्फ पुरुष ही प्रेम करने या प्रदर्शित करने का हकदार होता है क्या? और प्रेम भी कैसा? जिस पर तथाकथित प्रेम किया जा रहा है, उसके ‘मन की बात’ से कोई लेना-देना नहीं! संवाद मज़ेदार हैं मगर ये किन्हें मज़ा दे रहे हैं? उन्हें ही जो मानते हैं कि लड़की छेड़े जाने के लिए है। हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने हम सबके दिल-दिमाग को इसके लिए अनुकूलित कर दिया है। इसीलिए समाज में भी जब इसतरह की घटना घटती है तो लड़की के परिवारवालों के अतिरिक्त किसी की संवेदना नहीं जागती। और आजकल तो यह संवेदना धर्म-सम्प्रदाय-जाति की राजनीति में व्यक्त हो रही है।
फिल्म का अंतिम हिस्सा और भी आश्चर्यचकित करता है। रिंकू के माँ-पिता बिल्लू को घर बुलाकर उससे माफी माँगते हैं। किसलिए? क्या उनकी शिकायत पर उसे पीटे जाने के कारण? ठीक है कि उनमें यह संवेदना है कि उनके कारण एक गरीब युवक को काफी नुकसान उठाना पड़ा जबकि ज्यादा परेशानी अन्य युवकों से थी। मगर पूरी फिल्म में क्या बिल्लू का रिंकू के प्रति कोई स्वस्थ दृष्टिकोण दिखाई देता है? जिसे प्रेम कहा जा रहा है, वह महज़ एक खूबसूरत कम उम्र की आधुनिक किशोरी को निहारते रहने, उसे आकर्षित करने की अदम्य लालसा को ही व्यक्त करता है। प्रेम से उपजी गहन संवेदना के दर्शन कहीं नहीं हुए। बल्कि रिंकू पर उसका अधिकार है, अधिकार का यही अहसास ज्यादा दिखाई देता है। बिल्लू बाकी तमाम मर्दों से कहीं अलग नहीं लगता। बाद में दीवारों, होर्डिंग्स और नोटों पर ‘रिंकू ननोरिया बेवफा है’ लिखकर जेल चला जाता है। क्या मान लिया जाए कि बेचारे बिल्लू के प्रति अन्याय हुआ है? हाँ, पुलिस अफसर की मारपीट और उसके दुकान तोड़ने-फोड़ने का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। यह भी वही मर्दवादी तरीका है। रिंकू के मनोभावों को कोई तरजीह नहीं दी गई है सिवाय पान दुकान पर खड़े बिल्लू के एक चित्र के, जो उसके जाने के बाद बिल्लू को हवा में उड़ता हुआ मिलता है। क्या वह चित्र प्रेम की इबारत का प्रतीक मान लिया गया है? अगर पूरी फिल्म की यही स्थापना है तो इससे यही सिध्द होता है कि अपनी तरफ घूरते लड़के और उसकी रक्षा के लिए प्रतिबध्द लड़के ;एक दिन बिल्लू उसके पामेरियन कुत्ते को देसी कुत्ते के आक्रमण से बचाता है, अर्थात् उसकी भी देसी कुत्ते से रक्षा करता है; ही पसंद है। सदियों से समाज में यही भाव स्थापित किया जा रहा है कि लड़कियाँ या स्त्रियाँ कमज़ोर होती हैं, उनकी रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। किनसे रक्षा करना?? अन्य पुरुष से…। वाह! क्या समाज-दर्शन है! आक्रमणकारी भी पुरुष और बचाने वाला भी पुरुष!! पूरी फिल्म पुरुषप्रधान है। पुरुषों की सोच, उनकी गतिविधियाँ, उनके द्वारा फेंके गए जुमले और उनका मनोरंजन, सिर्फ पुरुषों के लिए रचा गया मनोरंजन इस फिल्म को देश-विदेश तक पहुँचा रहा है। अगर महिलाएँ भी इससे प्रसन्न है तो क्या कहने? ग्लोबल दुनिया में पितृसत्तात्मक सत्ता की जय हो!