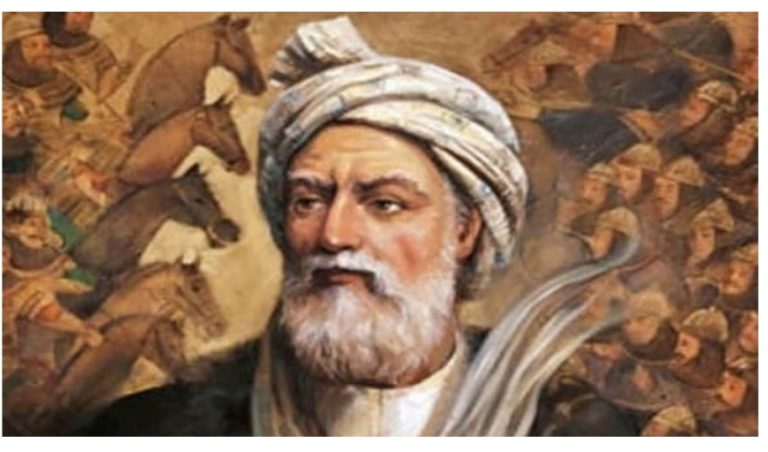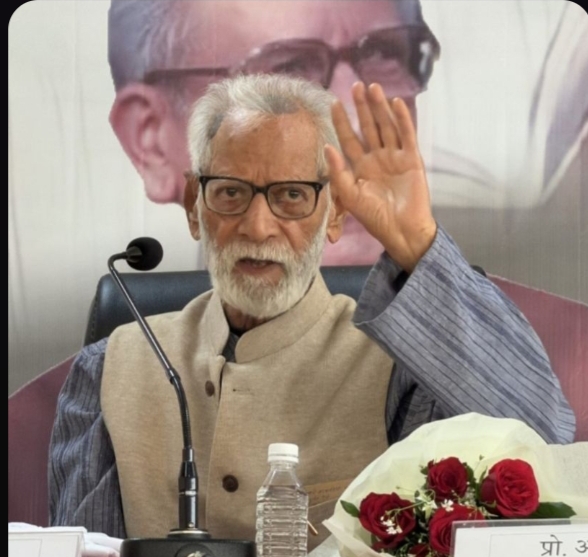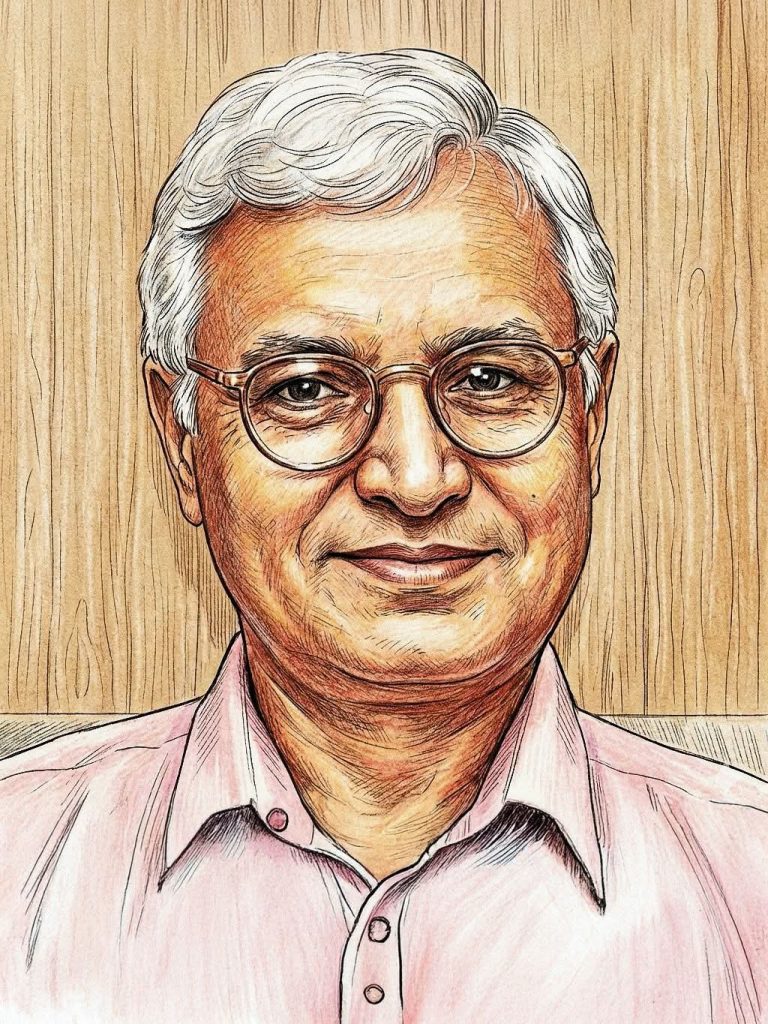ऑंखें कुछ अभ्यस्त हुईं तो सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए पेड़ों, टीलों और उनके पीछे के पहाड़ों की आकृतियाँ दिखलाई देने लगीं। अलबत्ता, घने अंधेरे के कारण इन आकृतियों की तराश अब भी दिखलाई नहीं दे रही थी। हवा न चलने के कारण सब कुछ स्थिर था, जिसने सन्नाटे को और अधिक गहरा और भयावह बना दिया था। कुछ ही देर पहले वह जिस बस से उतरा था, उसकी पिछली रौशनियाँ धुंधलाते-धुंधलाते खो चुकी थीं । अब आवाज का आना भी बंद हो गया था। ऐसे में सड़क के बीचों-बीच खड़ा हुआ वह सोच रहा था कि कितनी भयानक भूल कर चुका है।
दोनों तरफ के घने दरख्तों के बीच से छनकर रौशनी की एक भी किरण नहीं आ रही थी। इस समय वह जंगल में है या उसी गांव में जहां उसे जाना था- वह समझ नहीं पा रहा था। रास्ते के किसी ठीक-ठाक कस्बे में रात बिता कर यहाँ सुबह भी पहुँचा जा सकता था। पर अपनी पहली नौकरी पर पहुंचने के अतिरिक्त उत्साह और कल उपस्थिति दर्ज करवाने की आखिरी तारीख की विवशता ने उसे इस समय मुसीबत में डाल दिया था। वह नहीं जानता था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। अनिश्चय से कुछ समय वहीं खड़े रहने के बाद वह धीरे-धीरे बस के जाने वाली दिशा में ही बढ़ने लगा।
उसका दिल आशंकाओं से भरा था । वह सोच रहा था कि अगर यह गाँव वह नहीं है, जहाँ उसे पहुँचना था -तो वह कहाँ है!

काले कालीन सी बिछी हुई सड़क सामने के बड़े पहाड़ की स्याही में जाकर खो गई थी। पिट्ठू की तरह भारी सामान उठाए हुए, धीरे-धीरे चढ़ाई चढ़ती सड़क पर वह अभी बमुश्किल बीस-तीस कदम ही गया था कि उसे अपने बाईं ओर की कालिख में छोटा सा पीला धब्बा लरजता हुआ दिखलाई दिया। यह कोई दिया था या मद्धम रौशनी का बल्ब- तय करना मुश्किल था, पर वहाँ किसी के होने की सम्भावना ने उसके कदम उस ओर मोड़ दिए। इस समय ये छोटी सी रौशनी भी उसके लिए उम्मीद की किरण जैसी थी।
सड़क के किनारे की जमीन उठान लिए हुए थी । उस पर पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यदि ऐसी कोई जगह थी भी तो अंधेरे में दिखलाई नहीं दे रही थी। लिहाजा झाड़ियों को पकड़ कर वह ऊपर चढ़ा और सम्भाल-सम्भाल कर कदम रखते और टटोलते हुए, प्रकाश की दिशा में बढ़ने लगा। कद्दावर पेड़ों के बड़े-बड़े सायदार फैलाव ने आसमान पर टिमटिमाते जुगनुओं को भी ढक लिया था। पेड़ों के मोटे तने तो अंधेरे में काले साए की तरह सामने आ जाते और वह बच कर निकल जाता, पर उनकी उभरी हुई जड़ें दिखलाई नहीं दे रही थीं । वह लगातार ठोकर खा रहा था। यदि कहीं कोई रास्ता था भी, तो वह अंधा कर देने की हद तक गहरे अंधेरे में दिखलाई नहीं दे रहा था। वह रौशनी से पैदा हुई उस उम्मीद के बुझ जाने से पहले, उस तक पहँच जाना चाहता था।
रौशनी के बहुत करीब पहँच कर उसने देखा कि कच्चे आंगन से घिरा हुआ यह एक कच्चा मकान था। उसकी दीवारें मिट्टी कूट कर बनाई गई थीं मोटी शहतीरों पर टीन की छत बिठाई गई थी। मकान का मुँह सड़क की तरफ था । ठीक सामने वाले कमरे में ही मध्दम रौशनी का वह बल्ब जल रहा था जिसके सहारे वह यहाँ तक पहुँचा था। सामने बैठा हुआ आदमी किसी कपड़े पर तुरपाई कर रहा था । एक मशीन के पास कई कपड़े बेतरतीबी से फैले हुए थे। पहली ही नजर में समझा जा सकता था कि यह घर किसी दर्जी का है।
”कौन है?” उसके सांकल खड़काने से पहले ही उसकी पदचाप अंदर बैठे हुए आदमी तक पहुँच गई थी।
”जी मैं यहाँ स्कूल में नया मास्टर लगा हूँ।” अभिवादन करते हुए उसने कहा।
अपने आगे से कपड़ा खिसकाते हुए वह लम्बा आदमी उठकर खड़ा हुआ और झुककर दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोला।
”बड़ी देर से आए आप। गुलाम रसूल तो सो भी गया होगा। हांलाकि उसे आपके आने का पता है।”
गुलाम रसूल! उसे यह भूला नाम याद आ गया। शहर के दफ्तर में अचानक मिल गए हैडमास्टर साहब ने उसे यही नाम बताया था। उसे हैरानी हुई। समय बमुश्किल आठ-सवा आठ का ही था । ऐसे में किसी व्यक्ति का सो जाना उसे हैरान कर रहा था। शायद ये हैरानी इसलिए भी थी, कि इससे पहले कभी ऐसे किसी पहाड़ी गांव की जिंदगी से वाबस्ता नहीं हुआ था। इस समय वे दोनों एक पतली पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे। पगडंडी साफ थी । अब उसे ठोकरें नहीं लग रहीं थीं।
”रास्ते में लोहे के सरिए से भरा हुआ एक ट्रक टेढ़ा होकर फंस गया था। ढ़ाई-तीन घंटे वहीं फंसे रह गए, वरना तो शाम को पांच बजे ही पहुँच जाता।” उसने सफाई दी।
”इन रास्तों पर ये सब तो होता ही है। सड़कें पतली और ढलवां हैं। गाड़ी फिसली तो फिर या तो खाई में जाएगी या फिर पहाड़ से अटक कर रास्ता बंद कर देगी।” लम्बे दर्जी ने समर्थन में सिर हिलाया।
”पर इतनी जल्दी सोना – क्या गुलाम रसूल बीमार है?” उससे जिज्ञासा दबाई नहीं गई।
”नहीं” दर्जी हँसा ”ये शहर नहीं है- गांव है । यहां तो अंधेरा घिरते ही रात उतर आती है, फिर किसी को कोई काम नहीं रह जाता- सोने के सिवा।”
दर्जी एक छोटी सी कोठरी के सामने रुक गया । उसने बंद दरवाजे की सांकल को खटखटाते हुए गुलाम रसूल को पुकारा। कुछ देर बाद कोठरी का दरवाजा खुला । दरवाजे से बाहर आती मद्धम रौशनी के ठीक बीचों-बीच एक हष्ट-पुष्ट आकृति उभरी और फिर एक सिर ने दरवाजे से बाहर निकल कर झांका।
”तेरे मास्टर जी आए हैं।” दर्जी ने कहा तो गुलाम रसूल दहलीज लांघ कर बाहर निकल आया । उसके हाथ का बैग अपने हाथ में लेते हुए वह बोला –
”बड़े मास्टर जी ने बताया था। मैं शाम तक इंतजार करता रहा फिर लगा शायद आप कल सुबह आएंगे।”
गुलाम रसूल बाहर रास्ते पर चलने लगा, तो उसने भी दर्जी को धन्यवाद देकर विदा ली और गुलाम रसूल के पीछे-पीछे चल दिया। इस बार ज्यादा नहीं चलना पड़ा। स्कूल की छोटी सी इमारत पास ही थी । वहाँ एक कमरे में पहले से ही बान की चारपाई डाल दी गई थी। बल्ब की मद्धम रौशनी में आंखों को अभ्यस्त होने में समय लगा फिर सामने की दीवार पर बना ब्लैक बोर्ड, जमीन पर बिछी हुई दरी, सामने रखी गई कुर्सी, मेज और मेज पर रखा हुआ पीतल का बड़ा सा घण्टा साफ दिखलाई देने लगा।
”भाई गुलाम रसूल, कुछ खाने को मिलेगा क्या?” गंतव्य पर पहुँचने के बाद उपजी निश्चिंतता से उसके भीतर दबा हुआ भूख का अहसास उभर आया था।
”बस, कुछ देर रुकिए, पुलाव बनाता हूँ।” कहता हुआ गुलाम रसूल कमरे से बाहर निकल गया।
शहर से सैकड़ों मील दूर, किसी छोटे से पहाड़ी गांव में, अनजान लोगों के बीच, उसके जीवन की ये पहली रात थी। वह यहाँ की उदासी और सन्नाटे से थोड़ा सहम गया था और झिझक रहा था, पर गुलाम रसूल तत्पर था।
शिक्षा विभाग की मक्कारी के बावजूद वह नौकरी पर पहुँच गया था – इसकी उसे खुशी थी। विभाग द्वारा भेजे गए नियुक्ति पत्र के लिफाफे पर टिकट तो रजिस्ट्री डाक के थे पर उसे भेजा साधारण डाक से गया था। शायद कोई चाहता था कि यह पत्र खो जाए अथवा देर से पहुँचे, इस कारण नौकरी पर दस दिन के भीतर पहुँचने की शर्त पूरी न की जा सके और किसी दूसरे को यह नौकरी दिला दी जाए। पर ठीक आठवें दिन दोपहर को उसे यह पत्र मिल गया था। नौंवे दिन की उस अंधेरी-काली रात को भटकते-भटकते ही सही, पर वह सही जगह पहुँच गया था।
….. और आज दसवें दिन की सुबह स्कूल के बरामदे में बैठ कर, गुलाम रसूल के हाथों की बनी हुई चाय पीते हुए वह सोच रहा था कि कल रात बस से उतरने के बाद जो परिस्थितियां बनी थीं- वह सच थीं या किसी सपने की भटकन थी। अगर वह कुछ और देर से पहँचा होता और दर्जी भी सो चुका होता, तो क्या होता? वह अपने विचारों पर हँसा और दूर तक फैले हुए आम के बाग, घाटी और उसके पीछे उभरते हुए पहाड़ों को मुग्ध भाव से निहारने लगा।
कल रात के सन्नाटे से भरा हुआ यह पहाड़ी गांव इस समय धीमी-धीमी हलचल से भरने लगा था। दूर-दूर बने हुए मकानों के बीच में कहीं फलदार पेड़ों के बाग थे, तो कहीं ऊँची-ऊँची मक्की से खेत भरे हुए थे। पेड़ों के बीच से चौड़ा कच्चा रास्ता गुजर रहा था । उस पर इस समय देसी गायों के झुंड चल रहे थे । उनके गले में पड़ी हुई घंटियां बज रही थीं। पीछे-पीछे चलता हुआ चरवाहा हाँक लगा-लगा कर उन्हें बिखरने और इधर-उधर मुँह मारने से रोक रहा था। पेड़ों के सघन झुंड के कारण यहाँ से रात वाले दर्जी का घर दिखलाई नहीं दे रहा था, पर दूसरे घरों से उठते हुए धुएं की तरह ही धुएं की एक पतली सी लकीर, उस दिशा से भी उठ रही थी। दूर ऊँचाई पर बने हुए घर छोटे-छोटे खिलौनों जैसे लुभावने और आकर्षक लग रहे थे। पहली नौकरी के रोमांच और इस आकर्षक परिवेश ने उसे खुशी से भर दिया।
0 0 0
स्कूल के ठीक सामने एक बड़ा तालाब था । वह सूख चुका था और अब बच्चों के लिए खेल के मैदान का काम करता था। इसी तालाब के दूसरी तरफ की खाली ज़मीन पर गुलाम रसूल का छोटा सा मिट्टी की दीवारों वाला कच्चा कमरा था । इसे गुलाम रसूल की दुकान के नाम से जाना जाता था। इस दुकान में बच्चों को लुभाने के लिए मर्तबानों में भरी हुई रंग बिरंगी गोलियां, बिस्कुट और रस-बंद के अलावा बेसन के नमकीन सेव और गुड़ की सेव के मर्तबान भी थे। एक तरफ तख्तियों, कापी और पैंसिलों को सजाया गया था। एक छोटी सी मेज पर स्टोव रख कर स्कूल के मास्टरों के लिए चाय का प्रबंध भी किया गया था। इसी कमरे के एक कोने में गुलाम रसूल की चारपाई भी बिछी हुई थी।

नई नौकरी के उत्साह के बावजूद कुछ ही दिन में उसे उदासी घेरने लगी थी। पहाड़-पहाड़ और पहाड़। पहाड़ के पीछे पहाड़, उसके भी पीछे पहाड़ और सबसे पीछे बर्फ से ढके श्वेत-धवल पहाड़ों की एक और श्रृंखला । बर्फ से टकरा कर जब सूरज की किरणें लौटतीं तो चौंध पैदा कर देतीं। उसे लगता कि इन पहाड़ों के उस पार की दुनिया खो चुकी है और अब उसे ढूंढ पाना उसके लिए कठिन हो गया है। भीड़ से भरी हुई हलचल से अलग इस गहरे सन्नाटे से भरे एकांत का अवसाद उसे ग्रसने लगा था। स्कूल चलने तक तो रौनक रहती और लगता कि जिंदगी धड़क रही है, फिर अचानक सारे दृश्य जड़ हो जाते। रमणीक होते हुए भी स्पंदनहीन। लगता जैसे जिंदगी ही रुक गई है। ऐसे में उसका एक ही सहारा होता- गुलाम रसूल।
पैंतीस-अड़तीस साल का गुलाम रसूल इस स्कूल का कुछ न होते हुए भी सब कुछ था। स्कूल की ‘आया’ तो केवल नाम मात्र को आती और फिर जल्दी ही चली भी जाती। इसके एवज में वह हैड मास्टर साहब को घर का बना हुआ आम, पापड़, बड़ियां और आचार देती जिसका व्यापार वह गांव की पाँच-सात दुकानों वाले बाजार में किया करती थी।
स्कूल की झाड़-पौंछ, साफ-सफाई, धुलाई-पुताई से लेकर घंटी बजाने, मास्टरों को चाय पिलाने, पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी को स्कूल में झंडियां लगाने और झंडा फहराने के लिए बांस गाड़ने से लेकर, झंडे में फूल बांधने तक का सारा काम गुलाम रसूल ही करता था। झंडा फहराने के बाद वह पूरे मनोयोग से राष्ट्रगान गाता और फिर मास्टरों के लिए चाय सजाने के बाद, बच्चों को लड्डू बांटने की ड्यूटी भी वही निभाता। उत्सव के ऐसे अवसरों पर जब वह अपनी पेशावरी पोशाक और अमृतसरी जूतियाँ पहनता तो उसका व्यक्तित्व एकदम निखर जाता। तहमत-कुर्ते में सदा अस्त व्यस्त सा दिखने वाला गुलाम रसूल उस दिन किसी बडे खानदान का चश्मोचिरांग लगता। अपनी इन्हीं सब सेवाओं के एवज में ही गुलाम रसूल को स्कूल की हद में दुकान करने और रहने की अनुमति मिली हुई थी – जो लाख कोशिश के बाद भी किसी और को नहीं दी जाती थी।
गुलाम रसूल को अपने घर पहुँचने में आधे घंटे के बस के सफर के अलावा लगभग इतने ही समय की पहाड़ी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती थी। पैदल रास्ता उसके लिए मुश्किल नहीं था, पर रोज आने जाने में लगने वाले बस के किराये का जोड़-घटाव उसके पैर बांध देता। वैसे भी, इस गांव से होकर दो ही बसें निकलती थीं और उनके समय के साथ ताल-मेल बिठाने में गुलाम रसूल के कई काम छूट सकते थे।
इतवार के दिन गुलाम रसूल का गोश्त का कारोबार चलता। शनिवार की शाम को स्कूल बंद होने के बाद वह गांव के घरों मे घूम-घूम कर गोश्त की जरूरत मालूम कर लेता और फिर इतवार की सुबह किसी बकरे को इस नश्वर संसार से मुक्ति दिलाकर, उसका गोश्त घर-घर पहुँचाता। जब पहली बार गुलाम रसूल उसके लिए ‘दोधी’ बनाकर लाया, तो वह समझ नहीं पाया था कि बकरे के जिस्म का यह कौन सा हिस्सा है जो इतना नर्म और स्वादिष्ट है।
”मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई चीज है। ऐसा गोश्त तो मैंने पहले कभी नहीं खाया।” उसने हैरान होकर गुलाम रसूल से कहा था।
तब गुलाम रसूल ने बताया था कि किस तरह बकरे की एक आंत में उसका खून भरकर, उस आंत के दोनों सिराें को बांध दिया जाता है। फिर उस आंत को खौलते पानी में डाला और उबाला जाता है। कुछ देर बार खून जमकर बेहद नर्म और लज् ाीज् ा गोश्त में तब्दील हो जाता है।
”यहां पहाड़ के राजपूत जब देवता को बकरा चढ़ाते हैं तो देवता को इसी का परशाद लगाते हैं।” गुलाम रसूल ने बताया था ।
स्कूल के तीन मास्टरों में एक वही था जो बाहर से नौकरी करने आया था। बाकी दोनों आस-पास के गांव से आते थे और स्कूल खत्म होने के बाद लौट जाते थे। हैडमास्टर तो इसी गांव के थे। उसकी भी धीरे-धीरे गांव में पहचान हो गई थी, पर उसका ज्यादातर समय गुलाम रसूल के साथ ही बीतता था। ऊपर से मस्त और सख्त जान दिखने वाला गुलाम रसूल अपनी अंधी बेटी को लेकर बहुत संवेदनशील था। अभी वह छोटी थी पर गुलाम रसूल को उसके निकाह की चिंता सताने लगी थी। भला उससे कौन निकाह करेगा- वह यही सोच-सोच कर परेशान रहता। इसीलिए वह ज्यादा से ज्यादा रुपया इकट्ठा कर लेना चाहता था जिससे किसी गरीब लड़के के लिए रोजगार का बंदोबस्त करके उसे निकाह के लिए मनाया जा सके।
रक्षाबंधन की आहट के साथ ही गांव में पतंगबाजी को लेकर दीवानगी का आलम हो जाता। छोटे बच्चों से लेकर किशोर, अधेड़ और उम्रदराज लोग तक इस दीवानगी में शामिल रहते। यह हाल सिर्फ इसी गांव का नहीं, आस-पास के गाँवों का भी था। ऐसे में महीने भर के लिए गुलाम रसूल का नया कारोबार शुरु हो जाता।
तालाब के चारों कोनों पर बांस गाड़ कर उन पर ‘सद्दी’लपेटी जाती। फिर टीन के डिब्बे में मैदा, साबूदाना, अंडा और सरेस का घोल उबाला जाता। उसमें डोर को दिए जाने वाला मनपसंद रंग डाला जाता और फिर बल्ब के कांच को पीस कर बनाए गए बारीक चूरे को मिलाया जाता। सरेस उबलता तो सारा वातावरण अरूचिकर गंध से गंधिया जाता। पर ये दिन बच्चों और बड़ों के लिए भी कौतूहल का दिन होता। गुलाम रसूल मांजा सूत रहा है- इसी खबर के साथ उत्साहित बच्चे और बड़े, सुतते हुए मांझे को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते। आने जाने वालों का ये मेला शाम तक लगा रहता। तेज धूप में जब मांझा सूख जाता, तो उसके गोले बनाए जाते। उसे चरखियों पर लपेटा जाता । यह प्रक्रिया पूरी होते न होते खरीददारों की आवाजाही शुरु हो जाती।
गुलाम रसूल अपनी पतंगों में चमकीले कागज के चांद-तारे चिपकाता था। इसलिए आसमान में उड़ती हुई पतंगों में गुलाम रसूल की पतंगें अलग ही पहचानी जातीं। गुलाम रसूल के मांझे और ‘डग्गों’ की धूम गांव की हदों से बाहर तक थी। लोग पेशगी देकर भी उसका सूता हुआ मांझा और पतंग खरीद लेना चाहते थे। पर ये कारोबार बामुश्किल महीना भर चलता। इसीलिए उसकी साल भर की उम्मीद स्कूल पर ही टिकी रहती।
गांव से चार कोस के फासले पर किसी देवता की जगह थी जहाँ हर साल एक बडा मेला लगता था। इस देवता की मान्यता सूबे से बाहर तक थी । मेले के दिनों में हजारों लोग यहाँ जुटते। साल भर सन्नाटे में डूबी रहने वाली सड़कें लोगों को ढो कर लाते-ले जाते हुए टै्रक्टर, ट्रालियों और मोटर लारियों के शोर से भर जातीं। इस मेले में एक बड़ा बाजार भी सजता । नट, मदारी और कई दूसरे करतब दिखाने वाले कलाकार भी जुटते। यहाँ एक बड़े दंगल का भी आयोजन होता । इसमें आस-पास के पहलवानों के अलावा दूर दराज के पहलवान भी आते। आस-पास के पहलवान भी इसमें शिरकत करते। ये आयोजन इसलिए भी आकर्षण का केन्द्र था क्योंकि इतनी बड़ी इनामी राशि का और कोई दंगल सूबे में नहीं होता था।
गुलाम रसूल ने पहले साल जब उसे ‘छिंज’ देखने का न्योता दिया था, तो वह बिना इस शब्द का अर्थ समझे हुए, महज समय बिताने की गरज से उसके साथ चल दिया था। दंगल के आयोजन स्थल पर गुलाम रसूल की पूछ थी। तभी उसे पता चला था कि पाकिस्तान से पहलवान बुलाने की जिम्मेदारी गुलाम रसूल निभाता है। क्वेटा में गुलाम रसूल का फुफूजात भाई अखाड़ा चलाता था। उसी की मार्फत पाकिस्तान से पहलवान आते। पहलवान आते तो दो-चार चेले भी आते । गुलाम रसूल का भाई भी आता। खर्च तो आयोजन समिति ही उठाती पर उनकी आव-भगत और खान-पान का प्रबंध करने की जिम्मेदारी गुलाम रसूल की होती। गुलाम रसूल के लिए वे दिन रौनकों और तोहफों के दिन होते। गुलाम रसूल रोज पठानी सूट और अमृतसरी जूतियों में यहाँ-वहाँ भागता हुआ गोश्त जुटाता । दूध-बादाम का इन्तजाम करता। तमाम दूसरी खातिरदारियों में लगा रहता।
पूरे साल में यही वे आठ दस दिन होते थे, जब गुलाम रसूल की दुकान बंद रहती या फिर स्कूल की ‘आया’ दुकान खोलकर जरूरत निबटाती। आया पर ये आठ-दस दिन भारी बीतते।
”तुम तो ‘छिंज’ दिखाने को कह रहे थे।” उसने लौटते हुए गुलाम रसूल को याद करवाया था।
गुलाम रसूल ठहाका लगा कर हँस पड़ा था
”कुश्ती देखी न आपने, यहां इसी को ‘छिंज’ कहते हैं।”
पाकिस्तान से आते हुए भाई तोहफे लाता था और जाते हुए पहलवान गुलाम रसूल को कुछ न कुछ दे जाते थे। जिस साल पाकिस्तान का पहलवान दंगल जीतता, उस साल गुलाम रसूल को अच्छा इनाम मिलता । तब अक्सर गुलाम रसूल उससे कहता –
”बस कुछ और पैसा हो जाए तो सोचता हूँ कि सबा की ऑंखों का इलाज करवा लूं। सुना है अब तो आंखें बदल भी देते हैं।”
शायद वह सोचने लगा था कि निकाह पर ज्यादा खर्च करने से बेहतर है कि बेटी की ऑंखों के इलाज पर खर्च कर दिया जाए जिससे निकाह में होने वाली दिक्कत को टाला जा सके। फिर एक साल सर्दियों की छुट्टियों में उसने बेटी की ऑंखों का आपरेशन करवा भी दिया था। पर वह हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। पैंसठ साल के एक उम्रदराज आदमी और उसकी बेटी, दोनों का ‘कोरनिया’ एक साथ बदला गया था। उस उम्रदराज् ा आदमी की ऑंख में रौशनी लौट आई थी, पर उसकी बेटी की आंख में रौशनी नहीं उतरी थी। मायूस गुलाम रसूल सिर धुन कर रह गया था।
000

……. और ठीक छत्तीस साल बाद आज, वह उसी जगह फिर उतरा था, जहाँ छत्तीस साल पहले सन्नाटे से भरी हुए एक बेहद काली रात हमेशा उसके अनुभवों में शामिल रही थी। पर आज परिस्थितियाँ भिन्न थीं। उसकी आगवानी के लिए लोग पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने नजरें घुमा कर जगह का जायजा लिया। पक्के मकानों की आमद से सिलसिलेवार कतार में ख़डे रहने वालों पेड़ों का सिलसिला अब टूट चुका था। कुछ दूर दिखलाई देता वो मकान अगर दर्जी का ही था, तो वह अपनी ही जगह पर था। पर वह भी अब पक्का हो चुका था।
चलते-चलते अचानक उसे अपने स्वागत में आए लोगों में किसी की कमी खली, तो उसने बेसाख्ता पूछ लिया
”ग़ुलाम रसूल नहीं आया?”
युवा अध्यापकों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर कुछ झिझक कर पूछा ।
”कौन ग़ुलाम रसूल, सर!”
उसके जीवन का यह एक अप्रत्याशित सुखद संयोग था कि उसने जिस स्कूल से नौकरी आरम्भ की थी, आज उसी का मुखिया बनकर आया था । यह भी लगभग तय था कि अब यहीं से उसे सेवानिवृत्त भी होना था। वह उन युवा अध्यापकों के प्रश्न पर चौंका था – ”कौन गुलाम रसूल सर?”
स्कूल के सामने का तालाब भर कर सपाट मैदान बना दिया गया था। उसमें कतारबध्द खड़े हुए बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पी.टी मास्टर ने उसके पहुँचते ही ड्रम-ड्रिल शुरु करवा दी थी। स्कूल के बारहवीं तक हो जाने के बाद बनी हुई दो मंजिला इमारत शानदार दिखती थी। उसके सामने के मैदान पर अब हदबंदी करवा दी गई थी। हदबंदी के उस पार भी अब गुलाम रसूल नहीं था, न ही उसकी एक कमरे वाली कच्ची दुकान कहीं दिखलाई दे रही थी। अलबत्ता, कुछ नए उभरे हुए मकानों की छतें जरूर सामने थीं जिन्होंने कद्दावर सायेदार पेड़ों के साम्राज्य
को खंडित कर दिया था। स्कूल में लगी पानी की टंकी बता रही थी कि गांव में नल आ गए हैं।
”तुम पानी कहां से लाते हो?” पानी ढोते हुए गुलाम रसूल को देख कर तब उसने पूछा था -”बांई से।”
”बांई – वो क्या होता है?” उसने हैरानी से पूछा था
”शाम को चलना- दिखलाऊंगा।” हँसा था गुलाम रसूल।
शाम को गुलाम रसूल उसे साथ की पहाड़ों पर ‘बांई’ दिखने ले गया था। छोटी सी तलैया थी। वहाँ पहाड़ के भीतर से निकलता पानी छल-छला रहा था। ‘बांई’ के चारों तरफ आम के कद्दावर पेड़ कुछ इस तरह लगे हुए थे मानों ‘बांई’ को साया देने के लिए ही लगाए गए हों। कुछ दूरी पर पत्थरों की छोटी से दीवार खड़ी करके स्नानघर बना लिया गया था। ‘बांई’ के चारों तरफ पक्के चबूतरे बने हुए थे। अद्भुत शांति और रमणीयता थी इस जगह पर। स्कूल के बच्चों के पीने के लिए भी गुलाम रसूल यहीं से पानी ढोता था। सिर्फ स्कूल ही नहीं, तब पूरा गांव इसी छोटी सी तलैया से पानी भरता।
पर गुलाम रसूल है कहाँ? उसने जानना चाहा। सभी अध्यापक नए थे । गुलाम रसूल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दफ्तर के बड़े बाबू जो एक पुराना चेहरा हो सकते थे- आज छुटटी पर थे।
ये सच था कि गाँव बदल चुका था और अब वहाँ आबादी, फैशन और बाजार भी पहुँच चुके थे। बस के फेरे भी बढ़ गए थे । किसी बस के रुकते ही ‘कौन आया’ देखने के लिए उत्सुक चेहरे अब घरों से नहीं झांकते थे। पर फिर भी ये एक गाँव ही था। वाशिंगटन डी.सी. नहीं कि किसी इंसान को न ढूंढा जा सके। शायद इसीलिए दोपहर ढलते न ढलते उसने गुलाम रसूल को ढूंढ ही लिया था, और इस समय, गाँव से लगभग दो कि.मी. बाहर नरवाह मोड़ पर, जहां आती-जाती बसें सवारी उतारती-चढ़ातीं और पांच-सात मिनट रुका करती थीं, वहीं गुलाम रसूल के बदरंग ढाबे में बिछी एक बैंच पर बैठा हुआ और उसकी बातें सुनता हुआ, वह बेदिली से धीरे-धीरे चाय सुड़क रहा था।
गुलाम रसूल के चेहरे की बुढ़ियाती तराशों के बावजूद उसने जितनी सरलता से गुलाम रसूल को पहचान लिया था, उतनी सरलता से गुलाम रसूल उसे नहीं पहचान पाया था। कई परतें हटाने के बाद भी गुलाम रसूल के जेहन में उसके साथ बिताए दिनों का अक्स बहुत साफ होकर नहीं उभरा था। शायद यह स्वभाविक भी था। उस स्कूल के लिए गुलाम रसूल अकेला था, पर गुलाम रसूल के सामने उस स्कूल में सैकड़ों मास्टर आए और गए थे और उसने सबकी आवभगत समान निष्ठा से की थी। शायद इसीलिए वह मास्टरों के चेहरे जेहन में अलग-अलग सहेज कर नहीं रख सका था। फिर भी वह खुश था कि आज कोई मास्टर उसकी खैर खबर लेने तो आया है। पर गुलाम रसूल के स्वागत में वह गर्मजोशी नहीं थी जिसकी उम्मीद उसने की थी।
गुलाम रसूल ने अपने खिलाफ रचे गए षड़यंत्र की जो कहानी सुनाई थी- वह आततायियों की व्यूह रचना जैसी थी।
शुरुआत हुई थी उस साल दंगल में पाकिस्तानी पहलवान के जीतने से। पहले तो दंगल वाली जगह ही मारपीट हो गई थी। क्योंकि पाकिस्तानी पहलवानों का जत्था गुलाम रसूल की मार्फत ही आता था, इसलिए गुलाम रसूल द्वारा उन्हें बचाना और उनका पक्ष लेना स्वाभाविक था। पर इसका असर ये हुआ कि रात को गुलाम रसूल की दुकान जला दी गई। गुलाम रसूल ने इसे झगड़े की ही प्रतिक्रिया समझ कर लानत मलानत करते हुए अगले दिन साफ-सफाई की और दुकान को फिर से सजाने की कोशिश करने लगा, तभी उसे हैड मास्टर और सरपंच का हुक्मनामा सुनाया गया जिसमें स्कूल की जमीन की हदबंदी की बात थी और ये साफ कर दिया गया था कि गुलाम रसूल अब वहाँ दुकान नहीं बना सकता।
पहली बार गुलाम रसूल को अपने हकहकूक पता चले थे, वरना तो वह इस स्कूल को अपना ही समझ बैठा था। गुलाम रसूल गिड़गिड़या, मिन्नतें कीं पर हालात नहीं बदले। जल्दी ही दूसरी मार हुई गुलाम रसूल के गोश्त व्यापार पर। बात फैली कि गुलाम रसूल बकरे के नाम पर पता नहीं क्या काटता है, लिहाजा उससे गोश्त की खरीद बंद कर दी जाए। इसके बावजूद गुलाम रसूल भरभरा कर गिरने से इस उम्मीद पर बचा रहा कि रक्षाबंधन पास है और वह मांझे और पंतग से कुछ कमा कर कोई नया काम शुरू करेगा। पर उसके द्वारा पतंग पर चांद सितारे चिपकाना गुनाह हो गया। उसने चांद सितारे चिपकाना बंद भी कर दिया, फिर भी ग्राहक नहीं आए। गुलाम रसूल अपनी वर्षों पुरानी पहचान की दुहाई देता हुआ इस छोटे से गांव के एक-एक आदमी से मिला। वह नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि कोई भी पसीजने को तैयार ही नहीं है।
”पर आज समझ गया हूँ मास्टर जी।” गुलाम रसूल ने एक आहत हँसी हँसते हुए कहा ”और सोचता हूँ कि बेहतर होता कि अब्बा यहीं बसे रहने की जिद छोड़ कर सरहद पार चले गए होते। उस हाल में पाकिस्तानपरस्त कहलाने से पाकिस्तानी हो जाना कम तकलीफदेह होता।”
”नहीं गुलाम रसूल। ये सब चीजें वक्ती होती हैं। फिर धीरे-धीरे हालात सुधर जाते हैं। ये तुम्हारा अपना मुल्क है- किसी और से ज्यादा तुम्हारा।” उसने बात को सम्भालने की कोशिश की।
”हाँ साहब! पहले मैं भी यही समझता था।” गुलाम रसूल की ऑंखों में हिकारत और हंसी में जो व्यंग्य था, उससे बचने के लिए उसने आंखें घुमा लीं और बात बदलते हुए पूछा।
”तुम्हारी बेटी कैसी है?”
”ठीक है मास्टर साहब। एक खुदा का बंदा राजी हो गया था निकाह के लिए। निकाह करवाकर उसे साथ ही रख लिया। अब तो अल्लाह के ंफज् ाल से उसके दो जवान होते बेटे भी हैं।”
अचानक उसने महसूस किया कि गुलाम रसूल का स्वर बदल गया है। कुछ देर पहले की तल्ख बातों से उपजी खुश्की अब उसकी आवाज में नहीं थी। उसकी आवाज में एक पिता के स्नेह की नमी उतर आई थी। उसने भी राहत की सांस ली और खोके की खिड़की से बाहर घाटी को देखने लगा। दूर पहाड़ से धुंध का छोटा सा टुकड़ा उठकर फैलने लगा था और अब
धीरे-धीरे पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। कुछ देर पहले साफ-साफ दिखलाई देते बेल-बूटे अब इस धुंध के पीछे छुपते जा रहे थे। मौसम की इस रूमानियत ने अचानक उसे अपनी बीती हुई उम्र में पहुँचा दिया था। वह बेसाख्ता बोल पड़ा था।
”वाह! क्या नजारा दिखलाई देता है तुम्हारे खोके से।”
”नजारों का नहीं, इन्सानों का अच्छा होना जरूरी है मास्टर साहब।” गुलाम रसूल ने धीमे स्वर में कहा, तो उसके भीतर कसकती फांस से वह छिल गया।
गुलाम रसूल से विदा लेकर चला तो वह सोच रहा था कि क्यों न गुलाम रसूल को उसकी पुरानी जगह बसाने की एक कोशिश की जाए। पर क्या वो इस कोशिश में सफल हो पाएगा ? क्या गुलाम रसूल का खोया हुआ विश्वास भी लौट पाएगा?
गांव की हद में दाखिल होते हुए उसने देखा । इंसानी रिश्तों के परखचों पर बुद्धू बक्सों के एंटिने तने हुए खड़े हैं, जिनकी अबूझी तपिश से इन्सान धीरे-धीरे पिघलता जा रहा है। महज बिना रीढ़ का लिजलिजा गोश्त बनकर बहता हुआ ।
जितेन ठाकुर हिन्दी व डोगरी कहानी के खूब परिचित नाम हैं । चार उपन्यास, सात कहानी संग्रह, एक कविता संग्रह हिन्दी में प्रकाशित है । एक कहानी संग्रह डोगरी में प्रकाशित । जर्मन भाषा के अलावा देश की अनेक भाषाओं में इनकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं । स्थायी रूप से देहरादून में रहते हैं । सौज ‘अकार’
संपर्क : मो. : 9410925219 ईमेल : jitenthakurddn@gmail.com