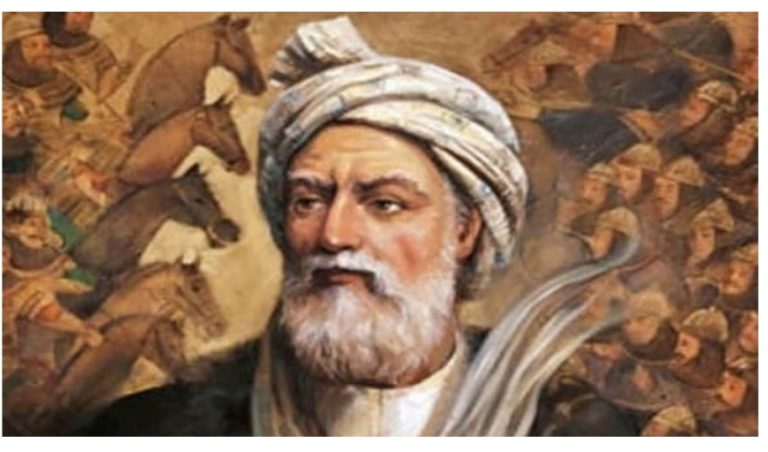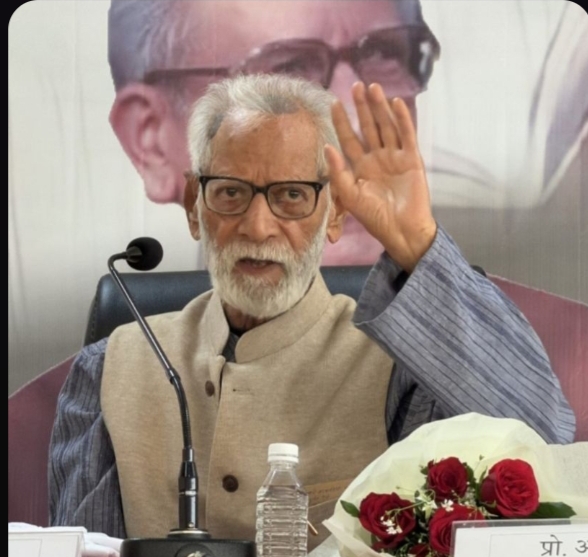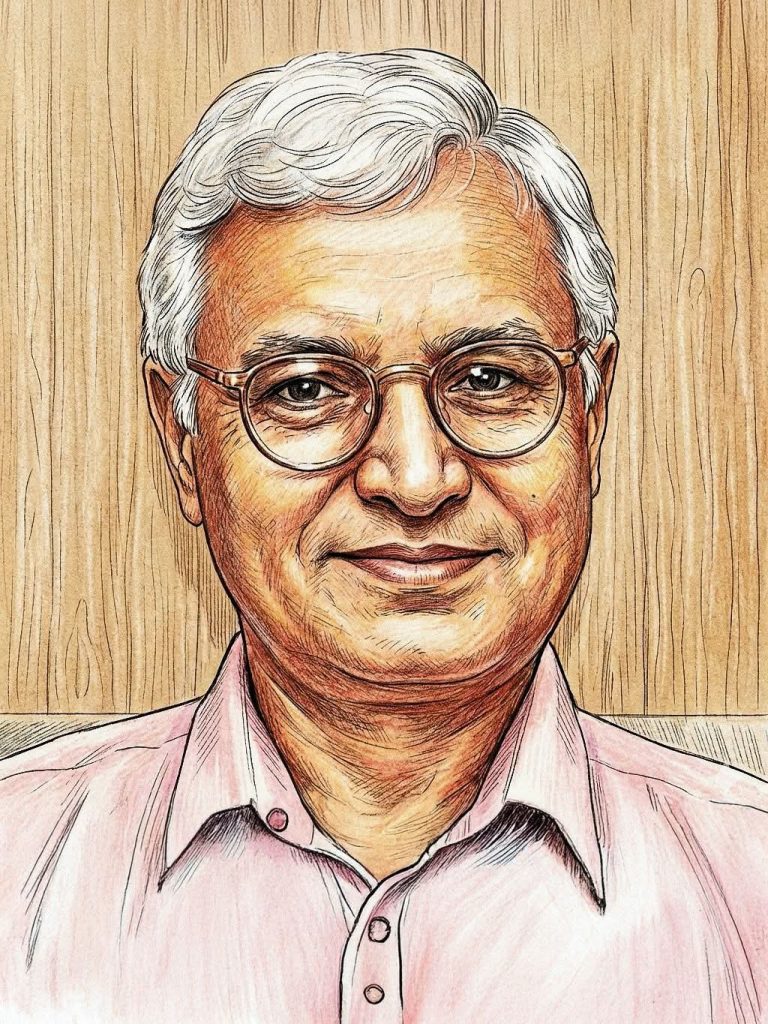कोविड के बाद की दुनिया में लोकलुभावन नेताओं ने महामारी के बहाने अपनी शक्तियों को संकेंद्रित और अपनी व्यक्तिगत नौकरशाही प्रणाली को मजबूत कर लिया है। भारतीय लोकतंत्र के गिरते स्तर पर हो रही बहस पर दो पश्चिमी विशेषज्ञ समूहों की तरफ़ से जारी हालिया रिपोर्टों में प्रकाश डाला गया है, अजीत सिंह इस लेख में लोकतंत्र में तेज़ी से आ रही इस गिरावट के पीछे के कारणों के बारे में लिखते हैं।
फ़्रांस के लोगों के लिए इतिहास कभी आसान नहीं रहा है। बास्तिल के पतन के 232 साल बाद भी फ़्रांसीसी क्रांति को लेकर पीड़ा और ख़ुशी दोनों ही तरह का जुनून है। 1789 की इस महान क्रांति ने स्वतंत्रता के सिद्धांत की उत्पत्ति और संवैधानिक क़ानून की अवधारणा को जन्म दिया था। गणतंत्र के लिए वह संघर्ष हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि रचनात्मक विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हर क़ीमत पर बचाये रखना चाहिए।
कोविड के बाद की दुनिया में इस महामारी का इस्तेमाल आगे के लिए ताक़त जुटाने और एक व्यक्तिगत नौकरशाही प्रणाली को सशक्त बनाते हुए मजबूत लोकलुभावन नेता विजेता के रूप में उभरे हैं। भारत जैसे लोकतंत्र इस घटना के अपवाद नहीं हैं; हालांकि, हमारी चुनाव प्रक्रिया अविकल और पारदर्शी हो सकती है (असम और पश्चिम बंगाल में हालिया घटनाओं से इसके कलंकित होने की एक धारणा ज़रूर बनी है), यह तो उन कई मानदंडों में से महज़ एक मानदंड है, जिसका इस्तेमाल इस बात को निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई देश एक कार्यशील और उदार लोकतंत्र रह गया है या नहीं।
हाल ही में व्यापक रूप से चर्चित नवीनतम फ़्रीडम हाउस रिपोर्ट में भारत के दर्जे को ‘आज़ाद’ से ‘आंशिक रूप से आज़ाद’ देश के तौर पर घटा दिया गया है। इसके पीछे की जो कुछ वजह रही है, उस पर आत्मनिरीक्षण करने के बजाय भारत की केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को “भ्रामक, ग़लत और अनुपयुक्त” क़रार देते हुए कड़ी आलोचना की है।
हालांकि, सवाल पैदा होता है कि हमें ख़ुद की तुलना उस देश से ही आख़िर क्यों करनी चाहिए, जिसे महज़ 9 अंक मिले हैं और उसे इसी रिपोर्ट में ‘आज़ाद नहीं’ वाली श्रेणी में रखा गया है और अपने नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता की अवहेलना को लेकर वह देश बदनाम रहा है ?
यहां उन शुरुआती कारणों में से कुछ कारणों का ज़िक़्र किया जा रहा है जो भारतीय लोकतंत्र में आयी गिरावट के लिए ज़िम्मेदार हैं:
कमज़ोर संस्थायें
हालांकि, हमारे संविधान में नियंत्रण और संतुलन का प्रावधान तो है, लेकिन इसकी एक स्पष्ट सीमा रेखा कुछ हद तक नहीं है। इसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए केंद्र सरकार ने न्यायपालिका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय सूचना आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को क़ाबू करने के लिए अपनी ताक़त का दुरुपयोग किया है।यहां कुछ संस्थाओं का ही ज़िक़्र किया गया है, ऐसी संस्थाओं का फ़ेहरिस्त काफ़ी लम्बी है।
कुछ सबक तो उस अमरीका से भी लिए जा सकते हैं जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीनेट, फ़ेडरल कोर्ट और फ़ेडरल रिज़र्व जैसे स्वतंत्र संस्थानों को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्हें इसमें निराशा ही हाथ लगी। उन्हें कभी भी अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पायी। भारत में संवैधानिक निकायों से उसी तरह से मज़बूती के साथ खड़े रहने और लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद रही है, लेकिन दुख की बात है कि अब तक ऐसा हो नहीं पाया है।
असहमित को दबाने के लिए प्रतिगामी क़ानूनों का इस्तेमाल
सरकार की नीतियों और इसके कामकाज के तरीक़े को लेकर आलोचनात्मक विचार रखने वाले लोगों को ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A (‘राजद्रोह क़ानून’ के रूप में ज़्यादा जाना जाने वाला क़ानून) के इस्तेमाल के ज़रिये लगातार चुप कराया जाता है।
इस साल की शुरुआत में जलवायु के लिए कार्य करने वाली कार्यकर्ता, दिशा रवि को ज़मानत देते समय दिल्ली की एक अदालत ने टिप्पणी की थी कि “सरकारों के चोट खाये अहंकार को बरकरार रखने के लिए राष्ट्रद्रोह का अपराध नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है”।
मानहानि और देशद्रोह क़ानून के हद से ज़्यादा इस्तेमाल के ज़रिये मीडिया को प्रभावी ढंग से चुप कराना ही वह मुख्य कारण है, जिसके चलते V-DEM इंस्टिट्युट की तरफ़ से प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत को ‘चुनावी निरंकुशता’ वाला देश कहा गया है।
शैक्षणिक और कलात्मक स्वतंत्रता को लेकर असहिष्णुता
पिछले महीने केंद्र सरकार के नियमित और मुखर आलोचक रहे प्रो. प्रताप भानु मेहता ने परोक्ष रूप से बढ़ते राजनीतिक दबाव के चलते अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके इस्तीफ़े के ठीक दो दिन बाद केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रो. अरविंद सुब्रमण्यन ने भी अपना पद छोड़ दिया। कुलपति को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में अब अकादमिक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की जगह नहीं बची है।
पिछले कुछ महीने इस बात के गवाह रहे हैं कि हिंदुत्व और अति-राष्ट्रवादी संगठनों ने किस तरह फ़िल्म निर्देशकों को भी उनके विचारों पर रोक अथवा काट-छांट करने के लिए दबाव बनाया है। कलाकारों की कल्पना और उनकी रचनात्मक स्वतंत्रता पर जानबूझकर किये जा रहे हमले की ऐसी घटनायें चिंताजनक हैं। ये घटनायें दुष्प्रचार और सख़्त क़ानून के ज़रिये धीरे-धीरे अपने आगोश में ले लेने को लेकर हमारे संदेह की ही पुष्टि करती हैं।
न्यूज़ मीडिया का ढोंग रचता गोदी मीडिया
प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसका सबसे अहम कार्य तीन अन्य स्तंभों-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर नज़र रखना है। अफ़सोस की बात है कि भारतीय न्यूज़ मीडिया ने इस मोर्चे पर बुरी तरह निराश किया है। इसके ज़्यादातर घटक खुले तौर पर ऑनलाइन नफ़रत को बढ़ावा देते हैं, सत्तारूढ़ दल के रट्टू तोता बने हुए हैं और राष्ट्रीय टेलीविजन पर ऐसे अप्रासंगिक मुद्दे उठाते रहते हैं, जिनकी सार्वजनिक जीवन में कोई प्रासंगिकता नहीं होती है।
बेहतर गुणवत्ता वाली पत्रकारिता के लिए अब संघर्ष नागरिकों केअहम ज़िम्मेदारी है।
यही मुनासिब समय है कि सनसनीख़ेज़ ख़बरों को परोसने वाले उन मीडिया समूहों का सामूहिक रूप से बहिष्कार किया जाए, जिसमें न तो कोई वस्तुनिष्ठता रह गयी है और न ही इस हद तक चेतना रह गयी है कि वे मीडिया के बुनियादी सिद्धांत का पालन कर पायें। उन्हें इस बात का भी संकेत दिया जाना चाहिए कि उनकी नफ़रत फ़ैलाने की कोशिश उनके ख़ुद के लिए भी लम्बे समय तक फ़ायदेमंद नहीं हो सकती।
बेबूझ और झूठा राष्ट्रवाद
भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1908 में एक मित्र को लिखे पत्र में लिखा था कि “देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकती। मैं बहुमूल्य चीज़ के एवज़ में सस्ती चीज़ नहीं ख़रीदूंगा और अपने जीते जी मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा।”
मौजूदा परिदृश्य में एक राजनैतिक दल, झूठे और ख़ुद के फ़ायदे पहुंचाने वाले जिस तरह के राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर चुनाव-दर-चुनाव जीत रहा है, और ‘विश्वगुरु’ (वस्तुतः ‘विश्व नेता’) बनने का खोखला सपने दिखा रहा है। उससे लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। लोगों को उनकी ज़िंदगी की हक़ीक़त के उलट राजनीतिक दलों की तरफ़ से जो कुछ दिखाया-समझाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए।
हालांकि, जब तक जनसंख्या का एक तबका संविधान के मक़सद के लिए संघर्ष करता रहेगा, तब तक रौशनी की एक किरण मौजूद रहेगी, और हमारे राष्ट्र का भाग्य तबतक पूरी तरह निराशाजनक नहीं लगता है।
उम्मीद है कि “हम, भारत के लोग” अपने राष्ट्र के साथ न्याय करेंगे।
हिटलर की कट्टरता के ख़िलाफ़ मशहूर अमेरिकी कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की 1940 की राजनीतिक कटाक्ष करती फ़िल्म, ’द ग्रेट डिक्टेटर’ आज भी प्रासंगिक है। इस फ़िल्म में उनके आख़िरी भाषण के ये शब्द अब भी हक़ीक़त हैं:
“इस समय हमारे ऊपर जो दुख आन पड़ा है, वह लालच के नतीजे के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल, यह उन लोंगों की कड़वाहट ही है जो प्रगति के रास्ते से डरते हैं। इन लोगों की नफ़रत हार जायेगी और तानाशाह मरेंगे। लोगों से उन्होंने जो ताक़त हासिल की है, वह लोगों के हाथों में फिर से होगी। और क्योंकि ये लोग मरते रहेंगे तब तक आज़ादी जिंदा रहेगी।”
यह वक़्त उन बहुत सारे भारतीयों के लिए एक मुश्किल समय है जो बढ़ती क़ीमतों के साथ-साथ ढहती अर्थव्यवस्था और जाती हुई नौकरी की वजह से कमज़ोर पड़ गये हैं। किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा हमें एक ऐसे राजनेता की ज़रूरत है जो लोगों की चिंताओं पर ध्यान दे, अलग-अलग विचारों को तरज़ीह दे और लिंग, जाति या धार्मिक जुड़ाव से परे होकर तमाम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे।
यह लेख मूल रूप से द लिफ़लेट में प्रकाशित हुआ था। (अजीत सिंह जबलपुर स्थित सेंट अलॉयसियस कॉलेज में छात्र हैं। इनके विचार निजी हैं।) अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें – सौज- न्यूजक्लिक