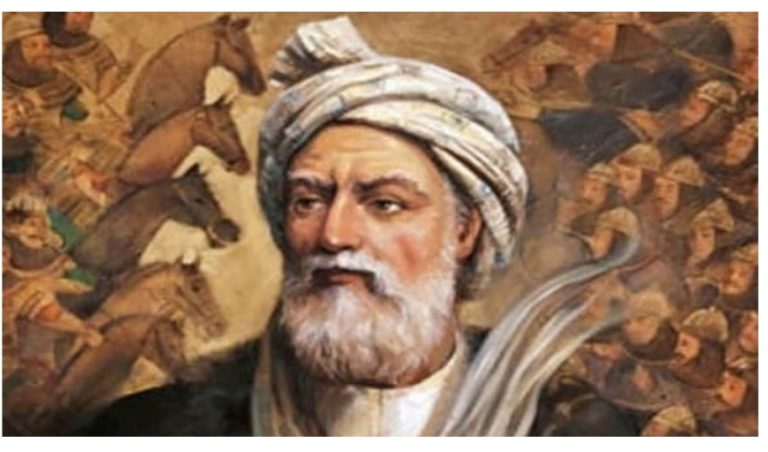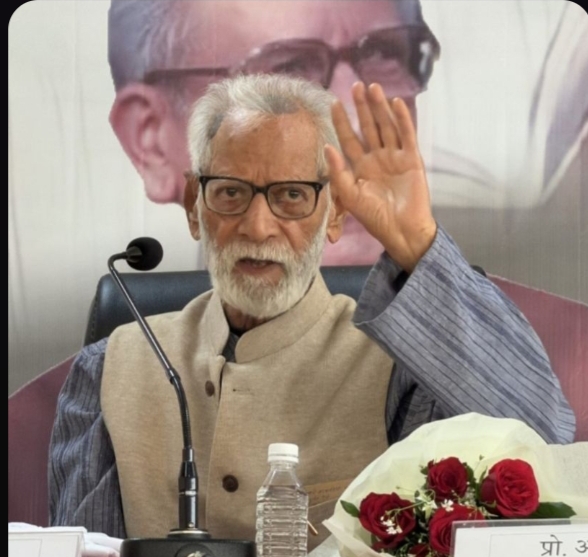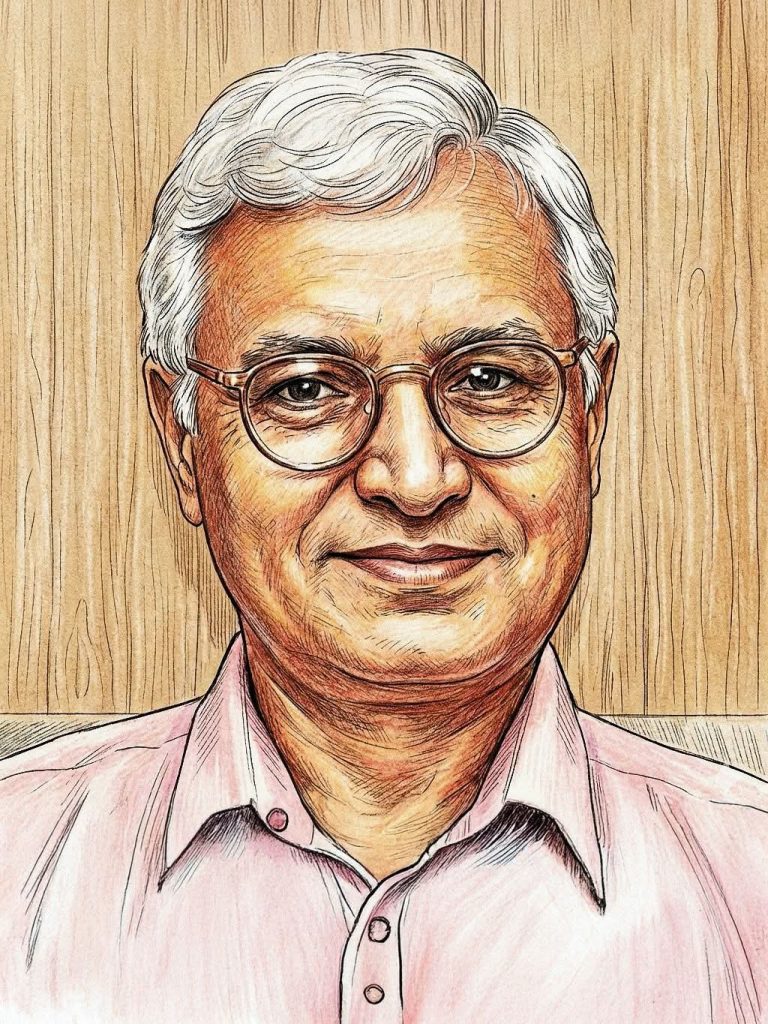महान फिल्मकार बिमल रॉय अपने आप में एक संस्था थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को सलिल चौधरी, ऋषिकेश मुखर्जी, ऋत्विक घटक और गुलज़ार जैसे कई नायाब लोग दिए सन 1953 में आई ‘दो बीघा ज़मीन’ ने दुनिया भर के फ़िल्मकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. इस फिल्म के जरिये पहली बार हिंदुस्तानी सिनेमा में ‘निओ-रिअलिस्म’ की तस्वीर पेश हुई. इतालवी सिनेमा से प्रेरित ‘नियो-रिअलिस्म का नज़दीकी हिंदी रूपांतरण ‘नव-यथार्थवाद’ हो सकता है. इस फिल्म के निर्देशक थे बिमल रॉय जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नया रास्ता दिखाया.
दूसरे विश्व युद्ध में फ़ासीवाद ने इटली के समाज की परतें उधेड़ कर रख दी थीं. मुसोलिनी के डर से जहां अन्य फ़िल्मकार सब हरा-हरा ही दिखा रहे थे तो रॉबर्ट रोसेलिनी, वित्तोरियो डी सिका और विस्कोन्ती जैसे कुछ फिल्मकार भी थे जो समाज में उपजे वर्ग संघर्ष को दिखा रहे थे. ‘नव-यथार्थवाद’, शोषित और शासक के बीच का द्वंद दिखाता है. यही द्वंद मैक्सिम गोर्की के उपन्यास ‘मदर’ या अप्टन सिंक्लैर के ‘जंगल’ में भी दिखता है. भारतीय परिपेक्ष्य में इस संघर्ष को सबसे पहले दिखाती बिमल रॉय की ‘उदेर पाथेय’(1944) ने बंगाली सिनेमा में तूफ़ान ला दिया था. स्वभाव से शांत रहने वाले बिमल रॉय को फ़िल्म पत्रकार बुर्जोर खुर्शीदजी करंजिया ने ‘साइलेंट थंडर’ की उपमा दी थी.
उनकी पुत्री रिंकी भट्टाचार्य की क़िताब ‘बिमल रॉय- अ मैन ऑफ़ साइलेंस’ में वे सारे पहलू हैं जो बिमल दा की ज़िंदगी को छूकर निकले. जैसे बिमल दा ने निर्माता निर्देशक बीएन सरकार की निगहबानी में न्यू थिएटर्स (कोलकाता) से बतौर कैमरामैन अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया था. पीसी बरुआ निर्देशित और केएल सहगल अभिनीत ‘देवदास’ फ़िल्म के वे फोटोग्राफर रहे. 40 के दशक में न्यू थिएटर्स और बंगाली सिनेमा का बिखराव हो रहा था. इस दौरान न्यू थिएटर्स के लिए बनाई गईं उनकी फिल्में जैसे ‘अंजनगढ़’, ‘मंत्रमुग्ध’ और ‘पहला आदमी’ फ्लॉप हो गयीं. ‘उदेर पाथेय’ के हिंदी रीमेक ‘हमराही’ (1945) ने औसत व्यवसाय किया. हां, बिमल रॉय की बतौर डायरेक्टर बहुत तारीफ हुई और इसमें पहली बार रबींन्द्रनाथ टैगोर के ‘जन गण मन’ गीत को लिया गया. अपनी किताब में रिंकी भट्टाचार्य आगे लिखती हैं, ‘मुंबई में ‘पहला आदमी’ के प्रीमियर पर मिली प्रतिक्रिया ने उन्हें और निराश कर दिया था, वो भारी मन से कोलकाता लौट गए.’
अब आगे जो क़िताब में नहीं है, वह यूं है कि क़िस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था. उन दिनों हिंदी सिनेमा पर बंगाली प्रभाव बढ़ रहा था. बिमल दा के अनन्य मित्र हितेन चौधरी ने अभिनेता अशोक कुमार से मिलकर उन्हें बॉम्बे टाकीज़ की एक फ़िल्म 25000 रु बतौर मेहनताना निर्देशन के लिए दिलवा दी. बॉम्बे टाकीज़ की स्थापना देविका रानी के पति हिमांशु रॉय और, संगीतकार मदन मोहन के पिता रायबहादुर चुन्नीलाल ने की थी. बिमल दा ने बॉम्बे टाकीज़ के लिए ‘मां’ (1952) फ़िल्म का निर्देशन किया जो अमेरिकी फ़िल्म ‘ओवर द हिल्स’ से प्रेरित थी. फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई और फिर बिमल दा हमेशा के लिए मुंबई के होकर रह गए. बाद में अशोक कुमार के ही कहने पर उनके प्रोडक्शन हाउस ‘फ़िल्मिस्तान’ के तले उन्होंने ‘परिणीता’ (1953) का निर्देशन किया.
इन फिल्मों की सफलता से हौसला बढ़ा तो उन्होंने ‘बिमल रॉय प्रोडक्शन्स’ की स्थापना कर ‘दो बीघा ज़मीन’ बनायी. इस फ़िल्म के बनने के पीछे अगर कोई शख्स था, तो वे थे, ऋषिकेश मुखर्जी. हुआ यह कि 1952 में मुंबई में अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फ़ेस्टिवल हुआ जिसमें ‘बायसाइकिल थीव्स’ और ‘रोशोमन’ जैसी फिल्मों का मंचन हुआ था. इन फ़िल्मों का ऐसा प्रभाव हुआ कि लौटते वक़्त बिमल दा और अन्य सभी ख़ामोश थे. तभी ऋषिकेश मुखर्जी उनसे बोले कि वे ऐसी फिल्में क्यूं नहीं बनाते. बिमल दा ने कहानी के न होने का अभाव बताया, तो ऋषि दा ने तुरंत कहा कि उनके पास एक कहानी है – ‘रिक्शावाला’. हालांकि यह कहानी महज़ कुछ ही पन्नों की थी. ऋषि दा ने इस पर 24 पन्नों की स्क्रिप्ट तैयार करके बिमल दा को फ़िल्म बनाने के लिए मजबूर कर दिया.
दुसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी वित्तोरियो डी सिका की ‘बायसाइकिल थीव्स’ एक पिता और पुत्र की कहानी है जो अपनी चोरी की गयी साइकिल को खोजने निकले हैं. अगर साइकिल न मिली तो पिता नौकरी नहीं कर पायेगा जिससे परिवार पर संकट आ जाएगा. ‘दो बीघा ज़मीन’ में पिता (बलराज साहनी) अपने बेटे के साथ कोलकाता आकर गांव में दो बीघा ज़मीन को बचाने के लिए साइकिल रिक्शा चलाता है. दोनों ही फिल्मों में ‘पिता’ हार जाते हैं!
बिमल दा की सिनेमाई सोच को समझने के लिए इस फिल्म से जुड़ा एक क़िस्सा जानना ज़रूरी है. बॉम्बे टाकीज़ के मालिक इसके कलाकारों के चयन को लेकर संतुष्ट नहीं थे. उनके मुताबिक़ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बलराज साहनी कुछ ज़्यादा ही गोरे थे और निरूपा रॉय फिल्मों में देवियों का किरदार निभाती थीं. दोनों का ग्रामीण परिवेश में फिट बैठना कुछ अटपटा था. बिमल दा अड़ गए. शायद इसलिए कि बलराज साहनी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे. फ़िल्म भी सर्वहारा की ज़िंदगी पर आधारित थी. लिहाज़ा बिमल दा के मुताबिक़ बलराज किरदार के साथ न्याय करने की कुव्वत रखते थे.
समाजवाद से प्रेरित और सिनेमा से सर्वहारा की आवाज़ उठाने वाले बिमल दा पर कमर्शियल यानी व्यावसायिक फ़िल्में बनाने का ज़बरदस्त दवाब था. उनका कमाल था कि बॉक्स ऑफिस की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए भी वे अपने मनपसंद विषयों पर फिल्म बना लेते थे. ‘नौकरी(1954) और ‘मधुमती’(1958) इसी का नतीजा थीं. ‘मधुमती’ बॉम्बे टाकीज़ की फ़िल्म ‘महल’ (1949) से प्रेरित थी. इसके एडिटर बिमल दा ही थे. ‘पुनर्जन्म’ की अवधारणा पर बनी ‘मधुमती’ हिंदुस्तान के सिनेमा में मील का पत्थर है जिसने हिंदी सिनेमा ही नहीं, हॉलीवुड को भी ‘रीइंकारनेशन ऑफ़ पीटर प्राउड’ बनाने के लिए प्रेरित किया था. आगा हश्र कश्मीरी की कहानी ‘यहूदी की लड़की’ से प्रेरित होकर उन्होंने ‘यहूदी’ बनाई. जात-पांत और छूत-अछूत के मुद्दे पर ‘सुजाता’ (1959) हो या लोकतंत्र पर व्यंग करती ‘परख’ (1960), या फिर स्त्री केंद्रित ‘बंदिनी’ (1963), ये सारी फिल्में उनकी रेंज दिखाती हैं. इत्तेफ़ाक है कि बॉम्बे टाकीज़ ने इसी विषय पर ‘अछूत कन्या’ बनाई थी, जिसमें देविका रानी ने ये किरदार निभाया था. दोनों ही कमाल की फिल्में हैं. पर टीस इस बात की है कि दोनों ही में तथाकथित ‘नीची जाति’ की लड़की को बलिदान करते हुए दिखाया गया है. गोकि सहानभूति के ज़रिये ही बराबरी पर आया जा सकता है.
बिमल दा शरतचंद के साहित्य से इतने प्रभावित थे कि उनकी कहानियों पर उन्होंने तीन फ़िल्में बनायीं. ‘देवदास’, ‘परिणीता’ और ‘बिराज बहू’. जानकारों का मानना है कि उनकी बनाई ‘देवदास’ शरत बाबू की कहानी के सबसे नज़दीक है. कुछ हद तक दिलीप कुमार की ‘ट्रेजेडी किंग’ की छवि के लिए ‘देवदास’ और ‘यहूदी’ भी ज़िम्मेदार हैं.
बिमल दा सिर्फ फ़िल्मकार ही नहीं थे. अपने आप में एक संस्था थे. उन्होंने सलिल चौधरी, ऋषिकेश मुखर्जी, ऋत्विक घटक, कमल बोस, नुबेंदु घोष, रघुनाथ झालानी और गुलज़ार जैसे नायाब लोग हिंदी सिनेमा को दिए. गुलज़ार और बिमल दा के ‘बंदिनी’ के दौरान मिलने की दास्तां आप इस वीडियो के ज़रिये जान सकते हैं. गुलज़ार के लिए वे डायरेक्टर या गुरू से बढ़कर पिता समान थे. उन्होंने शायरी की ज़ुबान में बिमल दा पर एक पोट्रेट भी लिखा है और अपनी क़िताब ‘रावी पार’ में बिमल दा के साथ हुए अंतिम दिनों की बातचीत का मार्मिक ब्यौरा भी दिया है.
आख़िर ऐसा क्या था एक कैमरामैन के महान डायरेक्टर बनने में जो आज भी हमें उनकी फ़िल्में देखते वक़्त विस्मृत कर देता है? शायद इसका जवाब भी उनकी बेटी की दूसरी क़िताब ‘द मैन हु स्पोक इन पिक्चर्स’ में श्याम बेनेगल के इंटरव्यू में मिलता है. बेनेगल बताते हैं कि कैमरे को लेकर बिमल दा की समझ कमाल की थी. फोटोग्राफी में रोशनी के प्रभाव को जितना बख़ूबी उन्होंने दिखाया है उसका मुकाबला बहुत कम फिल्मकार कर सकते हैं. याद कीजिये ‘बंदिनी’ का वह दृश्य जिसमें कामिनी (नूतन) के मन में द्वंद है कि क्या उसे किसी औरत का क़त्ल कर देना चाहिए. इस सीन में नायक के सामने लोहार काम कर रहे हैं और वेल्डिंग मशीन से निकलता ताप उसके चेहरे पर रोशनी बनकर गिर रहा है. दूसरे ही सीन में डायरेक्टर को यह दिखाना था कि कामिनी ने दूध के ग्लास में ज़हर मिलाया है. इसको दर्शाने के लिए उन्होंने ज़हर की शीशी और ग्लास की तस्वीरों को एक साथ मिला दिया है!
फ़िल्म का सेट बनाने के बजाय बिमल रॉय आउटडोर लोकेशन को ज़्यादा तरजीह देते थे. मसलन, ‘दो बीघा ज़मीन’ में हावड़ा ब्रिज पर शूटिंग करना उन दिनों वाक़ई कमाल की बात थी. उस वक़्त का सिनेमा जहां अतिरेक से लबरेज़ था तो वहीं बिमल दा ने किरदारों को हकीक़त की ज़मीन पर ही रखा. किसी को ‘लार्जर देन लाइफ’ नहीं बनाया. उनका कहानियों का चयन एक तरफ साहित्यिक था, जैसे रबींद्रनाथ टैगोर की ‘काबुलीवाला’ (बतौर प्रोडूसर) और शरत बाबू का ‘देवदास’, तो दूसरी तरफ ‘सुजाता’ या ‘दो बीघा ज़मीन’ ऐसी समकालीन कहानियां थीं जिनमें सर्वहारा इंसान समाज में अपना वजूद ढूंढ रहा था.
निर्विवाद रूप से सत्यजीत रे भारत के सबसे महान फ़िल्मकार हुए हैं और बिमल दा को उनसे एक पायदान नीचे खड़ा होना पड़ता है. शायद इसलिए कि सत्यजीत रे के सामने कमर्शियल फ़िल्म बनाने की मज़बूरी नहीं थी. उन्होंने बिमल दा की तरह ये समझौते नहीं किए. और दूसरा, बिमल दा जल्द ही दुनिया से विदा हो गए. आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी.
सौज- सत्याग्रह