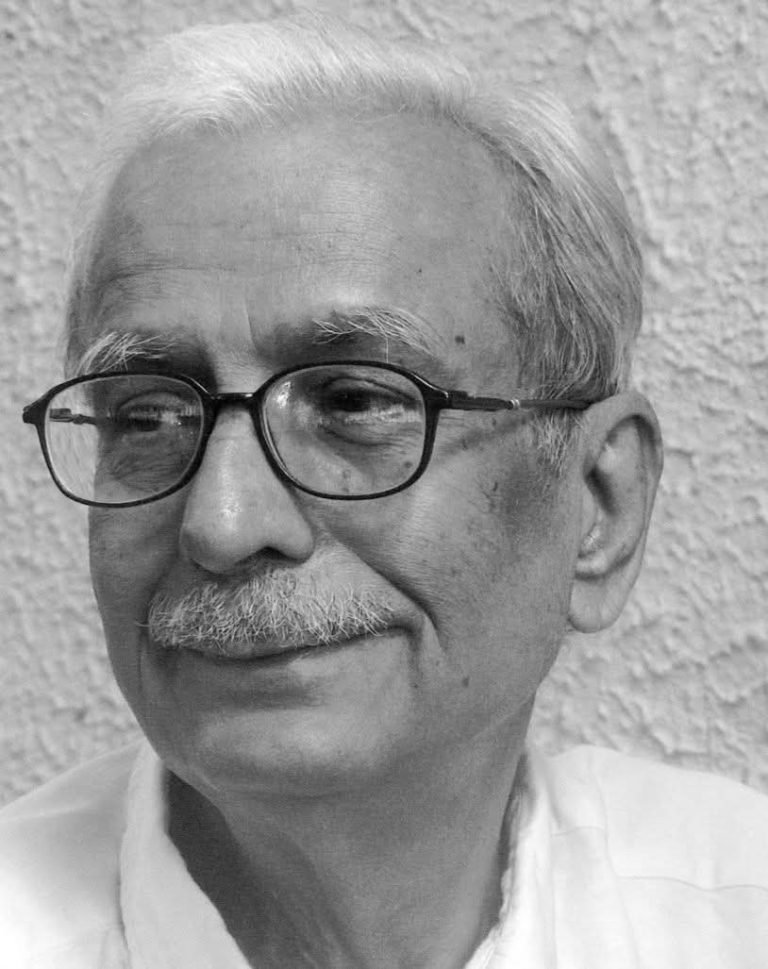‘हम भारत के
लोग’- यहां से शुरू होने वाली
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह ‘हम’ कौन है? यह सवाल कुछ वैसा ही है जैसा रघुवीर सहाय ने अपनी मशहूर
कविता में पूछा था- ‘जन गण मन में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता
है / फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हरचरना गाता है।’ लेकिन रघुवीर सहाय भारतीय राष्ट्र की जिस विडंबना की ओर
इशारा कर रहे थे, वह आज कुछ और समस्याग्रस्त हो गई है। भारतीय
राज्य नागरिकता की नई कसौटियां मांग रहा है, नागरिकों से उनकी पहचान मांग रहा है और नागरिक इस सवाल पर
बंटे हुए हैं कि वे सरकार के इस रुख़ पर कैसी प्रतिक्रिया दें।
दरअसल यह भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी
है। अच्छी बात यह है कि जिन्हें यह इम्तिहान देना है, वह आज़ादी की लड़ाई की विरासत की ओर देख रहे हैं। उनके
सामने जो तस्वीरें हैं उनमें महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर की सबसे प्रमुख
है। हालांकि इस अवसर पर यह ख़याल आना अस्वाभाविक नहीं है कि अपने जीवन काल में
अंबेडकर और गांधी कई बार एक-दूसरे से असंतुष्ट रहे, एक-दूसरे के खंडन में जुटे रहे। दलितों के लिए अलग निर्वाचन
मंडल बनाने के ब्रिटिश सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गांधी जी ने जो ऐतिहासिक अनशन
किया था, वह अंबेडकर को दलितों के प्रति अन्याय लगता
रहा। इस सिलसिले में गांधी जी के सचिव रहे प्यारेलाल ने ‘एपिक फ़ास्ट’ नाम की जो किताब लिखी है, उसमें वे बताते हैं कि अंबेडकर दबाव में जब गांधी से मिलने
गए तो उन्होंने पहला वाक्य यही कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। गांधी का
अनशन तुड़वाने के राष्ट्रीय दबाव में अंबेडकर ने उनके साथ पुणे का समझौता तो कर
लिया, लेकिन इसकी गांठ उनके आपसी संबंधों पर शायद
हमेशा पड़ी रही। बल्कि आने वाले दिनों में ख़ास कर जिस तरह दलित राजनीति में गांधी
विरोध का एक तत्व देखने को मिला और कुछ हद तक अब भी जारी है- वह इस लिहाज से मायूस
करने वाला है कि जिस समय हमें गांधी के तत्व और अंबेडकर के तर्क की सबसे ज़्यादा
जरूरत है, उस समय इनके अनुयायी इन्हें एक-दूसरे के
ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हैं। यह सच है कि महात्मा गांधी अगर भारत की आत्मा हैं तो
अंबेडकर को उसका मस्तिष्क होना चाहिए- आख़िर यह संविधान बनाने में उनकी सबसे
प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन न अंबेडकर का जीवन आसान रहा न उनको अब अपनाना आसान
है। वे इतने तार्किक हैं कि बड़ी से बड़ी भावना अगर उन्हें तर्कविरुद्ध लगे तो उस
पर कुठाराघात करने से हिचकते नहीं। उन्हें जब जाति-पांति तोड़क मंडल के सालाना
जलसे में अध्यक्षता के लिए बुलाया जाता है तो ऐसा वक्तव्य तैयार करते हैं जिसकी
वजह से ख़ुद को सदाशयी मानने वाले आयोजक भी पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं कि अंबेडकर
दुराग्रही हैं। बस वे तार्किक हैं- इतने प्रबल तार्किक कि इसी तर्क पद्धति से किसी
समस्या या सवाल के मूल तक पहुंच जाते हैं। वे जाति-पांति तोड़ने वालों की सदाशयता
पर संदेह नहीं करते, लेकिन तर्कपूर्वक साबित करते हैं कि जाति ने
पूरे भारत को कमज़ोर किया है और यह तब ख़त्म होगी जब पूरा हिंदू धर्म ख़त्म होगा।
उनके शब्द बहुत सख़्त हैं। जो बीजेपी नेता अंबेडकर का नाम जपते नहीं अघाते, उन्हें शायद नहीं पता कि अंबेडकर की हिंदुत्व के बारे में
क्या राय है। उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से अपने इस वक्तव्य में लिखा था- ‘हिंदू इस देश के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी दूसरे
देशवासियों की सेहत और ख़ुशहाली के लिए खतरा है।’
इस प्रश्न पर बाद में लौटते हैं कि ऐसे
अतिवादी लगने वाले अंबेडकर को इस देश ने क्यों स्वीकार किया और पहले यह देखते हैं
कि संविधान निर्माता के तौर पर अंबेडकर ने वह क्या किया कि आज का हिंदुस्तान भी
उन्हीं के पास लौटने की ज़रूरत महसूस करता है। दरअसल अंबेडकर ने भारत के लोगों को
उनकी उस भारतीयता की गारंटी दी जो आज़ादी की लड़ाई के दौर में विकसित हुई थी। जाति-पांति
में बंटे, तरह-तरह के भेदभाव और अस्पृश्यताओं के बीच
जीते, लगभग अमानवीय किस्म की जकड़नों को जीने का
आधार बनाए, धर्म और लिंग के तरह-तरह के पूर्वग्रहों को
जीते एक समाज को उन्होंने बिल्कुल बराबरी के आधार वाली नागरिकता प्रदान की। आज यह
बहुत मामूली सी बात लगती है लेकिन इस दौर तक पहुंचने से पहले की मुश्किलों को याद
करें तो पाएंगे कि दरअसल यह एक बहुत क्रांतिकारी विचार था जो सदियों की भारतीय
परंपरा को आधुनिकता और बराबरी के महास्वप्न से जोड़ता था। यह इसलिए भी संभव हुआ कि
अंबेडकर शायद खुद समाज के उस सिरे पर खड़े थे जिसकी पीठ पर इस असमानता का चाबुक
पड़ता था। हालांकि भारतीय समाज में भेदभाव का यह अनुभव इतना प्रत्यक्ष था कि कोई
भी उससे अनभिज्ञ या असंपृक्त होने का दावा नहीं कर सकता था। गांधी नेहरू या दूसरे
तमाम स्वाधीनता सेनानी इतने प्रगतिशील थे कि वह नागरिकों की बराबरी को आने वाले
जनतंत्र का आधार बनाते, लेकिन जैसा कि अंबेडकर और गांधी के संवाद से
स्पष्ट है, जाति-पांति से उपजे भेदभाव की चुभन गांधी में
वैसी नहीं थी जैसी अंबेडकर में थी। बल्कि गांधी के भीतर चातुर्वर्ण्य को लेकर एक
आदर्श सी कल्पना थी जिसे अंबेडकर उनका बचपना भी बताते हैं और उनकी राजनीतिक मजबूरी
भी। जाहिर है, अंबेडकर न होते तो सामाजिक बराबरी और न्याय
की प्रतिज्ञा इतनी प्रबल न होती जितनी हमारे संविधान में दिखाई पड़ती है।
यहां एक और महत्वपूर्ण अंतर की ओर ध्यान देना
आवश्यक है। अंबेडकर इस बात से निराश दिखाई देते हैं कि कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन
के अपने लक्ष्य को छोड़कर धीरे धीरे राजनीतिक परिवर्तन को अपना मुख्य लक्ष्य बना
रही है। उनका स्पष्ट मानना था कि भारत को राजनीतिक आजादी से पहले एक तरह की
सामाजिक आजादी चाहिए। अगर यह आजादी हासिल नहीं हुई तो राजनीतिक आजादी का कोई मतलब
नहीं रह जाएगा। इसी तर्क से वह कई मुद्दों पर अंग्रेजों के साथ खड़े दिखाई पड़ते
थे।
दूसरी ओर गांधी मानते थे कि भारत की सामाजिक
बुराइयां उसकी राजनीतिक गुलामी की देन हैं। यह राजनीतिक गुलामी खत्म हो जाएगी तो
देर-सबेर सामाजिक बुराइयां भी दूर हो जाएंगी।
कहने की जरूरत नहीं कि आजादी की करीब तीन
चौथाई सदी बीत जाने के बाद अंबेडकर ज्यादा सही प्रतीत होते हैं। राजनीतिक तौर पर
आजाद भारत कई तरह की सामाजिक बुराइयों का गुलाम है। पुरानी अस्पृश्यता नफरत की नई
शक्लों में विद्यमान है और हमारा पूरा लोकतंत्र एक बंटे हुए समाज की कटी-छंटी
महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया रह गया है।
बल्कि इस स्थिति का सबसे ज़्यादा लाभ उन
लोगों ने उठाया है जो शुरू से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में
स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने का सपना देखने
वाला संघ परिवार और उसकी राजनीतिक इकाई बीजेपी अब विराट बहुमत के साथ सत्ता में
है। हालांकि उसने अब अपने मुहावरे बदल दिए हैं- वह हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान का
पुराना नारा छोड़ चुकी है, लेकिन बहुसंख्यकवादी राजनीति के आक्रामक उभार
के साथ अपने पुराने एजेंडे को ही अमल में लाने में लगी है। पिछले दो साल में
बहुसंख्यकवादी लक्ष्यों को लेकर किए जाने वाले एकपक्षीय राजनीतिक फैसलों की जैसे
बाढ़ आई हुई है और ख़ुद को प्रगतिशील और लोकतांत्रिक मानने वाली ताकतें एक के एक
बाद इनके प्रहारों के आगे बेबस प्रतीत होती हैं। उसकी उपस्थिति का दबाव दूसरी सारी
लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी है। उसके फ़ैसलों पर सवाल उठाना अदालतों के लिए
मुश्किल होता जा रहा है।
नतीजा यह हुआ है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का सवाल हो, वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला हो, अयोध्या का फ़ैसला हो, तीन तलाक़ का मसला हो, नागरिकता संशोधन क़ानून हो, दिल्ली के दंगे हों, विरोधियों को देशद्रोही बताने की बात हो- अदालतें लगभग हर
मामले में या तो सरकार को लेकर बहुत नरमी भरा रुख़ अख़्तियार करती नज़र आ रही हैं
या फिर सुनवाई आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा नागरिकों पर एनआरसी की तलवार लटकी ही
हुई है। नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देश का एक बड़ा हिस्सा आंदोलनरत है।
लेकिन सरकार इस पूरे आंदोलन को ख़ारिज करने में लगी हुई है। उसके मुताबिक यह
आंदोलन विपक्ष के बहकावे का नतीजा है। वह इससे सख़्ती से निबटने की बात कर रही है।
दरअसल इसी मोड़ पर देश को अंबेडकर और गांधी
की नए सिरे से ज़रूरत है। खास बात यह है कि इस मौक़े पर देश उनको याद भी कर रहा
है। तमाम छोटे-बड़े शहरों और क़स्बों में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ जो
आंदोलन चल रहे हैं, वे अपने लिए आज़ादी की लड़ाई के दौर से ही
प्रतीक चुन रहे हैं, उसी दौर में विकसित साझा संस्कृति को अपनी
विरासत बना रहे हैं। दरअसल ये
सारे आंदोलन लोकतंत्र के नए, अनूठे और
अहिंसक प्रयोग हैं जिनमें वह आबादी अपनी भारतीयता का पुनराविष्कार कर रही है जिसे
या तो इससे वंचित करने की कोशिश की जाती रही या इससे दूर बताया जाता रहा। इन
आंदोलनों में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों की भागीदारी है। इस आधार पर इन्हें
मुसलमानों का आंदोलन साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिलचस्प यह है कि
मुसलमान अपनी भारतीयता को उन सभी प्रतीकों से व्यक्त कर रहे हैं जिन्हें खुद को
राष्ट्रवादी मानने वाली जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। यहां राष्ट्रगान हो रहा है, तिरंगा लहराया जा रहा है, वंदे मातरम गाया जा रहा है, भारत माता की जय बोला जा रहा है, हवन और नमाज़ साथ-साथ हो रहे हैं।
लेकिन इस पूरी सदाशयता का मोल क्या है? सरकार इसे देखने को तैयार नहीं है। बहुसंख्यकवादी रुझानों
से अतिक्रांत मानसिकता इस पर संदेह कर रही है। इसमें देशद्रोही तत्व खोजे जा रहे
हैं। दक्षिणपंथ की राजनीति से प्रेरित और भटके हुए लड़के यहां आकर गोली चला रहे
हैं। दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसके पीछे इन
आंदोलनों का उकसावा देखा जा रहा है। यह स्थिति बताती है कि हम किस बुरी तरह एक
बहुत गहरी कटुता और आपसी नफ़रत की गिरफ़्त में हैं।
इस कट्टरता और नफ़रत से हमें दो चीजें ही बचा
सकती हैं- एक तो गांधी जैसी करुणा जिसमें आपसी भेदों को याद रखते हुए भी पारस्परिक
सम्मान की मानवीय ऊष्मा हो या फिर अंबेडकर का तर्कवाद जो याद दिलाए कि हमारे भीतर
की श्रेष्ठता ग्रंथि कितनी नकली और किस कदर नुक़सानदेह है।
मगर सवाल फिर वही है। उपभोक्तावादी
विचारविहीनता के इस दौर में जब राजनीति शुद्ध स्वार्थों से परिचालित हो रही हो तो
महज गांधी या अंबेडकर का विचार कैसे बदलाव ले आएगा? यहां आकर एक बड़े संघर्ष की ज़रूरत का अनुभव होता है। यह
संघर्ष अपनी सामाजिक नियति और अवस्थिति की वजह से सबसे ज़्यादा और कारगर ढंग से
अंबेडकरवादी ही कर सकते हैं। फिलहाल भारत की राजनीतिक बाड़ेबंदी में जातिवाद का
अपने पक्ष में इस्तेमाल करने वाली पार्टियां दलित वोट भी बांट ले रही हैं, लेकिन दलित राजनीति चाहे जितनी बदल रही हो न दलित समाज उतना
बदल रहा है और न उसके प्रति लोगों का नज़रिया बदल रहा है। यह बदलाव तभी आएगा जब
जाति टूटेगी और जाति तभी टूटेगी जब वह होगा जो अंबेडकर चाहते थे- यानी हिंदुत्व का
शिकंजा टूटेगा।
बहरहाल, हम भारत के लोग अगर वाकई समता, स्वतंत्रता और न्याय में भरोसा करते हैं तो हमें इससे बड़ी लड़ाई
की ज़मीन तैयार करनी होगी। अभी वह बहुत दूर का सपना दिख रहा है। लेकिन उस सपने की
सीढी जिन तत्वों से बनेगी, उसमें अंबेडकर तो होंगे ही होंगे।
( लेखक की फेसबुक वाल से)