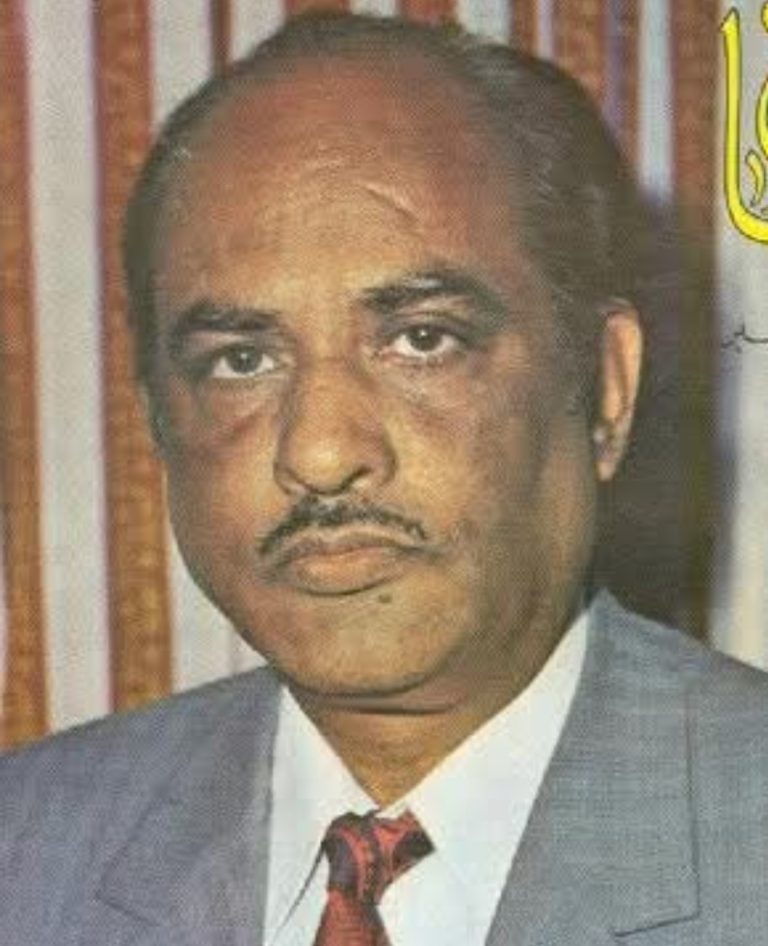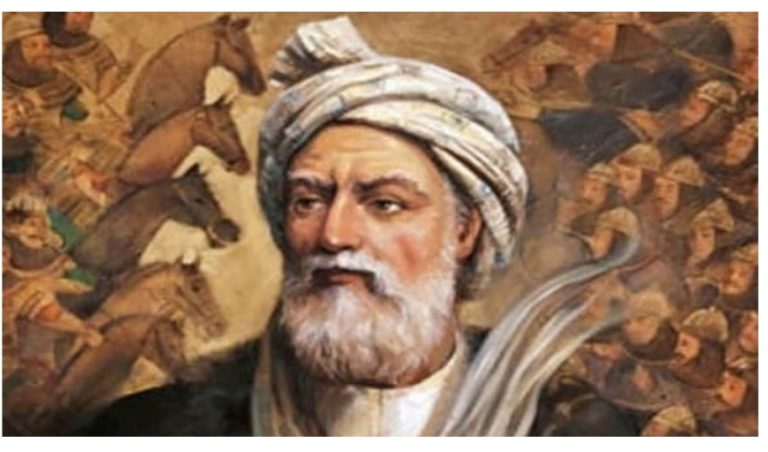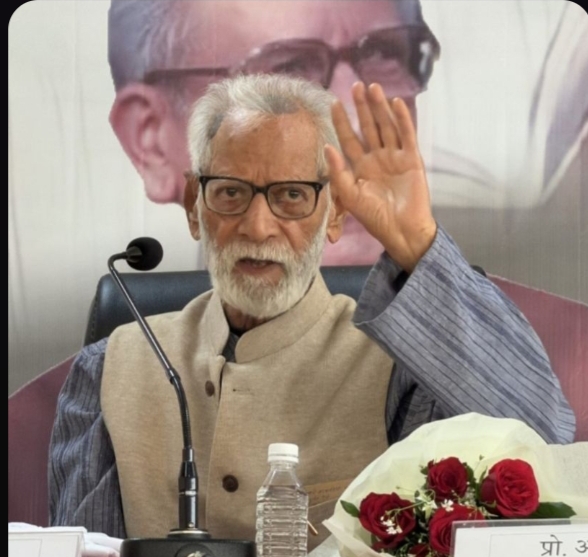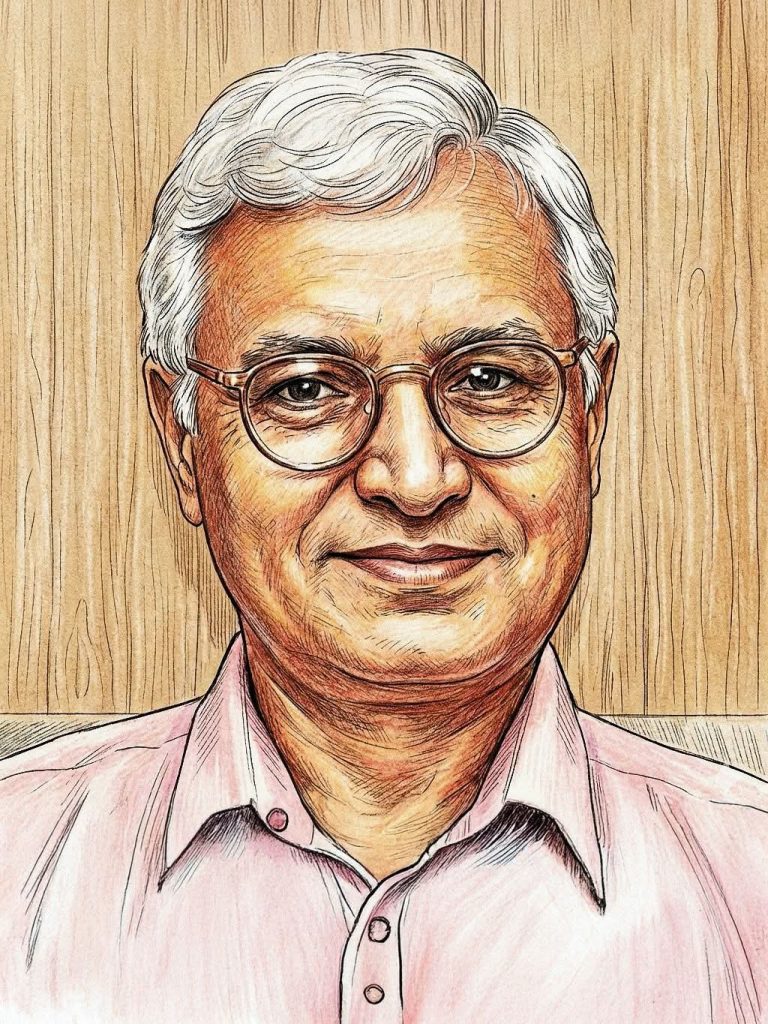अमितेश कुमार
गिरीश कर्नाड, नाम जेहन में आते ही वो बेधने वाली तस्वीरें सामने आ जाती है जिसमें एक शख्स नाक में ड्रिप लगाए ‘नॉट इन माई नेम’ की तख्ती लिए हुआ खड़ा है, जो अपने समय में अपनी उपस्थिति को भौतिक रूप से भी दर्ज कराना चाहता है. जिसके सरोकार का दायरा केवल रचनाओं तक सीमित नहीं है. चूंकि हमारी स्मृतियों का दायरा सीमित है इसलिए हमें सहज याद नहीं रहता कि लगभग अस्सी की आयु में देश के बेहतरीन दिमागों की हत्या और देश में चल रहे उन्माद के विरोध में खड़े इस शख्स गिरीश कर्नाड ने जब अपना पहला नाटक ‘ययाति’ (1961) लिखा तो आयु मात्र 23 साल की थी और दूसरे नाटक ‘तुग़लक’ (1964) के प्रकाशन के साथ ही वो राष्ट्रीय रंगमंच के केंद्र में आ गए थे. प्रकाशन के साथ ही ‘तुगलक़’ का कन्नड, मराठी और हिंदी में मंचन हुआ.
सुरेश अवस्थी, पु.ल.देशपांडे और इब्राहिम अल्काज़ी के संपादन में ‘आज के रंग नाटक’ (1973) के नाम से चार नाटकों का प्रकाशन हुआ उसमें मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार के साथ गिरीश कर्नाड को भी रखा, यह भारतीय नाटककारों का एक चतुर्भुज था. आजादी के बाद भारतीय रंगमंच में जिस राष्ट्रीय रंगमंच की खोज हो रही थी उसे इन नाटकों ने एक रास्ता सुझाया था. इसी तरह सत्तर के दशक में जब भारतीय रंगमंच को लगा कि पाश्चात्य रंगमंच से प्रभावित नाट्य युक्तियों में कुछ अधिक बंधन हैं तो खुलेपन और भारतीय रंग मुहावरे की तलाश नाटककारों को परंपराशील रंगमंच की युक्तियों तक ले गईं उस समय भी गिरीश कर्नाड ने हयवदन (1971) लिखकर रास्ता दिखाया, जिसमें कर्नाटक की शैली यक्षगान और भागवत मेला की युक्तियों का समावेश था, इसके बाद ‘थियेटर ऑफ रूट्स’ के नारे ने जोर पकड़ा. नाटककार के रूप में गिरीश कर्नाड लगभग छ: दशकों तक सक्रिय रहे.
गिरीश कर्नाड उन नाटककारों में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रंगमंच को कई आधुनिक नाटक दिये जिसमें दृश्य और पाठ का संतुलन था, या नाटक केवल मंच पर खेले जाने वाले आलेख या केवल पढ़ने के लिए लिखा साहित्य नहीं था बल्कि ऐसे नाटक थे जिनका मंचन भी खूब हुआ और पढ़ा भी खूब गया. गिरीश कर्नाड नाट्य लेखन के लिए मुख्यत: मिथक और लोकाख्यान, इतिहास और समसामयिक जीवन को चुनते हैं. इतिहास में भी वो मध्यकाल के इतिहास पर अधिक केंद्रित हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय रंगमंच पर नाट्यालेखन लगभग इन्हीं विषयों पर होता रहा. आधुनिकता को सीधे सीधे संबोधित तो किया गया ही है, आधुनिक बेचैनियों को इतिहास और मिथक के माध्यम से तलाश कर रंगमंचीय अभिव्यक्ति की गई है, गिरीश तीनों ही धाराओं में उत्कृष्ट नाटक लिखते हैं. इस लेख में हम इन तीन धाराओं में से कुछ नाटकों के आलेख और उनके मंचन की चर्चा करेंगे. हमने जिनको चुना है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और मराठी भाषा में मंचित नाटक है जिन्हें इन्हीं भाषाई क्षेत्रों से संबंधित निर्देशकों और समूहों ने मंचित किया है. गिरीश कर्नाड निस्सन्देह एक अखिल भारतीय उपस्थिति थे.
गिरीश कर्नाड नाट्यलेखन की शुरूआत मिथकीय कथा पर आधारित नाटक ‘ययाति’ से करते हैं. वृद्ध ययाति अपनी इच्छाओं का पूर्ण उपभोग करने के लिए अपने पुत्र की आयु तो ले लेते हैं लेकिन इससे एक द्वंद्वों की शृंखला शुरू हो जाती है जिससे सभी पात्र घिर जाते हैं. सत्तर के दशक के आरंभ में यक्षगान और भागवत मेला की रंग युक्तियों का आधुनिक नाट्यलेखन में सफल प्रयोग करते हुए गिरीश ‘हयवदन’ लिखते हैं जो टामस मान की कहानी ‘ट्रांसपोज्ड हेड्स’ और लोककथाओं पर आधारित है. यह नाटक भी संपूर्णता की व्यर्थ तलाश और बुद्धि तथा मन के बीच वर्चस्व के द्वंद्व की शाश्वत कथा कहता है. कर्नाड लोकाख्यान और लोकशैली के माध्यम से आधुनिकता के द्वंद्व की अभिव्यक्ति सहज, सरल और लचीले नाट्यशिल्प में करते हैं और यह रंगकर्मियों को व्यापक पैमाने पर मंचन के लिए तो आकर्षित करता ही हैं, आधुनिक नाट्यलेखन में परंपराशील रंगमंच की युक्तियों के प्रयोग के लिए भी नाटककारों को प्रेरित करता है. लोककथा पर ही एक और नाटक आधारित है ‘नागमंडल’ जिसमें इच्छाधारी नागों के जनप्रिय कथा को आधार बनाकर कर्नाड स्त्री की सामाजिक स्थिति और असहायता की कहानी कहते हैं. पंजाबी भाषा में नीलम मानसिंह चौधरी इस नाटक की प्रस्तुति करती रही हैं लेकिन यहां हम विस्तार से बात करेंगे गिरीश कर्नाड लिखित नाटक ‘अग्नि और बरखा’ की, जिसकी कथा का स्रोत मिथकीय है और महाभारत से हैं.
‘अग्नि और बरखा’ नाटक में सत्ता और ब्राह्मणों का गठजोड़, ब्राह्मणों के भीतर वर्चस्व की होड़, उनका पाखंड, स्त्रियों की स्थिति, उनकी यौनिकता, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अपने ही ग्रंथियों के कैदी, ब्राह्मणों और ब्राह्मणेतर जातियों का संबंध, सबंध से उपजी हिंसा, असुरक्षा इत्यादि कई तरह के बिंदु हैं. इनके बीच दो महिला पात्र हैं आदिवासी कन्या नितिलाई और ब्राह्मणी विशाखा जिनका जीवन कई स्तरों पर एक जैसा है. विशाखा का प्रेम पुरूषों की ग्रंथियों का केंद्र बन जाता है जहां उसकी निजी सत्ता पर ही प्रश्नचिह्न लग जाता है. विशाखा अपनी देह के लिये स्वतंत्र निर्णय लेती है जो उसके ससुर को नागवार गुजरता है क्योंकि उसकी नज़र भी उसके देह पर है. विशाखा हर तरफ़ से शोषित है. वैसे नाटककार से यह सवाल पूछा जा सकता है कि जहां पुरूष ज्ञान और सत्ता के लिये जूझ रहे हैं, देह उनके लिये प्राथमिकता नहीं है लेकिन स्त्री के लिये क्यों है? वर्चस्व और ग्रंथियों के इस समर में फंस जाती है आदिवासी कन्या नितिलाई. अरवसु नितिलाई से ब्याह के निमित्त उसकी जाति के पंचायत में समय से नहीं पहुंच पाता. ब्राह्मणों की व्यवस्था में दखल देने का दंड नितिलाई भुगतती है उसकी भी हत्या हो जाती है अरवसु को लगता है कि यह सब इसलिये हुआ है क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते कि वह नितिलाई से विवाह करे. नाटक में ग्रंथियों, इर्ष्याओं, महात्वाकांक्षाओं का सघन जाल है जिसमें सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं. ब्राह्मण समाज और आदिवासी समाज कहीं भी स्त्रियों की स्थिति मुक्त नहीं है. उसे पुरूष की अधीनता में ही रहना है वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती. ज्ञान प्राप्ति की खोज में लगा मनुष्य परम सत्य की आड़ में उन छोटे-छोटे सत्यों से विमुख रहता है जिनका सामना वह रोज करता है.
नितिलाई एक आदिवासी कन्या है जिसे ब्राह्मण अरवसु से प्रेम है, अरवसु नाटक करना चाहता है, ब्राह्मणों के कर्मकांड उसे प्रिय नहीं है इसलिये वह पिता को भी प्रिय नहीं है. प्रस्तुति नाटक मंचन की घोषणा से शुरू होती है और नाटक मंचन पर समाप्त. वर्षा से वंचित धरती पर वर्षा होने के लिये महायज्ञ का आयोजन है जिसके दौरान ही नट नाट्यामंचन करने की भी अनुमति लेते हैं. नाटक के भीतर नाटक परावसु को प्रबोधित करता है. वर्षा केलिये सात साल लंबा चलने वाले यज्ञ का महापुरोहित परावसु है लेकिन इससे उसके पिता के मन में ग्रंथि उपजती है कि वृद्ध होने के बाद भी उसे महापुरोहित नहीं बनाया गया. परावसु का चचेरा भाई यवक्री ज्ञान प्राप्ति के लिये किये गये लंबे तप से लौटता है. इसी बीच उसकी प्रेमिका विशाखा परावसु की ब्याहता हो चुकी है लेकिन परावसु उससे विमुख है. यवक्री अपनी ग्रंथि के शमन के लिये विशाखा से सबंध बनाता है. वह विशाखा को भोगते हुए दरअसल परावसु और उसके परिवार से अपना बदला ले रहा है, इसमें प्रेम कहीं नहीं है. विशाखा अपनी देह के लिये स्वतंत्र निर्णय लेती है जो उसके ससुर को नागवार गुजरता है क्योंकि उसकी नजर भी उसके देह पर है. वर्चस्व और ग्रंथियों के इस समर में फ़ंस जाते हैं आदिवासी कन्या नितिलाई और अरवसु. अरवसु नितिलाई के ब्याह के निमित्त उसकी जाति के पंचायत में समय से नहीं पहुंच पाता. अरवसु के पिता यवक्री को दंड देने के लिये ब्रह्मराक्षस का आह्वान करते हैं. यवक्री की हत्या का समाचार सुन परावसु यज्ञ छोड़ कर लौटता है और अपने पिता की हत्या करता है. यज्ञस्थल पर नाट्यमंचन के दौरान अरवसु पर वृत्रासुर का मुखौटा हावी हो जाता है इससे बचने के लिये परावसु अपनी आहूति देता है. ब्राह्मणों की व्यवस्था में दखल देने का दंड नितिलाई भुगतती है उसकी भी हत्या हो जाती है. आखिरकार इंद्र प्रकट होते हैं और अरवसु उनसे नितिलाई के पुनर्जीवन की जगह ब्रह्मराक्षस की मुक्ति मांगता है. नाटक में हरेक पात्र अपनी जीवनस्थिति के लिये दूसरे को जिम्मेदार मानता है. यवक्री यज्ञ का विध्वंस कर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करना चाहता है, परावसु को लगता है कि उसके पिता ने यवक्री की हत्या यज्ञ के विध्वंस के लिये की है, अरवसु को लगता है कि यह सब इसलिये हुआ है क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते कि वह नितिलाई से विवाह करे. ग्रंथियों, इर्ष्याओं, महात्वाकांक्षाओं का सघन जाल है जिसमें सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं.
निर्देशक के लिए ग्रंथियों और संबंधों के इस उलझाव को सरल बना कर मंच पर पेश करना आसान नहीं है, इसका प्रमाण पाठक चाहें तो इस नाटक पर बनी मल्टीस्टारर फ़िल्म ‘अग्निवर्षा’ को देख कर पा सकते हैं, जिसमें कथ्य नाटक से बहुत दूर चला गया है. ‘अग्नि और बरखा’ की एक बहुचर्चित प्रस्तुति प्रसन्ना ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के लिए की थी लेकिन वह जल्दी ही बंद हो गई. श्रीराम सेंटर रंगमंडल के साथ के. एस. राजेंद्रन ने ‘अग्नि और बरखा’ को निर्देशित किया और नाटक की उलझन और बहुस्तरीयता को बहुत सरल बना कर प्रस्तुत किया, इसका मंचन अब भी हो रहा है. इस नाटक का शिल्प शेक्सपीयर के नाटक हेलमेट की भी याद दिलाता है जहां चरित्र अपने भीतर के द्वंद्व और बाहर की दुनिया से सामंजस्य न होने की वजह से उत्पन्न हुए संघर्ष में लिप्त है. नाटक में मृत्यु की एक शृंखला शुरू हो जाती है जिसमें बचता वही है जो निर्दोष है, जिसमें प्रेम बचा है. शेक्सपीरियन त्रासदी की तरह नाटक का दुखांत नहीं होता बल्कि सकारात्मक बिंदू पर नाटक समाप्त होता है. बरसों से तपती धरती पर बारिश होती है और धरती के साथ मानव के भीतर की दाहक अग्नि को शीतलता मिलती है. महज संयोग है कि इस प्रस्तुति को करने के कुछ समय बाद राजेंद्रन ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों के साथ ‘हैमलेट’ की प्रस्तुति भी की. संस्कृत रंगमंच की युक्तियों का राजेंद्रन ने प्रस्तुति की भाषा में अच्छा समायोजन किया था और विशाखा के चरित्र की नई व्याख्या की थी.
गिरीश कर्नाड अपने नाटकों में इतिहास के माध्यम से भी वर्तमान को टटोलते हैं जिसमें एक तरफ ‘तुग़लक’ है जिसमें एक सुल्तान की अपनी महत्त्वाकांक्षा का द्वंद्व है जिसका असर उसकी रियाया पर होता है. दूसरी तरफ ‘रक्त कल्याण’ है जिसमें बसवण्णा के चरित्र के माध्यम से धर्म और धार्मिक समुदाय के भीतर चल रहे संघर्ष का विवरण है. उनका अंतिम प्रकाशित नाटक ‘राक्षसा तंगाड़ी’ भी तालीकोटा के युद्ध पर आधारित है. ‘बलि’ इतिहास के एक कालखंड के जरिए बलि प्रथा के औचित्य और जैन धर्म के प्रभाव में उसके बदले रूप जिसमें प्रतीक तौर पर बलि दी जाती है के बहाने हिंसा और उद्देश्य की हिंसा को टटोलता है. इसी तरह ‘टीपू सुल्तान के ख्वाब’ में कर्नाड टीपू सुल्तान के चरित्र को एक नये संदर्भ में पेश करते हैं. ऐसे दौर में जब कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर इतना संदेह और घृणा का वातावारण भरा जा रहा है यह नाटक टीपू के भारत के प्रति विचार औऱ भविष्य दृष्टि के साथ उसकी असफलता, अंग्रेजों की कुटनीति और अन्य भारतीय रजवाड़ों की आपसी वैमनश्य और इर्ष्या पर भी प्रकाश डालता है. यहां हम कर्नाड के दूसरे नाटक ‘तुगलक’ की एक प्रस्तुति की चर्चा करेंगे.
‘तुगलक’ हिंदी मे लिखा गया मौलिक नाटक नहीं है, इस वाक्य से शुरु करना थोड़ा अजीब जरूर है लेकिन तुग़लक के बारे में शायद ही किसी को लगता हो यह हिंदी का नाटक नहीं है. गिरिश कर्नाड ने इसे कन्नड में लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद या यूं कहिये हिंदुस्तानी अनुवाद ब.व.कारंत ने किया था. हिंदी रंगमंच के नक्शे पर कोई ऐसा शहर नहीं, जहां तुग़लक का मंचन ना हुआ हो या मंचन की कोशिश न हुई हो. तुग़लक अपने पहले मंचन के समय के बाद से आज तक प्रासंगिक इसलिये बना हुआ है क्योंकि यह अतीत के बहाने हमारे वर्तमान को अधिक संबोधित करता है. सत्ता और शासक के द्वंद्व और तनाव, जनता की स्थिति आज भी वही है. यहां हम चर्चा करेंगे दिल्ली में साहित्य कला परिषद के तत्वाधान में हुए मंचन की जिसका निर्देशन भानु भारती ने किया था.
कोटला के किले में हुए इस प्रस्तुति के शुरू होते ही बादशाह तुग़लक की छवि सामने आती है जनता के आपसी वार्तालाप के माध्यम से, उसके बाद मंच पर वह स्वंय नुमाया होता है अपनी हक और इंसाफ़ पसंदी के निश्चय से जनता को अवगत कराते हुए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने कि घोषणा करता है और रियाया को वहां आने की दावत देता है. इसके तुरंत बाद उसके फ़ैसले का परिणाम सामने आता है जिसमें एक ठग ने बादशाह के फ़ैसले का अपने हक़ में इस्तेमाल कर लिया है. इसके बाद हम नाटक में तुग़लक को फ़ैसले लेते, अपने फ़ैसले पर अमल के लिए जूझते, षडयंत्रों में घिरते, उनसे लड़ते और उन फैसलों को असफल होते हुए देखते हैं. वह पाता है कि उसकी बात जनता समझ नहीं रही, उसके सारे फ़ैसलों को कोई समझने वाला नहीं है या तो उसको उखाड़ फ़ेंकने की साजिश चल रही है या उसको अपने इशारो पर नचाने की तैयारी. इन सब के बीच वह चांदी के साथ तांबे के सिक्के चलाने, हिन्दू मुस्लिम आवाम को करीब लाने, राजधानी को अपने राज्य के केन्द्र में ले जाने इत्यादि फ़ैसले करता है. लेकिन किसी फ़ैसले को कारगर होते हुए नहीं देख पाता. तुगलक़ की त्रासदी यह है कि उसकी ज़बान कोई नहीं समझता. दौलताबाद के किले के प्राचीर पर टहलता हुआ वह खुद को निराशा में डूबता हुआ पाता है. साजिश और अपनी सता का अमल उसे क्रूर और शातिर भी बना देता है. वह अपने विरोधी इमामुद्दीन को अपने ही हक में इस्तेमाल कर उससे उसकी आवाम छीन लेता है, शहाबुद्दीन के षडयंत्र को विफ़ल कर उसकी क्रुरतापूर्वक हत्या कर उसे शहीद भी बना देता है. सियासत में घिरा हुआ वह राज्य में चोर उचक्कों को फ़ैलते, अपने फ़ैसलों के दुष्परिणाम झेलते हुए इस स्तर पर पहुंचता है कि इबादत पर भी पाबंदी लगा देता है. उसकी विडम्बना है कि उसे कोई समझ नहीं पाता और वह सबको समझाना चाहता है. जनता उसे सनकी बादशाह कहती है. वह अकेला पड़ता जाता है और उसके सभी अपने उसे बारी बारी से छोड़ कर चले जाते हैं. वह इतना न्यायपसंद है कि अपनी सौतेली मां को भी मौत की सजा सुना देता है, वह इतना चालाक है कि इमामुद्दीन के विरोध को दबा देता है, वह इल्म का इतना कद्रदान है कि विद्रोही इमान उल मुल्क को शतरंज की समस्या के हल के एवज में छोड़ देता है, वह इतना फिक्रमंद है कि बाप और भाई की हत्या का झूठे आरोप उसे परेशान करते हैं, इतना भविष्यदर्शी कि उसके लिए गये फ़ैसले भविष्य के समाज में चलन बनते हैं, इतना क्रुर की शहाबुद्दीन की बेरहमी से हत्या करता है और वह इतना उदार भी है कि एक चोर को सूबेदार बना देता है.
प्रस्तुति का बेहतरीन दृश्य वह था जब तुगलक शहाबुद्दीन की हत्या करता है, उस समय के संवाद और दृश्य योजना अभीभूत कर देने वाले रहे, फिर दौलताबाद के किले की प्राचीर पर टहलते हुए तुगलक जब सैनिक से बात करते हुए उसे समझा पाने में विफ़ल रहता है, जब अजीज यह कहता है कि ‘खुलेआम लूटो और कहो कि हुकूमत है’ और जब अकेला पड़ता हुआ तुगलक नींद के आगोश में समाने लगता है और दिल्ली लौटने का फ़ैसला करता है. प्रस्तुति में कुछ दृश्य सपाट रह गये जिसके अर्थ हैं. जैसे शेख इमामुद्दीन को कपड़े पहनाता हुआ तुग़लक, तुगलक उसे कपड़ा नहीं पहना रहा अपना इमेज अपना चरित्र उसे दे रहा है क्योंकि वे दोनों हमशक्ल है, दौलताबाद के किले पर टहलने का दृश्य इतनी जल्दीबाजी में शुरू होता है कि तुग़लक की बेचैनी नहीं उभर पाती, तुग़लक और उसकी सौतेली मां का संबंध विकसित नहीं हो पाता. कुछ अनावश्यक भी हैं, जैसे शहाबुद्दीन को मारते हुए तुग़लक कहता है ‘शहाबुद्दीन तुम भी’ यह जुलियस सीजर का संवाद है. तुग़लक जिस तरह से शहाबुद्दीन को मारता है उसी तरह अज़ीज़ गयासुद्दीन को मारता है. प्रस्तुति आलेख में नाटक के सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष को कमजोर कर दिया गया था वह था अज़ीज़ का चरित्र. वह एक हास्य के फीलर की तरह केवल ठग में तब्दील हो कर रह गया. नाटक में से उसके महत्त्वपूर्ण संवादों को भी हटा दिया गया. ‘तुग़लक’ में ही कर्नाड भारतीय शासन व्यवस्था की मूल खामी उजागर करते हैं अज़ीज़ जो मूलत: ठग है के जरिए. अज़ीज बादशाह तुग़लक की हर योजना की काट खोज लेता है और जहाँ बादशाह की सारी योजनाएं धाराशाई होती हैं वहीं अज़ीज़ हमेशा लाभ में रहता है. अब तो यह वक्त ही अज़ीज़ों के तख्तनशीन होने का है. नाटक के द्वंद्व का एक पक्ष तुग़लक और अज़ीज़ का चरित्र भी है. जिसको आमने सामने रखने से ही दोनों का चरित्र अच्छी तरह उभरता. इस नाटक को जब लिखा गया था तब यह नेहरू युग के स्वप्नों के बारे में था उसके महात्वाकांक्षी स्वप्नों और उसकी विफ़लता को एक आख्यान में ढालने की कोशिश थी. इस प्रस्तुति में सबकी नजर यहीं थी कि निर्देशक आज के यथार्थ से इस नाटक की प्रतीकात्मकता को कैसे जोड़ता है? नाटक के आलेख को ही अप्रासंगिक मान लेना एक ज़्यादती है क्योंकि ‘तुग़लक’ में राजनीतिक तत्व अधिक है बनिस्पत ऐतिहासिक तत्व के.

प्रस्तुति देखते हुए और नाटक पढ़ते हुए गिरिश कर्नाड के लेखन और ब.व.कारंत के अनुवाद की जीवंतता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता. निर्देशक की जिम्मेवारी थी कि वह अपनी व्याख्या से इस नाटक को वर्तमान संदर्भ में अर्थवत्ता प्रदान करता, जिसमें निर्देशक विफ़ल रहा और इस तरह से उन्होंने ‘अंधा युग’ (इससे एक साल पहले इसी तरह के सेट अप में की गई प्रस्तुति जिसका निर्देशन भी भानु भारती ने किया था) को ही दुहरा दिया जिसमें महत्वपूर्ण हिस्सों को संपादित कर के उसे निस्तेज बना दिया गया था. इस बार उन्होंने उन हिस्सों को संपादित किया जो इसे संदर्भवान बनाते. अज़ीज़ के एक संवाद को छोड़कर नाटक अतीत के आख्यान जैसा ही था. वर्तमान से जुड़ने की इसकी बेचैनी उसके नाटकों के संवादों में देखी जा सकती थी, जैसे यह संवाद आते उम्मीद बढ़ती लेकिन फिर नाटक को सपाट होता हुआ देखते खीझ महसूस होती. प्रस्तुति एक गौरवशाली नाटक की पुनर्प्रस्तुति जैसी बनके रह गई और इसका भीतरी अर्थ इसकी भव्यता, तामझाम, दृश्यबंध और फ़ैलाव में ही उलझ कर रह गया. ऐसा क्युं हुआ? क्या इसलिए कि यह राज्य प्रायोजित प्रस्तुति थी और इसमें राज्य के विरोध में जाने के सारे अर्थों को दबा के तुगलक के असफ़ल लेकिन दुरगामी निर्णयों को प्रतिष्ठित किया गया? एक दृश्य के अलावे जनता की विस्थापन की वेदना और निर्णयों से उपजे असंतोष सामने क्यों नहीं आए? जो दृश्य आए वह हास्यास्पद बन कर रह गए.
भानु भारती समग्र प्रस्तुति की जगह दृश्यों को संस्थापित कर देते हैं जिसे दर्शक टुकड़ो टुकड़ो में देखता है. ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अभिनेता अलग अलग जगहों पर काम करने वाले होते हैं. पूर्वाभ्यास के इन दिनों में भी आपस में कोई संगति नहीं बनती. नाटक में ऐसे कई चरित्र उभरते ही नहीं जैसे आजम, इमामुद्दीन और शमसुद्दीन का. सौतेली मां और तुगलक का संबंध का अर्थ भी दब जाता है. उभरता है तुगलक का चरित्र और इसे अपने बेहतरीन प्रतिभा से यशपाल शर्मा संभव बनाते हैं. और प्रस्तुति में सबसे अलग और ऊंचे दिखते है, इसके बावजूद कि उनके तलफ़्फ़ुज़ में कमी है और संवाद भूलते हैं लेकिन तुरत संभालते भी हैं. अपनी भूमिका के लिये उनकी मानसिक तैयारी जबरदस्त है जो दिखती है. तुगलक के शातिरपन, इल्म के प्रति उसकी दीवानगी, रियाया के लिये बेचैनी, इंसाफपसंदी, अपने फ़ैसलो के परिणाम का दु:ख, क्रूरता, सत्ता को बनाए रखने की जिद और अकेले पड़ जाने की हताशा सभी रंग उनके किरदार में है. अपने संवाद अदायगी में भी वे तंज के तेवर और उतार चढ़ाव को अनुकूल जगह पर ले आते हैं. बाकी के पात्र में टीकम जोशी असर छोड़ते हैं, उन्होंने आलेख में अपने लिए जगह बनाई है एक सजग अभिनेता की तरह. शेख इमामुद्दीन की छोटी सी भूमिका में सज्जाद प्रभावित करते हैं. शमसुद्दीन बने रवि झांकल, नजीब बने रवि खानविलकर, सौतेली मां बनी हिमानी शिवपुरी भी कुछ नया नहीं जोड़ते और प्रस्थान प्रवेश के समय उनकी गति भी प्रभावित होती है. बर्नी की भूमिका में लगता है कि अभिनेता थका हुआ है और शहाबुद्दीन का किरदार में उपयुक्त अभिनेता नहीं लिया गया. लगभग पात्र अपना संवाद भूलते हुए दिखे, अल्फ़ाज़ भी बहुत लापरवाही से बोला गया. ये समझना कठिन रहा कि बड़ी भूमिकाओं के अलावा छोटी भूमिकाओं में भी बाहर से अभिनेता क्यूं लिया गया?
संगीत बीच बीच में दृश्यों के गैप में इस्तेमाल किया गया था, कभी कभी पृष्ठभूमि के तौर पर भी. प्रकाश व्यवस्था अत्याधुनिक किस्म की थी. लाइटस के पैनल लगे थे और दूर दूर के हिस्सों के साथ साथ नीचे की जमीन को भी रोशन किया गया था लेकिन फिर भी कभी भी अभिनेता का चेहरा पर्याप्त रोशन ना हुआ. जो जरूरी था क्योंकि अभिनेता और दर्शक की दूरी अधिक थी. अभिनेता दिख नही रहे थे. तुगलक़ जैसे किरदार में जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है उसके चेहरे को अंधेरे में रखने से बात नहीं बनती? मुख्य हिस्सों में रोशनी चेहरे पर कम रही. प्रकाश ने भव्यता के लिए माहौल बनाया. रंगमंच में आजकल नीले प्रकाश का प्रचलन बढ़ा है और नीला रंग सुकून देता ही है, विभिन्न कोणों से पड़ रहे प्रकाश प्रभावित भी करते हैं.
प्रस्तुति की भव्यता में हम किले में प्रवेश के साथ ही रु-ब-रु होते हैं. किले के सबसे अंतिम भाग में एक दीवार के सहारे नाटक का पूरा दृश्यबंध बनाया गया है जो पांच भागों में है, और पीछे एक पुल जैसा है जो यमुना पर बने पुल का आभास दिलाता है. समस्त कार्यव्यापार इन्हीं पांच जगहों पर होता है. पहला स्थल है आम सभा का जहां आम सभा होती है, जनता आपस में बात करती है, और इसकी बहुधरातलीयता इसे गुप्त बैठकों का ठिकाना भी बना देती है. दूसरा, तुग़लक का कक्ष, इस कक्षा में कुरान और आलमारी की योजना थी लेकिन उस पर किताबें नहीं थी जिससे तुगलक के अध्य्यनशील होने का पता चलता. तीसरा हिस्सा था दिल्ली से दौलताबाद के बीच के रास्ते का शिविर, चौथा था दौलताबाद के किले की प्राचीर और पांचवा था जंगल का हिस्सा जहां अज़ीज़ खलीफ़ा के वशंज गयासुद्दीन को मारता है. नाटक का अधिकांश भाग पहले दो स्थलों पर ही था अंतिम के तीन स्थलों पर एक एक दृश्य था. इन पांच स्थलों की वज़ह से स्पेस योजना बहुत ही विस्तृत हो गई और दर्शकीय दृष्टि के अनूकूल नहीं थी.
गिरीश कर्नाड ने समसामयिक जीवन को भी अपने नाटकों का विषय बनाया. इन नाटकों को पढ़ते देखते हुए लगता है कि अपने सामने के जीवन की खामोशी के भीतर छिपी हलचल को वो कितनी तल्लीनता से देखते हैं जिसके कई स्तरों को अपने नाटकों के उपपाठ के रूप में उभारते हैं. ‘वेडिंग एलबम’, ‘बिखरे बिंब’, ‘बेंडा कालू ऑन टोस्ट’ जैसे नाटक हमें अपने ही वर्तमान को देखने का एक नजरिया देते हैं. मैं ‘बेंडा कालू ऑन टोस्ट’ की एक मराठी प्रस्तुति और बिखरे बिंब की तीन प्रस्तुतियों की चर्चा करूंगा.
‘बेंडा कालू ऑन टोस्ट’ जिसकी एक प्रस्तुति मैंने मोहित ताकलतर के निर्दशन में देखी थी मराठी में ‘उने पूणे शहर एक’ नाम से. यह नाटक महानगर के रूप में पसरते उन शहरों की गाथा है जिसमें कई तरह की संस्कृतियां शहर के अलग अलग छोरों पर रहती हैं जिनके आपसी मेल से शहर बनता है लेकिन ये एक दूसरे से अनजान बने रहते हैं. शहर के बदलने की राजनीति क्या है और उसके बदलाव से शहरवासियों पर क्या असर पड़ता है, कॉस्मपोलिटन का दावा करने वाले शहरों की संकीर्णता कैसी है इसको सूक्ष्मता से नाटक में बुना गया है. ‘उन्हें पूरे शहर एक’ जंगल बनते हुए शहर और उसमें पनपते मानवीय संबंधों की कोलाजनुमा प्रस्तुति है. पुणे और बेंग्लोर जैसे शहरों में, जो तेजी महानगर का चरित्र अपनाते जा रहे हैं, जीवन कई छोरों पर चलता है. चमचमाती सड़कों और बजबजाती नालियों, रिहाइशी सोसाइटियों और झुग्गी झोपड़ियो, तंग गलियों और रेस के मैदान जैसे विरोधी युग्मों से शहर बनता है. ये आपस में मिलते भी हैं लेकिन अधिकांशतः एक दूसरे से अनजान रहते हैं. इस शहर में एक सिरे पर लोग इतने अधिक विपन्न हैं कि वो हिंसात्मक हो रहे हैं. दूसरी तरफ़ अर्थ इतना अधिक है कि उसे घोड़ों की रेस में गंवाया जा रहा है. एक तरफ़ जिंदगी गलीज मोहल्लों और गलियों में है एक आलीशान अपार्टमेंट और कोठियों में. एक सिरे पर कौन बनेगा करोड़पति बनने के सपने देखते हुए निरंतर छले जा रहे हैं दूसरी तरफ़ वे भी है जो उन्हें छल रहे हैं. अपार्टमेंट का जीवन इन झुग्गियों में रहने वालों के बिना रूक जाता है, शहर की इमारतें गांवों के श्रम पर निर्भर हैं. हर तरफ़ मूल्य छीज रहे हैं विपन्नता में भी और संपन्नता में भी. झूठ अब आदत बन चुका है. लालच हावी है और हर चीज़ की कीमत है. शहर का जीवन इन्हीं विरोधी रंगो के मेल और उनके अलगाव से बनता है.
गिरिश कर्नाड के नाटक को निर्देशक मोहित ताकलकर ने राजनीतिक दृष्टि से व्याख्यायित किया है. जनसंख्या के दबाव में फैलते शहर, उसमें बनती सड़कों, कटते पेड़ों और बढ़ते यातायात इत्यादि अनेक कोण प्रस्तुति में उभरते हैं. कर्नाड ने शहरों के विषम विकास और उसके कारण शहरों के निजी चरित्र के विलुप्त होने और पर्यावरण के नष्ट होने की प्रक्रिया की जैसी शिनाख्त बेंग्लुरु शहर के माध्यम से नाटक में की है मोहित आलेख को पुणे में केंद्रित करके इसे एक सार्वजनिक कथ्य बना देते हैं. और विकास की राजनीति का अंतर्विरोध बखूबी उभरता है, मराठी रंगमंच के दिग्गज अभिनेताओं ज्योति सुभाष, विभावरी देशपांडे, राधिका आप्टे आदि ने प्रस्तुति में प्रभावि अभिनय किया है.
गिरीश कर्नाड ने लेखकीय जीवन और व्यक्ति के अहम को केंद्र बनाकर नाटक लिखा है ‘बिखरे बिंब’. मैंने इस नाटक की तीन प्रस्तुतियां देखी है. पहली प्रस्तुति जो देखी उसका निर्देशन स्वयं गिरीश कर्नाड ने किया था जिसमें अभिनय अरूंधती नाग का था. यह नाटक एकल नाटक है. दूसरी प्रस्तुति अलकी पद्मसी निर्देशित थी अंग्रेजी भाषा में जिसमें शबाना आज़मी ने अभिनय किया था. तीसरी प्रस्तुति का निर्देशन राजेंद्रनाथ का था जिसमें पदातिक, कोलकाता के अभिनेता काम कर रहे थे. इसमें अनुभा फतेहपुरिया और चेतना जालान ने अभिनय किया था. यह नाटक ऐसे शिल्प में लिखा गया है जिसमें मुख्य किरदार की प्रतिछवि टेलीविजन पर आती है और दोनों का संवाद आता है. पहली दो प्रस्तुतियों में अभिनेता प्री रिकार्डेड वीडियो के साथ संवाद करते हैं. राजेंद्रनाथ ने नाटककार प्रदत्त इस युक्ति को छोड़ दिया था और प्रतिछवि के रूप में एक अन्य अभिनेता को खड़ा किया था.
नाटक, लेखक मंजुला नायक के आत्मसाक्षात्कार को केंद्र में रखता है. उसके जीवन के खोखलेपन, फ़रेब, विवशता, अकेलेपन… को उसका ही अपना प्रतिबिंब सामने ला देता है जिससे लेखिका अंततः पीछा छुडाना चाहता है…पर असफल रहती है. कैरीयर के पीछे भागते हुए मंजुला नायक अपने परिवार की उपेक्षा करती है पति से बढ़ती दूरी के परिणामस्वरुप पति मंजुला की अपाहिज बहन की तरफ आकर्षित हो जाता है. यह आकर्षण जिस्म से परे है जिसे मंजुला अपने जिस्म में महसूस करती है. शातिर मंजुला बहन की मौत के बाद उसके उपन्यास को अपने नाम से छपवाकर प्रसिद्धि तो पा जाती है लेकिन वह अंतत: अपने मृत बहन से हार जाती है. मंजुला के इस चरित्र को अरुंधती नाग और शबाना आज़मी दोनों ही ने बड़ी शिद्दत से निभाया है। स्वर का उतार चढ़ाव, देह भाषा, गति सब कुछ नियंत्रण में. स्क्रीन पर चल रहे संवाद से तालमेल। का निर्वाह करना सहज नहीं था. नाटक इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति का अंतर्मन जानता है कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत. इसलिए व्यक्ति अपने आत्मासाक्षात्कार से भागता है. जबकि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके प्रभाव और कारण को वह स्वंय तो जानता ही है. साहित्यकार होना अच्छे मनुष्य होने की गारंटी नहीं है इसको भी लेखक उभारता है लेकिन इस प्रक्रिया में लेखकीय सहानुभूति मंजुला के चरित्र के साथ नहीं है यह स्पष्ट है. उसकी कुंठा, उसकी हताशा और अपनी अपाहिज बहन से ही प्रतिद्वंद्विता उसके चरित्र को दयनीय बना देते हैं.
गिरीश नेहरूवियन आधुनिकता की दौर की उपज थे – लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन मूल्य था. अंग्रेजी के विद्वान थे, कन्नड में लिखते थे और हिंदी समेत अनेक भाषाओं में काम किया. एक में विविध की समाई के सच्चे उदाहरण. कर्नाड कला के विभिन्न माध्यमों से सहज तालमेल स्थापित करते हैं. उनका नाट्यालेखन लगभग छ: दशकों में फैला हुआ है जिसे उन्होंने अभिनय, निर्देशन और अन्य गतिविधियों के साथ जारी रखे. यहां पर जिन प्रस्तुतियों का जिक्र हुआ उसमें एक के निर्देशक वो स्वयं है, एक उनके समकालीन अलीक पद्मसी का, दो का निर्देशन उनकी बाद वाली पीढ़ी के रंगकर्मियों राजेंद्रन और भानु भारती का है, एक का निर्देशन अपेक्षाकृत नौजवान निर्देशक मोहित ताकलकर का है. उनके नाट्यलेखन की तरफ हर दौर में निर्देशक और रंगकर्मी आकर्षित होते रहे हैं. अब वह सही वक्त है, जहां हमें उनके अवदान की फिर से शिनाख्त करनी चाहिए. ज़ाहिर है इसके लिए हमें उनके नाटकों को फिर से पढ़ना होगा, उनके मंचन को देखना होगा कि किस तरह संवेदना पाठ और दृश्य दोनों में स्पंदित होती रही है.
ctc sanvaadnes