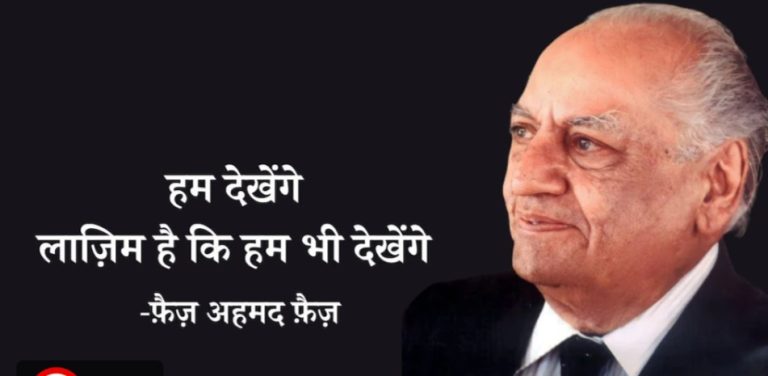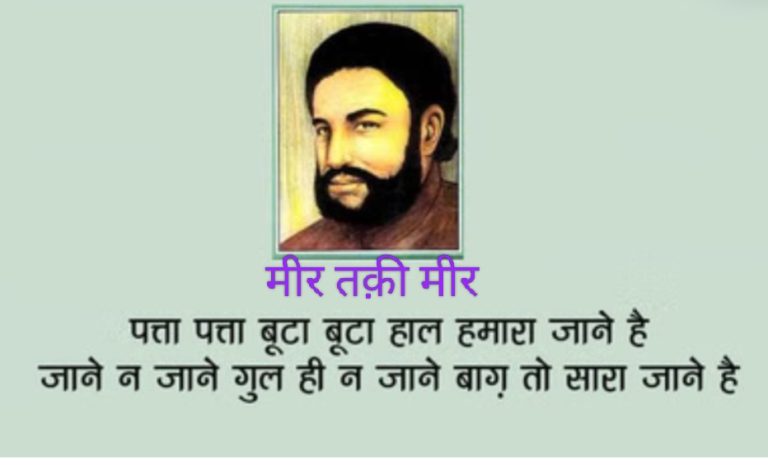अगर प्राइवेट बैंक बहुत ही शानदार थे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? क्या प्राइवेट बैंक जनकल्याण से जुड़े क्षेत्रों में पैसा लगाएंगे? जब कॉरपोरेट लोगों ने सरकारी बैंक का पैसा नहीं लौटाया तो जब वह बैंकों के मालिक होंगे, तब क्या करेंगे?
बैंकों के निजीकरण का विरोध करने के लिए बैंक के सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं। वही सरकारी कर्मचारी जिनमें से अधिकतर सड़क के आंदोलन को देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। लेकिन जब बात अपने पर आईं तो वह भी सड़क पर हैं। चाहे कुछ भी हो लेकिन यह बात तो अच्छी है कि सरकारी नौकरी पा लेने के बाद जीवन को बहुत अधिक सुरक्षित समझने वाला एक समूह सड़क के संघर्ष में खुद उतरा है। हल्का-फुल्का ही सही लेकिन इस दौरान इन लोगों ने यह जरूर महसूस किया होगा कि आखिर कर लोग सड़क पर क्यों उतरते हैं?
बैंक कर्मचारियों के विरोध और हड़ताल की मुख्य वजह सरकार का यागवएलान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा दो सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है।
तो क्या बैंक के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? अगर यही बात है तो बैंक के कर्मचारियों ने अभी विरोध करना क्यों शुरू किया? क्योंकि इससे पहले तो कई सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो चुका है? जिसमें बैंक के कर्मचारियों की भूमिका शायद न के बराबर ही होगी?
इन सवालों का जवाब कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है। इन सवालों का स्वभाविक जवाब है, आदतन हम तभी हमलावर बनते हैं, जब हम अपना नुकसान देखते हैं। सरकारी बैंक के कर्मचारियों को लग रहा है कि उनकी नौकरी वेतन सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं और कई तरह की सरकारी सुविधाओं पर आंच आने वाली है। इससे बचने के लिए उन्हें सड़क पर उतरना चाहिए, इसलिए वह सड़क पर हैं। उनके इस विरोध में कोई गलत बात भी नहीं। गलत बात महज इतनी है कि इसी तरह से अपनी उपज का वाजिब कीमत पाने के लिए कई महीने से किसान संघर्ष कर रहे हैं। कई किसान मर गए हैं। सरकारी अधिकारी होने के नाते और समझ के पदानुक्रम में दूसरों से बेहतर होने के नाते उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वह सड़क पर आंदोलन करने वाले लोगों को देशद्रोही न कहें। खालिस्तानी न कहें। देश के विकास में रोड़ा डालने वाला न कहें। जैसे उनका संघर्ष जायज है ठीक वैसे ही दूसरों का संघर्ष भी जायज होता है। यह उपदेशात्मक किस्म की बात इसलिए लिखी गई है ताकि एक बड़ा नागरिक समाज नागरिक संघर्ष के महत्व को अपने ओछे स्वार्थ से खारिज करने से बचें। जायज मांगों से चल रहे नागरिक संघर्ष का सम्मान करना सीखे। ऐसे माहौल में ही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत संभावनाएं पनपती हैं।
साल 1969 के पहले देश के सभी बड़े बैंक प्राइवेट हाथों में हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार को साल 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा? इस सवाल के जवाब से यह समझा जा सकता है कि क्यों बैंकों पर प्राइवेट लोगों की जगह सरकार के नियंत्रण की जरूरत है?
मशहूर आर्थिक टिप्पणीकार विवेक कौल कहते हैं कि उस जमाने के प्राइवेट बैंक में जमा अधिकतर पैसे का कर्ज के तौर पर इस्तेमाल प्राइवेट बैंक के निदेशक ही कर लिया करते थे। और यह कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था। बल्कि बैंक में जमा राशि का तकरीबन एक चौथाई हिस्सा बैंक के निदेशक कर्ज और निवेश के तौर पर खुद इस्तेमाल कर लेते थे।
बैंकों का विस्तार नहीं हो पा रहा था। वह कुछ जगहों पर सिकुड़ कर रह गया था। ग्रामीण आबादी तो बैंकों का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पा रही थी। इसलिए साल 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद बैंक धीरे-धीरे उन दूरदराज इलाकों में फैला शुरू हुए, जहां वह जाना नहीं चाहते थे। ग्रामीण आबादी के पास राष्ट्रीयकृत बैंक ही पहुंचे न कि निजीकृत बैंक।
अब थोड़ा बैंकिंग के प्रक्रिया को मोटे तौर पर समझ लेते हैं। हम लोगों की बचत का पैसा बैंकों में जमा होता है। जमा पैसे का इस्तेमाल बैंक कर्ज देने में करता है। इस कर्ज को वह लोग लेते हैं जिन्हें अपने बिजनेस, उद्योग या किसी भी दूसरे तरह के काम के लिए पैसे की जरूरत होती है।
जैसे कि उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोग कर्ज के तौर पर बैंकों से पैसा इसलिए लेते हैं ताकि पूंजी की जरूरत पूरी हो पाए। कच्चा माल, मानव संसाधन, मशीन और भी कई कई तरह के कामों के लिए जरूरी पैसा उनकी जेब में रहे। बैंक कर्ज पर देने वाले पैसे से अधिक ब्याज वसूलते हैं और अपने यहां जमा पर रखी गई राशि के लिए कम ब्याज देते हैं। इस तरह से बैंकिंग का कारोबार चलता है। इसी बैंकिंग के कारोबार पर आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है।
यहां समझने वाली बात यह है कि अगर बैंक के मालिकाना हक में परिवर्तन कर दिया जाए तो बैंकों में जमा होने वाले पैसे का इस्तेमाल किस तरह से होगा इसके बारे में ठीक ठाक अंदाजा लगाया जा सकता है।
जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंकों में जमा होने वाला पैसा किसानों तक कर्ज के तौर पर पहुंचने लगा। सरकार यह निर्धारित करने लगी कि बैंकों में जमा होने वाले पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा? प्राथमिक सेक्टर जैसी अवधारणाएं आईं, जिनके मुताबिक बैंकों को अपने जमा राशि से कर्ज के तौर पर उन क्षेत्रों को सबसे पहले देने का नियम बनाया गया जो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हो। इसका मतलब यह था कि वित्तीय दुनिया में प्राइवेट लोगों के लिए पहले के मुकाबले राष्ट्रीयकरण के बाद वित्तीय संसाधन तक पहुंच की गली थोड़ी और संकरी हुई। यह सब महज इसलिए हो पाया क्योंकि सरकार ने बैंकों के मालिकाना हक की प्रकृति बदल दी।
उसके बाद 1980 का दशक आया। सरकार राजीव गांधी की थी। सरकार ने निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया। कहने का मतलब यह कि पहले सरकार यह मानती थी कि कुछ क्षेत्र में सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनीयां ही काम करेंगी। पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बैंक से आसानी से पूंजी मिल जाएगी। क्योंकि यह पूंजी उस बैंक से मिली होगी जिसकी मालिक संप्रभु सरकार होगी, इसलिए वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से बैंकों पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा कि वह टूट जाए। न ही लोगों के पैसा डूबने का खतरा होगा। सरकार के इस सोच में ढिलाई आई। और अब 1980 के दशक के दौरान सरकार ने प्राइवेट उद्यमिता को प्रोत्साहन देने का राग अलपना शुरू कर दिया।
तब आया साल 1990। भारत सरकार ने अपने सभी दुखों का इलाज प्राइवेटाइजेशन से हासिल करने की योजना बनाई। अगले दो दशकों तक प्राइवेट कंपनियों ने बड़े-बड़े ठेके लिए। वैसे कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी में अपना हाथ लगाया, जिन्हें सरकार पूरा करते आ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियों के हाथ में गए। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों ने पूंजी का जुगाड़ स्टॉक मार्केट से किया और बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर के बैंकों से लिया।
प्राइवेट कंपनियां अपना काम पूरा कर पाने में पूरी तरह से असफल रही। पूरी तरह से नाकामयाब रही। इसलिए सरकारी बैंकों का बहुत बड़ा पैसा जिन्हें प्राइवेट कंपनियों ने लिया था वह एनपीए में तब्दील होते चला गया। इसमें प्राइवेट कंपनियों को अधिक घाटा नहीं सहना पड़ा। क्योंकि जानकारों का कहना है कि अगर एक प्रोजेक्ट की कीमत 1000 करोड़ रुपए हुआ करती थी तो प्राइवेट कंपनियों ने बैंकों से तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बता कर कर्ज लिया। ऐसे में अगर पहली ही किस्त में 1000 करोड़ रुपए मिल जाता था तब भी प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा नुकसान नहीं सहना पड़ा। इस नुकसान की सारी गाज सरकारी बैंकों पर गिरी। सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ता चला गया।
यहीं पर उस तर्क का जवाब मिलता है जिसमें यह कहा जाता है कि सरकारी बैंकों के एनपीए बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। उनका निजीकरण कर देना चाहिए। यहीं पर समझ में आता है कि क्यों यह तर्क पूरी तरह से एक तरह के भ्रम जाल के सिवाय और कुछ भी नहीं है।
हां यह बात सही है कि सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ा है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए तकरीबन दो लाख करोड़ से अधिक का है। लेकिन उसका कहीं से भी यह मतलब नहीं है कि इसका निजीकरण कर दिया जाए।
क्योंकि सरकारी बाबू बैंक के प्रबंधन और नेताओं के आपसी गठजोड़ की वजह से सरकारी बैंक में सेंधमारी की गई। साल 2000 से लेकर साल 2014 तक प्राइवेट लोगों को गैर जिम्मेदारी के साथ पैसे बांटे गए। बैंक के प्रबंधन ने ठीक से काम नहीं किया। इसलिए जरूरत निजीकरण की नहीं है। बल्कि जरूरत खराब हो रहे बैंकिंग प्रबंधन को सुधारने की है।
अब थोड़ा प्राइवेट बैंकों का संक्षिप्त इतिहास देख लीजिए। प्राइवेट बैंकों के उदाहरण में आईसीआईसीआई बैंक का उदाहरण देखिए जहां पर बैंक के निदेशक ने ही अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। यस बैंक डूब गया तो उसे उबारने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी गई। लक्ष्मी विलास बैंक टूटने के कगार पर पहुंच चुका था तो उसे बचाने के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिया गया। यानी प्राइवेट बैंकों का इतिहास भले सरकारी बैंकों से कम क्यों न हो लेकिन यह बताता है कि प्राइवेट बैंकों में धांधली जमकर की जा सकती है। पब्लिक सेक्टर बैंक खस्ताहाल के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन प्राइवेट बैंक अच्छे हैं ऐसा कहना उचित नहीं लगता। पब्लिक बैंक को सुधारने की जिम्मेदारी उसे प्राइवेट बैंक में बदलकर पूरी हो सकती है यह तो सरासर भ्रम की तरह लगता है।
आम धारणा यह भी होती है कि ग्राहक से बड़े अच्छे ढंग से पेश आया जाता है। चमक-दमक से भरपूर एक ऑफिस होता है। प्राइवेट बैंक बड़े ही करीने से अपना काम करते हैं। इन शब्दों में उतनी ही सच्चाई है जितना विज्ञापन की आज की दुनिया में विज्ञापन के जरिए प्रचार करने वाले लोगों में होती है। यह एक तरह की ब्रांडिंग है। जहां पर प्राइवेट बैंक की छवि अच्छी बताई जाती है और पब्लिक बैंक की छवि बुरी बताकर उसे खारिज किया जाता है। सच्चाई यह है कि प्राइवेट बैंक में भी एटीएम खराब होता है। प्राइवेट बैंक में भी ग्राहकों को दिक्कत होती है। प्राइवेट बैंक के कर्मचारी भी लोगों से बुरी तरह से पेश आते हैं। एक कंपनी होने के नाते यह सारी स्वाभाविक कमियां हैं जो प्राइवेट और पब्लिक बैंक दोनों जगह रहती हैं। जिसका मतलब कहीं से भी यह नहीं है कि सरकार अपना मालिकाना हक बदल दे।
क्या प्राइवेट बैंक धूल धक्कड़ भरे गांव में जाएंगे जहां पर सरकारी बैंक काम करता है? क्या प्राइवेट बैंक अपना मुनाफा छोड़कर उन लोगों के काम आएंगे जो वंचित हैं, गरीब हैं, कृषि जैसे कामों से जुड़े हुए हैं? जिनके मौजूद होने भर से सरकारी बैंक का माहौल, प्राइवेट बैंक के माहौल से थोड़ा सा अलग थोड़ा सा भदेस नजर आने लगता है। इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात क्या प्राइवेट बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी उतनी सैलरी मिलेगी जितने सरकारी बैंक के कर्मचारियों को मिलती है? क्या सरकारी बैंक के कर्मचारी जब प्राइवेट बैंक के कर्मचारी बनेंगे तो उनको व सुविधाएं मिलेंगी जो सरकारी बैंक के होने के नाते उन्हें मिलती हैं? क्या नौकरी की वैसी सुरक्षा प्राइवेट बैंक में मिलेगी जैसी सरकारी बैंक में मिलती है? इन सारे सवालों का जवाब शायद हर कोई जानता हो।
इसके अलावा एक और तर्क दिया जाता है कि जब खराब बैंक बिकेंगे तो सरकार को आमदनी होगी। सरकार को आमदनी होगी तो उसका इस्तेमाल सरकार जरूरी जगहों पर कर पाएगी। राजकोषीय घाटा कम होगा।
राजकोषीय घाटे के भ्रम को मशहूर अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने न्यूज़क्लिक के अपने कई लेखों में समझाया है। प्रोफेसर पटनायक लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था के जर्जर माहौल में अधिकतर मामले में निजी कंपनियां सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज लेती हैं।
अब अगर सरकार का राजकोषीय घाटा 100 रुपये का है, तो वह वह इस घाटे के वित्तपोषण के लिए बैंक से कर्ज लेकर पूरा करेगी। लेकिन इसे इतनी ही मात्रा के सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों के निजीकरण के जरिये हासिल किया जाता है तो निजी खरीदार को इन संपत्तियों को खरीदने के लिए 100 रूपये बैंक से उधार लेना होगा।
यह कहना कि अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटा “ख़राब” है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों की बिक्री का कदम “ठीक” है, यह कहने का मतलब यह कहना है कि जो खर्चे सरकार द्वारा बैंक से 100 रूपये के कर्ज द्वारा वित्त पोषित किये जाते हैं वे “ख़राब” हैं, लेकिन वही खर्च किसी निजी संस्थान या व्यक्ति द्वारा बैंक के जरिये जुटाए जाते हैं तो “ठीक” है! यह पूरी तरह से किसी भी आर्थिक औचित्य और समझदारी से बिल्कुल परे है। सरकार के पास अगर पैसा कर्ज की तौर पर जाता है तो उसकी संप्रभु शक्तियों की वजह से कम से कम बैंक में जमा करने वाले लोगों की जमा राशि हमेशा सुरक्षित रहती है। लोगों को यह डर नहीं रहता कि बैंक टूट जाएगा।
निजीकरण का कोई आर्थिक औचित्य नहीं है तो निजीकरण किया क्यों जाता है? जब सरकारी और निजी कंपनियों दोनों में इंसान ही काम करते हैं, तब कैसे निजीकरण को बढ़ावा देने वाला तर्क जायज हो सकता है? निजीकरण के समर्थक तर्क देते हैं कि इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और आर्थिक विकास होगा। लेकिन 1990 के बाद से हमने देखा है कि जहां निवेश की जरूरत थी वहां पर निजी कंपनियों ने निवेश नहीं किया है। कंपनियों के जरिए बाजार चलाने की वजह से बाजार से समाज कल्याण का तत्व गायब हो चुका है। सब कुछ केवल मुनाफा है। लोगों ने पौने दाम पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। केवल आर्थिक आंकड़े बढ़ते हैं। पूंजीपतियों की जेबें भरती है। लोगों का शोषण जारी रहता है।
आर्थिक पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती कहते हैं कि सरकार के पास पैसा कमाने के कई तरह के जरिए हैं। लेकिन वह बार-बार सरकारी संपत्तियां बेचने में ही लगी रहती है। वह चाहे तो अमीरों के अकूत पैसे पर टैक्स लगा सकती है। उन्हीं अमीरों के जिनकी कोरोना के समय में कमाई प्रति घंटे तकरीबन ₹90 करोड़ थी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है।
जब बैंकों को प्राइवेट हाथ में सौंपा जाएगा तब भी तो वही कॉरपोरेट के मालिक बैंकों के शेयर धारक बनेंगे जिन्होंने बैंकों से पैसा लेकर बैंकों को नहीं लौटाया। अगर उनके हाथ में बैंक चले जा रहे हैं तो इसे निजीकरण कहा जाएगा या निजीकरण के बहाने बैंकों में रखे हुए पैसे की लूट।
सौज- न्यूजक्लिक