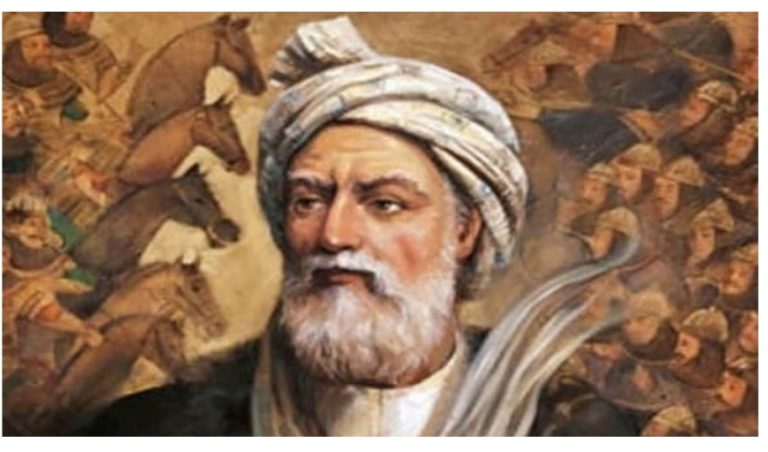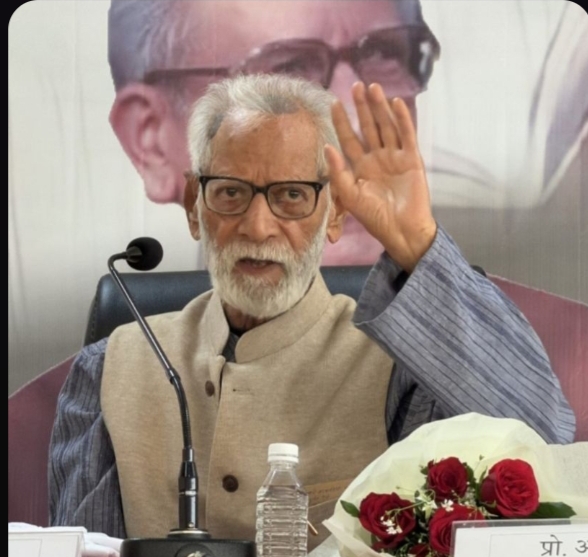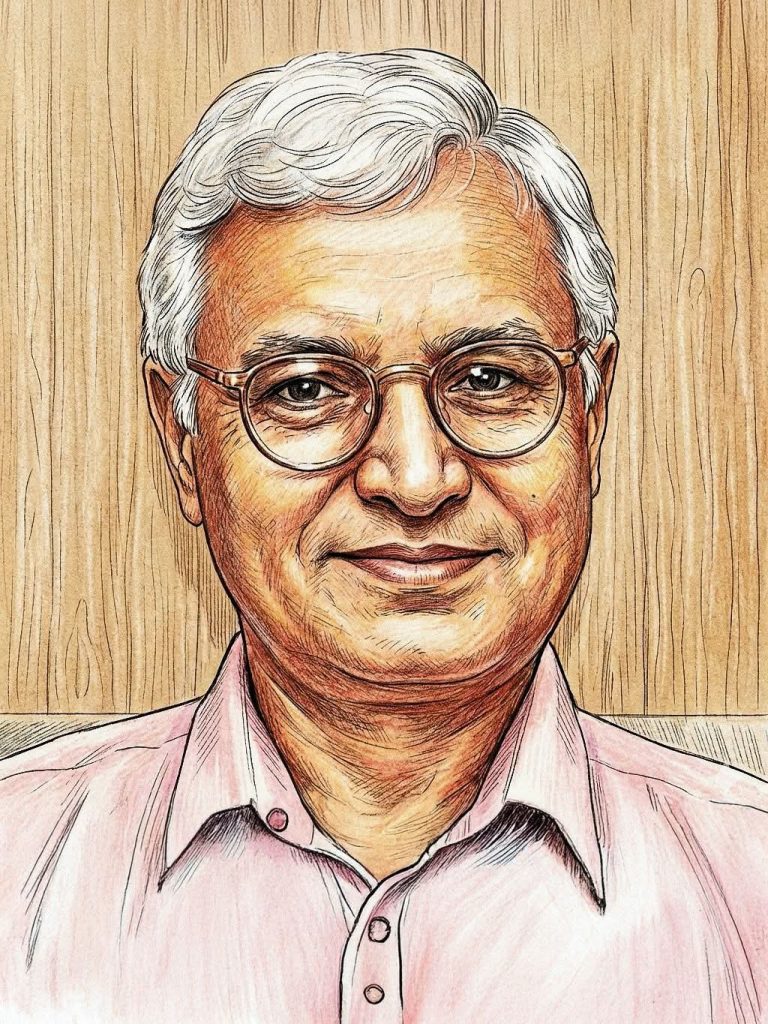खेती-बाड़ी का जो अर्थशास्त्र है उसे क्या देश के किसान, अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी से बेहतर जानते-समझते हैं ? बात आपको अटपटी लगेगी और हास्यास्पद भी लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है- हां!
प्रोफेसर अशोक गुलाटी भारत के अग्रणी कृषि-अर्थशास्त्री हैं. वे उन विद्वानों में हैं जिनका लिखा मैं गौर से पढ़ता हूं, अक्सर सलाह-मशविरा करता हूं और जिनके लिए मेरे मन में सम्मान का भाव है. प्रोफेसर गुलाटी किसानों के हमदर्द हैं और हमदर्दी का यह भाव उनके विद्वतापूर्ण लेखन पर किसी धार की तरह चढ़ा रहता है. सरकारों के खिलाफ उठ खड़े होने का उनमें दमखम है और ऐसा उन्होंने नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के वक्त भी किया है. अगर उचित जान पड़ा तो वे किसान-आंदोलनों के खिलाफ भी उठ खड़ा होने से परहेज नहीं करते. बरसों से उनकी जो एक टेक चली आ रही है, उसी के अनुकूल उन्होंने इस बार तीन नये कृषि-विधेयकों के लिए स्वागत-भाव दिखाया और इसे भारतीय कृषि के लिए वैसा लम्हा करार दिया जैसा कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आया था. दिप्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता समेत इन कृषि-विधेयकों के ज्यादातर हिमायतियों ने प्रोफेसर अशोक गुलाटी के तर्कों के सहारे ही इन कानूनों की तरफदारी में अपनी बात कही है.
लेकिन अफसोस ! प्रोफेसर गुलाटी इस बार हक की बात कहने से चूक गये, मसले को समझने में उन्होंने भारी भूल कर दी. बात ये नहीं है कि इस बार मसले पर सोच-विचार करने में उन्होंने किसी पूर्वाग्रह से काम लिया या फिर उनके आंकड़ों में कोई खोट है या फिर उनकी तर्कयुक्ति में ही कोई झोल है. लेकिन उनसे भारी भूल हुई है और यह भूल हुई है एक ऐसे अर्थशास्त्री से जो सरकार को नीति-निर्माण में सलाह देता है. मुझे ये बात पहली बार स्पष्ट हुई जब मैंने दो अर्थशास्त्रियों ज्यां द्रेज और अशोक कोटवाल के बीच चल रहे एक गंभीर विचार-विमर्श को पढ़ा. इस विचार-विमर्श में अशोक कोटवाल का पक्ष था कि गरीबों को अनुदानित मूल्य पर अनाज देने की जगह नकदी फराहम करना कहीं ज्यादा अच्छा है. इसके जवाब में ज्यां द्रेज का कहना था कि सरकार को सलाह देने वाले अर्थशास्त्री और गरीबों को सलाह देने वाले अर्थशास्त्री के बीच हमें अन्तर करके चलना चाहिए. सरकार को नीति-निर्माण में सलाह देने वाला अर्थशास्त्री यह मानकर चल सकता है कि उसकी सलाह हू-ब-हू मान ली जायेगी और पूरी इमानदारी से उनपर अमल किया जायेगा और ऐसे में वह नीति के पालन से होने वाले संभावित फायदे की बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है. लेकिन गरीबों को सलाह देने वाले अर्थशास्त्री को अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करना होता है कि किसी नीति के क्रियान्वयन के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, कोई नीति जमीनी स्तर पर किस तरह क्रियान्वित की जाये. ज्यां द्रेज का कहना है कि अगर कागजी गुणा-भाग के हिसाब से देखें तो प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण गरीबों की मदद करने का सबसे कारगर और किफायतमंद तरीका जान पड़ेगा लेकिन असल की जिन्दगी के हिसाब से देखें तो लगेगा कि राशन दुकान के जरिये खाद्यान्न का आबंटन करना गरीबों की मदद का सबसे अच्छा तरीका है. यही बात तीनों कृषि-विधेयक के बारे में भी सच है.
अर्थशास्त्री बनाम किसान
इन कानूनों के पक्ष में जो आर्थिक दलील पेश की जा रही है वह बड़ी किताबी और पंडिताऊ किस्म की है और इस दलील को समझने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम द इंडियन एक्सप्रेस में छपे प्रोफेसर गुलाटी के लेख के शब्दों पर गौर करें. प्रोफेसर गुलाटी लिखते हैं : ‘इन कानूनों से किसानों को अपने उत्पाद बेचने के मामले में और खरीदारों को खरीदने और भंडारण करने के मामले में ज्यादा विकल्प और आजादी हासिल होगी. इस तरह खेतिहर उत्पादों की बाजार-व्यवस्था के भीतर प्रतिस्पर्धा कायम होगी. इस प्रतिस्पर्धा से खेतिहर उत्पादों के मामले में ज्यादा कारगर मूल्य-ऋंखला (वैल्यू चेन) तैयार करने में मदद मिलेगी क्योंकि मार्केटिंग की लागत कम होगी, उपज को बेहतर कीमत पर बेचने के अवसर होंगे, उपज पर किसानों का औसत लाभ बढ़ेगा और साथ ही उपभोक्ता के लिए भी सहूलियत होगी, उसे कम कीमत अदा करनी पड़ेगी. इससे भंडारण के मामले में निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा तो कृषि-उपज की बरबादी कम होगी और समय-समय पर कीमतों में जो उतार-चढ़ाव होते रहता है, उसपर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.’ किसी ने अपनी आंखों में खास विचारधारा की पट्टी नहीं बांध रखी है तो फिर वह ऐसे उपायों से कैसे असहमत हो सकता है ? एक और अर्थशास्त्री हैं स्वामीनाथन अय्यर. उनके लिखे का भी मैं बड़ा सम्मान करता हूं. उन्होंने लिखा है: विपक्ष का यह दावा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा एक ‘सफेद झूठ’ है.
प्रोफेसर गुलाटी या फिर स्वामीनाथन अय्यर की दलील यों बुरी नहीं है. लेकिन जमीनी सच्चाइयों को लेकर उन्होंने अपने मन में जो धारणा बना रखी है, वह बड़ी पोली है. और, उन्होंने कृषि-विधेयकों के क्रियान्वयन को लेकर जो अनुमान लगा रखा है, वह कोरी कल्पना भर है. जाहिर है, फिर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसमें चूक होनी ही है. किसान अर्थशास्त्र की बारीकियों को तो नहीं जानते लेकिन उन्होंने अपने दिल से सच्चाई भांप ली है. अर्थशास्त्रियों का तर्कबुद्धि की सधी हुई लीक पर चलने वाला दिमाग तो नहीं परख पाया लेकिन किसानों ने अपनी सहजबुद्धि से ये जरुर समझ लिया है कि इन कानूनों का जमीनी असर क्या होने वाला है. लेकिन अगर आपको किसानों के दिल के कहे पर यकीन नहीं है, आप तर्कयुक्ति पर ही यकीन करते हैं तो फिर आपको मानव-विज्ञानी मेखला कृष्णमूर्ति का लिखा पढ़ना चाहिए जो कविता कुरुंगती की ही तरह एक एक्टिविस्ट भी हैं, या फिर आप जमीनी सच्चाइयों पर बारीक नजर रखने वाली अर्थशास्त्री सुधा नारायणन का लिखा देख सकते हैं.

मान्यता बनाम वास्तविकता
इन कानूनों की तरफदारी में कहा तो कुछ यों जा रहा है मानों किसानों के दोनों हाथ में लड्डू लगने वाले हैं लेकिन ऐसा कहने के पीछे चार मान्यताएं काम कर रही हैं. यहां हम एक-एक करके चारों मान्यताओं की कुछ पड़ताल कर लेते हैं. पहली मान्यतायह है कि किसानों के पास उपज बेचने के मामले में कोई खास विकल्प नहीं होते क्योंकि उन्हें उपज सरकारी मंडी यानि कि कृषि-उपज विपणन समिति(एपीएमसी) को बेचनी होती है. यह झूठी बात है क्योंकि कृषि-उपज का एक चौथाई हिस्सा ही सरकारी मंडियों के सहारे बिकता है. तीन चौथाई किसानों को सरकार इन कानूनों के जरिये जो आजादी देने की बात कह रही है, वह उन्हें पहले से ही हासिल है. किसानों दरअसल सरकारी मंडी में उपज बेचने की बाधा से आजादी नहीं चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि सरकारी मंडियों की तादाद ज्यादा हो और उनका संचालन बेहतर रीति से हो. जगह-जगह घूम-फिरकर और किसानों से बातचीत करके हाल के जो साल मैंने बिताये हैं, उसमें मैंने किसानों को ये शिकायत करते सुना है कि हमारी तरफ तो कृषि-मंडी ही नहीं है या फिर यह कि कृषि-मंडी में कामकाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है. लेकिन मुझे एक भी किसान ऐसा ना मिला जो कहे कि उसे अपनी उपज कृषि-मंडी के बाहर बेचने नहीं दिया जा रहा.
दूसरी मान्यता ये है कि इन कानूनों के कारण अब किसान कमीशन एजेंट यानि आढ़तियों के शोषण के शिकार होने से बच जायेंगे. यह भी लचर मान्यता है. ऐसी बात नहीं कि आढ़तिया किसानों को ठगते नहीं लेकिन एक सच्चाई यह भी है कृषि-उपज का बाजार बहुत बड़ा है और इसमें बिचौलिये से बचा नहीं जा सकता. बड़ी कंपनियां लाखों की तादाद मे मौजूद किसानों से सीधे-सीधे तो निबट नहीं सकतीं सो उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इन किसानों और कंपनियों के बीच मोल-भाव के मामले में एक पुल का काम करे. अब ऐसे में बड़ी संभावना यही है कि जो आढ़तिए सरकारी मंडी में काम कर रहे हैं वे कंपनियों के हाथों निजी मंडी कायम होने पर उन्हें भी अपनी सेवा देने लगें. ऐसे में किसानों को निजी मंडियों के कायम होने पर बिचौलियों की दोहरी कतार से होकर गुजरना होगा: पहले से चला आ रहा पुराना कमीशन एजेंट उनसे वसूली करेगा ही साथ ही उन्हें कारपोरेट जगत के लिए काम कर रहे नये बांके-वीर बिचौलिए से भी निबटना होगा.
तीसरी मान्यता है कि बाजार का कामधाम समुचित रीति से होगा और स्टॉकिस्ट या फिर ट्रेडर जो अतिरिक्त लाभ कमायेंगे उसका कुछ हिस्सा किसानों की भी जेब में जायेगा क्योंकि नई प्रणाली में कामधाम ज्यादा प्रभावी तरीके से होगा, लागत कम आयेगी और खरीद-बिक्री की मात्रा बढ़ जायेगी. लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर ऐसा मानने का आधार क्या है. निजी क्षेत्र का कोई व्यापारी अतिरिक्त लाभ कमायेगा तो आखिर उसमें से वो किसी को क्यों देना चाहेगा ? ऐसा भी तो हो सकता है कि निजी व्यापारी आपसे में मिल जायें और किसानों को उचित दाम ना दें ? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये व्यापारी आपस में मिल जायें और कृषि-उपज की खरीद-बिक्री के बाजार को एक खास ढर्रे पर चलने के लिए मजबूर करें जिसमें रीत ये बन जाये कि कुछ कृषि-मौसमों में किसानों को उपज का सही दाम मिल जाये और फिर उसके बाद ये व्यापारी किसानों की जेब निचोड़ने-खंगालने में लग जायें ? सारा कुछ किसानों की मोल-भाव करने की कूबत पर निर्भर करता है और जहां तक अभी की बात है, अभी किसान व्यापारियों और मंडी के अधिकारियों की ताकत के आगे बड़े कमजोर हैं. हां, इतना जरुर है कि अभी की हालत में वे अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों की मदद से मंडी के अधिकारियों और व्यापारियों को मनमानी करने से कभी-कभार रोक-टोक पाते हैं. लेकिन, नई व्यवस्था में किसानों के पास इतने भर की भी ताकत ना रह जायेगी. नई व्यवस्था में विवादों के निपटारे के लिए जो समाधान सुझाये गये हैं उन्हें एक मजाक कहना अनुचित नहीं. अर्थशास्त्रियों को भरोसा इस बात का है कि किसान सहकारी संघ(सरकारी भाषा में कहें तो फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन) के रुप में एकजुट हो जायेंगे. लेकिन ऐसा साल- दो साल में तो होने नहीं जा रहा, ऐसा होने में दशकों लगेंगे.
चौथी मान्यता है कि सरकार कृषि के आधारभूत ढांचे में निवेश जारी रखेगी और बढ़ाते जायेगी. अब विश्वास के ऐसे भोलेपन पर क्या कहा जाये. अर्थशास्त्रियों की तुलना में किसान इस बात को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं ये तीन कृषि-विधेयक सिर्फ नीतिगत उपाय भर नहीं बल्कि इनके जरिये सरकार अपनी मंशा का ही इजहार कर रही है. इन तीन कानूनों के जरिये मोदी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि कृषि-क्षेत्र में निवेश, नियमन तथा सहवर्ती विकास कार्यों से वह अपने हाथ खींच लेगी. निजी क्षेत्र के निवेशक भंडारघरों और प्रशीतन केंद्रों(कोल्ड स्टोरेज) में निवेश करेंगे ताकि सरकार इधर से हाथ खींच सके. कृषि उपज विपणन समिति(एपीएमसी) के बाहर व्यापार-केंद्र (ट्रेडिंग जोन) बनाने का मतलब यह नहीं कि कृषि उपज के निजी व्यवसायियों के लिए रास्ता खोला जा रहा है(क्योंकि एपीएमसी में भी पूरा का पूरा व्यापार निजी हाथों से ही होता है) बल्कि इसका मतलब यह है कि सरकार कृषि उपज के व्यापार के नियमन के काम से हाथ खींच रही है. इन कानूनों के कारण अब हम एक ऐसी अवस्था को पहुंचने वाले हैं जब कृषि-उपज का व्यापार मनमाने का हो जायेगा, कोई पारदर्शिता नहीं रह जायेगी, ऐसी कोई व्यवस्था ना होगी कि आंकड़ों को दर्ज और संग्रहित किया जाये और फिर उनका आपस में मिलान किया जाये. व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन तक कराने की जरुरत नहीं रह जायेगी. और, जहां तक अनुबंध आधारित खेती का सवाल है, यह सरकार के लिए विस्तार-सेवाओं से कन्नी काटने के बहाने का काम करेगा.
किसानों के लिए संकेत
किसान वक्त की दीवार पर लिखी तहरीर साफ पढ़ सकते हैं: कृषि-क्षेत्र से सरकार के कदम पीछे खींचने का अर्थ होगा कि जो थोड़ा-बहुत दबाव वे समय-समय पर बना पाते थे, उसकी ताकत भी उनके हाथ से निकल जायेगी. कृषि-उपज के उपार्जन से सरकार हाथ खींचने वाली है, ऐसी सिफारिश के बाबत किसानों ने सुन रखा है. वे इस बात को समझ सकते हैं कि कृषि उपज विपणन मंडी के खात्मे के क्या नतीजे होने जा रहे हैं; किसान भांप चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी अब उनके हिस्से से जाने वाली है. और, हाल में प्याज के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उससे भी किसानों को संकेत मिल चुका है कि जब कोई ऐसा वक्त आएगा जब किसानों के लिए कमाई का मौका होगा तो सरकार इसमें अडंगा लगाने से नहीं चूकेगी. किसान राजनीतिक संदेश को अर्थशास्त्रियों की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से समझते हैं.
(योगेंद्र यादव राजनीतिक दल, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं. व्यक्त विचार निजी है)सौज- दप्रिंटःलिंक नीचे दी गई है-