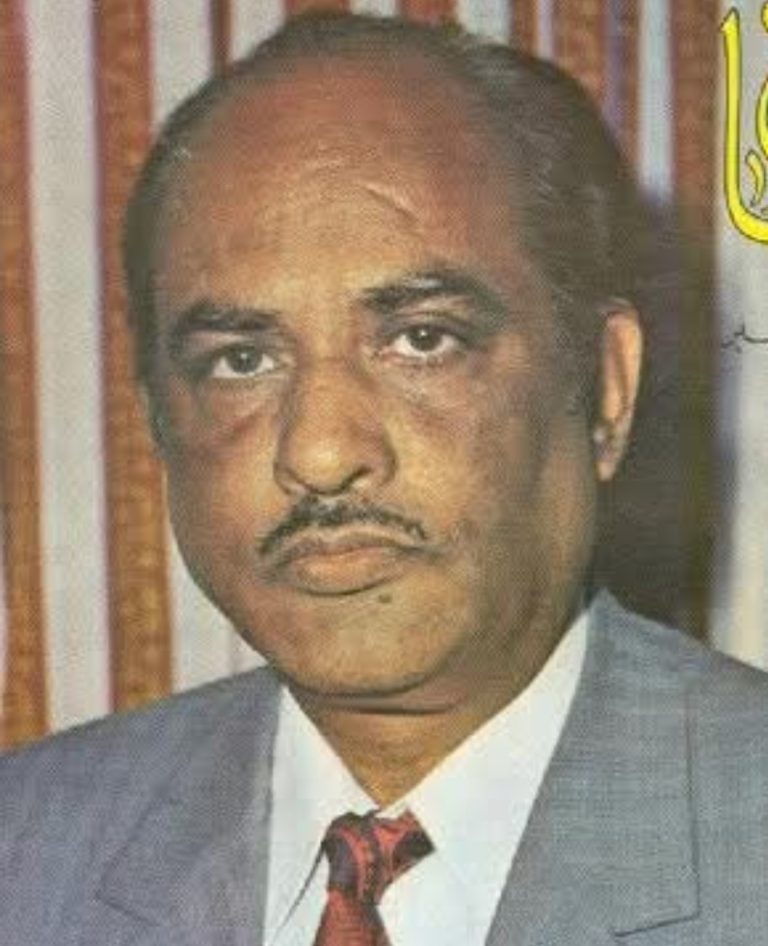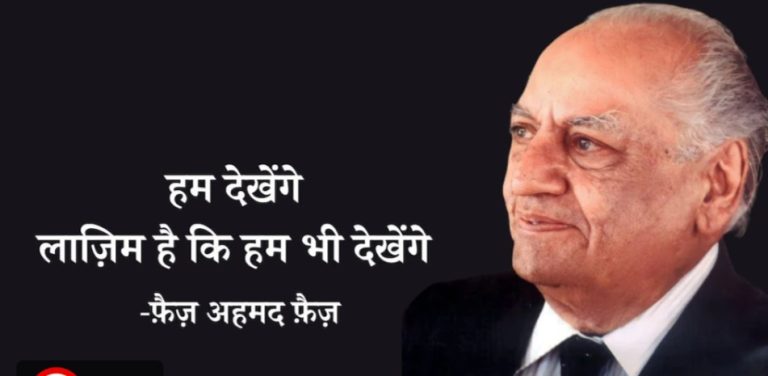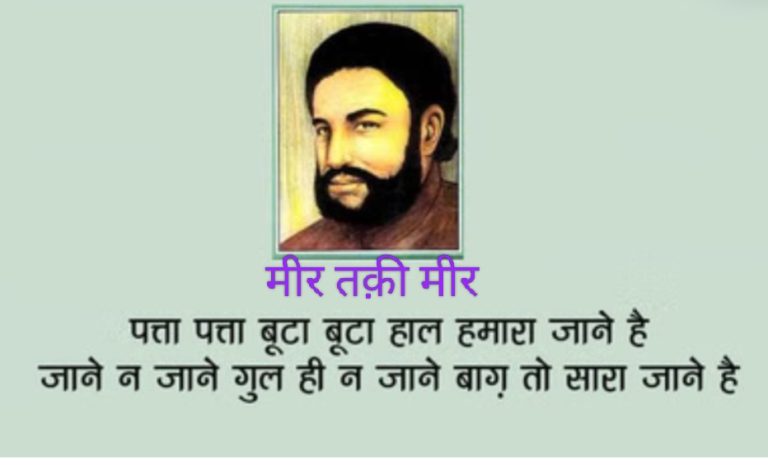यह किस तरह का समाज है जो निस्संकोच और निडर होकर हिंसा, हत्या और बलात्कार को प्रोत्साहित करने लगा है! उस पर दबंग पौरुषवादी गुण्डागर्दी हावी है. उसका उदार वर्ग अगर बचा है तो चुपचाप है और अपनी कायरता में बन्द है. हिन्दू मानस सदियों से विकेन्द्रित और सराजक रहा है. अब वह केन्द्रित और अराजक है.
राजकीय अराजकता
हमने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि भारतीय लोकतंत्र, जिसकी सशक्त जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम, संविधान और परम्परा में थीं और हैं, कभी ऐसे मुक़ाम पर पहुंच जायेगा कि राजनीति तंत्र का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग कर ऐसी हालत पैदा कर देगी जिसे राजकीय अराजकता ही कहा जा सकता है. राजव्यवस्था और न्यायव्यवस्था में जो अनिवार्य और संवैधानिक दूरी थी वह भी जैसे मिट गयी है और लगता है मानो न्यायव्यवस्था भी उन्हीं हितों और पूर्वग्रहों से परिचालित है जिनसे कि राजव्यवस्था. दोनों के इस एकीकरण में न्यायबुद्धि लगभग अप्रासंगिक हो गयी है.
बाबरी मसजिद ध्वंस को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और विशेष अदालत के फ़ैसले, इस सिलसिले में, देखे जा सकते हैं. विशेष अदालत ने सभी राजनेताओं और धर्मनेताओं को उस ध्वंस के लिए ज़िम्मेदार ठहराये जाने के आरोप से साफ़ बरी कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस ध्वंस को ग़ैरक़ानूनी तो माना पर उसके लिए जो धार्मिक समुदाय दोषी था उसी को अपना मन्दिर बनाने के लिए वह ज़मीन उदारता से सौंप दी. विशेष अदालत में जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं पाया गया. यह पूरी तरह से प्रत्याशित था. जिस अराजकता का हम ज़िक्र कर रहे हैं उसका यह सोचा-समझा और पूर्वनियोजित पहलू है कि जांच का नाटक करो, अपर्याप्त साक्ष्य अदालत के सामने पेश करो और जघन्य से जघन्य अपराधी को बरी करा लो.
हाथरस में एक दलित लड़की के गैंग बलात्कार के (और उसके शरीर को बुरी तरह से इतना घायल किये जाने से कि उसकी मृत्यु हो गयी) आरोपितों को गिरफ़्तार कर लिया गया है पर इसमें शक है कि उन्हें सज़ा हो पायेगी. वे सवर्ण हैं भले पाशविक और अमानवीय हैं. उनके समर्थन में एक सवर्ण परिषद् आ भी गयी है. आजकल अक्सर जघन्य से जघन्य अपराधों के दोषियों के पक्ष में खुलेआम निडर होकर कुछ समूह आ जाते हैं. उनका बाल भी बांका नहीं होता लेकिन इससे जांच-प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है. उत्तर प्रदेश में यह कैसा समाज हो गया है जो निस्संकोच और निडर इस तरह की हिंसा-हत्या-बलात्कार को प्रोत्साहित करने लगा है? राज की निमर्मता और समाज की बर्बरता एक-दूसरे को पोसने में संलग्न हैं. राज ने न्यायव्यवस्था और तंत्र ही अपने कब्जे में नहीं कर लिये हैं, समाज भी वह हजम कर रहा है.
इस बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव से बचा नहीं जा सकता कि हिन्दू समाज बुरी तरह से टूट रहा है. लगता है उसकी लोकतंत्र बचाने-पोसने में कोई आस्था नहीं बची है. वह भयावह जातिवाद और साम्प्रदायिकता की चपेट में है जो कि सिरे से लोकतंत्र-विरोधी वृत्तियां हैं. उस पर दबंग पौरुषवादी गुण्डागर्दी हावी है. उसका उदार वर्ग अगर बचा है तो चुपचाप है और अपनी कायरता में बन्द है. हिन्दू मानस सदियों से विकेन्द्रित और सराजक रहा है. अब वह केन्द्रित और अराजक है.

वैचारिक ईमानदारी
हाल ही में शानी फ़ाउण्डेशन ने ‘हिन्दी साहित्य में वैचारिक ईमानदारी’ पर एक संवाद आयोजित किया. साहित्य में तरह-तरह की ईमानदारी दरकार होती है जिनमें से वैचारिक ईमानदारी भी है. पर वह अकेली या असम्बद्ध नहीं होती, भाषा, परम्परा, समय, सचाई, आत्म, समाज सभी के प्रति ईमानदारी का हिस्सा होती है. यह भी कि साहित्य निरे विचार से नहीं लिखा जाता. विचार साहित्य की रचना और आलोचना में एक तत्व होता है और यह तत्व सृजन के ताप में, संवेदना के दबाव में, सचाई की आंच में, आत्मा की खोज में पिघलता-बदलता रहता है. फिर, साहित्य की अपनी वैचारिक सत्ता होती है. वह जीवन-जगत्-सचाई-आत्म आदि पर सोचने-विचारने की विधा है. साहित्य में सारे विचार बाहर से नहीं आते, कुछ स्वयं उसकी रचना में अपने आप उभरते हैं. साहित्य भी ज्ञान है इसको स्वीकार करने में हमारे यहां बड़ी हिचक रही है. मुक्तिबोध के दो पद याद करें: संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन. साहित्य में दोनों होते हैं, आवयविक ढंग से गुंथे हुए.
जब सचाई, समाज, समय परिवर्तनशील हैं तो विचार का परिवर्तनशील होना स्वाभाविक और अनिवार्य है. महत्वपूर्ण लेखकों और कृतियों में वैचारिक एकतानता हो यह ज़रूरी नहीं है. परिवर्तनशीलता और अवसरवादिता में अन्तर है. अक्सर अवसरवादिता लोकप्रियता, मान्यता, सत्ता की अनुकूलता आदि पाने के लिए होती है. लेकिन ईमानदारी वफ़ादारी नहीं होती जबकि ऐसे विचारधारात्मक संगठन और शक्तियां होती हैं जिनकी मांग वफ़ादारी की होती है, ईमानदारी की नहीं. यह भी याद रखना चाहिये कि अभिमत विचार नहीं होता. साहित्य के सन्दर्भ में वही विचार ध्यान देने योग्य होता है जो रचना में रसा-बिंधा हो, उसमें सक्रिय हो. कई बार घोषणाओं को विचार मानने की भूल होती है. हमारी अपनी आधुनिक परम्परा में बड़े लेखकों ने अपनी ईमानदारी के अन्तर्गत ही कई तरह के अन्तर्विरोधों को अपने सृजन में प्रश्रय दिया और जब-तब अपनी विचारधारा का अतिक्रमण किया है. ईमानदारी अतिक्रमण में होती है, वफ़ादारी में नहीं. याद यह भी रखना चाहिये कि ईमानदारी काफ़ी नहीं होती हालांकि ज़रूरी होती है.
शमशेर के यहां अपनी मार्क्सवादी निष्ठा का बराबर उद्घोष है और वह असंदिग्ध है. पर उनकी श्रेष्ठ कविताएं वे हैं जहां उनकी तथाकथित सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं, अद्वितीय सौंदर्य बोध सक्रिय है. उनकी रूमानियत लगभग क्लैसिकल है. मुक्तिबोध जब अपनी कविता में अन्तःकरण के संक्षिप्त होने की चेतावनी देते और आत्मसम्भवा अभिव्यक्ति की तलाश को सबसे ऊपर रखते हैं तो वे ईमानदारी से अपनी विचारधारा का अतिक्रमण कर रहे हैं. निर्मल वर्मा अपने जीवन के उत्तर काल में अपने हिन्दू आग्रहों के लिए बदनाम हैं लेकिन उनके साहित्य में ऐसे सुझाव का कोई साक्ष्य नहीं मिलता. श्रीकान्त वर्मा सत्ता का अंग होते हुए ‘मगध’ में सत्ता की अन्ततः विफलता का आख्यान रचते हैं. साहित्य में, मुझे लगता है, ऐसा हर वैचारिक स्खलन सृजनक्षम होता है और वैचारिक ईमानदारी का सत्यापन भी होता है. इन्हें अन्तर्विरोधों की तरह भी देखा जा सकता है. ऐसे बड़े या महत्वपूर्ण लेखक हमारे समय में कम हुए हैं जिनमें ऐसे अन्तर्विरोध न हों, और जिनमें वैचारिक एकतानता हो. मानवीय स्थिति और नियति, समय और समाज, आत्म और पर सभी अन्तर्विरोधग्रस्त हैं तो भला साहित्य उसका साक्ष्य क्योंकर न हो?
यूटोपिया
संसार में जिन विचारधाराओं का प्रचलन, प्रभाव और वर्चस्व रहा है, वे सभी निरपवाद रूप से कोई न कोई यूटोपिया प्रस्तावित करती रही हैं. कई बार उन विचारधाराओं के आधार पर जो राजसत्ताएं बनी हैं, उन्हें ऐसे ही यूटापिया के आधार पर जांचा-परखा जाता रहा है. यह भी सही है कि अधिकांश यूटोपिया वास्तविकता नहीं बन पाये और उनका दुरुपयोग सत्ता में बने रहने के लिए किया गया. हिटलर और नाज़ी यहूदी-मुक्त ईसाई बनाना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने करोड़ों का सुनियोजित नरसंहार किया. लेनिन और स्टालिन एक वर्गहीन शोषण-मुक्त नया समाज गढ़ना चाहते थे और उन्होंने भी राजशक्ति का दुरुपयोग कर विकराल नरसंहार किये. अब हमारे समय के ये दो बड़े यूटोपिया इतिहास के घूरे पर पड़े हैं.
अपने छोटे भाई कवि-कथाकार उदयन से बात हो रही थी. उसने जिज्ञासा की कि इस समय जो शक्तियां सत्तारूढ़ हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यूटोपिया क्या है. उसने जोड़ा कि अगर वह हिन्दू राष्ट्र स्थापित करना है तो वह अपने मूल में ही अभारतीय है. उसके अनुसार इस यूटोपिया का सिर्फ़ इतना ही अर्थ है कि राष्ट्र-राज्य पर हिन्दू काबिज हो जायेंगे और करोड़ों लोग दोयम दर्ज़े के नागरिक हो जायेंगे. भारत में तो राष्ट्र-राज्य की कल्पना कभी नहीं थी और यह विचार अंग्रेजों के साथ आया. गांधी के पास यह समझ थी और उन्होंने ग्राम स्वराज और रामराज्य की जो परिकल्पना की वह भारतीय परम्परा से निकली थी. उसका लक्ष्य था और है, सत्ता का विकेन्द्रीकरण. जबकि इस समय राज्य-व्यवहार है सत्ता का अभूतपूर्व केन्द्रीकरण. उदयन का कहना है यह यूटोपिया सिरे से अभारतीय है और उसका हिन्दू चिन्तन से भी कोई सम्बन्ध नहीं है. इस पर बहस की गुंजाइश है. पर हमें इस पर गम्भीरता से सोचने की ज़रूरत है कि हम जो आज देख रहे हैं वह राष्ट्र-राज्य की ही विकृत परिणति है. उदयन इस पर इसरार करते हैं कि जो यूटोपिया ‘दूसरे’ रचकर उनका अपवर्जन करता है और करोड़ों लोगों को बाहर करने की चेष्टा करता है वह न मानवीय है, न भारतीय, न हिन्दू.
सौज- सत्याग्रहः लिंक नीचे दी गई है-
https://satyagrah.scroll.in/article/136075/hindu-dharm-arajakta-kabhi-kabhar-ashok-vajpeyi