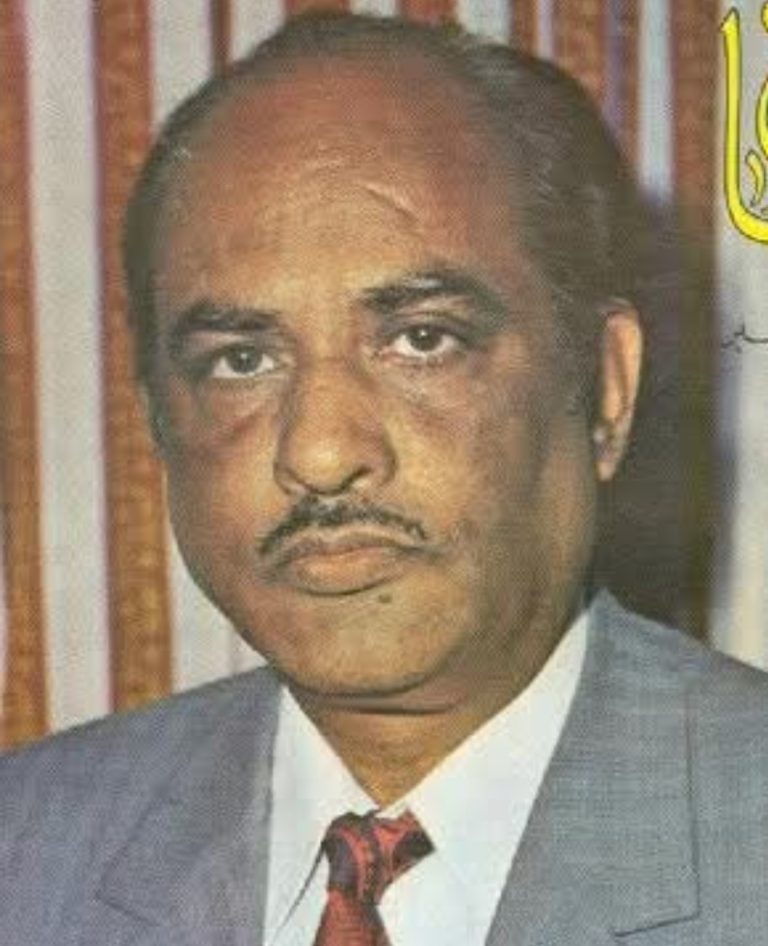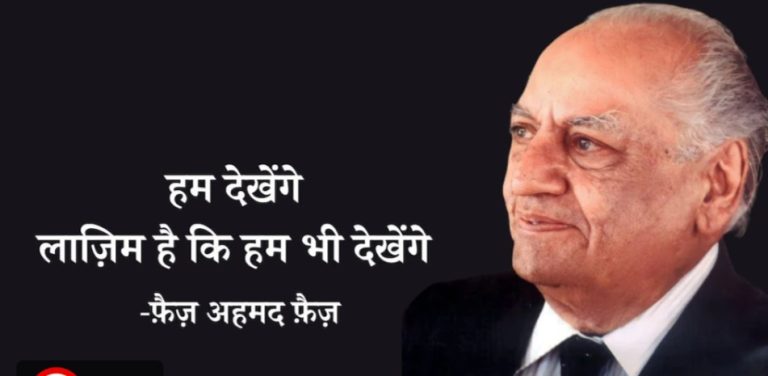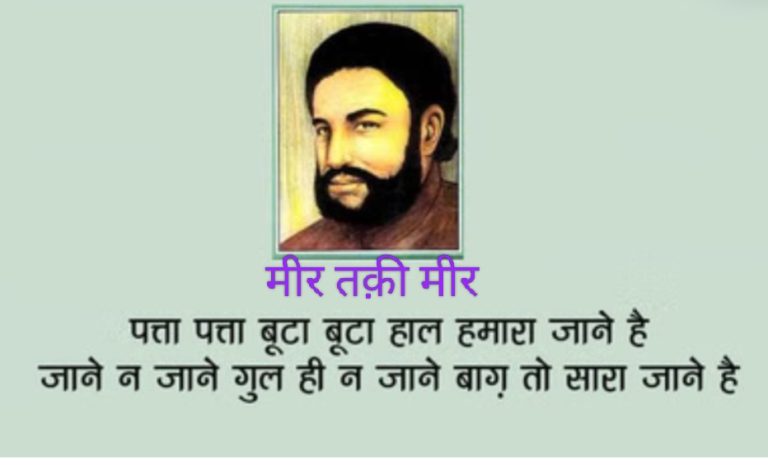एकात्म राष्ट्रवाद ने अपना सारा ध्यान मतदाताओं, निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानीय मुद्दों पर लगा रखा है, जो राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने वाले जवाबी नैरेटिव को भोथरा बना दे रहा है। कई लोगों के दिलोदिमाग में निश्चित तौर पर यह सवाल गहरा रहा होगा कि क्या दो महीनों से चले आ रहे किसानों के जबर्दस्त विरोध प्रदर्शनों के चलते भारतीय जनता पार्टी को झटका महसूस हो रहा होगा या नहीं। क्या भाजपा खुद को अलगाव में पा रही रही है, और क्या मोदी-शाह की जोड़ी खुद को बेनकाब होते देख पा रही है? क्या टेफ्लान में लिपटी इसकी अतिरंजित छवि, जिससे यह किसी भी आलोचना से बची रहती थी, अब मुरझाने लगी है?
क्या किसानों का यह विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सरकार में अपने बाकी के बचे कार्यकाल के दौरान एक नए सिरे से पहलकदमी लेने के लिए विवश करने जा रहा है? इस सबको जानने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि यह शासन खुद किस प्रकार से सोचता है। इसके साथ ही साथ कैसे इस शासन के मूल संगठन, जिसके शीर्ष पर एक सर्वोच्च नेता विराजमान है, ने किसी भी संकट का अहसास कराने को लेकर किस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षित किया है।
एक प्रश्न शुरू से ही सबसे अधिक महत्व का रहा है, वह यह कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर इस विरोध का किस प्रकार का असर पड़ने जा रहा है? याद रखें कि शाह के कुशल नेतृत्व प्रबंधन के तहत देश में चुनावी प्रक्रिया की पहले से ही किलेबंदी की जा चुकी है, और चुनावों को वृहत्तर सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों से विमुख किया जा चुका है।
इसीलिए हम पाते हैं कि प्रवासी संकट बिहार के चुनावी नतीजों पर कुछ ख़ास असर डाल पाने में नाकामयाब रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता राहुल गाँधी द्वारा इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिशों के बावजूद वर्तमान में जारी आर्थिक संकट एक प्रमुख मुद्दा बनकर नहीं उभर पा रहा है। यहाँ तक कि आसमान छूती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ-साथ प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं ने शायद ही कोई प्रभाव छोड़ा हो, जो कभी सरकारों का तख्ता-पलट तक करने का काम कर दिया करती थीं।
ऐसा महसूस होता है मानो वर्तमान में चुनावों ने अपने स्वयं के लिए एक स्वतंत्र तर्क को विकसित कर लिया है। आज वे घरों और परिवारों के बारे में हासिल बेहद सूक्ष्म-सूचनाओं जैसे विशाल आंकड़ों पर आधारित हैं। चुनावों में धन-बल का अभूतपूर्व इस्तेमाल देखने को मिलता है, जिसमें यदि सत्तारूढ़ दल के पास आवश्यक विधायकों की कमी होने पर विपक्षी विधायकों को खरीदने की क्षमता शामिल है।

अन्य प्रचलन में शामिल रणनीति में विपक्षी दलों में विभाजन को अंजाम देने के लिए वित्त पोषण और डमी उम्मीदवारों को प्रायोजित किया जाता है, या सम्भावित वोट-काटू उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। इस सबके जरिये वोट प्रतिशत पर बेहद सटीक आंकड़े को हासिल कर पाना संभव हो जाता है और नतीजे में कितनी सीटों पर जीत या हार हो सकती है, इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है।
इसलिए वे लोग जो किसानों की अभूतपूर्व गोलबंदी को देखकर राहत महूसस कर रहे हैं या उनमें से कुछ तो अभिभूत हैं, उन्हें एक बार खुद को विराम देना चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या इस सबसे भाजपा को चुनावी तौर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है। विपक्ष के पास निश्चित तौर पर भाजपा के समान न तो संसाधन हैं और न ही संगठनात्मक कौशल क्षमता ही है। इसके अलावा अपनी खोजी मशीनरी को इस्तेमाल में लाकर वे एआईएमआईएम और टीआरएस जैसे दलों को वोटों के विभाजन और झूठे नैरेटिव को खड़ा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
यह निश्चित ही एक चिंता का विषय है यदि कोई यह सोचता है कि वर्तमान में जारी किसानों की गोलबंदी का आगामी पश्चिम बंगाल और असम के आगामी चुनावों पर निर्णायक असर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि वहां पर यह अभी तक एक चुनावी मुद्दा नहीं बन सका है। इसके बजाय पश्चिम बंगाल ने खुद को सुभाष चन्द्र बोस और रबिन्द्रनाथ टैगोर की विरासत पर बहसों में उलझा रखा है। यह समझ से परे है कि क्यों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस नैरेटिव को नहीं खड़ा कर पा रही हैं कि कैसे भाजपा किसानों के लिए एक खतरा बन चुकी है। इसका एक संभावित कारण यह हो सकता है कि उन्हें लगता होगा कि राज्य की मतदाता उन मुद्दों से प्रभावित नहीं होने जा रही है, जिसे ‘पंजाब की घटना’ के तौर पर देखा जा रहा है।
यह देखना बेहद दिलचस्प है कि पश्चिम बंगाल में जो कि मुख्यतया एक कृषि प्रधान राज्य है, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक मोदी की किसान-विरोधी छवि को नहीं भुनाया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जबसे मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर आसीन हुए हैं, तबसे कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बचा है। हम चाहे भले ही किसानों के विरोध पर जश्न मना लें, लेकिन मोदी-शाह की जोड़ी ने जिस प्रकार से इस चुनाव को अति-स्थानीय निर्वाचक मण्डल के चश्मे के माध्यम से रुख किया है – उसका आशय है कि यह उनके लिए कहीं कम चिंता का विषय है, जबकि कईयों के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था।
इसके अलावा सामाजिक तौर पर भी किसान आन्दोलन के एक एकीकृत नैरेटिव को गढ़ पाने में असफल रह जाने की उम्मीद है। भाजपा के मूल संगठन, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा भारत को प्रांतीय चश्मे के माध्यम से जरिये प्रतिरूपित किया जा रहा है, और इस दृष्टिकोण को वह चुनावी आख्यानों के स्थानीयकरण के साथ समायोजित करने में व्यस्त है।
जिस प्रकार से अधिकांश मीडिया द्वारा किसानों के विरोध को प्रस्तुत किया जा रहा है या अधिकांश मध्य वर्ग और प्रगतिशील तबके की कल्पना में भी इसे देखा जा रहा है, वे भी धारणा की मात्र एक परत भर हैं।
इसके नीचे और इसके परे जाकर आरएसएस इस मुद्दे को गहराई से विखंडित और एक प्रांतीय चश्मे से देखता है। कृषि क्षेत्र में व्याप्त संकट और केंद्र सरकार द्वारा लाये गए कानूनों के प्रति इसकी पूर्ण उदासीनता को चिन्हित करते हुए इसकी धारणा में एक विरोधाभास देखने को मिल सकता है।
आरएसएस इसे परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को सक्रिय तौर पर जुटाने और गहराने के द्वारा अंजाम में लाता है। ऐसे में हम हमेशा की तरह इस बात को पाते हैं कि आरएसएस से सम्बद्ध किसान यूनियन ने जहाँ नए कानूनों के प्रति अपने विरोध को जताया है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने खुद के जिम्मे इन कानूनों के बारे में “समझाने” के लिए अभियान चलाने की कसम खाई है।
आरएसएस निरंतर लोकप्रिय धारणा के आकलन का काम करता रहता है ताकि इस बात का पता रहे कि झूठी सूचनाओं, अफवाहों और झूठ को फैलाने के लिए कितनी जगह बची हुई है। इसी वजह से वे कम चिंतित रहते हैं, जबकि कईयों को लगता है कि उन्हें चिंतित होना चाहिए। इसने लगता है यह रणनीति भी विकसित कर ली है, जिसमें यह कृषक आंदोलन को हस्तगत करने, इंकार, पुनर्जीवित, खंडन करने और दूरी बनाने को अपनाने में सक्षम है। ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और आमजन से जुड़े कई अन्य मुद्दों से इसने कैसे निपटा है, के सन्दर्भ में भी इस सच्चाई को देखा जा सकता है।
उदहारण के लिए आरएसएस और उससे सम्बद्ध संगठनों पर आरोप है कि महात्मा गाँधी की हत्या में उनका हाथ था। इस सबके बावजूद उन्होंने गाँधी को अपने में समायोजित कर लिया है और साथ ही वे गोडसे जयंती को भी मनाने से नहीं चूकते हैं। गाँधी जयंती के अवसर पर वे इसके आयोजन का नेतृत्व करते हैं और गाँधी के राम राज्य पर भी चर्चा करते हैं। फिर वे गोडसे को समर्पित एक मंदिर या पुस्तकालय का भी उद्घाटन करते हैं। एक ही सांस में वे विभाजन के लिए गाँधी को दोषी ठहराते हैं और अंतर-जातीय सद्भावना पर गांधी की रणनीति की सराहना करने लगते हैं। इसी प्रकार से बीआर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरु, भगत सिंह और कई अन्य लोगों को आरएसएस द्वारा समायोजित करने और अपमानित करने के सन्दर्भ में भी देखा जा सकता है।
इसी प्रकार से आरएसएस ने सामाजिक गतिशीलता में भी अपने स्थान को हासिल कर रखा है, जिसकी वह एक ही साथ समायोजित और आलोचना करने में सक्षम है। इसके द्वारा बिना यह सोचे-विचारे कि कैसे यह नैरेटिव विश्वसनीय से कम हो सकता है, अनेकों विरोधाभासी नैरेटिव को पेश कर दिया जाता है।
इस परिघटना से कुछ समझे जाने की आवश्यकता है। आरएसएस विविधता का विरोध तो कर सकती है लेकिन वह बाहुल्य (या दुहराव) के खिलाफ नहीं नहीं जा सकती है। उदाहरण के लिए आरएसएस इस बात को समझता है कि राष्ट्र का “विचार” एक अमूर्तन विचार है और यह कि आम लोग इसे स्थानीय सन्दर्भों में कहीं अधिक विचार में रखते हैं। यह उनकी इस जागरूकता को अपने उपयोग में लाता है और एकता के बारे में बातें करते हुए इकलौते राष्ट्रीय हित के मुद्दे को परवान चढ़ाने के अजेंडे को आगे बढ़ाता है।
आरएसएस के लिए यहाँ तक कि हिन्दू धर्म भी विभिन्न संप्रदायों और जातियों के तौर पर समूचे क्षेत्रों में पृथक होने में कहीं अधिक है। इसी भेदभाव को ध्यान में रखते हुये यह एक समान नियम पर आधारित हिन्दू धर्म को लागू किये जाने को लेकर प्रयासरत है। आरएसएस की इस निचली सतह पर बनी सूक्ष्म-दृष्टि ही इसके आत्मविश्वास का वह स्रोत है, जो भाजपा को किसानों के इस अभूतपूर्व लामबंदी के बावजूद चुनावी असर से महफूज रखने का काम करती है।
जो लोग आरएसएस-भाजपा द्वारा इन अंतर्दृष्टि के औजार के तौर पर इस्तेमाल में लाने का विरोध करते हैं, वे कैसे इसे अपने राजनीतिक प्रदर्शनों की फेहरिस्त में उपयोग में ला सकते हैं? इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि जो लोग विविधता में विश्वास रखते हैं, वे एक “राष्ट्रीय” कल्पना को बढ़ावा देने में प्रयासरत हैं, जबकि एकात्म राष्ट्रवादियों द्वारा सूक्ष्म-विविधता में निवेश किया जा रहा है। यह विडंबना बताती है कि क्यों इस शासन के दौरान ऑप्टिक्स ने हमेशा से वास्तविक परिणामों से विचलन का काम किया है।
भारत को वर्तमान शासन के खिलाफ किसानों के आंदोलन सहित तमाम गोलबंदियों से पड़ने वाले प्रभावों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। यह जन-आंदोलनों को सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर और अधिक धारदार बनाने में कारगर साबित हो सकता है।
सौज- न्यूजक्लिकः लेखक सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं। अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-