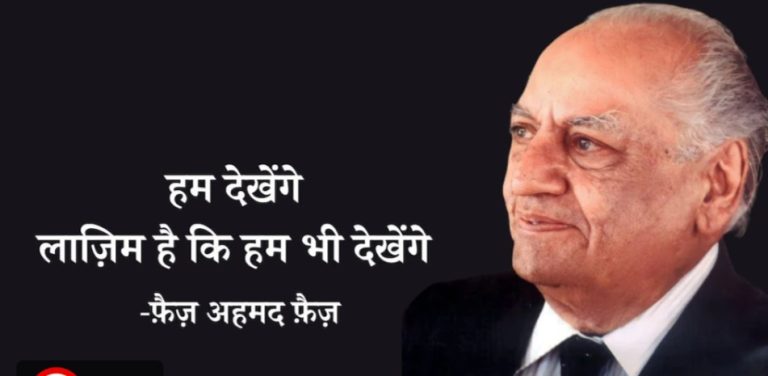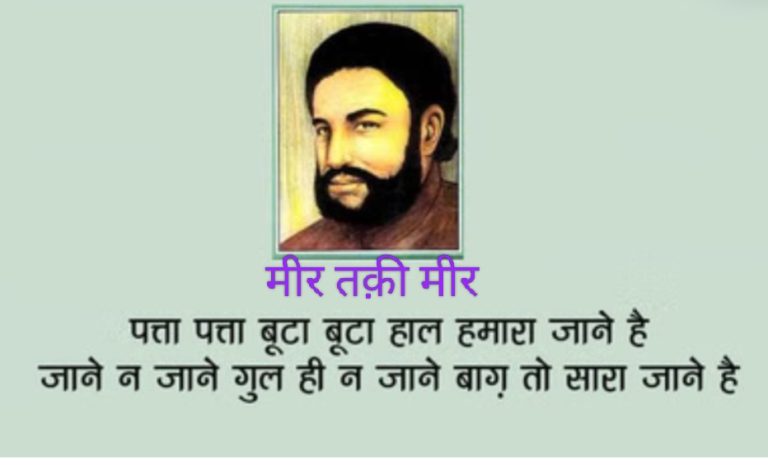अनामिका को साहित्य अकादेमी सम्मान मिलने की घोषणा के साथ ही हिंदी के सोशल मीडिया संसार में जैसे जश्न शुरू हो गया है। मुझे याद नहीं आता, हिंदी में किसी पुरस्कार पर ऐसे सामूहिक उल्लास का माहौल पहले कब बना था। यह उनको हासिल व्यापक स्वीकृति और स्नेह का सूचक है। इसका श्रेय जितना अनामिका के कृतित्व को जाता है उतना ही उनके व्यक्तित्व को, जिसमें सबको समेटने की अद्भुत क्षमता है। उन्हें जिस कृति ‘टोकरी में दिगंत’ पर यह सम्मान मिला है, उस पर कभी एक टिप्पणी मैंने भी लिखी थी।
ये कविताएं नहीं, सभ्यता की अनसुनी आवाज़ें हैं
अनामिका हिंदी की ऐसी विरल कवयित्री हैं जिनका परंपरा-बोध जितना तीक्ष्ण है आधुनिकता- बोध भी उतना ही प्रखर। उनकी पूरी भाषिक चेतना जैसे स्मृति के रसायन से घुल कर बनती है और पीढ़ियों से नहीं, सदियों से चली आ रही परंपरा का वहन करती है। उनकी पूरी कहन में यह वहन इतना सहज-संभाव्य है कि उसे अलग से पकड़ने-पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह उनकी निर्मिति में नाभिनालबद्ध दिखाई पड़ता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि उनका स्त्रीत्व सहज ढंग से इस परंपरा की पुनर्व्याख्या और पुनर्रचना भी करता रहता है- उनके जो बिंब कविता में हमें बहुत अछूते और नए लगते हैं, जीवन की एक धड़कती हुई विरासत का हिस्सा हैं, उसी में रचे-बसे, उसी से निकले हैं और अनामिका को एक विलक्षण कवयित्री में बदलते हैं।
वैसे तो अनामिका का पूरा लेखन ही इस प्रक्रिया का साक्ष्य है, लेकिन उनका नया काव्य संग्रह ‘टोकरी में दिगंत: थेरी गाथा 2014’ तो जैसे पूरब से पश्चिम तक, सभ्यता के सूर्योदय से इस शाम तक, बौद्ध थेरियों से अन्ना केरेनिना तक- अनामिका के विपुल-विराट सांस्कृतिक-दार्शनिक चिंतन का समाहार है- वाकई यह टोकरी अनुभव और संवेदना के इतने दिगंत समेटे हुए है कि इससे गुज़रना सुख-दुख, करुणा और यंत्रणा के उस द्वंद्व की यात्रा करना है जिसका नाम मानव सभ्यता है।
कविता या सभ्यता की इस यात्रा में हमें बुद्ध को भात का न्योता देती आम्रपाली मिलती है और याद करती है जो बुद्ध ने कहा था, ‘रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ढह जाएगा।‘ लेकिन क्या रहा और क्या ढहा? रहने और ढहने के बीच न जाने क्या-क्या सहती-कहती और बांटती थेरियों की एक पूरी बस्ती है जो ज्ञान और करुणा के जल से कवयित्री को और उसके सहचर पाठक को सींचती चलती है। तृष्णा थेरी, भाषा थेरी, स्मृति थेरी, सरला थेरी, मुक्ता थेरी, जिजीविषा थेरी जैसी थेरियां इतिहास के परिपार्श्व में चल रहे जगत के एक विराट नाटक में मंच पर आती हैं और अपने हिस्से के अनुभव, अपनी यातनाएं, अपने दुख और उम्मीद कुछ इस तरह साझा करती हैं जैसे स्त्रियां ही कर सकती हैं। इन स्त्रियों के बीच ढाई हज़ार साल का फ़ासला जैसे नज़र नहीं आता और अगर आता है तो यही याद दिलाता है कि समय के आरपार जाता, सदियों और सहस्राब्दियों से लंबा एक धागा है जो इन स्त्रियों को बांधे रखता है। ‘मैं आदिम भूख हूं बेटी, मुझे पहचान रही हो? / दुर्भिक्ष में चूल्हा / फ़कीर की एक आंख सा धंसा / जांचता है गौर से मुझको, हंसता है! / और अट्टहास की तरह / फैल जाती हूं मैं हर तरफ़’ यह तृष्णा थेरी कहती है और सुनने-लिखने वाली बताती है कि ‘मैं आपको जानती हूं मां।‘
यह बतकही जैसे पूरी किताब में पसरी हुई है। काल के आरपार जाती थेरियां बात कर रही हैं- अपने से, लिखने वाली से, बुद्ध से- उनकी शिकायतें हैं, उनके संशय हैं, उनके सवाल हैं, उनका सच है- और यह पूरी बातचीत ऐसी बीहड़ स्त्री भाषा के उपमानों और बिंबों से भरी है कि जैसे हम पुराने घर की रसोई में, उसके ओसारे में, उसके आंगन में खड़े हैं और अदहन चढ़ाती, सूप फटकारती, धान सुखाती स्त्रियों की बातचीत सुन रहे हैं।
इस बातचीत में जितनी कविता है, उतना ही उसमें बहुत गहरे धंसा हुआ एक सभ्यता विमर्श भी है जो याद दिलाता है कि वर्चस्वशाली सत्ताओं और समूहों के लिखित और प्रचारित इतिहास के विराट राजपथ के समानांतर सभ्यता की एक छोटी सी पगडंडी स्त्रियों की पदचापों से भी बनी है। इस पगडंडी के दोनों तरफ सहेज कर रखे गए दुखों की झड़बेरियां हैं, उनकी खऱोंच खाकर भी निकाले गए सुखों की फलियां हैं और राग-विराग, निस्संगता-असंगता और संलग्नता के तारों पर सूखती अनगिनत यादें भी हैं। ऐसी ही पगडंडियों से निकलती कवयित्री अचानक क्रांति चौक पर पहुंच जाती है और बताती है- ‘आज मैं इतिहास से टकरा गई / लेकिन वह मुझको पहचान ही न पाया। / भूल चुका था मुझको पूरा वह / भूल चुका था कि मैं उसकी ही कक्षा में थी।‘
कविता यहां दरअसल ख़त्म नहीं, शुरू होती है- और वह समस्या भी जो अनामिका का अनायास अनगढ़पन पैदा करता है। दरअसल अनामिका के रचना संसार में परंपरा का यह महासागर बहुत बड़ा है, लेकिन इस महासागर में आधुनिकता के छोटे-छोटे टापू नहीं, बड़े-बड़े महाद्वीप तैरते हैं- अतीत के जल के बीच पड़ी वर्तमान की उन विराट शिलाओं की तरह जिनसे गुजरे बिना, जिनको बसाए बिना यह दुनिया बस नहीं पाती है। यह आधुनिकता हर परंपरा के साथ जैसे गुंथी हुई है। वह थेरियों की बातचीत के बीच कुरियर भी ले सकती हैं, मोबाइल फोन भी सुन सकती हैं और लाखों अनाम पाठकों की टीपें भी पढ़ सकती है। अचानक एहसास होता है कि यह जो थेरियां हैं, यह जो उनका संवाद है, इतिहास के सदियों लंबे रास्तों पर यह जो चहलकदमी है वह पहले कभी हो चुकी है, अब उसे नए सिरे से जिया और रचा जा रहा है- यह इतिहास को, दुख को, संवाद को ज्यों का त्यों रख देने की, मंचित कर देने की युक्ति नहीं है, उसे अपने भीतर उतार कर कुछ नया बनाकर प्रस्तुत करने की यातना भी है। इसी रास्ते ‘तिलोत्तमा थेरी’ मिल सकती है जो याद करती है- “’तुम्हारा सुधार नहीं, / व्यर्थ मैंने ऊर्जा ज़ाया की’,/ खासे संताप से उसने कहा / और चला गया! / जब वह चला ही गया / राममोहन राय, ईश्वरचंद्र, कार्वे, राणाडे, ज्योतिबा फुले, / पंडित रमाबाई, सावित्री बाई- / सब मुझसे मिलने आए! / उन्होंने मेरा माथा सहलाया / और बोलीं धीरे से- / ‘इतिहास के सुधार आंदोलन / स्त्री की दशा को निवेदित थे, / और सुधरना किसे था, यह कौन कहे।‘”
क्या इसके बाद भी यह संशय रह जाता है कि अनामिका इतिहास की किन ताकतों के विरोध में ख़डी हैं और किन हाशिए पर पड़े मूल्यों का घर बसाने निकली हैं? बहुत गहरी परंपरा में अनुस्युत और उसकी बहुत सारी परतों से परिचित कोई लेखिका ही इतनी सुघड़ता से इतिहास के सुधारों की कलई खोल सकती है। ऐसी सुघड़-दृष्टिसंपन्न कवयित्री ही ‘गणिका गली’ जैसी कविता लिख सकती है और साहसपूर्वक कह सकती है- ‘सभ्यता से भी प्रचीन / ये नदियों का तट थीं विस्तीर्ण- / चोर, नपुंसक, मूर्ख, संन्यासी, लंपट, सामंत / इनके तट आते डूबती नौकाओं पर / और ये उन्हें उबार लेतीं।‘ ऐसा नहीं कि अनामिका इस गणिका गली का कोई आभामंडित और वायवीय भाष्य रच रही हों, वे बिल्कुल ठोस ढंग से इस बंद गली की विडंबनाओं को पहचानती हैं और अपने अधेड़ होते समय से उनकी थकी हुई मुठभेड़ को भी जानती हैं। यह कविता अपनी अगली पंक्तियों में ही बिल्कुल बदल जाती है- ‘अब इनके प्रेमी अधेड़ विस्थापित मजूर, “इनसे तो पैसे भी नहीं मांगते बनता ऐ हुज़ूर! पर हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं विस्तृत क्षितिज पर ककहरे- “ उन्होंने उमग कर कहा और खांसने लगीं। लेटी हुई छत निहारती अपभ्रंश का विरह गीत दीखती हैं ये गणिकाएं पुराने शहर के लालटेन बाज़ार में लालटेन तो नहीं जलती, पर ये जलती हैं लालटेन वाली धुंधली टिमक से।‘
यह अनामिका हैं। उन्हें उस बुझती हुई कमज़ोर रोशनी का इतना साफ पता मालूम है कि जैसे यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे सर्वस्थानीय से नितांत अतिस्थानीय हो उठती हैं, सार्वकालिक से बिल्र्कुल कालबद्ध। वे स्त्रियों की ठीक उस रग पर उंगली रख पाती हैं जहां से दर्द फूटता है। उनके यहां एक विराट स्त्री गाथा है जो पुराने शोषण और उपेक्षा के जाने-पहचाने मुहावरों से नहीं बनी है, जो लैंगिक समानता की सूक्तियां गढ़ने के मोह में नहीं पड़ती, लेकिन जिसमें अतीत के मर्मभेदी अकेलेपन का सिर्फ अपनी सामूहिकता से सामना कर रही स्त्रियां मिलती हैं हालांकि वे भी सभ्यता के इस सफ़र में महसूस करती हैं कि, ‘हकासी-पियासी सड़क / चल रही थी साथ मेरे / एक आरंभ अधबना सा / बीच में ही ढह गया था। एक अर्थ फूट गया था / प्याऊ के दूसरे घड़े सा / एकदम बीच रास्ते।‘
कहने की ज़रूरत नहीं कि यह करुणा की कविता है, उस रचनात्मकता की जो सभ्यता की कोख से फूटती है। इसलिए इन कविताओं में सूक्तियां नहीं हैं, मगर एक दार्शनिक तत्व है- कहीं छुपा हुआ नहीं, बेहद प्रत्यक्ष और कहीं-कहीं इतना प्रगल्भ कि कविता के बीच उसकी उपस्थिति खटकने तक लगे- या लगे कि इस दर्शन के लिए ही यह कविता लिखी जा रही है।
बहरहाल, हिंदी में एक ख़तरा यह है कि जब भी आप किसी कविता के भीतर कोई स्त्री गाथा देखते हैं, उसे फौरन स्त्री विमर्श की चालू शब्दावली में स्वीकार करने या ख़ारिज करने का खेल शुरू हो जाता है। यह बात स्पष्ट ढंग से कहनी होगी कि यह स्त्री विमर्श नहीं है, यह समकालीन विमर्श है जिसमें अपने समय के बाकी सवालों के प्रति भी एक सख्य भाव है। अनामिका के कविता संसार में सांप्रदायिकता के उभार से लेकर बाज़ारवाद के प्रभाव तक की, उत्तर आधुनिकता और भूमंडलीकरण के विस्तार से लेकर रोज़मर्रा की उन कहानियों तक की, जो अख़बारों की मार्फत बनने वाले सूचनाओं के समंदर में बुलबुले की तरह उठती और फिर बिला जाती हैं- एक गहन चीरफाड़ अनवरत देखी जा सकती है। अपनी किताब ‘स्त्रीत्व के मानचित्र’ में अनामिका ने जो यह लक्ष्य किया है कि दुनिया भर में स्त्री आंदोलन अकेला नहीं चला है, कहीं वह अश्वेत आंदोलन से जुड़ा है, कभी पर्यावरण की लड़ाई से और कहीं मानवाधिकार के एजेंडे से- यह सख्य भाव इन कविताओं में भी दिखता है- यह एक समकालीन गाथा है जिसे इतिहास की दूरबीन लेकर एक स्त्री आंख देख रही है और इस आंख में संवेदना और करुणा का जल है- उसकी हलचल है।
कई बार यह विराट हिलती-डुलती दृश्यमयता इतनी चंचल हो जाती है कि कविता की लय बिखरती मालूम होती है, कई बार घटनाओं, जगहों और कालों का एक-दूसरे में अतिक्रमण ऐसी असुविधा पैदा करता है, जैसे लगता है कि हम सुव्यवस्थित, सुरचित कविता नहीं पढ़ रहे, एक कवयित्री के भीतर उमड़-घुमड़ रहे बहुत सारे भावों के बीच आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन यहीं से यह समझ भी बनती है कि दरअसल कोई बड़ी कविता कई बार अपने काव्यत्व और काव्य-विन्यास में तोड़फोड़ करके ही संभव होती है।
एक खिलंदड़ापन भी इन कविताओं में लगातार मिलता रहता है। ‘अन्ना करेनिना: चैपमैन बहूद्देश्यीय कन्या विद्यालय के पुस्तकालय में’ कवयित्री रूस जाने और रूठ जाने को मिलाती हैं- याद करती हुई कि रूसना क्रिया दरअसल रूठने की भी पर्याय है और बताती हैं कि स्त्रियां बार-बार रूस जाती हैं। और इस कन्या विद्यालय के पुस्तकालय में बैठे-बैठे की जा रही इस रूस की प्रदक्षिणा में क्या मिलता है? ये पंक्तियां बताती हैं: ‘अन्ना केरेनिना टहल रही थी / वोल्गा के किनारे / अपने बड़े गाऊन में। / मैं उससे लिपट गई / एक पूरी ज़िंदगी / मैं घूमती ही रही मॉस्को की गलियों में / उससे बतियाती! / फिर वक़्त चलने का आया, / चलते समय मैंने देखा- बंद ही नहीं हो रहा था मेरा सूटकेस! / लगातार तब से तहा रही हूं कपड़े और स्मृतियां’।‘
अनुभव और अध्ययन की यह जो संपदा है, वह रोज़मर्रा के अनुभवों को भी, बड़े और सुंदर प्रतीकों में बदल डालती है। ‘चल पुस्तकालय’ में वेद कुरआन के पड़ोस में निश्चिंत सोए मिलते हैं और टॉल्स्टाय, चेखव, रवींद्र और प्रेमचंद सटे हुए बैठे हैं। बड़े दिल से लिखती है कवयित्री – ‘घर के सब कामकाज निबटा कर / चल पुस्तकालय चली आई / उन सब गृहणियों के जीवन का / पहला और अंतिम रोमांस / वही थे।‘
तो सारी दुनिया को देखती, परंपरा और आधुनिकता को घोल कर फेंट कर, आती-जाती सभ्यताओं को खंगाल कर, अपने हिस्से की कविता गढ़ती यह कवयित्री दरअसल एक नए जीवन का संधान करती है- कविता छूटे तो छूट जाए, यह जीवन-दृष्टि न छूटे, यह मार्मिक और मानवीय खयाल जैसे इस संग्रह की केंद्रीय धूरी है। ‘टोकरी में दिगंत’ निश्चय ही हमारे समकालीन रचना समय की एक उजली उपलब्धि है।
प्रियदर्शन की फेसबुक वाल से साभार