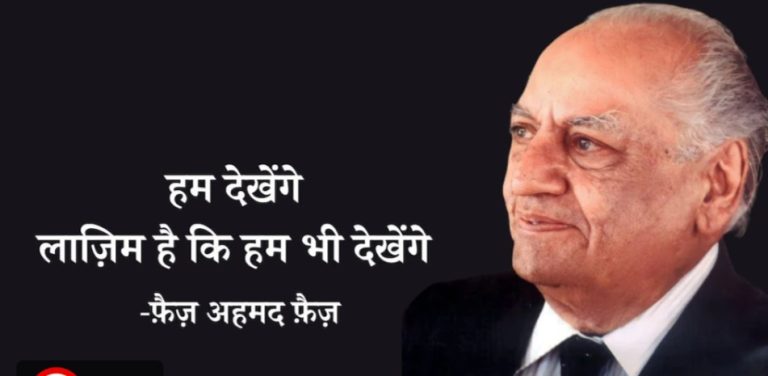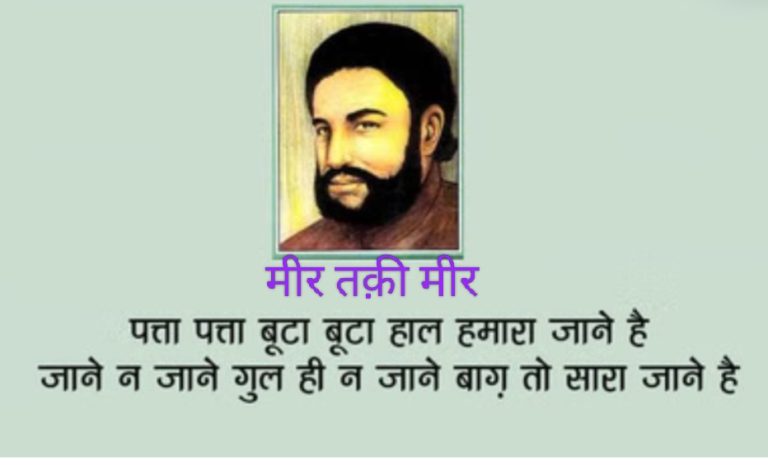महामारी से निपटने को लेकर मोदी और उनकी सरकार की योजनाएं लोगों की समझ से परे हैं। सामाजिक विश्वास का जिस क़दर क्षरण हुआ है, उसकी भरपाई कोई भी चुनावी जीत से नहीं हो पायेगी।
कोविड-19 की दूसरी लहर में पिस रहे भारत को दिलासा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 20 अप्रैल की रात को सम्बोधित किया था, मगर तबतक काफ़ी देर हो चुकी थी, शहरों से प्रवासी श्रमिक पहले ही अपने गृह राज्य लौटना शुरू कर चुके थे। वे उन नियोक्ताओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने उन्हें शहरों में रुक जाने की विनती की थी, और इस बात की संभावना भी नहीं थी कि वे मोदी की उन बातों पर ध्यान दें, जिन्होंने अपने 20 अप्रैल के भाषण में कहा था, “मैं राज्य प्रशासन से श्रमिकों में विश्वास को बढ़ाने और उन्हें उन शहरों में रहने के लिए समझाने-बुझाने का आग्रह करता हूं, जहां वे रहते हैं। ”
प्रवासी श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पलायन भारत में सामाजिक विश्वास या सामाजिक थाती में गिरावट का एक स्पष्ट सबूत है। सामाजिक विश्वास इस धारणा से जुड़ा होता है कि सरकारें, सार्वजनिक संस्थान और बड़े पैमाने पर लोग आम लोगों के फ़ायदे के लिए काम करेंगे या फिर ये सब उन्हें कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी भी समाज में विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक विश्वास का अलग-अलग स्तर होता है।राजनीतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट पुटनाम अपनी किताब, बॉलिंग अलोन: द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ़ अमेरिकन कम्युनिटी लिखते हैं, “‘ ‘समृद्धों’के मुक़ाबले ‘वंचित’ कम विश्वास करने वाले होते हैं, शायद इसलिए कि समृद्धों के साथ दूसरे लोग ज़्यादा ईमानदारी और सम्मान के साथ पेश आते हैं।”
यक़ीनन पिछले साल दुनिया के सबसे सख़्त लॉकडाउन के अपने तजुर्बे से डर हुए प्रवासी श्रमिक अपने-अपने घर की तरफ़ तेज़ी से कूच कर गये हैं, हालांकि उनमें से कुछ संक्रमित भी हो सकते हैं, जिनके साथ यह वायरस भी पहुंच रहा हो, लेकिन ऐसा वे इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि एक-एक करके राज्य सरकारों ने पूरे भारत को आगोश में लेने वाले कोविड-19 की दूसरी लहर पर क़ाबू पाने के लिए कर्फ़्यू लगा दिया है। उनका घर की तरफ़ कूच कर जाना दरअस्ल सामाजिक विश्वास और कोविड-19 के प्रसार के बीच की एक ऐसी कड़ी को दिखाता है, जो कई देशों में सर्वेक्षण और अध्ययन का विषय बन गया है।
इस तरह के बारह अध्ययनों की समीक्षा चार राजनीतिक वैज्ञानिकों-डैनियल डिवाइन, जेनिफ़र गस्केल, विल जेनिंग्स और गेरी स्टोकर्स ने अपने शोध-पत्र, ’ट्रस्ट एंड द कोरोनवायरस महामारी: व्हाट आर द कन्सेक्वेंसेजेज ऑफ़ एंड फ़ॉर ट्रस्ट ?’ में की है, जो पॉलिटिकल स्टडीज़ रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने इस बात का अनुमान लगाने के लिए चार आधार-तत्वों को निर्धारित किया कि सामाजिक विश्वास उस SARS-CoV-2 के वायरस संचरण को किस तरह प्रभावित कर सकता है, जो कोविड-19 का कारण है। उन्होंने इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया कि इस महामारी का सामाजिक विश्वास पर क्या असर पड़ सकता है।
इन चार राजनीतिक वैज्ञानिकों के निर्धारित आधार-तत्वों को भारत पर लागू करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर मोदी की तरफ़ से अपनायी गयी नीतियों ने भारत की सामाजिक थाती को नष्ट कर दिया है, उस मध्यम वर्ग का सामाजिक विश्वास जाता रहा है, जो पुटनाम के विश्लेषण का बड़ा आधार है और जिस तबके का व्यवस्था में बहुत विश्वास रहा है और उनके भीतर यह सवाल भी हाहाकार मचा रहा है कि SARS-CoV-2 का प्रचंड ज्वार जब भारत को अपने आगोश में लेने को आतुर था, तब उसपर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की गयी। हक़ीक़त तो यही है कि इस तरह के अविश्वास जताने वाले लोगों की तादाद में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
अमल
इन चारों राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है, “उच्च सामाजिक और राजनीतिक विश्वास प्रतिबंधात्मक नीतियों को राजनीतिक रूप से अपनाने से जुड़ा हुआ है।” सरकारें अपने ऊपर भरोसा करने वाले उन लोगों की तरफ़ झुकी होती हैं, जिन्हें किसी प्रतिबंधात्मक नीतियों को अमल में लाने के आदेश जारी करने के बजाय सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने या मास्क पहनने जैसे अपने व्यवहार को विनियमित करना पसंद है। लोगों ने बड़े पैमाने पर उस विश्वास को अपनी सरकारों में बनाये रखा था, जो विश्वास उन पर सरकारों ने की थी। लॉकडाउन की घोषणा तभी की गयी, जब आत्म-संयम वायरस के संचरण को रोक पाने में नाकाम रहा।
लेकिन, इस वायरस के मौजूदा वैरिएंट के विपरीत, पिछले साल SARS-CoV-2 को लेकर भारत ने जो लॉकडाउन लगाया था, वह बेहद सख़्त था। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का स्वेच्छा से अपने व्यवहार को संयमित करने को लेकर लोगों पर बहुत ही कम विश्वास रह गया था। लोगों में मोदी के विश्वास की कमी के चलते उन्हें जवाबी कार्रवाई के तौर पर उस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने के लिए विवश होना पड़ा, वे जैसे-तैसे अपने-अपने घर की तरफ़ चल पड़े, ऐसा इसलिए हुआ था, क्योंकि उनसे रोज़गार छिन लिया गया था और उन्हें पगार देने से इन्कार कर दिया गया था। इस तरह, लॉकडाउन भूख और अभाव का पर्याय बन गया था, ठीक वही वजह है कि वे देश में दूसरी लहर के सैलाब के बीच भी वे फिर से अपने-अपने घर की ओर कूच कर गये हैं।
सरकार का लोगों में विश्वास की कमी के दो मनोवैज्ञानिक निहितार्थ हैं। एक तो पिछले साल के मध्य में भारत में लॉकडाउन का ख़त्म किया जाना कहीं न कहीं लोगों के अवचेतन में सामान्य स्थिति की वापसी के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे में लोग एहतियाती क़दम उठाने के मामले में सुस्त पड़ गये थे। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने सरकार के इस क़दम को तर्कहीन इसलिए पाया था, क्योंकि सरकार ने देश में तब लॉकडाउन लगा दिया था, जब कोविड-19 के मामले महज़ 500 के आसपास थे। सितंबर में एक ही दिन में कोविड संक्रमण के तक़रीबन एक लाख के आस-पास तक मामले के चरम तक पहुंच जाने के बावजूद सरकार ने लॉकडाउन हटाना भी शुरू कर दिया था। चूंकि इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार ने जो बात कही, उसकी कोई साख रही नहीं।
इससे भी बदतर तो यह हुआ कि लॉकडाउन लोगों के लिए यह फ़ैसला करने का मापदंड बन गया कि सरकार वास्तव में यह मानती है कि यह वायरस सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है भी कि नहीं। 2020 के उनके अनुभव ने उन्हें यह सबक दे दिया था कि राज्य सरकारों की तरफ़ से लगा जाने वाले लॉकडाउन के पहले संकेत के बाद ही उन्हें अलग-अलग शहरों से अपने-अपने घर के लिए कूच कर जाना चाहिए।उनकी यही धारणा दूसरी लहर की शुरुआत के साथ सामने आयी है।
अनुपालन
इन चार राजनीतिक वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सामान्य नियम के तौर पर प्रतिबंधात्मक उपायों का अनुपालन “उन उच्चतर विश्वास वाले लोगों (समाज में) में कहीं ज़्यादा है।” लेकिन, वे एक चेतावनी भी देते हैं, “यह उन लोगों पर विश्वास करने के लिहाज़ से सशर्त हो सकता है, जो आदेश देते हैं।”
भारतीयों ने मोदी पर व्यापक रूप से भरोसा किया है, यह बात 14 घंटे के उस जनता कर्फ़्यू की कामयाबी से साफ़ हो गयी थी, जिसे मोदी ने पिछले साल 22 मार्च को लोगों से स्वेच्छा से पालन करने के लिए कहा था। यहां तक कि पिछले साल 25 मार्च से शुरू होकर 1 जून तक चलने वाला लॉकडाउन भी काफ़ी हद तक तबतक कामयाब रहा, जबतक कि भूख और डर से मज़दूर वर्ग हिल नहीं गया। उस लॉकडाउन को वास्तव में मध्यम वर्ग का समर्थन मिला था।
मगर इस दूसरी लहर में सामाजिक अविश्वास का विस्तार इस मध्य वर्ग तक भी हुआ है। जैसे-जैसे अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन कम पड़ते जा रहे हैं, कोविड-19 के शिकार लोगों के अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान और क़ब्रिस्तान के बाहर कतारें लग रही हैं, दवाओं की कालाबज़ारी हो रही है, वैसे-वैसे मध्यम वर्ग मुसीबत से राहत पाने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करने में भी असमर्थ होता जा रहा है। यहां तक कि जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं, उन्हें अपने संक्रमण होने के डर से कंपकपी छूट रही है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें इस बात पर अचरज होता है कि आख़िर इस दूसरी लहर को लेकर भारत सावधानी क्यों नहीं बरत पाया। इसका एक कारण तो यह है कि मोदी इस पर क़ाबू पा लेने की स्थिति से पहले ही कोरोना पर विजय पा लेने का ढिंढोरा पीटने लगे थे। मसलन, 28 जनवरी को मोदी ने कहा था, “पिछले साल फ़रवरी-मार्च में बहुत सारे विशेषज्ञों ने देश में 20 लाख लोगों की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। आज दुनिया की 18% आबादी वाले भारत ने स्थिति पर क़ाबू पाकर दुनिया को आपदा से बचा लिया है।”
इस तरह की टिप्पणियों ने लोगों को एकदम निश्चिंत कर दिया था, हालांकि मोदी ने ख़ुद को श्रेय देते हुए लोगों को अपने बचाव के उपायों में कमी लाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन, उनकी कार्यशैली ने लोगों के सामने कोरोनावायरस को लेकर पूरी तरह से एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी है। उदाहरण के लिए, मेक-इन-इंडिया मंत्र के साथ उनके जुनून ने भारत में उत्पादित हो रहे दो टीकों के अलावे और भी टीकों की उपलब्धता को बढ़ावा देने को लेकर दवा कंपनियों के साथ अनुबंध करने में उनकी सरकार ने देरी की है। उनकी वैक्सीन नीति बताती है कि उनका मानना रहा है कि भारत ने SARS-CoV-2 को दबा दिया है, और इसे लेकर हड़बड़ी की कोई वजह नहीं है।
उनके इस आत्मविश्वास, यानी लापरवाही के और भी स्पष्ट संकेत थे। भारत का चुनाव आयोग, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शायद ही कभी केंद्र सरकार की इच्छा के ख़िलाफ़ काम करता है, उसने एक महीने चलने वाले विधानसभा चुनाव के आठ चरण निर्धारित किये। भाजपा को पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए अनुकूल समय सीमा की ज़रूरत थी। इस अवधि के दौरान भाजपा ने कोविड-उपयुक्त व्यवहार को ख़ुद ही नहीं अपनाया, मसलन गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किये; मोदी ने अपनी रैलियों में भारी भीड़ को संबोधित किया। मानों इतना ही काफ़ी नहीं था, ऊपर से उत्तराखंड और केंद्र की दोनों सरकारों ने महाकुंभ के लिए हरिद्वार में लाखों लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति देने का फ़ैसला कर लिया।
इस पृष्ठभूमि को देखते हुए बातों में आ जाने वाला कोई मासूम ही कोविड-19 की विनाशकारी इस दूसरी लहर के लिए आम लोगों पर यह दोष मढ़ेगा कि उन्होंने वायरस के प्रसार को रोकने की ख़ातिर उपयुक्त व्यवहार नहीं अपनाया गया।
जोखिम का बोध
शोध पत्र पेश करने वाले उन चार राजनीतिक वैज्ञानिकों का कहना है, “जोखिम का बोध तब ज़्यादा हो जाता है, जब लोगों को विज्ञान और चिकित्सा पेशेवरों पर कम भरोसा रह जाता है।”
भारतीयों को जिस तरह का विश्वास चिकित्सा पेशेवरों में नहीं है, उसी तरह का विश्वास विज्ञान में भी नहीं है। आख़िरकार, मोदी का भी तो यही कहना रहा है कि अंग प्रत्यारोपण और स्टेम सेल थेरेपी जैसी आधुनिक चिकित्सा से भारत के प्राचीन ऋषि परिचित थे। वायरस से निपटने के लिए घरेलू उपाय तबतक ख़तरनाक नहीं हो सकते, जब तक कि आधुनिक दवाओं का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों से तौबा नहीं कर लिया जाता।
इसके बावजूद, उन चार राजनीतिक वैज्ञानिकों के मुताबिक़, पारंपरिक ज्ञान में आम विश्वास के चलते भारत में जोखिम के बोध की संभावना ख़तरनाक और मूर्खतापूर्ण हद तक कम है। इससे उनमें वायरस को लेकर इम्युनिटी का ग़लत बोध पैदा हो सकता है। भारत के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन जैसा शख़्स भी हैं, जिन्हें पतंजलि आयुर्वेद के कोरोनिल नामक उस उत्पाद का समर्थन करने का कोई मलाल नहीं है, जिसे कोविड-19 के इलाज के तौर पर प्रचारित किया गया था और इसका स्वामित्व भाजपा के पसंदीदा स्वामी, बाबा रामदेव हाथ में है।भला हो उस भारतीय चिकित्सा संघ का, जिसने इसका ज़ोरदार विरोध करते हुए कहा था, “स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ़ से पूरे देश में एक अवैज्ञानिक दवा का झूठा और मनगढ़ंत प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और इस दवा का डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा ख़ारिज किया जाना देश के लोगों के मुंह पर एक तमाचा है और देश के लिए अपमानजनक भी है।”
अब आइये, ज़रा उस संभावित कारण की छानबीन करें कि सरकार ने उस महाकुंभ का आयोजन पहले ही किस लिए करा दिया, जिसे पारंपरिक तौर पर 2022 में आयोजित होना था। ऐसा इसलिए किया गया, “क्योंकि ‘मेष राशि में प्रवेश करने वाले सूर्य और कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले बृहस्पति’ का ‘ज्योतिषीय विन्यास’ इस बार 2021 तक ही उपलब्ध थे।” श्रद्धालुओं की धर्म में आस्था दरअस्ल विज्ञान को प्रभावित करता है, यही वजह है कि हमें उन चार वैज्ञानिकों के उस स्वत:सिद्ध प्रमाण को पढ़ने की जहमत उठानी चाहिए, जिसमें वे कहते हैं कि जब लोगों का धर्म में ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है, तो जोखिम का बोध तबाही आने के स्तर तक कम हो जाता है। शायद धर्म की उपचार शक्ति में भारत का विश्वास अब भी है, क्योंकि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1% से थोड़ा ही ज़्यादा ख़र्च करता है। स्वास्थ्य के चरमराये हुए बुनियादी ढांचे के साथ भी भगवान पर आस्था उतना ही ज़्यादा है, जितना कि कोविड-19 पर क़ाबू पा लेने का बेवजह विश्वास बना हुआ है।
मृत्यु-दर
भारत का चरमराया हुआ स्वास्थ्य ढांचा इन चार राजनीतिक वैज्ञानिकों के एक और सिद्धांत की गंभीरता को रेखांकित करता है कि “संस्थागत भरोसा मृत्यु दर के निम्न स्तर के साथ जुड़ा हुआ है।”
बीमार लोगों की सहायता के लिए सामने आती बुनियादी ढांचे की चरमरहाट शायद बचे-खुचे संस्थागत विश्वास को भी ख़त्म कर दें, क्योंकि अब कुछ ही लोग सरकार के आंकड़ों पर विश्वास कर पा रहे हैं। मसलन, न्यूज़क्लिक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल में भोपाल में तक़रीबन 1, 000 कोविड-संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया या दफनाया गया, लेकिन सरकारी आंकड़ों में दावा किया गया है कि उसी अवधि में 50 से भी कम लोग मारे गये हैं। इसी तरह, बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से है और यहां लोग मुसीबत में हैं, लेकिन इस राज्य के अधिकारी स्थिति के नियंत्रण में होने की बात करते हैं। राउटर की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि लगातार जलाये या दफ़नाये जा रहे शवों ने कोविड-19 से दम तोड़ने वाले लोगों के बारे में भारत की तरफ़ से बतायी जाने रही संख्या पर ऊंगली उठा दी है।
भारत सरकार की तरफ़ से मिली सूचना के मुताबिक़ 20 अप्रैल को कोविड-19 के 2, 94, 290 मामले थे और मरने वालों की संख्या 2020 थी। मीडिया और लोगों के बीच कही-सुनी बातों से पता चलता है कि इससे कहीं ज़्यादा संख्या होने की संभावना है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या पहले ही 1, 82, 570 तक पहुंच चुकी है, इसके साथ ही ऐसा लगता है कि जब तक भारत इस महामारी से बाहर आयेगा, तब तक यह भारत पस्त हो चुका होगा और बुरी तरह से हिल चुका होगा। जैसा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में प्रोफ़ेसर डॉ. संजय राय ने पिछले सप्ताह न्यूज़क्लिक से बातचीत में बताया था कि यह पता लगाना भी मुश्किल है कि भारत में और कितनी लहरें आयेंगी।
पिछले अनुभवों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कि मोदी ने महामारी से मुक़ाबला करने के बजाय भारत की महामारी पर जीत हासिल करने की कहानी गढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। पिछले साल कोविड के उफ़ान से निपटने के लिए जो विशेष अस्पताल बनाये गये थे, उन्हें बंद कर दिया गया है; भले ही स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने की रौशनी में भी 2020 का लॉकडाउन लगाया गया हो, लेकिन वेंटिलेटर की आपूर्ति अब भी कम बनी हुई है। मोदी की दोषपूर्ण वैक्सीन नीति उनके उस बेबुनियाद विश्वास का नतीजा थी, जिसके तहत यह प्रचारित किया गया था कि उनके नेतृत्व में भारत ने SARS-CoV-2 पर क़ाबू पा लिया है।
विश्वस के नतीजे
ये चार राजनीतिक वैज्ञानिक बताते हैं, “कोविड-19 का व्यक्तिगत जोखिम भरोसे के कम होते जाने के साथ जुड़ा हुआ है; लॉकडाउन के अमल में लाये जाने से लोगों में बेहतर विश्वास पैदा हो सकता है।” इस सैद्धांतिक आधार का पहला भाग बहुत आसान है और वह यह कि जो लोग दूसरी लहर में बीमार पड़ गये, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के साथ हुए अपने सामना के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं थी, वे भी चिंतित थे कि विशेष देखभाल की ज़रूरत होने पर उनकी किस तरह की दुर्दशा हो सकती है।
कम सामाजिक विश्वास वाले लोग लॉकडाउन को अपनी चिंताओं के समाधान के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक संपर्क में होने वाली कमी के बढ़ने से ही कोविड-19 के सामुदायिक संचरण में कमी आयेगी। लेकिन, यह एक ऐसा समाधान है, जिसे मोदी सरकार पेश करने से कतरा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से ही संकुचन की शिकार है, ऊपर से एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन आर्थिक सुधार की संभावना को और भी कम कर देगा।
यही कारण है कि 20 अप्रैल के उनके भाषण को पिछले साल 22 मार्च के जनता कर्फ़्यू जैसे उपाय का सहारा लेने के लिए तैयार किया गया था। अगर सीधे-सीधे शब्दों में कहा जाये, तो मोदी चाहते हैं कि भारतीय घर के अंदर रहें, लेकिन वह किसी भी सूरत में वह लॉकडाउन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। मोदी को उन चार राजनीतिक वैज्ञानिकों की बात पर ध्यान देना चाहिए, जो सामाजिक विश्वास और महामारी के बीच की कड़ी पर 12 अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर कहते हैं, “सरकार, जो संगठित है, उसे अपने संदेश में एकदम स्पष्ट होना चाहिए और बढ़े हुए निष्पक्ष विश्वास के रूप में उसे तभी देखा जाता है।”
लेकिन, मोदी का 20 अप्रैल का भाषण भ्रमित करने वाला था। उन्होंने उन्हीं राज्य सरकारों के कांधे पर महामारी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश की है, जिनकी शक्तियों को उन्होंने पिछली बार छीनने की कोशिश की थी। वह चाहते हैं कि राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों को शहरों में ही रहने के लिए मनायें। यह अजीब बात है कि मोदी एक तरफ़ जहां लोगों से अपने घर के अंदर ही रहने की अपील करते हैं, वहीं वह यह भी चाहते हैं कि कारखाने अपना उत्पादन जारी रखें। वह चाहते हैं कि नौजवान अपने-अपने पड़ोस में स्वयं सहायता को बढ़ाते हुए समितियों का गठन करें ताकि क़ानून के बिना हस्तक्षेप के कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। वह चाहते है कि बच्चे अपने माता-पिता पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वे बाहर क़दम न रखें, ऐसा करते हुए अपने बुज़ुर्गों के साथ अनिवार्य रूप से भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने से भी नहीं चुकें। वह एक ऐसे नेता के रूप में सामने आये हैं, जिन्होंने संकट के समय लोगों को प्रेरित करने के लिहाज़ से अपनी ताक़त खो दी है।
कोविड-19 के साथ भारत की यह लड़ाई दरअसल भारत की सामाजिक थाती को कम करने में मोदी की भूमिका का एक अध्ययन है। उनकी चुनावी जीत अक्सर ध्रुवीकरण की राजनीति के ज़रिये सुनिश्चित भले ही हो जाती हो, लेकिन उनकी चुनावी जीत भारत में सामाजिक विश्वास के तेज़ क्षरण की भरपाई कभी नहीं कर सकती।
सौज- न्यूजक्लिकः लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और इनके विचार निजी हैं।अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें