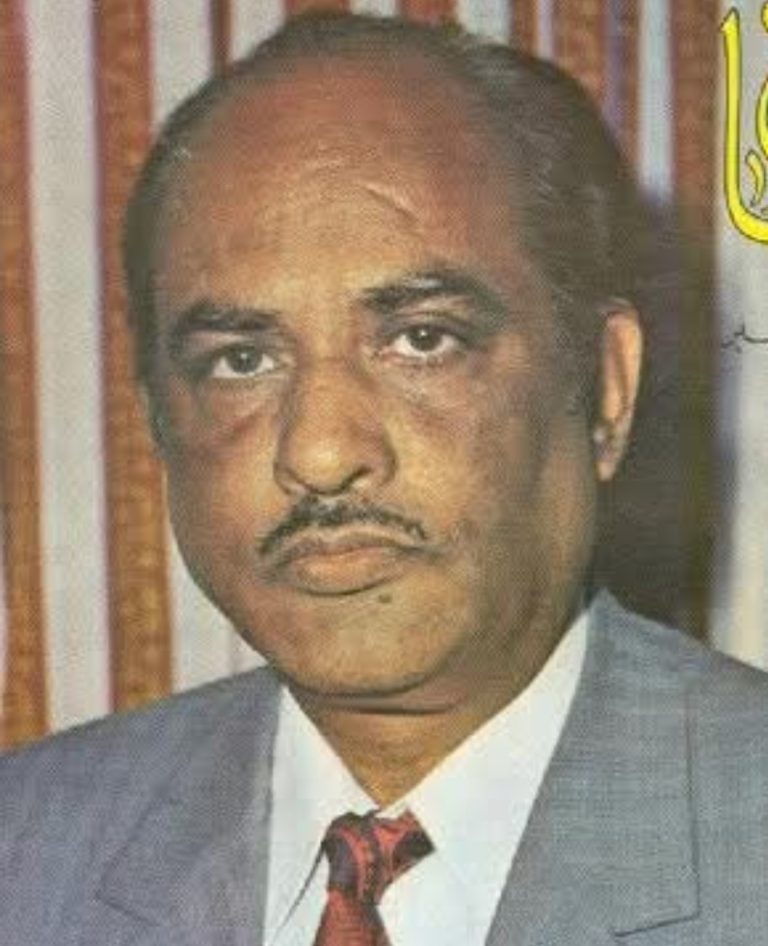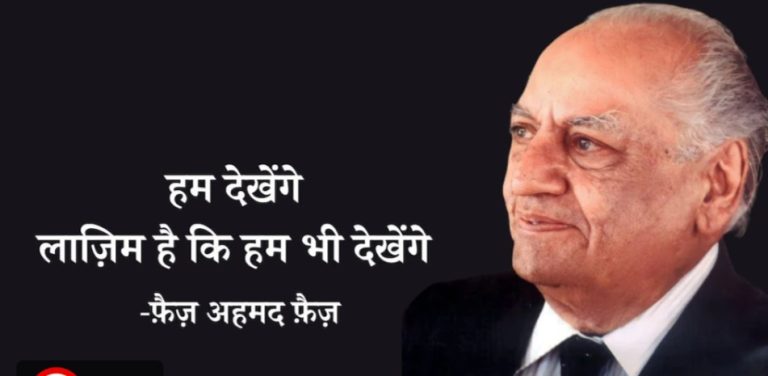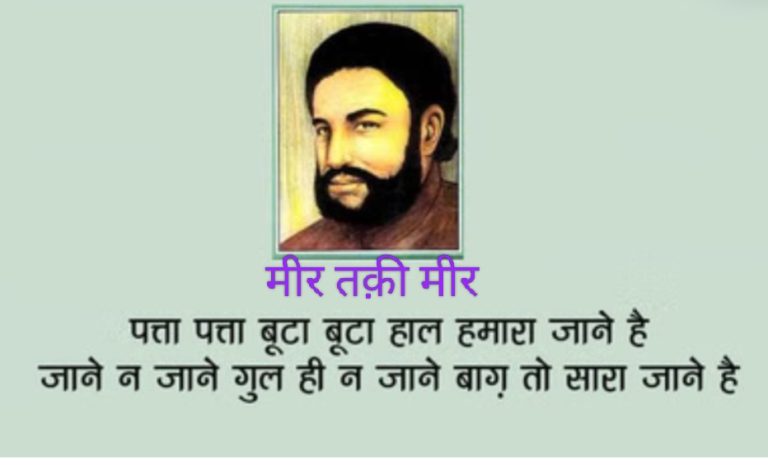जाने-माने मार्क्सवादी इतिहासकार का कहना है कि अपने विषय को वास्तविक रूप से पेश किये जाने को लेकर प्रतिबद्ध सभी इतिहासकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसे तत्काल वापस लेने की मांग को उठाने में शामिल हो जाना चाहिए।
यह लेख इस साल मार्च में जाने-माने मार्क्सवादी इतिहासकार प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब के लिखे एक लेख का संशोधित संस्करण है। यह लेख मूल रूप से सोशल साइंटिस्ट पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और इसे SAHMAT या सफ़दर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से न्यूज़क्लिक को उपलब्ध कराया गया है।
हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इतिहास पाठ्यक्रम के मसौदे पर विवाद की उस पृष्ठभूमि में इस लेख पर फिर से विचार कर रहे हैं, जिसमें डीडी कोसंबी, आरएस शर्मा, डीएन झा और इरफ़ान हबीब जैसे मशहूर इतिहासकारों की किताबों को छोड़ दिया गया है। इसके बजाय, इस मसौदा पाठ्यक्रम में ऐसे कुछ लेखकों की किताबों को शामिल करते हुए भगवाकरण के एजेंडे को अपनाने का प्रस्ताव है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी निष्ठा संघ परिवार के प्रति हैं। उदाहरण के लिए, इस सिलेबस (प्राचीन भारत) का मक़सद इतिहास के बजाय पौराणिक कथाओं का महिमामंडन करना प्रतीत होता है, साथ ही इस लेख में प्रोफ़ेसर हबीब यह भी लिखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का द्रविड़ संस्कृति से किसी भी तरह के जुड़ाव को खारिज कर दिया गया है।
हमें हमेंशा इस बात को याद रखना होगा कि हमारे पास एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसके असरदार शख़्सियत ने 2014 में देश के प्रधान मंत्री पद पर काबिज होने के तुरंत बाद यह ऐलान कर दिया था कि भारत को प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक का उस पौराणिक काल से ही जानकारी थी, जब हमारे सर्जनों ने भगवान गणेश के शरीर पर हाथी का सिर लगा दिया था। यह अपेक्षित ही था कि विश्वविद्यालय स्तर पर इतिहास के सिलेबस को फिर से संशोधित किये जाने ज़रिये इतिहास में जल्द ही इस तरह के ज्ञान को शामिल किया जायेगा।
इस सिलसिले में पहला क़दम अब एक कर्तव्यनिष्ठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कथित “लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ़्रेमवर्क (LOCF): बीए हिस्ट्री अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, 2021” के ज़रिये उठाया गया है। इसमें जो कुछ भी होगा, यह ज़ोरदार शीर्षक उस बात की महज़ एक भूमिका है। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालयों से अब इस “ढांचे” को अपनाने और इस मूल तत्व में निर्दिष्ट विषयों के मुताबिक़ अपने-अपने शिक्षण और परीक्षाओं की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि ग्रंथ सूची में सूचीबद्ध किताबों को इन विषयों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना है।
यह माना जाना चाहिए कि इस ‘ढांचे’ में शामिल नहीं किये गये विषय-वस्तुओं पर बीए डिग्री परीक्षाओं में सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। इस तरह, इन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षण से बाहर रखा जायेगा। दूसरी ओर यहां जिन प्रसंगों पर ज़ोर दिया गया है, वे स्वाभाविक रूप से परीक्षाओं में ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले विषय-वस्तु होंगे और इसलिए, ज़ाहिर सी बात है कि कक्षाओं और छात्रों के निजी अध्ययन में इन विषय-वस्तुओं पर ज़्यादा समय दिया जाना ज़रूरी माना जायेगा।
ऐसा होने की स्थिति में कोई भला सोच भी सकता है कि यूजीसी की ओर से इस समय जो “ढांचा” सामने रखा जा रहा है,उसमें अनुभवी शिक्षकों और विद्वानों का भी योगदान हो सकता है। लेकिन,चकित करने वाली बात यह है कि इस ढांचे के लेखकों के नाम इसमें नहीं दिये गये हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा लगता नहीं है कि ख्याति प्राप्त और अनुभवी इतिहासकार इस बेहद गंभीर और इतिहास शिक्षण के लिहाज़ से बेहद अहम क़वायद में शामिल भी रहे हों।
हमारे ख़्याल से इस “ढांचे” की समीक्षा भारतीय इतिहास के पेपरों के लिए निर्धारित उस पाठ्यक्रम तक ही सीमित है, जहां स्वाभाविक ही है कि मौजूदा शासन के वैचारिक आक्रमकता की ख़ास तौर पर अपेक्षा की जा सकती है।
इस समय जो कुछ भी हो रहा है, उसका सबसे पहला संकेत भारतीय इतिहास पर जिस तरह से इन पेपरों का यहां संयोजन किया जा रहा है,उससे मिल जाता है। हमारे देश के इतिहास को छह पेपरों में शामिल किया गया है, जिसमें मध्ययुग (1200-1707) के लिए सिर्फ़ एक पेपर है, ताकि इसे छात्रों के कुल समय का महज़ छठा हिस्सा ही मिल सके, जबकि इस सिलेबस के मुक़ाबले इस समय के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों के इतिहास पाठ्यक्रम में इस मध्ययुग को तक़रीबन एक-तिहाई या एक-चौथाई हिस्सा हासिल है।
प्रस्तावना
हमारे सामने पहले एक प्रस्तावना आती है, जिसमें वे शब्द,जिनपर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है,उनमें व्याकरण और वर्तनी के हिसाब से बार-बार की गयी असहज कर देने वाली चूकें दिखायी पड़ती हैं। प्रस्तावना में हमें छात्रों के बीच “अपने स्वयं के इतिहास के स्वामित्व की भावना” को बढ़ावा देने की ज़रूरत के बारे में बताया गया है – अगर इसका मतलब यह है कि आप इतिहास को अपनी पसंद के मुताबिक़ आकार दे सकते हैं, क्योंकि आप इसके मालिक हैं,तो यह एक बेतूका सूत्र है।
हमें पहले ही वाक्य में बता दिया गया है कि इतिहास से हम “एक राष्ट्र की आत्मा के बारे में ज्ञान” हासिल करते हैं। इसका निश्चित रूप से अर्थ यह है कि पढ़ाये जाने वाले इतिहास को गौरवान्वित करना चाहिए –चाहे जो भी सही तथ्य हों- अतीत में जो कुछ भी हुआ (या नहीं हुआ) हो । किसी इतिहासकार को साक्ष्य के इस्तेमाल में “वस्तुनिष्ठ” होने की ज़रूरत होती है,इस बात को छोड़कर दुर्भाग्य से इस संपूर्ण “प्रस्तावना” में जिस इतिहास को पढ़ाया जाना है,उसमें पूरी सटीकता के साथ-साथ व्यापक तथ्यों को शामिल किये जाने की ज़रूरत पर कोई ज़ोर नहीं दिया गया है।
प्राचीन भारत
जब हम प्राचीन भारत के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम (पेपर III: ‘आदि काल से 550 सीई’ तक) पर आते हैं, तो हमें जल्द ही अहसास हो जाता है कि इसे तैयार करने वालों का मुख्य लक्ष्य इतिहास नहीं,बल्कि पौराणिक कथायें हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खोजी गयी सभ्यता,जिसे दुनिया “सिंधु सभ्यता” के रूप में जानती है, और आधिकारिक भारतीय पुरातत्व (अब तक) इसे “हड़प्पा संस्कृति” के रूप में पेश करता रहा है,इस पाठ्यक्रम में अचानक यह सभ्यता “सिंधु-सरस्वती सभ्यता” बन जाती है।
शिवालिक से निकलने वाली एक छोटी मौसमी नदी सरस्वती का नाम यहां सिंधु से जोड़ दिया गया है, ऐसा सिर्फ़ यह स्थापित करने के लिए किया गया है कि नये नामाकरण के हिसाब से हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख मिलता है। यहां चिंता इस बात को लेकर भी है कि हड़प्पा संस्कृति से द्रविड़ों के किसी भी तरह के जुड़ाव को खारिज कर दिया गया है, हालांकि, इस तरह के जुड़ाव का मामला सिंधु मुहरों पर ख़ुदे चिह्नों में मछली और तीर चिह्न के बार-बार इस्तेमाल के कारण बेहद मज़बूत है।
दरअसल, हमारे ‘आर्य’ मूल की भावना इतनी मज़बूत है कि इस पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय, “आर्यों का मूल निवास स्थान” को भी सुनिश्चित किया गया है। प्राचीन भारत को लेकर इस पाठ्यक्रम के इस विषय से बेहद चिंतित होने की ज़रूरत है,क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि इसके लेखक नाज़ियों की तरह आर्य जाति से प्रेम का समर्थन करते हैं। पाठ्यक्रम तैयार करने वालों के पक्षपात वाला रवैया अगले ही विषय से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है और यह विषय है: “आर्यों के आक्रमण का मिथक”। सवाल है कि अगर यह “मिथक” ही है, तो इससे परेशान होने की क्या ज़रूरत है ! वैदिक काल की संस्कृति को यहां “आर्य सभ्यता” का शीर्षक दिया गया है,इससे ऐसा लगता है कि मानो भारतीयों का “आर्य” जाति से जुड़ाव इसके लिए कुछ विशेष सम्मानकी बात हो। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं,उसमें नस्लवाद के किसी भी तरह के संकेत से गंभीरता के साथ बचा जाता है, ऐसे में इस तरह की चीज़ें इतिहासकारों का नहीं,बल्कि विक्षिप्त दिमागों का उत्पाद लगती है।
उसी रुख़ के तहत इसमें एक अजीब विषय “महाकाव्य साहित्य और संस्कृति” भी है,इस पाठ को ऐसे रखा गया है कि मानों एक समय ऐसा भी था, जब रामायण और महाभारत में वर्णित घटनायें वास्तव में घटित हुई हों, इस पाठ्यक्रम का मक़सद छात्रों के भीतर उन महाकाव्यों की “ऐतिहासिकता” को स्थापित करने के कार्य को निर्धारित करना है। ज़ाहिर है,इस पाठ्यक्रम को तैयार करने वाले “महाकाव्य” काल को ‘वैदिक युग’ और गौतम बुद्ध के काल के बीच होने वाले वास्तविक ऐतिहासिक चरण के रूप में देखते हैं।
अगला पाठ (छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक) की ओर मुड़ जाता है और यह पाठ्यक्रम महाजनपद का अर्थ उस ‘गणराज्य’ के रूप में लेता है, जिसकी पुष्टि हमारे स्रोत नहीं करते हैं।
यह पाठ्यक्रम ख़ुद ही एक अहम कमी को सामने रख देता है। बुद्ध के समय तक जाति व्यवस्था ख़ुद को अपने वर्ण और जाति घटकों के साथ मज़बूती से स्थापित कर चुकी थी और ग़ुलामी के साथ शूद्रों और बहिष्कृत जातियों का उदय हो चुका था। मगर, आश्चर्य है कि इस पाठ्यक्रम में जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास के लिए कोई जगह नहीं है। वास्तव में इस पाठ्यक्रम में मध्यकालीन भारत (1200-1707) में जाकर ही ‘जाति’ का संदर्भ मिलता है, मानो यह महज़ मध्यकालीन परिघटना हो !
यह तो हैरान करने वाली बात है कि अगर हम बहिष्कृत जातियों और शूद्रों के उत्पीड़न को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, तो हमसे अपने अतीत को समझ पाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस लिहाज़ से ख़ास तौर पर आर.एस. शर्मा की ‘प्राचीन भारत में शूद्र’ नामक अहम किताब को प्राचीन भारत के पेपर की ग्रंथ सूची में ही शामिल नहीं किया गया है।
मैं यहां आगे बढ़ते हुए पाता हूं कि सिकंदर का आक्रमण (‘ग्रीक आक्रमण’) को मौर्य काल के बाद रखा गया है और यह इंगित किये बिना ‘इंडिका’ शब्द का महज़ ज़िक़्र कर दिया गया है कि आख़िर मेगस्थनीज़ की इंडिका (जो अब खो चुका है) का मतलब क्या है।
मौर्य काल के बाद की राज-व्यवस्थाओं के सिलसिले में सबसे पहले यह पाठ्यक्रम हमें एक विशेष पाठ सामने रख देता है और वह है- ‘गणराज्यों का पुनर्गठन’,जो कि सिर्फ़ नाम से ज्ञात कुछ जनजातियों या रियासतों के वजूद पर आधारित एक विशुद्ध रूप से काल्पनिक विषय है और इसकी अहमियत इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर, शिलालेख, सिक्के और बौद्ध परंपरा के ज़रिये उस कुषाण साम्राज्य के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी है,जिसके केन्द्र में कनिष्क है,लेकिन यह कुषाण साम्राज्य इस पेपर में विभिन्न राजवंशों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है।
इस पाठ्यक्रम से गुज़रते हुए किसी को यह लगेगा ही नहीं कि (a) प्राकृत 300 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी की अवधि की एक अहम लिखित भाषा थी, और (b) इसके साथ-साथ इसी अवधि में संस्कृत साहित्य: मौर्योत्तर काल के व्याकरणविद् पतंजलि की रचना और मनुस्मृति, महाभारत और रामायण, और कामसूत्र जैसे ग्रंथ भी रचे गये थे। बौद्ध ग्रंथ, मिलिंदपन्हो भी उसी अवधि की रचना थी, जिस दौरान बौद्ध धर्म की वह महायान शाखा भी सामने आयी थी, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पदार्पण चीन तक में हुआ था। इस सिलेबस में इन सबकी अनदेखी की गयी है।
भारतीय इतिहास: सांप्रदायिक विभाजन
इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती कि प्राचीन भारत पर पेपर (पेपर III) में इतनी लंबी अवधि को क्यों शामिल किया गया है, जबकि भारतीय इतिहास पर जो अगला पेपर (पेपर V) है,उसके तहत महज़ 650 साल ही शामिल हैं, हालांकि शायद ही कोई यह तर्क दे सकता है कि इसके बारे में जो जानकारियां हैं,वह पिछली अवधि की तुलना में कहीं ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि इसे लेकर हमारे पास राजनीतिक इतिहास के जो मुख्य स्रोह हैं,उनमें हर्षवर्धन के बारे में लिखी गयी वाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी,कश्मीर पर लिखी गयी राजतरंगिणी के अलावे शिलालेख भी हैं।
उल्लेखनीय है कि जिस शख़्स,यानी हर्षा (पाठ्यक्रम में ‘हर्ष’ नहीं) के बारे में जिन दो स्रोतों,अर्थात् युआन च्वांग (ज़ुआन ज़ुआंग) और बाओ के ज़रिये हम बहुत कुछ जानते हैं,उनकी यहां अनदेखी की गयी है। अलबरूनी भी यहां इसी अनदेखी के शिकार हैं, जिन्होंने 1035 में अपनी किताब, ‘किताब-उल-हिंद’ में हमें भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वासों और पूरी तरह से संस्कृत स्रोतों पर आधारित विज्ञान का उल्लेखनीय विवरण दिया है। दूसरी ओर,राजपूतों (राजापुत्रों) के मूल और उनके कथित ‘पतन’, दोनों के लिए इसमें असाधारण चिंता दिखायी देती है।
जैसी कि उम्मीद थी,इस सिलेबस में सिंध में अरब शासन (8 वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित) और भारतीय धार्मिक धारणाओं, खगोल विज्ञान और गणित (विशेष रूप से ब्रह्मगुप्त के लेखन) और भारतीय अंकों का इस्लामिक जगत (जहां ये अंक यूरोप पहुंचे) में प्रसारित होने में इस अरब शासन की भूमिका की ओर आंखें बंद रखी गयी हैं।
इतिहासकारों के बीच चर्चित डी.डी. कोसंबी के लेखन और आर.एस. शर्मा के भारतीय सामंतवाद में इस अवधि के दौरान कृषि की स्थितियों की प्रकृति के साथ-साथ सोने और चांदी के सिक्कों का अचानक से ग़ायब हो जाना चर्चा के विषय रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम बनाने वाले इस बहस और इस अवधि के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में हमारे पास मौजूद बहुत सारी जानकारियों से पूरी तरह अनजान हैं ।
दूसरी ओर, एक ऐसे विषय को भी शामिल किया गया है, जो विषय इस अवधि से सम्बन्धित नहीं है,यानी कि “दिल्ली में मुस्लिम शासन” और “भारत पर मुस्लिम शासन का प्रभाव”। इस सिलेबस को तैयार करने वाले स्वयं कोई विवरण को प्रस्तुत किए बिना आख़िर इसमें क्या-क्या रखने का इरादा रखते हैं, इसे अनकहा छोड़ दिया गया है। हालांकि,कोई भी यह आसानी से अनुमान लगा सकता है कि इसके पीछे का इरादा “मुस्लिम शासन” पर निंदात्मक टिप्पणियों को आमंत्रित करना है।
यह जानना दिलचस्प होगा कि इकाई V के तहत सूफ़ीवाद (जिसकी एक प्रमुख किताब काशफूल महजूब,जिसकी रचना 1071 ईस्वी से पहले ‘अली हुजविरी ने लाहौर में की थी) के साथ एक मज़हब के रूप में इस्लाम के आगमन का विषय में इस सिलेबस में कोई ज़िक़्र तक नहीं मिलता है।
‘हिस्ट्री ऑफ इंडिया (1206-1707)’ नामक पेपर VII पर यूजीसी के ढांचे को तैयार करने वाले लेखकों ने शायद ख़ास तौर पर ध्यान दिया है, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने “मध्ययुगीन काल का गंभीर निरुपण (ऐसा ही लिखा है) किया है … ताकि राष्ट्र(यही शब्द है) के इतिहास की बेहतर समझ बन सके”।
असल में ‘पुनर्निर्माण’ (remodelling) चौंकाने वाला शब्द है। पूरी दिल्ली सल्तनत को इकाई I की चार उप-इकाइयों में से सिर्फ़ एक उप-इकाई में शामिल किया गया है। इसके ज़रिये अलाउद्दीन खिलजी के कृषि और मूल्य-नियंत्रण उपायों या मुहम्मद तुग़लक़ के कृषि के दुरुस्त किये जाने की कोशिश को समझाना एक मुश्किल काम हो गया है। ‘ तुर्क, खिलजी, और तुग़लक़ (और) तैमूर के शुरुआती हमले, इन तमाम परिघटनाओं को सिर्फ़ एक इकाई में रख दिया गया है।
इसी तरह की चूकें यूनिट II में भी व्यापक रूप से मिलती हैं। बाबर के “हमले” से पहले ‘सूर’ को रखने की विचित्रता के अलावा छात्रों को अकबर से जुड़ी उन तमाम चीज़ों से मुक्त कर दिया गया है, चाहे वह अकबर का राजपूतों के साथ सुलह हो, उसका भू-राजस्व उपाय हो, उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति और सुलह-ए-कुल (संपूर्ण शांति) का सिद्धांत) हो, संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हो, या फिर उसके मंत्री, अबुल फ़ज़ल का देश के आधुनिक काल से पहले के सांख्यिकीय, सांस्कृतिक और प्रशासनिक सर्वेक्षण (आइन-ए अकबरी) ही क्यों न हो,सबके सब सिरे से ग़ायब हैं। यहां तक कि अकबर के नाम तक का भी ज़िक़्र नहीं है। दूसरी ओर, जिन मुख्य किरदारों पर छात्रों के ध्यान को केंद्रित किया गया है, वे तमाम किरदार विधिवत दर्ज हैं,इनमें “हेमू विक्रमादित्य, राणा प्रताप, रानी दुर्गावती और चांद बीबी” हैं !
इसी तरह, जहांगीर और शाहजहां को मुग़ल बादशाहों के इतिहास से बाहर कर दिया गया है,बाबर के अलावा इसमें सिर्फ़ औरंगज़ेब का ज़िक़्र किया गया है, लेकिन जिस बात पर ज़ोर दिया गया है,वह है- मुग़लों के ख़िलाफ़ विद्रोह या प्रतिरोध। यहां अज्ञानता की हद दिखायी देती है। हिंदू पद-पदशाही, मुहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान पेशवा बाज़ी राव के लिए इस्तेनमाल की जाने वाली एक शब्दावली है, जबकि इसके इस्तेमाल को औरंगज़ेब के शासनकाल में किया गया दिखाया गया है, और इसे एक ऐसा अहम विषय बना दिया गया है, जिसका अध्ययन छात्रों को जिस पेपर में करना है,उसमें ही यह नहीं है।
इस सांप्रदायिक विभाजन को इकाई IV के तहत सामाजिक इतिहास के ज़रिये आगे बढ़ाया गया है, जिसमें “हिंदू समाज” का “मुस्लिम समाज” से अलग अध्ययन किया जाना है। ऐसा लगता है कि मानो “दो-राष्ट्र” के सिद्धांत को पीछे ले जाते हुए मुग़लों के दौर तक ले जाना है।
पेपर IX में 1707 से लेकर 1857 तक से सम्बन्धित भारत का इतिहास है, जिसका मतलब यह है कि पारंपरिक रूप से ब्रिटिश सत्ता के उदय के लिए जिस प्लासी युद्ध (1757) को काल-निर्धारण घटना के रूप में देखा जाता रहा है,उसे नहीं माना गया है,और इस लिहाज़ से औरंगज़ेब (1707) की मौत की अहमियत मिलती दिखायी देता है। जब यूनिट II में रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के दौर को 18वीं शताब्दी की घटनाओं से पहले रख दिया जाता है, तो कालक्रम का और भी गडमड हो जाता है। यहां भी मैसूर को हैदराबाद के साथ जोड़ते हुए (उप-इकाई 3) यह सुनिश्चित किया जाता है कि सवालों को सेट करते समय ब्रिटिश विस्तार का विरोध करने में मैसूर की साहसिक भूमिका की भी अनदेखी की जा सकती है।
इस पेपर मे उल्लेखित अवधि में ही उस समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके साथ राम मोहन राय का नाम बेहद गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। मगर, इस पेपर में इस आंदोलन को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इस सिलेबस के मुताबिक़ सती और दासता को शायद पूरी तरह ख़त्म नहीं किया गया होगा। दूसरी ओर, यह पेपर किसी व्यक्ति विशेष या आंदोलन को निर्दिष्ट किये बिना ‘सांस्कृतिक प्रतिरोध’ की बात करता है।
ऐसा साफ़-साफ़ लगता है कि सिलेबस तैयार करने वालों ने उस नज़राने और आगे चलकर मुक्त व्यापार वाले उस साम्राज्यवाद के बारे में शायाद कभी कुछ सुना ही नहीं है, जिन दो प्रक्रियाओं के ज़रिये ही भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया गया था और और देश को और ज़्यादा ग़रीबी के हवाले कर दिया गया था। यह बात भी कम दिलचस्प नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कृषि से जुड़े उपाय, ख़ास तौर पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवारी प्रणाली, जिसकी वजह से सभी किसानों पर भारी बोझ डाला गया था, उस बोझ को “भूमि राजस्व” (इकाई IV। 2) के तहत ‘बैंकिंग’ की आड़ में छुपा लिया गया है।
राष्ट्रीय आंदोलन
जब हम भारतीय इतिहास के अगले पेपर,यानी पेपर X की ओर बढ़ते हैं, तो हम इस पेपर को “इंडियन नेशनल मूवमेंट (1857-1947)” शीर्षक के रूप में पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के साथ-साथ ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था और उस काल की ‘संवैधानिक व्यवस्था’ को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। यहां तक कि इसमें 1943-44 का बंगाल का अकाल भी कहीं नज़र नहीं आता है। यह एक गंभीर त्रुटि है और इस पेपर को ठीक से फिर से शीर्षक दिये जाने की ज़रूरत है और ब्रिटिश शासन के पिछले 90 वर्षों के इतिहास को निर्मित करने वाले सभी प्रमुख तत्वों को यहां प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि उद्देश्यों और विकास के क्रमिक चरणों को देखते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को भी बेहतर ढंग से समझा जा सके।
असहयोग आंदोलन (इकाई III, i) के बजाय ख़िलाफ़त के मुद्दे को रौलट सत्याग्रह (इकाई II, iv) के साथ जोड़ने या त्रिपुरा संकट (इकाई III, iv) के साथ भारत छोड़ो आंदोलन को रखने जैसी सामान्य ग़लतियों को छोड़कर पहले की उप इकाई i में राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न पहलुओं और चरणों को ठीक से शामिल करता हुआ दिखायी देता है।
आधुनिक भारत
अंत में भारत के 1947 के बाद के इतिहास को दर्शाने वाला पेपर XI है, जिसे ‘आधुनिक भारत’ (‘समकालीन भारत’ के बजाय) नाम दिया गया, और जो साल 2000 में आकर समाप्त हो जाता है। यहां कुछ दिलचस्प चूकों का ज़िक़्र करना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहली चूक तो 1947-48 के उस साम्प्रदायिक क़त्लेआम और उसके खिलाफ गांधीजी की उस साहसी लड़ाई को पूरी तरह से भुला देना है,जिसका अंत उनकी शहादत से होता है। जैसा कि इस सिलेबस से पता चलता है कि शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में सबसे बड़ी जातीय सफाई और बड़े पैमाने पर नरसंहार की उतनी भयानक घटना को ‘राष्ट्रीय’ स्मृति से आसानी से मिटाया जा सकता है,यह बेहद डरावना अहसास है।
अगर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान (इकाई I, i) के प्रारूप बनाने को इस सिलेबस में रखा जाता है, तो हैरत होती है कि एक मिश्रित, लेकिन नियोजित अर्थव्यवस्था और व्यापक पैमाने पर भूमि सुधार के साथ-साथ एक धर्मनिरपेक्ष ‘समाजवादी’ भारत का दृष्टिकोण देने वाले जवाहरलाल नेहरू को आख़िर कैसे छोड़ा जा सकता है। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार-प्रसार का भी इसमें कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है।
यूनिट II (iv) ‘संसदीय लोकतंत्र’ के लिए समर्पित है, ऐसे में इस सिलेबस में 1975-77 के दौरान आपातकाल और मूलभूत स्वतंत्रता में कटौती किये जाने को कुछ जगह मिलनी चाहिए थी।
इकाई III की उप-इकाई iv के तहत ‘सामाजिक न्याय’ का सामान्य उल्लेख पर्याप्त नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू संहिता, 1955 और बाद में दहेज विरोधी क़ानून जैसे महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में बने क़ानूनों का ख़ास तौर पर उल्लेख होना चाहिए था। इसी तरह, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के मामले में सकारात्मक कार्रवाई का भी विशिष्ट उल्लेख होना चाहिए था। इकाई IV की उप-इकाई iv में सिर्फ़ “पहचान की राजनीति” (एक पसंदीदा भाजपा वाक्यांश) के बारे में ज़िक़्र करना, जबकि “धर्मनिरपेक्षता” शब्द से बचना कचोटता है।
सांस्कृतिक विरासत
ऊपर भारतीय इतिहास के जिस पेपर की चर्चा की गयी है,उसके बाद पेपर XII है, जिसका शीर्षक है-‘भारत की सांस्कृतिक विरासत’। इस पेपर की परिकल्पना कुछ इस तरह से की गयी है कि इसकी चार इकाइयों में से दो का सम्बन्ध धार्मिक अनुष्ठानों, मेलों, त्योहारों और किंवदंतियों से है। ये विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी चीज़ें भले ही हों, लेकिन शायद ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ये हिस्सा हैं।
सांस्कृतिक विरासत के तहत जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें सीखने और ललित कला में भारत के योगदान के अलावे ख़ास तर पर भारत का मानवतावादी विचार,तर्क और कालक्रम में विज्ञान में भारत के योगदान की चर्चा होनी चाहिए । उदाहरण के लिए, इसमें ऋग्वेद में सृजित श्लोक, उपनिषदों, धम्मपद, अशोक के शिलालेख, कालिदास, अमीर ख़ुसरो और टैगोर की रचनाओं के अंश जैसे अन्य साहित्यिक योगदान की चर्चा हो सकती है। इसी तरह, राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक के तमाम सुधारकों की विरासत पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। इसे यूनिट I-III की जगह होना चाहिए। इकाइ III और इकाई IV में (तकनीकों पर ध्यान देने के साथ-साथ) वास्तुकला की शैलियों के अकादमिक रूप से ज़्यादा उन्मुख विवरण के अलावे मूर्तिकला और पेंटिंग को शामिल किये जाने की ज़रूरत है।
पेपर XIV (भारत में संचार का इतिहास) में एक महत्वपूर्ण चूक संचार में आयी वह क्रांति है, जो काग़ज़ की शुरूआत की वजह से हुई थी (यह एक मध्यकालीन परिघटना थी और ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से इस सिलेबस में इसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया हो ?)
यह समझ में नहीं आता है कि “सामान्य ऐच्छिक” खंड के तहत अकेले दिल्ली पर दो पेपर क्यों होने चाहिए थे, और प्राचीन दिल्ली के पेपर में “आधुनिक गांव के मंदिरों में प्राचीन प्रतिमाओं की पूजा” क्यों शामिल होनी चाहिए थी। निश्चित रूप से दिल्ली पर एक ही पेपर पर्याप्त होगा, लेकिन देश भर के संस्थानों के लिए बने इस पाठ्यक्रम के लिहाज़ से इसे सही ठहराना भी मुश्किल होगा।
ऊपर उल्लिखित अंधराष्ट्रीयता और पूर्वाग्रह की विकृतियों और उसके प्रदर्शनों के अलावा, यूजीसी के इस “फ़्रेमवर्क” में पिछले सौ वर्षों में हुए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विस्तार को कहीं चिह्नित नहीं किया गया है। इसमें आम लोगों के जीवन के हालात, आर्थिक प्रवृत्तियों, तकनीकी प्रगति, महिलाओं के इतिहास, क्षेत्रीय साहित्य आदि पर कुछ भी नहीं है, इसे तैयार करने वालों को साफ़ तौर पर यह पता नहीं है कि एक समुचित इतिहास पाठ्यक्रम को आख़िर होना कैसा चाहिए।
ग्रंथ सूचियां
आख़िर में हम इसकी ग्रंथ सूचियों पर आते हैं। हर एक पाठ्यक्रम या हर एक पेपर के लिए तैयार की गयी पठन सूची या ग्रंथ सूची पाठ्यक्रम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होना चाहिए। ग्रंथ सूची को एक मानक स्तर वाली पुस्तकों के साथ-साथ व्यापक और चयनात्मक होने की भी आवश्यकता है। इस लिसेबस मे प्रत्येक पेपर के लिए पाठ्यक्रम के साथ संलग्न ग्रंथ सूची को सही मायने में बेहद फूहड़ तरीक़े से तैयार किया गया है। इसका एक उदाहरण है: बारहवां पेपर (‘मॉडर्न इंडिया, 1947-2000)। इसस जुड़ी पठन सूची से इतिहासकार बिपन चंद्र का राष्ट्रवादी नेता बिपिन चंद्र पाल होने का भ्रम पैदा होता है।इस ग्रंथ सूची में बिपिन चंद्र की दो किताबों को बिपिनचंद्र पाल की किताबें बतायी गयी हैं, जिनमें से एक 1947 के साथ ख़त्म हो जाती है और इसलिए इस पेपर के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता भी नहीं है।
इसी तरह, एच.ए.एल. फिशर की हिस्ट्री ऑफ़ यूरोप, ओपी हेंडरसन की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन द कंटिनेंट, जॉल जेम्स की यूरोप सिंस 1870, डब्ल्यूआई लैंगर की डिप्लोमेसी ऑफ़ इंपेयरियलिज़्म,एंड यूरोपियन एलायंस एंड इलाइनमेंट, मजूमदार, रायचौधरी और दत्ता की ऐडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया, तारा चंद की हिस्ट्री ऑफ़ फ़्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, वॉल्यूम IV, ए.जे.पी. टेलर की द ओरिजिन्स ऑफ़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और डी. थॉम्पसन की यूरोप सिंस नेपोलियन को बिना सोचे-समझे इस सूची में शामिल कर लिया गया है, हालांकि उनका 1947 के बाद भारत से या फिर भारत से ही कोई लेना-देना नहीं है।
चार मामले तो ऐसे हैं,जिनमें लेखकों के नाम तो दिये गये हैं, लेकिन उनकी किताबों का कोई शीर्षक नहीं दिया गया है। भारतीय इतिहास पर छह मुख्य पेपरों से जुड़ी सभी ग्रंथ सूची में इसी तरह का फूहड़पन दिखायी देता है।
बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण होने के अलावा, यह ग्रंथ सूची दर्शाती है कि कुछ लेखकों और उनकी किताबों को जानबूझकर निकाल दिया गया है। मिसाल के तौर पर लगता है कि प्राचीन भारत से डी.डी. कोसांबी, आर.एस. शर्मा, डी.एन.झा, और के.एम. श्रीमाली को जानबूझकर इन ग्रंथ सूची से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर,सिंधु सभ्यता को आर्य या वैदिक सभ्यता का उत्पाद बताने की खुलकर वकालत करने वाली एक किताब को शामिल कर लिया गया है, भले ही वह किताब हिंदी में है। जब प्राचीन भारत का यह हाल है, तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मध्यकालीन और आधुनिक भारत में शामिल ग्रंथ सूची का हाल कितना दयनीय और ईर्ष्या भरा होगा। उदाहरण के लिए, पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया श्रृंखला के तमाम संस्करण यहां पूरी तरह नदारद हैं, जबकि इसके 15 संस्ककरण प्रकाशित हो चुके हैं।
इस तरह, स्नातक कक्षाओं को भारतीय इतिहास पढ़ाने के लिए यूजीसी का यह प्रायोजित “ढांचे” का इरादा न सिर्फ़ भारतीय इतिहास का एक झूठा, स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक व्यंग्यचित्र प्रस्तुत करने का है, बल्कि यह गुणात्मक रूप से एक अक्षम, ग़ैर-शैक्षणिक क़वायद भी है। अपने विषय को वास्तविक रूप से पेश किये जाने को लेकर प्रतिबद्ध सभी इतिहासकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसे तत्काल वापस लेने की मांग को उठाने में शामिल हो जाना चाहिए।
प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब प्राचीन और मध्यकालीन भारत के एक भारतीय इतिहासकार हैं। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अवकाशप्राप्त प्रोफ़ेसर हैं। इनके विचार निजी हैं।– सौजः न्यूजक्लिक । अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें
UGC Framework –A Communalised Caricature of Indian History: Irfan Habib